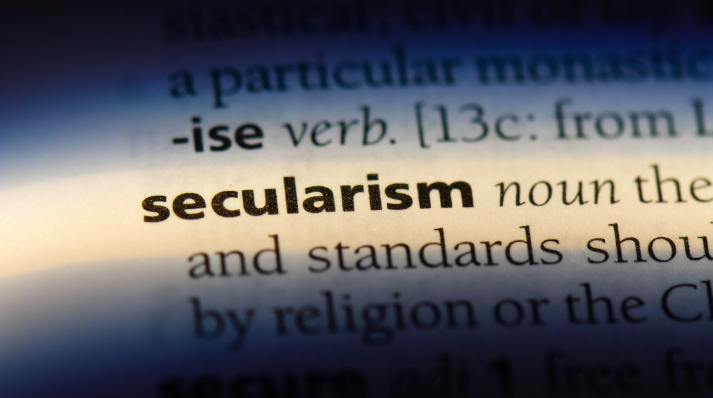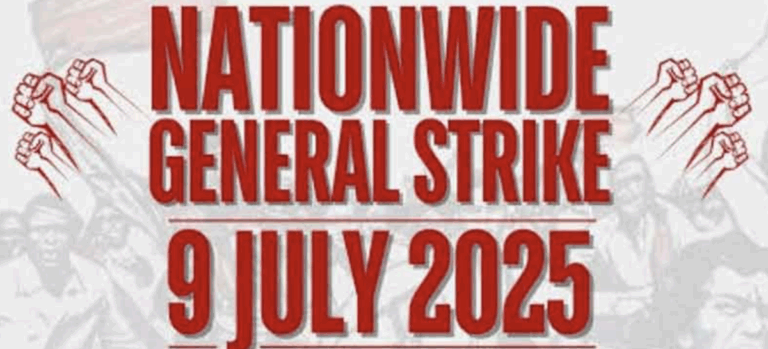जब बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी तब उसे पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही थी कि किन संगठनों के नेतृत्व में ढांचे को गिराया जा रहा है। ठीक इसके विपरीत मंदिर के पक्ष में फैसला देते समय सुप्रीम कोर्ट ने यह कही नहीं पाया कि कभी भी वहां कोई मंदिर था जिसे गिरा कर मस्जिद बनाया गया। तब ऐसे में जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था उस समय दो बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो कि नहीं दिया जा रहा है। एक ये कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समाज के मानस पटल पर किस किस्म का दूरगामी नकारात्मक असर पड़ रहा होगा? और दूसरा ये कि आने वाले समय में राज्य और धर्म के बीच रिश्ता क्या होगा?
हमारा समय और धर्मनिरपेक्षता
मुख्य धारा का विपक्ष या यूं कहिए कि लगभग समूचा विपक्ष और नागरिक संगठनों के अधिकांश लोगों ने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष शब्द से अलग कर लिया है, धीरे-धीरे पर सतत प्रयास के जरिए सांप्रदायिकता की जगह धर्मनिरपेक्ष शब्द को नकारात्मक शब्द के बतौर स्थापित किया ज रहा है और इस तरह धर्मनिरपेक्ष शब्द को एक राजनैतिक गाली में तब्दील कर दिया गया है, दुःखद यह है कि विपक्ष ने भी इस शब्द के नये अर्थ को चुनौती देने के बजाय समर्पण का आसान रास्ता लगभग चुन लिया है जो कि आने वाले समय के लिए बेहद ख़तरनाक संकेत है।
अल्पसंख्यक और धर्मनिरपेक्षता
अल्पसंख्यक समाज ख़ासकर मुस्लिम और ईसाई, राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को संदेह की नज़र से देखने लगे हैं, संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के विचार से उनका विश्वास डिगने लगा है, जिस तरह से लगातार लिंचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, छोटे-बड़े राज्य प्रायोजित दंगे कराए जा रहे हैं, हिंदू प्रतीकों, अल्पसंख्यक विरोधी मुहावरों-नारों का सार्वजनिक इस्तेमाल किया जा रहा है और पुलिस तंत्र का संरचनागत सांप्रदायिक रवैया व अदालतों का जो बहुसंख्यकवाद है इन सबने मिलकर इस समाज को भारी असुरक्षा बोध की ओर धकेल दिया है जिसके चलते एक तो ये हुआ है कि भविष्य बेहतर बनाने की जगह अस्तित्व रक्षा की सोच ने प्रधानता ग्रहण कर ली है और समाज सामूहिक अवसाद की तरफ बढ़ रहा है।
दूसरा ये कि इस समाज के अंदर की जो विविधता थी यानि भाषाई, भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या जाति और वर्ग की जो विविधता थी वह सब अब धार्मिक पहचान नीचे दबती जा रही है, संघ-भाजपा की यही मंशा भी थी और विपक्ष भी अपने तात्कालिक चुनावी चिंताओं के तहत इसी पहचान को प्रश्रय देता रहा है। और तीसरा ये कि लोकतांत्रिक प्रतिवाद के सारे रास्ते बंद कर दिए जाने के चलते हर तरह की कट्टरता और अराजकता के लिए जगह का विस्तार हो रहा है।
धर्मनिरपेक्षता और भाजपा
भारत एक बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है और यही वजह है कि धर्मनिरपेक्षता का विचार उसके बुनियाद में है। इस बुनियाद को हिलाए बिना बहुसंख्यक राष्ट्र के विचार को एक कदम भी आगे नही बढ़ाया जा सकता, संघ-भाजपा के लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे। हालांकि सभी धर्मों का समान सम्मान वाली धारणा के चलते हमारे यहां धर्मनिरपेक्षता के बहुसंख्यक समुदाय की ओर झुक जाने की संभावना भी लिए हुए थी और इस कमजोरी से भी बहुसंख्यक राष्ट्रवाद के प्रवर्तक अच्छी तरह परिचित थे। और फिर वे हिन्दू राष्ट्र की परियोजना लेकर आए, हिंदू होना ही सेकुलर होना बताया और यह भी कहा गया कि अन्य धर्म और संस्कृति के लोग अगर यहां रह रहे हैं तो केवल और केवल हिंदुओं की सहिष्णुता के चलते।
धर्मनिरपेक्षता को छद्म धर्मनिरपेक्षता कहा और उसे बाहरी विचार बताया और इस तरह लंबे प्रचार अभियानों के जरिए जनता के बड़े हिस्से को संघ-भाजपा यह समझाने में कामयाब हो गए हैं कि धर्मनिरपेक्षता, न केवल अल्पसंख्यकों ख़ासकर मुसलमानों का तुष्टिकरण करने वाला विचार है बल्कि घनघोर हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी भी है। और अब तो जो भी राजनीतिक -नागरिक संगठन या व्यक्ति धर्मनिरपेक्षता का पक्षधर है उस पर भी हिंदू और राष्ट्र विरोधी होने का ठप्पा लगाना आसान होता जा रहा है।
भारतीय राज्य और धर्मनिरपेक्ष पक्षधर राजनीति
वैसे तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया पर उससे तीन साल पहले ही और फिर 1994 में भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ कर दिया कि धर्मनिरपेक्षता, संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। धर्मनिरपेक्षता आजादी आंदोलन के दौरान भी केंद्रीय मूल्य बना रहा और इतिहास में ऐसे कई मोड़ आए जब मिलजुल कर रहने का विचार, भारतीयों को आकर्षित करता रहा। पर ज्यादातर धर्मनिरपेक्षता समर्थक राजनीतिक धाराओं ने सेकुलरिज्म का मतलब राज्य का धर्म से पूर्णतः अलगाव नहीं बल्कि हर धर्म को समान सम्मान देना माना।
पर सर्व धर्म समभाव वाली दिशा के चलते एक बड़ी दिक्कत शुरू हुई। धर्मनिरपेक्षता को हरदम बहुसंख्यकवादी दबाव के मातहत रहना पड़ा, भारतीय राज्य और उसकी हर मशीनरी नौकरशाही, पुलिस, न्याय प्रणाली हर जगह एक अघोषित हिंदू वर्चस्व कायम रहा, चाहे वो 1949 में राम की मूर्ति रखवाना हो, बाद में मंदिर का ताला खुलवाना हो या 84 का दंगा हो हर जगह भारतीय राज्य का झुकाव और सेकुलर राजनीति और ख़ासकर कांग्रेस पर बहुसंख्यकवादी दबाव को साफ़-साफ़ देखा जा सकता है। आज जब हम संघ-भाजपा के साथ साम्प्रदायिकता के विचार के ताकतवर उभार को देख रहे हैं तो हमें कम-से-कम सेकुलर राजनीति की विरासत और वर्तमान पर बार-बार ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आजादी आंदोलन के दौर में भी और बाद में बंधुता, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता की फसल के साथ-साथ खर-पतवार भी कैसे उगता रहा, इसकी भी शिनाख्त करनी चाहिए।
आज़ादी आंदोलन के दौरान साम्प्रदायिकता के सवाल पर दो बातें प्रमुखता से बार-बार कही जाती रहीं। पहला तो ये कि यह समस्या उपनिवेशवादी सत्ता द्वारा प्रायोजित-संचालित है और दूसरा ये कि यह समस्या आर्थिक वजहों से भी है, मध्यवर्गीय तनाव और आकांक्षा महत्त्वाकांक्षाओं की उकसावा मूलक कार्रवाइयों के चलते भी है, इन दोनों ही प्रस्तावनाओं से स्वाभाविक अर्थ यह निकाला गया कि उपनिवेशवाद से मुक्ति और भारतीयों का अपना राज़ इस समस्या को हल कर सकता है,
पर इसका एक वैचारिक पक्ष भी था जो खुद एक भौतिक ताकत में बदल गया है और इस पर अलग से एक ताकतवर वैचारिक अभियान की जरूरत है इसे आमतौर पर कभी शिद्दत से महसूस नहीं किया गया बल्कि तात्कालिक जन गोलबंदी की जरूरतों और उस समय अतीत के गौरव की वापसी जैसी राष्ट्रवादी जरूरतों के चलते जाने- अनजाने, बहुसंख्यक हिंदू शब्दावलियों-मुहावरों और नारों का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह यह समझ तो ठीक है कि बहुसंख्यक सांप्रदायिकता ज्यादा ख़तरनाक है पर अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता को बिल्कुल ही छूट दे देना या हल्के में लेने के चलते भी बहुसंख्यक सांप्रदायिकता को और ताकत मिलती गई।
आज़ादी के बाद भी कई दौर ऐसे आए जब सेकुलर दलों ने सत्ता में रहते हुए सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ बेहद उदार रूख़ रखा या फिर जब सत्ता में नहीं रहे तो उसे हासिल करने के लिए उन्हीं ताकतों से गठजोड़ भी बनाए और इस तरह उन्हें हर समय फलने-फूलने दिया, गांधी जी की हत्या के बाद जल्दी ही संघ पर लगे प्रतिबंध को हटा देना और उसे शाखाओं और स्कूलों के जरिए सांप्रदायिक जहर फैलाने की खुली छूट दे देना या 75 में जनसंघ के साथ या 89 में भाजपा के साथ गठजोड़ कर संघ को फिर से मुख्यधारा में ले आने वाले ये कुछ प्रमुख उदाहरण आपके सामने हैं।
फिर 1992 का समय आया जब केंद्र में सेकुलर सरकार रहते हुए ही बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और फिर एक हिंदू समय का आरंभ हुआ और आज़ बहुत सारी मुख्यधारा की राजनीतिक ताकतों को धर्मनिरपेक्षता से दूरी बनाने और अपने हिंदू होने का प्रमाण देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और अब तो बात यहां तक चली आई कि 22 जनवरी को राममंदिर के उद्घाटन की भव्यता 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को विस्थापित करती नज़र आ रही है।
धर्मनिरपेक्षता और जनता
तब आज़ भारतीय गणराज्य के सामने रास्ता क्या है? यह मान लेना कि हजारों साल पुरानी सभ्यता आज अपने सामने आयी चुनौती का सामना खुद कर लेगी? या यह कि हमारी गंगा-जमुनी विरासत के अंदर ही इस विराट मसले का समाधान है?या फिर साम्राज्यवाद विरोधी और राष्ट्रीय एकता पर केंद्रित आजादी आंदोलन और उसकी विरासत से निकले हमारे संविधान में इतनी क्षमता है कि भारतीय गणतंत्र,’विविधता के साथ एकता’ के मूल्य को अपना केंद्रीय विचार बनाए रख सके? ह
म समझते हैं कि यह मान लेना ठीक नहीं है, क्यों कि हम देख रहे हैं कि भारतीय गणराज्य और उसके संविधान का अपने नागरिकों से दूरी बढ़ती जा रही है, इसका एक मतलब यह भी है कि आज़ादी के बाद सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर असमानता को खत्म कर सही मायने में लोकतंत्र और देश को हासिल करने का वादा जो हमने अपने नागरिकों से किया था वो कहीं बीच में ही छूट गया है, उसे खोजना और जनता के साथ मिलकर आगे बढ़ाना ही आज हमारा मुख्य कार्यभार होना चाहिए। उम्मीद है कि हम ऐसा करेंगे।
(मनीष शर्मा राजनीतिक-सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और आजकल बनारस में रहते हैं।)