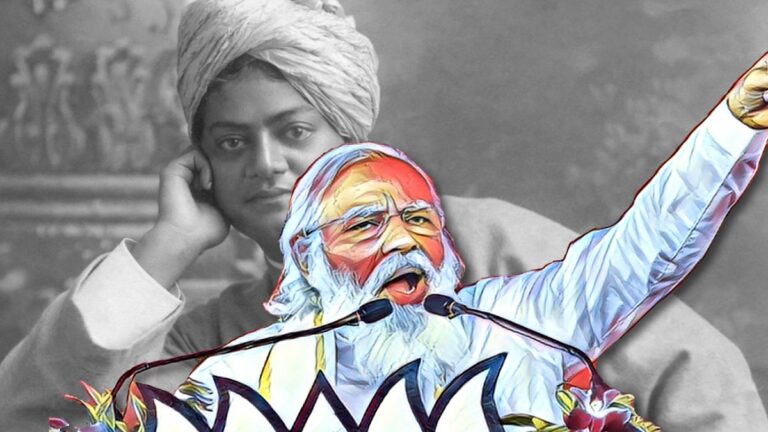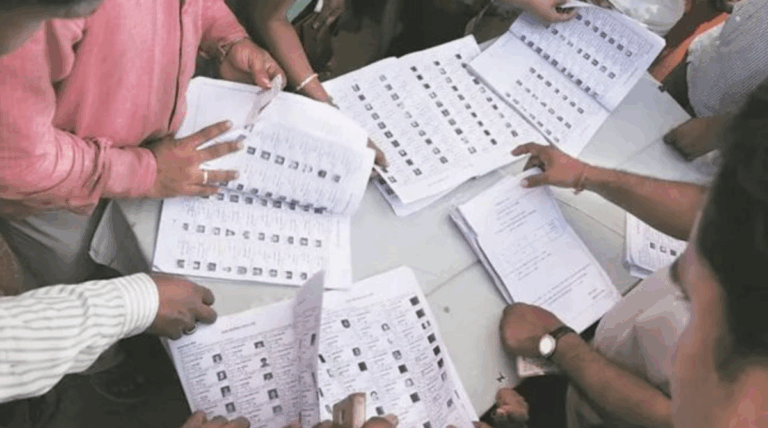आज विज्ञान अपने विकास के चरम पर पहुंच गया है, जिसके बल पर आज लोग चन्द्रमा तथा अन्य ग्रहों पर बस्तियां बसाने की बात करने लगे हैं। दुनिया में अनाज की पैदावार इतनी अधिक होने लगी है कि सभी लोगों का पेट भर सकता है। विज्ञान ने आज दुनिया भर के लोगों के लिए सभी भौतिक वस्तुओं पर पहुंच बहुत सुगम बना दिया है, इसके बावज़ूद आज दुनिया भर में करोड़ों लोग भुखमरी के शिकार हैं तथा खाली पेट सोने के लिए मजबूर हैं।
पिछले दिनों लंदन की एक संस्था ने एक नयी रिपोर्ट जारी करते हुए संसार में बढ़ते भुखमरी के संकट पर प्रकाश डाला है। रिपोर्ट के अनुसार जहां एक ओर भोजन का अति-उत्पादन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर संसार के 230 करोड़ लोगों की भोजन या पौष्टिक भोजन तक पहुंच नहीं है।
जहां आज के युग को ज्ञान-विज्ञान का युग कहा जाता है, इंसान अनंत प्रगति कर रहा है, हर रोज़ नयी-नयी खोजों की ख़बरें सामने आती हैं, जो इंसान के जीवन को आसान बना सकती हैं और इंसान की ज़रूरत की कई चीज़ों की जहां बहुतायत है, लेकिन इसके बावजूद यहां लोगों की ज़्यादातर संख्या बहुत मुश्किल जीवन जीने के लिए मजबूर है।
हालात ये है कि हमारी धरती पर हर सातवां व्यक्ति भूखे पेट सोने के लिए मजबूर है, हर तीन में से एक व्यक्ति को पेट भर खाना नहीं मिलता और संसार की 9.8 फ़ीसदी आबादी यानी 83 करोड़ लोग भुखमरी का शिकार हैं। ऐसी हालत में हर साल इस समस्या को हल करने के लिए अलग-अलग लक्ष्य तय करने का नाटक किया जाता है और कई प्रकार के समाधान पेश किए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये स्थितियां सुधरने का नाम क्यों नहीं ले रहीं।
यहां हम भोजन सुरक्षा और भोजन से मिलने वाली ज़रूरी ऊर्जा की बात करेंगे। अगर संतुलित और पौष्टिक भोजन की बात की जाए, तो इसकी उपलब्धता के बारे में पूंजीवादी व्यवस्था बुरी रही असफल साबित होती है। मानवता के पूरे इतिहास में देखें तो मनुष्य के पास कभी भी इतना भोजन उपलब्ध नहीं था, जितना आज के समय में है। पिछले लगभग तीन दशकों में भोजन उत्पादों के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है।
इस रिपोर्ट के अनुसार आज संसार में इतना अनाज पैदा होता है कि धरती के हर व्यक्ति को रोज़ाना 6 हज़ार कैलोरी जितना भोजन प्रदान किया जा सकता है, जो एक आम व्यक्ति की ज़रूरत का 2.6 गुना है। संयुक्त राष्ट्र की भोजन और कृषि संस्था के आंकड़ों के अनुसार 2005-2020 में लगातार संसार स्तर पर भोजन उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई थी।
जहां गन्ना, मक्की, चावल, गेहूं, फल के उत्पादन में 50 फ़ीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई, वहीं यह आंकड़ा सब्जि़यों के लिए 65 फ़ीसदी, दूध के लिए 53 फ़ीसदी और मांस के लिए 40 फ़ीसदी था। इसके बावजूद 2019 के बाद विश्व स्तर पर भुखमरी के शिकार और कुपोषित लोगों की संख्या में भयानक बढ़ोतरी (लगभग 15 करोड़) हुई है।
अगर अनाज का उत्पादन बढ़ रहा है तो लाज़िमी ही इंसानी आबादी और भी तेज़ी के बढ़ रही होगी? हमारे समाज में एक आम विचार फैला हुआ है या यह कहना अधिक सही होगा, कि फैलाया गया है कि मानवता की अधिकांश समस्याएं चाहे वह ग़रीबी, भुखमरी, पानी, पर्यावरण की समस्या क्यों ना हो, इसकी जड़ विशाल जनसंख्या है। स्कूल की किताबों से लेकर अख़बारों तक में लगातार इस बात का शोर मचाया जाता है।
यह सिद्धांत सबसे पहले अट्ठारहवीं सदी के अंत में इंग्लैंड के माल्थस नामक एक अंग्रेज़ पादरी ने पेश किया था, जिसके अनुसार जनसंख्या अनाज के उत्पादन की तुलना से कहीं तेज़ी से बढ़ती है, जिसका लाज़िमी नतीज़ा धरती पर अतिरिक्त-जनसंख्या पैदा होना है। तथ्य माल्थस के इन दावों का बुरी तरह खंडन करते हैं।
इसके बावज़ूद आज भी समाज में मुख्य तौर पर यही विचार प्रचलित है और समय-समय पर विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं जनसंख्या में वृद्धि को आर्थिक और सामाजिक विकास में सबसे बड़ी रुकावट करार देती हैं और सभी समस्याओं का दोष इसी के सिर मढ़ती हैं।
बढ़ती भोजन असुरक्षा का असल कारण मौजूदा व्यवस्था है, जहां उत्पादन का मक़सद लाभ कमाना है। यहां हर चीज़ इंसान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि मुनाफ़ा कमाने के लिए पैदा की जाती है। मौजूदा व्यवस्था में मनुष्य के इस्तेमाल की हर चीज़ माल में बदल दी जाती है और आज भोजन क्षेत्र तक में इन पूंजीपतियों का क़ब्ज़ा है।
संसार के भोजन क्षेत्र की सभी शाखाओं में जैसे बीजों, कृषि रसायनों, उत्पादन और विनिमय के बुनियादी ढांचे पर कुछ नामी कंपनियों का क़ब्ज़ा है। बीजों के क्षेत्र में बेयर नाम की कंपनी का बहुत दबदबा है, इसके बाद कोर्टेवा, कैमचाइना, बी.ए.एस.एफ़. और ग्रुप लिमाग्रेन का स्थान है।
ऐसी ही हालत कृषि रसायन के क्षेत्र में है। कुल मिलाकर संसार की बीजों की मंडी के 58 फ़ीसदी और कृषि रसायन मंडी के 77.6 फ़ीसदी हिस्से पर केवल छह कॉर्पोरेशनों का दबदबा है। जहां करोड़ों लोगों के लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करना भी मुश्किल है, वहीं पिछले सालों में इन कंपनियों ने रिकार्ड तोड़ मुनाफ़े कमाए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक़, इस समय संसार की 9.8 फ़ीसदी आबादी यानी 83 करोड़ लोग भुखमरी का शिकार हैं, लेकिन संसार स्तर पर लगभग एक तिहाई अनाज किसी के पास पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाता है, क्योंकि इसे मुनाफ़े में नहीं बेचा जा सकता। यह तस्वीर मौजूदा व्यवस्था की बर्बरता को दर्शाती है, जहां अनाज का गल-सड़ जाना मंजूर है, लेकिन उसे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जाता, क्योंकि इससे मुनाफ़ा कम हो जाएगा।
इससे भी बड़ी बात यह है कि कंपनियां अकसर ही अनाज की जमाखोरी और सट्टेबाजी जैसी कार्रवाइयों से अनाज की दरों को नकली रूप से बढ़ाती हैं। 2008-2011 में ऐसी कंपनियों; मुख्य तौर पर गोल्डमैन सैच ने ऐसी गतिविधियों से गेहूं की क़ीमतों को 40 फ़ीसदी तक बढ़ा दिया है।
केवल यही नहीं वे जगहें जहां सबसे ज़्यादा अनाज उत्पादन होता है, उनमें भूख से पीड़ित लोगों की संख्या सबसे अधिक है। थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और म्यांमार जैसे देशों की लगभग 50 फ़ीसदी कृषि भूमि पर सोयाबीन, गेहूं, चावल, मक्का की फ़सलें उगाई जाती हैं, जोकि संसार के कुल अनाज निर्यात का 86 फ़ीसदी हिस्सा है, इसके बावज़ूद थाईलैंड और पाकिस्तान के 17 फ़ीसदी, म्यांमार के 25.5 फ़ीसदी लोग भोजन सुरक्षा से वंचित हैं।
कई पिछड़े देशों में मुख्य तौर पर व्यापारिक फ़सलों को ही उगाया जाता है, इसलिए ये देश अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर अनाज दूसरे देशों से आयात करते हैं, जिसके कारण इन देशों में लगातार जनता पर भोजन असुरक्षा की तलवार लगातार लटकती रहती है। ये सभी बातें इस धारणा को झुठलाती हैं कि भुखमरी का असल कारण जनसंख्या है।
बेरोज़गारी, ग़रीबी और भुखमरी के लिए माल्थस के सिद्धांत का जवाब देते हुए मज़दूर वर्ग के शिक्षक फ्रे़डरिक एंगेल्स ने लिखा है, कि–
“भूख उत्पादन की कमी के कारण नहीं, बल्कि इस मुनाफ़ा-केंद्रित ढांचे के कारण बनी रहती है, इसलिए नहीं कि उत्पादन की सीमाएं आज वर्तमान संसाधनों के साथ समाप्त हो गई हैं, ऐसा नहीं है।लेकिन उत्पादन की सीमाएं भूखे पेटों की संख्या से नहीं बल्कि ख़रीदने और भुगतान करने में सक्षम लोगों की संख्या से निर्धारित होती हैं।..
..पूंजीवादी समाज और इससे अधिक उत्पादन की इच्छा नहीं रखता और ना ही ऐसी इच्छा कर सकता है। पैसा रहित पेट व श्रम; जो लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और इसलिए वह भोजन ख़ुद नहीं ख़रीद सकता और उसकी मौत का दर आंकड़ों के लिए छोड़ दिया जाता है।”
एक ऐसा समाज जो मानवता को इस बाज़ार के पागलपन से मुक्त करेगा, जहां उत्पादन का मक़सद इंसानी ज़रूरतों को पूरा करना होगा, ऐसे समाज में ही इस समस्या का हल संभव है।
(स्वदेश कुमार सिन्हा स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)