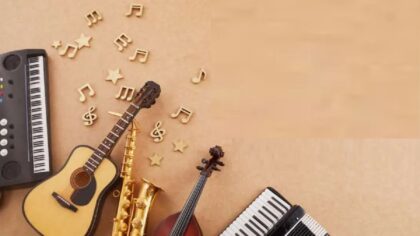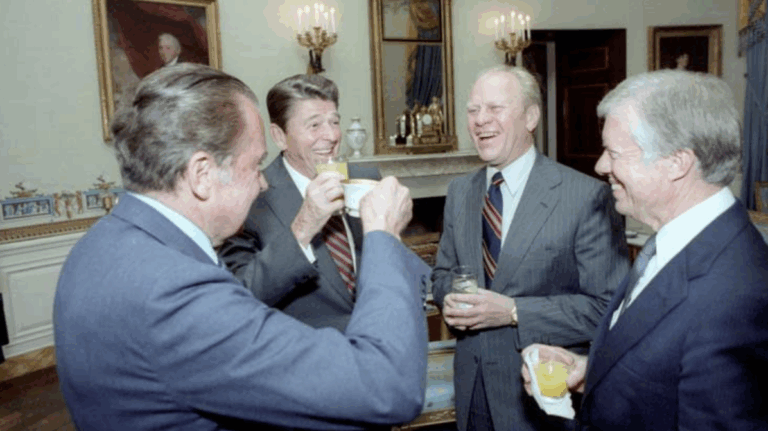न्यायाधीश विशिष्ट होते हैं या न्याय विशिष्ट होता है? यह एक ध्यान खींचने वाली बात है, इसलिए नहीं कि यह बुझौवल जैसा है। यह मसला कोर्ट की अवमानना के मुख्य धुरी से जुड़ा हुआ है। इसके पहले दो बार इस मसले पर चर्चा हो चुकी है। लेकिन मानवाधिकारवादी वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ कोर्ट अवमानना के दो केस सर्वोच्च न्यायालय में आ जाने की वजह से यह बहस तीखे तरीके से वापस आयी है।
पहला केस जिसे तहलका केस कहा जाता है, 2009 का है और इस पर पिछले आठ सालों में सुनवाई ही नहीं हुई है। अब जबकि कोविड संकट का दौर चल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय वर्चुअल तकनीक पर काम कर रहा है और बहुत सारे केसों को ‘एकदम जरूरी नहीं है’ बताकर खारिज कर दिया गया, ऐसी स्थिति में इस केस को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है? जबकि न्यायपालिका के पास नागरिक संशोधन अधिनियम के लिए समय नहीं है या जम्मू और कश्मीर से बंदी प्रत्यक्षीकरण की अपील पड़ी है; तो क्या हम यह मान लें कि यह मसला इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है?
निश्चित ही, कोर्ट की चिंता न्यायपालिका पर लगे आरोपों और भ्रष्टाचार पर है। ये आरोप प्रशांत भूषण ने लगाये और तहलका ने इसे प्रकाशित किया। लेकिन यदि इसने इस कदर कोर्ट पर अफवाहें बना दीं तब कोर्ट ने 11 सालों में कार्रवाई क्यों नहीं की? दूसरी अवमानना रहस्यमयी है। यह भूषण के एक ट्वीट से बन गया जिसमें वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के फोटोग्राफ पर टिप्पणी की गई है। न्यायपालिका का दावा है कि ट्वीट ‘‘न्याय प्रशासन को विवाद के घेरे में ला दिया …सर्वोच्च न्यायालय की आम तौर पर एक संस्था के बतौर और खासकर भारत के मुख्य न्यायाधीश की सत्ता और अस्मिता को कमजोर किया है।
कोर्ट की अवमानना के इन दो मसलों ने न्यायपालिका का ध्यान खींचा है। यही कारण है कि जो प्रश्न उठा रहा हूं वह बेहद महत्वपूर्ण है। जहां तक केस की बात है उसे पिछले सप्ताह (चौथी और पांचवीं) में सुनवाई हुई और इन दोनों केसों में तीन जजों की बेंच थी जिसकी अध्यक्षता न्यायाधीश अरुण मिश्रा कर रहे थे। इस बेंच ने निर्णय को सुरक्षित रखा। इसे संभव है एक हफ्ते या 10 दिन में सुना दिया जाए। यदि अच्छी बातें बनी रहीं तो उन्हें सजा तो नहीं ही होनी चाहिए। मैं सारा दांव अच्छी समझ पर लगा रहा हूं जो इस मसले में जरूरी है। इस सवाल का जवाब शुरुआत से ही इसी पर निर्भर है।
कोर्ट की अवमानना की अवधारणा सदियों पुराने ब्रिटिश कानून से जुड़ा हुआ है जिसे (खुद ब्रिटेन में) 2013 में खत्म कर दिया गया। जब कानून बना था तब ब्रिटिश लाॅ कमीशन ने कहा था कि उद्देश्य सिर्फ ‘‘न्यायाधीशों की गलत बातों में जनता के घुसने से रोकना ही नहीं है …यदि गलतियां हो जाती हैं तो उतना ही जरूरी है कि जनता को सही बात तक पहुंचने से रोक दिया जाए।’’ दूसरे शब्दों में यह कि न्यायपालिका के भ्रष्टाचार को छुपा लिया जाए। यह अवधारणा पारदर्शिता की जरूरत और निश्चित ही बोलने की आजादी से भी टकराती है।
1968 की बात है, लार्ड डेनिंग जो ब्रिटेन के पूर्व मास्टर ऑफ रोल्स थे, ने कोर्ट की अवमानना पर कहा थाः ‘‘मुझे एक बात तो एकदम से कह देनी है कि हमें अपनी ही अस्मिता की रक्षा में इस न्यायिक तरीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ….न ही उन लोगों को दबाना चाहिए जो हमारे खिलाफ बोलते हैं। हमें आलोचनाओं से नहीं डरना चाहिए और न ही इससे बेचैन होना चाहिए। इन बातों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बातें दांव पर लगी हैं। यह बोलने की आज़ादी से कम तर नहीं हैं। यह हरेक इंसान का अधिकार है, जो संसद में हैं या जो संसद के बाहर हैं; यह प्रेस में हो या उसके प्रसारण में हो, न्यायपूर्ण टिप्पणी हो भले ही जनता के हितों से जुड़े मसलों में बढ़कर बोला गया हो ….हमें अपने व्यवहार पर निर्भर होना ही चाहिए, यही खुद को स्थापित करेगा।’’
1987 में स्पाईकैचर निर्णय के बाद जब डेली मिरॅर ने ब्रिटिश लाॅ लाॅर्ड्स को ‘‘तुम बूढ़े मूखों’’ शब्दों से नवाजा या 2016 में जब ब्रेक्जिट लागू हुआ तब डेली मिरॅर ने ब्रिटिश न्यायपालिका के तीन जजों को ‘‘जनता के दुश्मन’’ लिखा तो इस सचेत और समझ के साथ इन शीर्षकों को नजरंदाज कर दिया गया और इन बातों को कोर्ट की अवमानना में नहीं गिना गया। वास्तव में लार्ड टेम्पल्टॅन की स्पाईकैचर पर की गई टिप्पणी को दोहरा लेना अच्छा रहेगाः ‘‘मैं कैसे नकार सकता हूं कि मैं बूढ़ा हूं। यह सच्चाई है। जहां तक रही बात इसकी कि मैं मूर्ख हूं या नहीं, यह लोगों की अवधारणा का मसला है …सत्ता की अवमानना लागू करने की कोई जरूरत ही नहीं है।’’
मार्कंडेय काटजू ने भी 2008 के एक व्याख्यान में इसी तरह की अवस्थिति ली। ‘‘यदि कोई मुझे मूर्ख कहता है, चाहे वह कोर्ट हो या बाहर मैं इस पर कोई कार्रवाई नहीं करूंगा जब तक कि वह मेरे काम में बाधा नहीं खड़ा कर देता। मैं इस टिप्पणी को या उसकी टिप्पणी से मुतमईन लोगों के दावे को यूं गुजर जाने दूंगा। अंततः बात यही है कि शब्द हड्डियां नहीं तोड़ते।’’
न्यायाधीश काटजू एक जरूरी बात बोलते हैंः ‘‘कोई कार्रवाई कोर्ट की अवमानना है या नहीं यह तय करने के लिए यह देखना है- क्या इससे जज को काम करना असंभव या एकदम कठिन बन गया है? यदि ऐसा नहीं होता है तब यह कोर्ट की अवमानना नहीं है, भले यह कठोर आलोचना हो ….केवल एक ही स्थिति में जहां मैं कार्रवाई करूंगा जब एक जज की तरह काम करना ही संभव नहीं रह जायेगा ….मुझे तो काम करना ही होगा कि जो मुझे वेतन मिलता है उसके साथ न्याय कर सकूं।’’
मेरी समझ में मेरे सवाल के साथ ही जवाब लगा हुआ है। जबकि न्याय महत्वपूर्ण है तब न्यायाधीशों को खुद को तवज्जो में नहीं रखना चाहिए। तब भी जब उनके आत्मसम्मान पर सवाल उठ गया हो। इसका अर्थ यह नहीं होता है कि संस्था पर ही सवाल उठ गया है या न्याय को अनादृत कर दिया गया है। जज न्याय करते हैं लेकिन वे खुद ही न्याय नहीं हैं। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कोर्ट सर्वोच्च है क्योंकि अनंतिम है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यह गलतियों से परे है। यदि कमी रह जायेगी तो उनकी आलोचना भी हो सकती है, जो निश्चय ही उचित और शिष्ट तरीके से हो।
मुझे उम्मीद है कि भूषण के दो केसों पर निर्णय देते समय इन बातों का खयाल रखा जायेगा।
(वरिष्ठ स्तंभकार करन थापर का यह लेख 10 अगस्त को दि इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ था। इसका हिंदी अनुवाद लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता अंजनी कुमार ने किया है।)