साथियों, तवारीख़ के पन्नों में 28 सितम्बर मार्च सिर्फ एक दिन के रूप में दर्ज नहीं है।यह वह तारीख़ थी जब हिन्दुस्तान की जवानी ने अपने सबसे मजबूत फूल को खिलते हुए देखा। इस फूल की गंध ने एक नए रास्ते को रौशन किया था। वह रास्ता जिस पर चल कर दुनिया भर के सताए हुए लोगों और राष्ट्रों को साम्राज्यवादी शोषण के जुए को उतार फेकना था।
इस रास्ते ने हमे एक दिशा दी है, ताकी अन्याय पर आधारित मौजूदा समाज-व्यवस्था में आमूल परिवर्तन किया जा सके और मजदूर-किसान एकता पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की जा सके। यह दिन हमारे सच्चे साथ शहीद और उनकी वैचारिक विरासत को याद करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर करने का दिन है।
मैं अपनी बात क्रांतिकारी कवि पाश की कविता की इन पंक्तियों से शुरू करना चाहूँगा-
‘हथौड़ा अब भी चलता है, उदास निहाई पर
हल अब भी चलता है चीख़ती धरती पर
यह काम हमारा नहीं बनता है, सवाल नाचता है
सवाल के कन्धों पर चढ़कर
हम लड़ेंगे साथी’
आज मैं अपनी बात वर्तमान समय में भगत सिंह के विचारों की प्रासंगिकता पर केन्द्रित करूंगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम उन परिस्थितियों से परिचित हो जाएं जिनमें भगत सिंह के व्यक्तित्व का विकास हुआ। यहां मैं कुछ पंक्तियां उधृत करना चाहता हूं, जिन्हें मैंने चमनलाल जी की पुस्तक से लिया है।
“एक युवक, जो साढ़े तेईस वर्ष की आयु में देश की स्वाधीनता के लिए क्रांतिकारी कार्यवाहियों के अपराध में फांसी चढ़ गया हो, वह युवक फांसी चढ़ने वाले सैंकड़ों अन्य युवकों से अलग या सम्मिलित रूप से उन सबका प्रतीक कैसे बन सकता है?
लेकिन यदि वह युवक बारह वर्ष की आयु में ही जलियांवाला बाग की मिट्टी लेने पहुंच जाए और इस छोटी उम्र से ही लगातार सोचने विचारने की प्रक्रिया में पड़ जाए तो वह युवक 1923 में सोलह वर्ष की आयु में ही घर छोड़ देता है और सत्रह साल की आयु में ‘पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या’ पर एक प्रौढ़ चिंतक की तरह लेख लिखने लगता है।
और क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ-साथ निरंतर अध्ययन, चिंतन और लेखन में भी लगा रहता है तो ऐसे युवक के क्रांतिकारी चिंतक का प्रतीक बनने की स्थितियां बन ही जाती हैं।“
भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह आर्यसमाजी होने से कुछ हद तक तार्किक स्वभाव के थे। भगतसिंह के दो चाचा स्वाधीनता संग्राम में अपना जीवन समर्पित कर चुके थे। एक चाचा स्वर्ण सिंह जेल की यातनाओं से 23 वर्ष की आयु में 1910 में प्राण दे चुके थे और एक चाचा अजीत सिंह देश से 1909 में निर्वासित हो चुके थे।
भगत सिंह के पिता किशन सिंह कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। भगत सिंह के पिता व भगत सिंह की राजनीतिक गतिविधि का केन्द्र लाहौर था। जब भगत सिंह एफ.ए. पास कर बी.ए. कक्षा में पढ़ रहे थे, तब वे पढ़ाई छोड़ कर क्रांतिकारी दल के बौद्धिक चिंतक व संगठनकर्ता बन कर उभरे।
आखिर भगत सिंह के विचारों लक्ष्य क्या था ?
हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भगत सिंह का लक्ष्य था साम्राज्यवाद का नाश। भगत सिंह की साम्राज्यवाद को लेकर समझ बिलकुल साफ थी। वे साफ़ शब्दों में कहते हैं- मनुष्य द्वारा मनुष्य का तथा राष्ट्र द्वारा राष्ट्र का शोषण ही साम्राज्यवाद है।
उस समय हिन्दुस्तान बर्तानिया हुकूमत के बूटों तले रौंदा जा रहा था। औपनिवेशिक सत्ता हिन्दुस्तानी अवाम का बेतरह शोषण कर रही थी। जनता के शोषण में ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों की रक्षा करने वाले भारतीय शासक वर्ग की भूमिका भी उतनी ही क्रूर थी।
इस शासक वर्ग में बड़े भारतीय पूंजीपति और सामन्तवादी शक्तियां शामिल थीं। इसलिए भगत सिंह न सिर्फ ब्रिटिश शक्ति को भारत से बाहर करना चाहते थे बल्कि वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के भारतीय दलालों को भी सत्ता से बहार करना चाहते थे।
अब सवाल उठता है कि भगत सिंह किस तरह का इन्कलाब चाहते थे और सत्ता पर किसका हक चाहते थे?
इसका जवाब भगत सिंह के लेखन में मिलता है- वे साफ़ तौर पर कहते हैं कि, “इन्कलाब का अर्थ मौजूदा सामाजिक ढांचे में पूर्ण परिवर्तन और समाजवाद की स्थापना है। आगे वे कहते हैं कि ऐसा इन्कलाब लाने के लिए हमारा पहला कदम ताकत हासिल करना है।
अपनी शहादत के 15 वर्ष पहले ही भगत सिंह ने यह अनुमान लगा लिया था कि यदि अंग्रेज भारत से बाहर गए भी तो ये सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण होगा। गोरे अंग्रेजों की जगह भूरे अंग्रेज ले लेंगे। इससे आम जनता के कष्ट कम नहीं होंगे।”
आज इसे हम साफ़ तौर पर देख रहे हैं।
अब सवाल है कि यह ताकत केन्द्रित कहां होती है?
भगत सिंह कहते हैं- निश्चित रूप से ‘राज्य’ के हाथों में। वास्तव में ‘राज्य’ यानी सरकारी मशीनरी, शासक वर्ग के हाथों में अपने हितों की रक्षा करने और उन्हें आगे बढ़ाने का यंत्र ही है। हम इस यंत्र को छीनकर अपने आदर्शों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं।
आगे वे कहते हैं कि साम्राज्यवादियों को गद्दी से उतारने के लिए भारत का एकमात्र हथियार श्रमिक क्रान्ति है। भगत सिंह और उनके साथी भारत सहित पूरी दुनिया में मजदूर-किसान एकता पर आधारित लोकतांत्रिक-समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। यही था उन शहीदों का वह महान लक्ष्य जिसके लिए वे अपनी अंतिम सांस तक लड़े।
अब सवाल है कि ये विचार आज के दौर में कैसे लागू किये जाएं और हम अपने लिए कौन से कार्यभार तय करें?
इसके लिए हमें भगत सिंह के विचारों के आलोक में वर्तमान भारतीय राज्य और समाज व्यवस्था को समझना होगा। इसे एक सामान्य से सवाल से शुरू करते हैं। क्या वास्तव में भारत में जनवादी लोकतंत्र स्थापित है या यह भूरे अंग्रजों की सत्ता है?
क्या आज भी औपनिवेशिक दौर की तरह जनता बदहाल नहीं है? क्या आज भी युवा बेरोजगारी से तंगहाल नहीं? क्या आज भी धर्म और साम्प्रदायिकता के जहर ने समाज को बांट नहीं रखा है? जाति का नशा क्या अभी टूटा है?
जरा ध्यान दीजिए अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई पर। क्या इस देश के राजनेता भ्रष्टाचार में गले तक नहीं डूबे हैं? इस देश को पूंजीवादी-साम्राज्यवादी शक्तियां घुन की तरह खाए जा रही हैं।
दूसरे विश्व-युद्ध के बाद अपने आंतरिक संकटों के चलते साम्राज्यवादियों के लिए गुलाम राष्ट्रों पर सीधे नियंत्रण रखना संभव नहीं था। रूस की समाजवादी क्रांति और दुनियाभर के गुलाम राष्ट्रों में उठते विरोध के चलते साम्राज्यवादियों ने सत्ता का हस्तांतरण ऐसे हाथों में किया जिससे वे अप्रत्यक्ष रूप से अपना शासन-शोषण जारी रख सकें।
इसके लिए नव-औपनिवेशिक व्यवस्था को लाया गया। अब साम्राज्यवादी देश गुलाम राष्ट्रों पर सीधे नियंत्रण न रख के अपने स्थानीय भारतीय दलालों की मदद से जनता का शोषण कर रहे हैं।
ये भारतीय दलाल कोई और नहीं बल्कि इस देश के बड़े पूंजीपति, सामंती शक्तियां, भ्रष्ट राजनेता और नौकरशाही में उच्च पदों पर बैठे लोग हैं।
आज विश्व-साम्राज्यवाद आर्थिक संकट में है। अपने मुनाफे को बनाये रखने के लिए जनता के शोषण को लगातार बढ़ाने अलावा इसके पास और कोई चारा नहीं है। ऐसे में दुनिया भर में जनता आंदोलनरत है। भारत, फ्रांस, स्पेन, अमेरिका, ब्राजील, और दुनियाभर के तमाम देशों में कृषि संकट के कारण किसान बड़े पैमाने पर आन्दोलन कर रहे हैं।
मजदूरों की खस्ता हालत ने उन्हें सड़कों पर आने को मजबूर कर दिया है। ऐसे में जनता पर युद्ध लादा जा रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध दो देशों का युद्ध न होकर साम्राज्यवादियों के आपसी अन्तर्विरोध का परिणाम है। इजरायल का फिलिस्तीन पर हमला और फिलिस्तीनी जनता का नरसंहार इन्हीं साम्राज्यवादियों की देन है।
भगत सिंह ने साफ़ कहा था कि जबतक हम अन्याय पर आधारित इस साम्राज्यवादी व्यवस्था का अंत नहीं कर देते तब तक ये हमारे ऊपर युद्धों को लादती रहेगी।
आज साम्राज्यवाद अपने संकटों के कारण फ़ासीवाद में बदल गया है। हम इसे भारत के सन्दर्भ में आसानी से देख सकते हैं।शोषण के खिलाफ बढ़ते जनता के आन्दोलनों को दबाने के लिए यह फासीवादी सत्ता जाति, धर्म, क्षेत्रीयता, लिंग, भाषा आदि को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है।
जाति भारत की सच्चाई है।आप यदि ध्यान से आंकड़ों को देखें तो पायेंगे की जाति और आर्थिक स्थिति में काफी ओवरलैप दिखता है। जातीय शोषण ने इस देश की बड़ी आबादी से सामान्य इंसानी आधिकार तक छीन लिए।
उन्हें अछूत करार दिया गया। इनके छूने भर से पानी गन्दा हो जाता है, देवता नाराज हो जाते हैं, उनके स्पर्श मात्र से तथाकथित ऊंची जाति के अमानुषों का धर्म भ्रष्ट हो जाता है। यह 21वीं सदी का सच है।
जाति आधारित इस शोषण को एक वास्तविक समस्या के रूप में स्वीकार करने से भारत की वामपंथी पार्टियों ने लगातार इनकार किया है। और उनकी बदहाली का एक बड़ा कारण भी ये है। पर भगत सिंह ने जातीय शोषण को खत्म करने के लिए जो रास्ता सुझाया था वो हमारे काफी काम का है।
‘अछूत का सवाल’ नामक अपने लेख में भगत सिंह ने जाति के सवाल पर कहा था कि जाति व्यवस्था हिन्दू धर्म के सिद्धांतों पर टिकी है। पुनर्जन्म के सिद्धांत द्वारा लोगों को भ्रमित करती है साथ ही कार्यों के प्रति घृणा को भी जन्म देती है। भगत सिंह ने कहा था कि अछूतों को अपने को संगठित करना चाहिए और उन्हें अपने समुदाय से अपने नेता भी चुनने चाहिए।
उन्होंने कहा था की गांधीवादी सुधारवादी विचारों के भरोसे यह समस्या हल नहीं हो सकती बल्कि इसके लिए एक सम्पूर्ण राजनीतिक और आर्थिक क्रांति की जरूरत होगी। क्या यही वे कार्यवाहियां नहीं हैं जिनकी आज जरूरत है।
धर्म के मसले पर ‘धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम’ नामक लेख में भगत सिंह ने सभी धर्मों की कट्टरता को निशाने पर लिया है।वे इसे समानता के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। उस समय चलने वाले धर्म-सुधार आन्दोलनों को उन्होंने निशाने पर लिया था।
दयानंद स्वारस्वती के धर्म-सुधार आन्दोलन की आलोचना करते हुए उन्होंने इसके वर्णवादी विचारों पर निशाना साधा था। भगत सिंह ने साफ़ कहा था कि “धर्म घर में रखते हुए भी, लोगों के दिलों में भेदभाव बढ़ाता है।” ‘मैं नास्तिक क्यों हूं’ जैसा लेख उनके इन्हीं विचारों का उत्स था।
आगे वे ‘सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज’ नामक लेख में साम्प्रदायिकता को बढ़ाने में मीडिया और राजनेताओं की भूमिका की भी आलोचना की थी। क्या आज भी फासीवादी राज्य इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल दंगे भड़काने व जातीय जनसंहार के लिए नहीं कर रहा है।
साम्प्रदायिकता से लड़ने के लिए आर्थिक उन्नति को भगत सिंह एक इलाज के रूप में पेश करते हैं। आज हम देखते हैं कि ऐसे दंगों या नरसंहार में मुख्य रूप से बेरोजगार युवा ही शामिल होते हैं। यही लम्पट सर्वहारा धर्म की राजनीति करने वालों के काम आते हैं।
साथ ही वे राजनीति से धर्म की बेदखली की भी बात करते हैं। पर क्या आज हमारे देश में संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए नेता धर्म की राजनीति खुले तौर पर नहीं कर रहे? इसके खिलाफ सिर्फ वर्ग-चेतना ही सभी शोषित जनों को एक कर सकती है। इसके बिना फ़ासीवाद के खिलाफ कोई भी सम्पूर्ण लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है।
(ज्ञानवर्धन सिंह केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हैं)

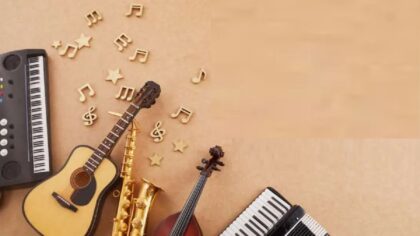





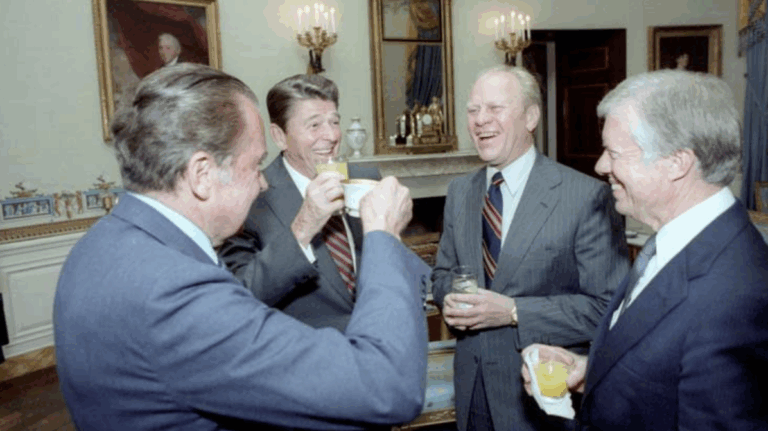

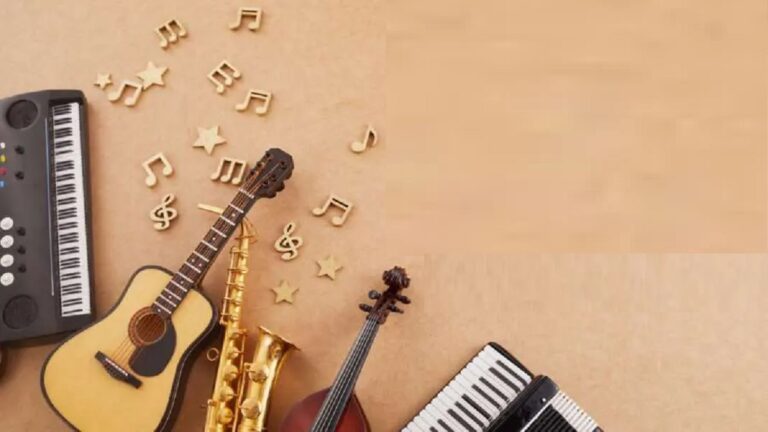




आपका आभार,बहुत उन्नत लेख है,यह वर्तमान समय में क्रांतिकारिता के लिए पहला पन्ना हो सकता है।