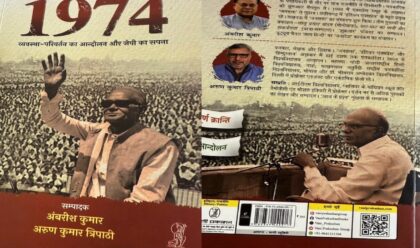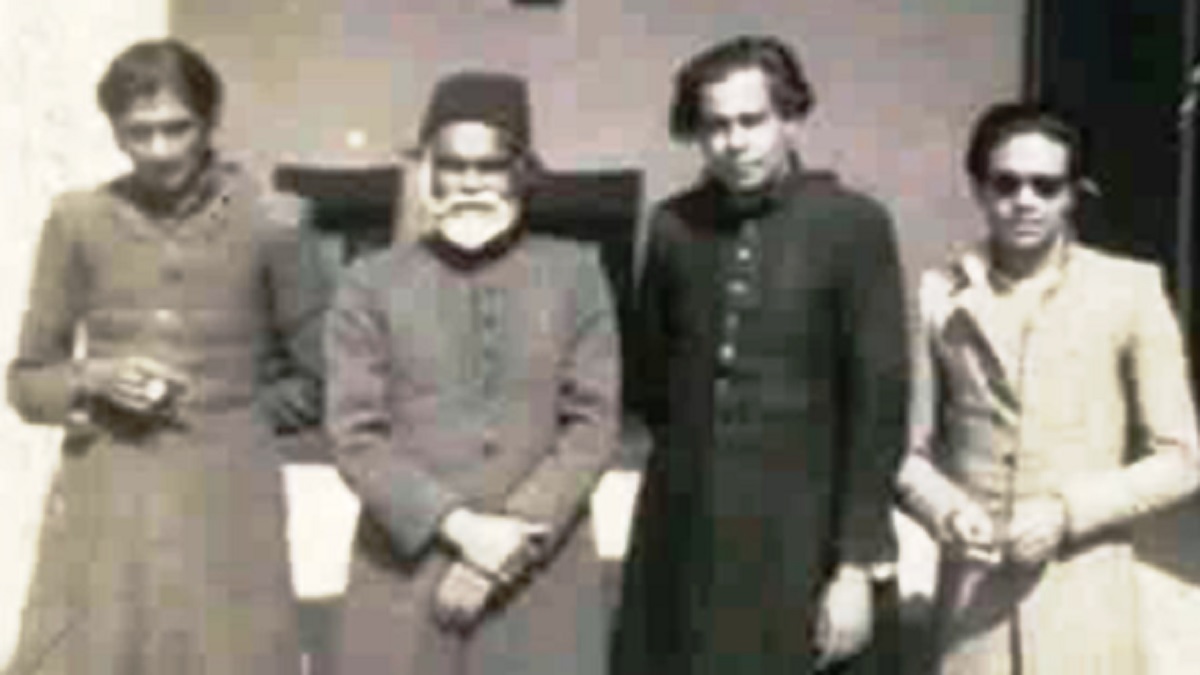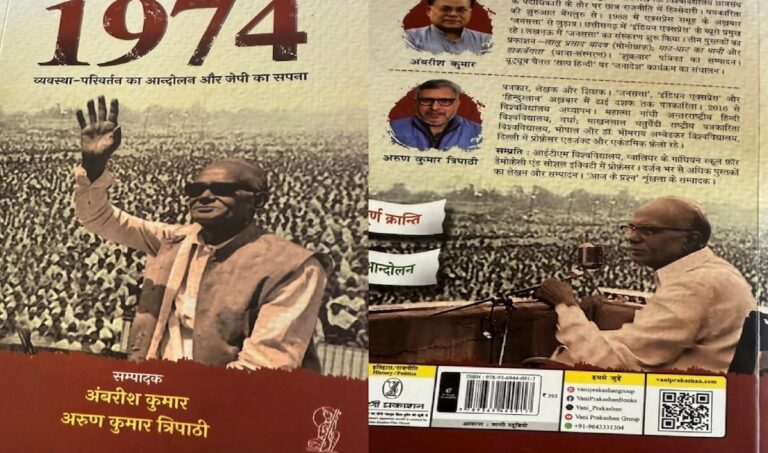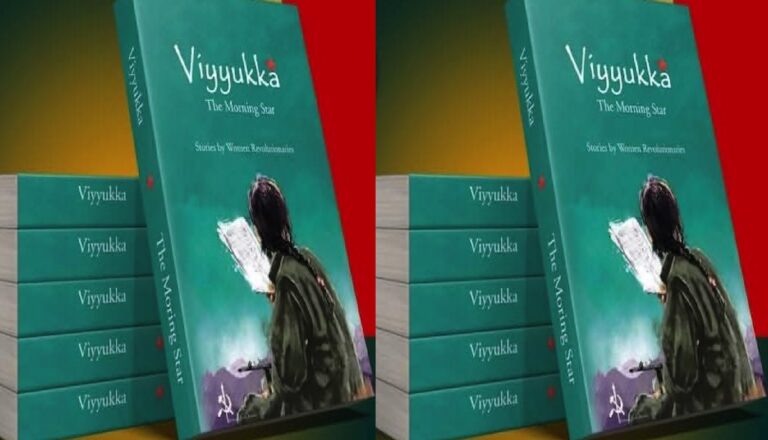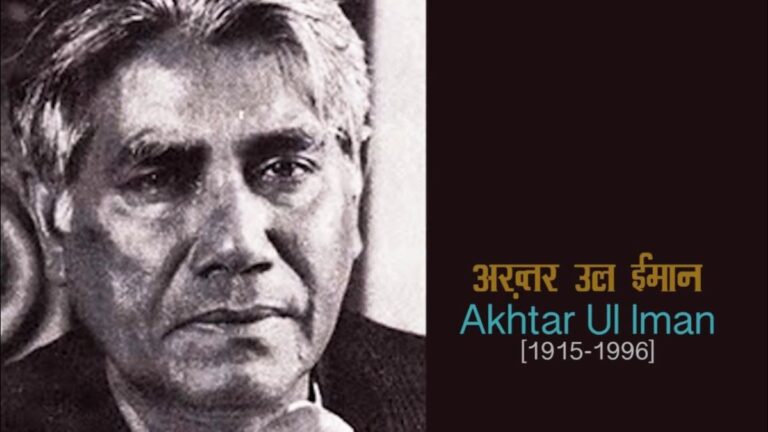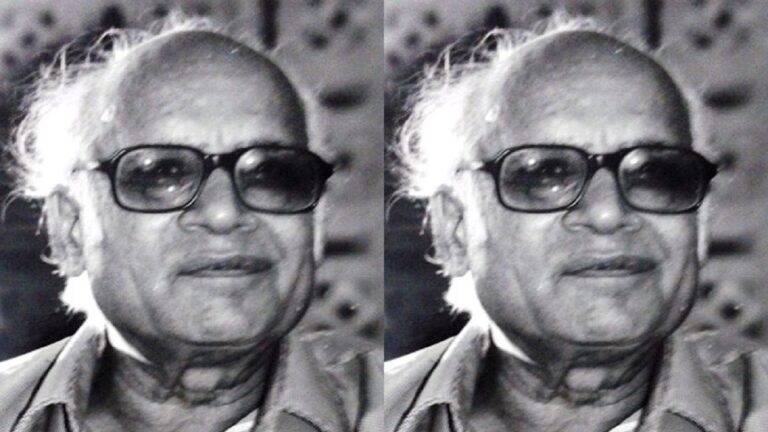आज 19 अक्टूबर हर-दिल-अज़ीज़ शायर मजाज़ का जन्मदिवस है। अपनी चवालीस साला ज़िंदगी में मजाज़ ने अदबी दुनिया में ख़ूब नाम कमाया। तरक़्क़ीपसंद शायरों में उनका एक अहम मुक़ाम है। भारतीय उप महाद्वीप के मशहूर शायर फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने मजाज़ की एक मात्र किताब ‘आहंग’ की भूमिका लिखी थी। अपनी भूमिका में फ़ैज़ उनकी शायरी का मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं, ‘मजाज़ इंक़लाब का ढिंढोरची नहीं, इंक़लाब का गायक है। उसके नग़मे में बरसात के दिन की सी सुकूनबख़्श खुनकी है और बहार की रात की सी गर्मजोश तास्सुर आफ़रीनी (आंतरिक अनुभूति पैदा करती) थी।’
मजाज़ के कलाम के बारे में कमोबेश यही बात अली सरदार जाफ़री ने भी कही है,‘मजाज़ की शायरी शमशीर, जाम और साज का इम्तिज़ाज (मिश्रण) है।’ सज्जाद ज़हीर की नज़र में ‘मजाज़ इंक़लाब, तब्दीली और उम्मीद का शायर है।’ बल्कि उनका तो यहॉं तक मानना था, ‘मजाज़ ने उर्दू की इंक़लाबी शायरी का रिश्ता फ़ारसी और उर्दू की बेहतरीन शायरी से जोड़ा है।’ फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, मजाज़ की ‘ख़्वाब-ए-सहर’ और ‘नौजवान ख़ातून से ख़िताब’ नज़्मों को सबसे मुकम्मल और सबसे कामयाब तरक़्क़ीपसंद नज़्मों में से एक मानते थे।
अली सरदार जाफ़री से मजाज़ का काफ़ी याराना और साथ रहा। जाफ़री उन्हें और उनकी शायरी को बेहद पसंद करते थे। तरक़्क़ीपसंद अदबी तहरीक के पचास साल पूरा होने पर सरदार जाफ़री ने एक किताब ‘तरक़्क़ीपसंद तहरीक निस्फ़ सदी’ में लिखी, जो उस वक़्त बहुत मक़बूल रही। किताब में एक जगह उन्होंने मजाज़ को भी याद किया है, लेकिन फ़िराक़ गोरखपुरी के बहाने। फ़िराक़ साहब ने जब पहली बार मजाज़ की शायरी पढ़ी, तो उसका उन पर क्या असर पढ़ा ? फ़िराक़ ने यह सब बातें बड़ी तफ़्सील से लिखी हैं। जो कि किसी ज़माने में एक मैगज़ीन में एक लेख के तौर पर प्रकाशित हुई थीं।
(‘जनचौक’ के पाठकों के लिए पेश है, किताब ‘तरक़्क़ीपसंद तहरीक निस्फ़ सदी’ का एक हिस्सा, जिसमें मजाज़ की दिल-आवेज़ शख़्सियत और उनकी शायरी की ख़ासियतें क्या ख़ूब उभरकर सामने आई हैं। -ज़ाहिद ख़ान)
1937 का ज़माना था, कोई हफ़्तावार अख़बार जिसका नाम ग़ालिबन ‘हिंदुस्तान’ था, लखनऊ से मेरे नाम आने लगा। उस अख़बार में एक नज़्म मेरी नज़र से गुज़री, उस ज़माने में ऐसी नज़्म बहुत कम देखने में आती थीं। मिसरे दरिया की तरह जोश मारते बढ़ रहे थे। रात के अंधेरे और सन्नाटे को रेल की गड़गड़ाहट चीरती-फाड़ती चली जा रही थी। ये नज़्म थी मजाज़ की, जिनका नाम मैंने उस वक़्त तक नहीं सुना था। मुझे महसूस हुआ कि एक नई आवाज़ ने उर्दू में जन्म लिया है।
अभी इस नज़्म का असर धीमा नहीं पड़ा था कि इस पर्चे में कुछ हफ़्तों बाद मजाज़ की दूसरी नज़्म ‘अंधेरी रात का मुसाफ़िर’ नज़र आई। ये नज़्म और भी भूचाल पैदा करनेवाली थी। दोनों नज़्म यथास्थिति के ख़िलाफ़ थीं। ये नज़्में तरक़्क़ीपसंद शायरी के ऐलान, मेनिफेस्टो की हैसियत रखती थीं। ये आवाज़ इक़बाल, जोश, अख़्तर शीरानी या उर्दू शायरी के दूसरे शायरों की प्रतिध्वनि नहीं थीं। शायरी के आसमान पर एक नये सितारे के नृत्य का सरगम, इस नई आवाज़ में सुनाई दे रहा था।
ये आवाज़ सुनकर, हज़ारों लोगों के जिस्मों में दिल की धड़कन और ख़ून की ग़र्दिश तेज़ हो जाती थी। सामूहिक ज़िंदगी की रफ़्तार बढ़ जाती थी। ये आवाज़ क़ौमी ज़िंदगी की तक़दीर की आवाज़ मालूम होती थी। वो तक़दीर जो यकायक जाग उठी थी। दोनों नज़्में पुनर्जागरण के उत्सव की हैसियत रखती थीं। दोनों नज़्मों में ‘रात’ एक नई सुबह की पृष्ठभूमि बन जाती थी। मिसरों से किरणें फूटती थीं। शोले लपकते थे।
इसके कुछ हफ़्तों बाद इसी अख़बार में मजाज़ की तीसरी नज़्म ‘आवारा’ शाए हुई। कलात्मक और संकेतों की दृष्टि से ये नज़्म और भी निकलती हुई थी। इस तेवर की नज़्म इससे पहले शायद ही देखने में आई होगी। मुझ पर इस नज़्म ने दोहरा असर डाला। एक तो असर वही, जिसे मैंने अभी बयान कर दिया है। दूसरा असर, अल्प चेतन या अवचेतन था।
ये नज़्म, शायर की ज़िंदगी के आख़िरी छह-सात साल और उसके दु:खद अंत की जैसे भविष्यवाणी थी। ये नज़्म बारूद पर चिंगारी के मंडलाने का मंज़र पेश कर रही थी। नज़्म की नोक पलक आँख का धोका भी थी। और ख़तरे का ऐलान भी कर रही थी। एक सोये हुए ज्वालामुखी के अनक़रीब फट जाने की गड़गड़ाहटें इस नज़्म में सुनाई देती थीं।
नज़्म में एक ख़तरनाक दिल-कशी थी। इसमें चुंबकीय कशिश थी। पहली दोनों नज़्मों में स्वस्थ्य वस्तुनिष्ठता और विषयपरकता थी। इस तीसरी नज़्म में एक संवेदनशील शायर को तोड़कर रख देनेवाली, रोंगटे खड़े कर देनेवाली व्यक्तिगत भावनाओं और आंतरिक स्थितियों का चित्रण था। मगर नज़्म के जादू और आकर्षण से इंकार नामुमकिन था।
ये नज़्म मजाज़ के अंदर छुपी हुई उस आग का पता देती थीं, जो शायर को एक दिन फूंक कर रख देगी। इस नज़्म के मुताल्लिक़ मैं इतनी बातें एक सांस में कह गया। लेकिन ये प्रभाव एक सांस में नहीं पिरोए थे। बात ये हुई कि इस नज़्म में जो बार-बार याद आने की ख़ासियत यानी मानवता का गुण था। इसके प्रभाव में धीरे-धीरे मन में इस नज़्म से संबंधित ये विचार संकलित होते रहे।’’
मजाज़ की नज़्में ‘आवारा’ और ‘अंधेरी रात का मुसाफ़िर’ देहली और लखनऊ के दौर की नज़्में हैं। जब तरक़्क़ीपसंद तहरीक बाक़ायदा शुरू हो चुकी थी। लेकिन ‘रात और रेल’ तहरीक के शुरू होने से पहले, अलीगढ़ के दौर की यादगार है। उसी ज़माने की मजाज़ की वो नज़्में हैं, जो देखने में रोमांटिक मालूम होती हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर एक समाजी चेतना की प्रतिनिधि हैं, जो उसकी एक सोच में सिमट आई हैं।
तेरे माथे पे ये आँचल बहुत ही ख़ूब है लेकिन
तू इस आँचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था।
ये औरतों की तहरीक-ए-आज़ादी का परचम है। जिसकी चेतना मजाज़ को अलीगढ़ की डॉ. रशीद जहाँ की नज़दीकी के अलावा डॉ. अंसारी के देहली के घर से मिला था। जहाँ उनकी ख़ूबसूरत भतीजी जे़हरा मेजबान होती थीं और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू और महात्मा गांधी भी मेहमान होते थे। और मजाज़ की नज़्में शौक़ से सुनते थे। उसी ज़माने की नज़्म वो भी है, जो ख़ालिदा अदीब ख़ानम के अलीगढ़ आने पर मजाज़ ने कही थी। और अपनी चेतना और भावना को इस तरह से पेश किया था,
‘रूह-ए-इशरत-गाह-ए-साहिल जान-ए-तूफ़ान-ए-अज़ीम’
ये आवाज़ इक़बाल और जोश की शायरी की प्रतिध्वनि नहीं थी। क्योंकि दोनों औरत की आज़ादी के ख़िलाफ़ थे। इसका शे’री माधुर्य भी इक़बाल और जोश के अंदाज़ से अलग है।
(उर्दू से हिंदी अनुवाद: ज़ाहिद ख़ान और इशरत ग्वालियरी)