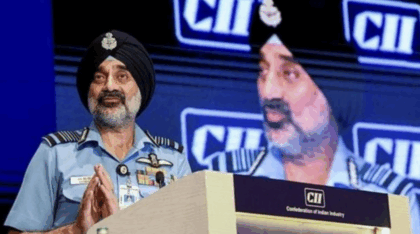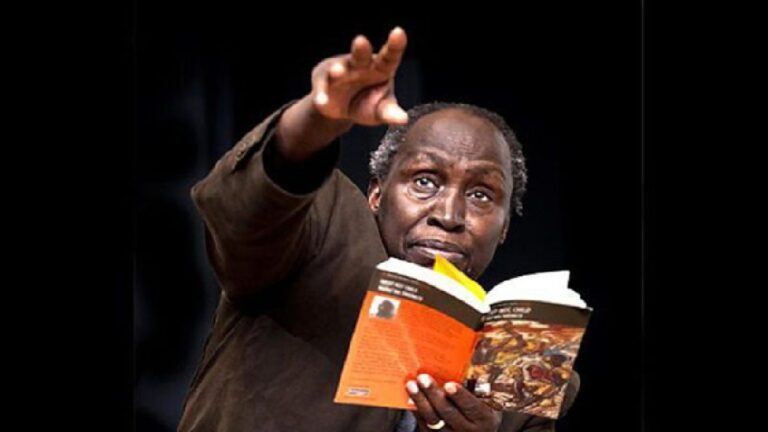23 जुलाई, 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब संसद में अपना बजट भाषण पेश कर रही थीं, तब अप्रत्याशित तौर पर उन्होंने ‘रोजगार’ शब्द का सात बार प्रयोग किया। बजट से पूर्व जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए प्रतिवर्ष 78.5 लाख नौकरी अगले पांच साल तक देने का प्रस्ताव रख चुका था। मोदी 1.0 विकास, 15 लाख रुपये और सबके लिए रोजगार का वादा करते हुए शुरू हुआ था। मोदी 2.0 रोजगार को प्रतिवर्ष एक करोड़ देने के वायदे के साथ आया। मोदी 3.0 इसमें से किसी भी वायदे को दुहराने की बजाय, इसे न्यूनतम स्तर पर हल करने के वायदे के साथ सामने आया है। यह बजट भाषण भारत में भीषण बेरोजगारी का स्वीकरण है, जिसका निदान इस बजट में फिलहाल नहीं दिख रहा है। इस संदर्भ में जो वायदे किये गये हैं, उसमें कुछ ऐसी विसंगितयां हैं जिसका सीधा फायदा युवा मेहनतकशों के हिस्से में आने की बजाय बड़ी कंपनियों के हिस्से में जाएगा।
सरकार रोजगार देने के प्रावधानों में मेहनतकशों को लेकर चिंतित होने की बजाय ज्यादा चिंता मालिकों की करती दिख रही है। इस संदर्भ में एक योजना ऐसी है जिसमें युवा रोजगार के खाते में सीधे 15 हजार रुपये की मदद तीन किस्तों में जाएगी। यह उन नौकरियों में दी जाएगी जिस नौकरी में साल की एक लाख से कम भुगतान किया जा रहा हो। नौकरी करने वाले युवा को जो पहली बार इपीएफओ में नामांकित हो रहे हैं, उन्हें उसका फायदा होगा। अनुमान के आधार पर ऐसे युवाओं की संख्या 2 करोड़ 10 लाख मानी गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाले युवाओं को भी प्रोत्साहन राशि देने का वादा किया गया है। यह कितना होगा, स्पष्ट नहीं है। लेकिन, एक दूसरी योजना के बारे में भी बात किया गया जिसमें कार्यरत कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड में मालिकों की हिस्सेदारी में से प्रति महीने 3000 हजार रुपये 2 साल तक सरकार वापस करेगी। ऐसी ही एक और योजना की घोषणा इस बजट भाषण में की गई।
सरकार ने दावा किया है कि पांच साल में 1 करोड़ युवाओं को कौशलयुक्त बनाया जाएगा। इसमें से 25 हजार छात्रों को ऋण और छात्रवृत्ति उपलब्ध कराया जाएगा। इसी योजना में देश की टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षु के तौर पर भर्ती किया जाएगा। प्रशिक्षुओं की यह संख्या प्रतिवर्ष 20 लाख बनती है। यहां सरकार ने इन प्रशिक्षुओं को 5000 हजार प्रति महीने ‘अलाउंस’ देने की घोषण की है। प्रशिक्षण पर रखने वाली कंपनियां प्रशिक्षुओं पर अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांस्बिलिटी का 10 प्रतिशत हिस्सा खर्च करेगी और उनके प्रशिक्षण का खर्च वहन करेगी। भर्ती के दौरान सरकार 6000 हजार रुपये देगी।
भारतीय श्रम कानूनों में, जिसमें फैक्टरी प्रबंधन और नियोजन भी हिस्सा है, रोजगार की विविध श्रेणियों को वर्गीकृत किये हुए है। इस संदर्भ में, कर्मचारियों को देय भुगतान की श्रेणियां भी तय हैं। प्रशिक्षुओं के संदर्भ में बाकायदा एक कानूनी संरचना है जिसमें ‘अलाउंस’ जैसे शब्द का न तो प्रयोग है और न ही मालिकों की ओर से सीएसआर में से भुगतान करने का प्रावधान है। ‘द अपै्रंटिस एक्ट, 1961’ जो अस्त्तिव में आने के बाद से 1973, 1986, 1997, 2007 और 2014 में संशोधित किया गया है, में साफ तौर पर प्रशिक्षण के दौरान मालिक को ‘स्टाईपेंड’ देने का प्रावधान है। यह एक तरह का वजीफा, अनुदान है जो उसके आवश्यक जीविका के लिए तय मानदंडों से कम नहीं होना चाहिए। यह अधिनियम तय करता है कि प्रशिक्षु का भुगतान उसके उत्पादन और मुनाफे के आधार पर नहीं होगा।
इस अधिनियम पर फैक्टरी एक्ट 1948 के कुछ पक्ष प्रशिक्षु के स्वास्थ्य, जीवन और काम की अवस्थितियां लागू हैं। साथ ही प्रशिक्षु के घायल होने पर मालिक को जिम्मेवारी लेनी होगी और भुगतान करना होगा। प्रशिक्षण के संदर्भ में यह एक्ट मालिकों को यह भी सुनिश्चत करने के लिए प्रावधान रखे हुए है जिससे कुल कार्यशक्ति के एक हिस्से के तौर पर प्रतिवर्ष प्रशिक्षु रखने और प्रशिक्षण पूरा होने पर सरकार को इसकी जानकारी देना जरूरी माना गया है। यह प्रावधान सिर्फ टॉप 500 कंपनियों के लिए नहीं, अपितु सभी फैक्टरी एक्ट के तहत आने वाली कंपनियों के लिए है।
सरकार ने किस आधार पर टॉप 500 कंपनियों का चुनाव किया है, यह स्पष्ट नहीं है। यहां यह बताना जरूरी है भारत की टॉप 500 कंपनियों ने अपने विकास दर में अमेरिकी कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया है। यह सिर्फ श्रम अवदानों के बल पर संभव नहीं है। इसमें निश्चित ही अधिग्रहण और शेयर बाजार से हासिल पूंजीकरण एक बड़ी भूमिका निभा रही है। इस कथित विकास को लेकर पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी से लेकर कई विशेषज्ञों ने गंभीर सवाल खड़ा किया है।
बजट 2024 को पेश करते हुए कई सारी घोषणाएं भाषणों के माध्यम से हो रही थीं। निश्चित ही इसे प्रिंट माध्यम से आने के बाद ही विस्तार से समझा जा सकेगा। लेकिन, प्रावधान के संदर्भ में घोषणाएं उपयुक्त शब्दावलियों की मांग करती हैं। मोदी सरकार के पिछले दो कार्यकाल इस संदर्भ में कई तरह की समस्याएं पैदा करती रही हैं। एक बड़ी समस्या आंकड़ों को लेकर है। मोदी सरकार के दौरान या तो आंकड़े आ नहीं रहे हैं, और यदि आ रहे हैं तब उन्हें संदर्भित करना और समझना भी एक दुरूह काम हो गया है। लंबे समय बाद, इस जुलाई के शुरूआत में ‘सांख्यिकी और योजना कार्यान्वयन मत्रालय’ की ओर से 2021-22 और 2022-23 का वार्षिक सर्वेक्षण जारी किया गया, तब यह साफ हो गया था कि मोदी 3.0 सरकार बरोजगारी और छोटे उद्यम की बर्बादी को एक सीमा तक स्वीकार करने के लिए तैयार हो चुकी है।
इस सर्वेक्षण में यह स्वीकरण दिखता है कि नोटबंदी और कोविड-19 की महामारी के दौरान किया गए लॉकडाउन ने लाखों उद्यमों को बर्बाद कर दिया और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी को पैदा किया। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण का वर्तमान रिपोर्ट सामने आता है जिसमें प्रतिवर्ष 78.5 लाख रोजगार पांच साल के सृजन की जरूरत को रखा गया है। इन दोनों के बीच अचानक ही रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में लगभग 4 करोड़ लोगों के रोजगार का आंकड़ा सामने रखा है। जबकि बेरोजगारी का संकट नौकरियों के लिए आवेदन करने वालों की संख्या, गांव में मनरेगा के तहत काम मांगने वालों और गांव से शहर की ओर जा रहे मजदूरों की संख्या से अनुमान लगाना इतना कठिन नहीं रह गया है।
रोजगार का संकट सिर्फ यह नहीं है कि भारत की कुल श्रम अवदानों में कितने लोग इससे वंचित रह जा रहे हैं। यह एक ऐसा भ्रामक आंकड़ा है जिसमें नियमित, अनियमित काम का बंटवारा ही खत्म हो जाता है। साल में महज 100 दिन के काम का वादा भी जब सरकार पूरा न करा पा रही हो, उसे सिर्फ काम के चंद घंटों के आधार पर श्रम अवदान मान लेने और भुगतान पूरा जाने का अनुमान कर लेने से भारत की बरोजगारी की समस्या हल नहीं होने वाली है।
मोदी सरकार ने नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना महामारी के दौरान भीषण लॉकडाउन ने सिर्फ उत्पादन की व्यवस्था को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, इसने युवाओं के शिक्षण-प्रशिक्षण से वंचित किया। इसने कार्यशैली में बदलाव का पैदा किया और उत्पादन संरचना को काफी हद तक बदल दिया। इस दौरान विभिन्न राज्य सरकारों ने श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ा दीं। वहीं तेजी से बढ़ रहे डिजिटल आधार पर उभरी कार्यसंचरनाओं में काम करने वाले मजदूरों को उनके मालिकों के हवाले कर दिया गया।
श्रम अवदानों के नाम पकौड़ा छानने का तर्क जब मोदी ने दिया था, तब यह साफ होने लगा था कि ‘श्रमिक’ होने की शब्दावली ही खत्म की जा रही है। लेकिन जब तक पूंजी है और उसमें मुनाफे की चाह है ‘श्रमिक’ शब्द बना रहेगा। एक लंबे समय बाद बजट में रोजगार और प्रशिक्षण की शब्दावली का आना अर्थव्यवस्था की उस ठोस जमीन पर आना ही है जहां से ‘विकसित’ होने की उड़ान भरी गई थी।
इस बजट में खेती से जुड़े श्रमिकों के बारें में कुछ खास बात नहीं है। किसानों के लिए पिछले बजटों की तरह आय दुगुनी करने का वादा फिलहाल दिखाई नहीं दिया। सब्सिडी के मद में खर्च अपने न्यूनतम स्तर पर दिखाई दे रहा है। आज भी खेती पर निर्भर श्रमिकों की संख्या में जो नोटबंदी और कोरोना लॉकडाउन से बढ़ गया था, उल्लेखनीय तौर पर कम नहीं हुआ है। बजट युवाओं की शिक्षा के ऋण की व्यवस्था करने की बात कर रही है। लेकिन, इस क्षेत्र में कोई गुणात्मक फर्क नहीं दिख रहा है। आईटीआई, पॉलिटेक्टिनिक, बीफार्मा जैसी तकनीकी पढ़ाई के संस्थानों में निजी क्षेत्र की घुसपैठ और वहां नाम मात्र की पढ़ाई और प्रशिक्षण ने श्रम की स्थितियों को और भी बदतर बनाया है।
दूसरी और उच्च शिक्षा में स्थिति न सिर्फ पहले से खराब हुई है, इसका स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है। उत्पादन की व्यवस्था में एक ओर क्रोनी कैपिटलिज्म सर चढ़कर बोल रहा है, वहीं श्रमिक समुदाय को निरंतर अशिक्षा की ओर ठेला जा रहा है। यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की भयावह त्रासदी है। इस बजट में इस त्रासदी से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ‘विकसित भारत’ का यदि यही रोडमैप है तब कहा जा सकता है ऐसा भविष्य फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है।
(अंजनी कुमार लेखक एवं स्वतंत्र पत्रकार हैं)