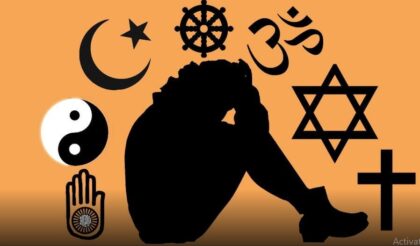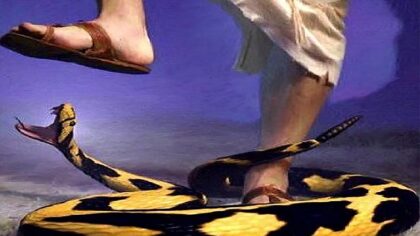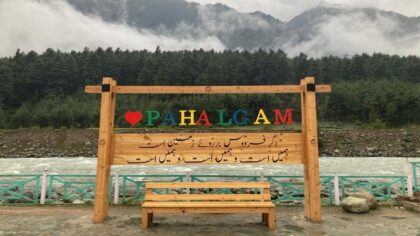अगर किसी मुल्क की रूह पर सबसे गहरा ज़ख्म है, तो वो है- इंसानों की जबरन बनाई गई हैसियतें। वो बंटवारा जो ख़ून से नहीं, ख़ानदान से तय हो, वो पहचान जो हुनर से नहीं, बल्कि हज़ारों साल पुराने जन्म के दाग़ से बनती हो- और यही है भारत की जाति व्यवस्था। यह कोई महज़ सामाजिक ढांचा नहीं, बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर किया गया वह षड्यंत्र है, जिसने लाखों ज़िंदगियों को पैरों के नीचे कुचलकर, चंद जातियों को आसमान की चौखट पर बिठा दिया।
अगर इसे हम बीमारी कहें- तो यह कोई मामूली ज़ुकाम नहीं, बल्कि एक ऐसी पुरानी, दिमाग़ी, रूहानी और तवारीखी बीमारी है जो सदियों से पीढ़ियों को खा रही है। और हर बीमारी का इलाज तभी मुमकिन होता है, जब पहले उसकी सही और साफ़ तश्ख़ीस (Diagnosis) की जाए। जातिगत जनगणना उसी तश्ख़ीस की पहली और बुनियादी कड़ी है। बिना इसका सहारा लिए, सामाजिक न्याय के हर वादे की बुनियाद खोखली रह जाएगी।
जातिगत जनगणना, दरअसल उस आईने की तरह है जिसमें भारत को पहली बार अपनी असली तस्वीर देखनी होगी- वह तस्वीर जो काले-सफ़ेद आंकड़ों में दर्ज़ होगी, पर जिसमें रंग, धर्म और सत्ता की असमानता की पूरी कहानी लिखी होगी। यह कोई साधारण गणना नहीं, बल्कि उस ‘ग़ैर-बराबरी’ की गवाही है जिसे सदियों तक छुपाया गया, मिटाया गया, और फिर भी जो हर नुक्कड़, हर गली, हर चौपाल और हर परीक्षा केंद्र में आज भी ज़िंदा है।
जो लोग कहते हैं कि जातिगत जनगणना से समाज में बँटवारा बढ़ेगा, वे शायद यह भूल रहे हैं कि समाज पहले ही टूटा हुआ है- और यह टूट फूट आंकड़ों से नहीं, व्यवस्था से पैदा हुई है। यह जनगणना बंटवारे की वजह नहीं, बल्कि बंटे हुए समाज की पहचान है। यह उस असलियत की दस्तक है जिसे सुनकर सत्ता की नींद उचटती है, और इसलिए वह इसे टालना चाहती है।
दरअसल, जातिगत जनगणना उस स्याही की तरह है, जिससे इतिहास का वह पन्ना लिखा जाएगा जो अब तक फाड़कर छुपा दिया गया था। यह स्याही आंकड़ों से भरी होगी, पर उसकी रोशनाई में पीढ़ियों की चीख़ें, दुआएं, और उम्मीदें होंगी।
यह गिनती दरअसल गिनती नहीं, एक सदी की पुकार है। यह सवाल है- कि जब संविधान ने सबको बराबरी दी, तो फिर आंकड़ों में इतनी गैर-बराबरी क्यों है? यह गिनती बताती है कि कौन अब भी हाशिए पर है, और किसे अब भी हिस्सेदारी की बजाय ‘ख़ैरात’ मिल रही है।
सियासत अक्सर जाति को केवल वोट बैंक की नज़र से देखती है, लेकिन यह जनगणना उस नज़रिए को चुनौती देती है। यह कहती है कि अब जातियों को केवल गिना नहीं जाएगा, बल्कि सुना जाएगा। उन्हें उनके हिस्से का इंसाफ़ मिलेगा, न कि वादों का कर्ज़।
जातिगत जनगणना एक ऐसा दस्तावेज़ है जो आज़ादी के 75 साल बाद यह पूछता है- कि किसके हिस्से में सच में आज़ादी आई? किसके नाम की आज़ादी, केवल किताबों में रह गई?
यह जनगणना उस लोकतंत्र की कसौटी है, जो केवल मतों से नहीं, बल्कि मौक़ों से साबित होता है। और जब तक यह आंकड़े सामने नहीं आते, तब तक हर योजना, हर आरक्षण, हर विकास नीति अधूरी और अंदाज़ों पर आधारित रहेगी। कल्पना की गई नीतियां, सच्चाई से दूर रहकर, उन्हीं को लाभ देती रहेंगी जिनके पास पहले से शक्ति है।
जातिगत जनगणना के विरोध का अर्थ है- डर, डर उस सच्चाई से जो हाशिए पर पड़े तबक़ों के संघर्ष को वैधता देगी। डर उस आंकड़े से जो बताएगा कि सत्ता और संसाधन किन जातियों के हाथ में केंद्रित हैं। डर उस सवाल से जो पूछेगा- कि क्या वास्तव में हम लोकतंत्र की बराबरी के रास्ते पर चल रहे हैं?
यह विरोध, सत्ता के उस डर का नाम है जो हिसाब देने से कतराती है। लेकिन वह दिन दूर नहीं जब हर दर से आवाज़ उठेगी-“हमें गिनो, हमें जानो, और हमें मानो।”
इसलिए जातिगत जनगणना कोई सांख्यिकीय अभियान नहीं, यह सामाजिक ईमानदारी का पहला इम्तिहान है। यह गिनती नहीं, गवाही है। यह आंकड़ा नहीं, अदालती दस्तावेज़ है। यह मांग नहीं, हक़ है।
और सबसे बढ़कर-यह वह उम्मीद है, जो कहती है:
अगर बीमारी को पहचान लिया गया है,
तो अब इलाज को टालना सिर्फ़ नाइंसाफ़ी नहीं, बल्कि ज़ुल्म है। क्या अब भी इस देश को वह आईना दिखाने से डर लग रहा है, जिसमें उसे अपनी सच्ची सूरत देखनी है?
(जौवाद हसन स्वतंत्र पत्रकार हैं।)