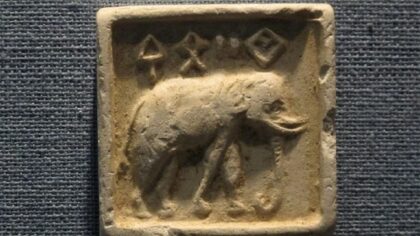जिस समय नगालैंड में आम नागरिकों की सेना की गोलीबारी में हत्या के बाद जनाक्रोश चरम पर है, मोदी सरकार ने राज्य में अफस्पा को छह महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इसके बाद कांग्रेस ने गुरुवार को भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उसकी ‘सत्ता की लालसा’ ने पूर्वोत्तर को उग्रवाद और अराजकता के रसातल में भेज दिया है।
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ‘मोदी सरकार ने अब तक शांतिपूर्ण पूर्वोत्तर को अराजकता, उग्रवाद की खाई में धकेल दिया है।’
गुरुवार को केंद्र ने पूरे राज्य को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित करते हुए नगालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा) को अगले साल 30 जून तक बढ़ा दिया।
नगालैंड के मोन जिले में 4 दिसंबर को सेना के 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस द्वारा गांववासियों के एक समूह को ‘गलती से उग्रवादी’ समझने और गोलीबारी करने के बाद 14 नागरिकों की मौत हो गई। भारतीय सेना ने इसे ‘गलत पहचान का मामला’ कहा। हालांकि, स्थानीय निवासियों ने दावे को दृढ़ता से खारिज कर दिया है। इलाके में सैनिकों के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प में सेना के एक जवान और सात और लोगों की मौत हो गई। बाद में, सेना के एक शिविर पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद बलों द्वारा एक और नागरिक की मौत हो गई। पीड़ित परिवारों द्वारा अपने करीबी लोगों को सामूहिक कब्र में दफनाने के दिल दहला देने वाले दृश्य सामने आए। एक भावनात्मक समारोह में पुरुष और महिलाएं दिल खोलकर रोते दिखे जबकि अन्य रिश्तेदारों ने उन्हें दिलासा दिया। राज्य में गोलीबारी के बाद तनाव की स्थिति बनी रही और अधिकारियों ने इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया और किसी भी कानून-व्यवस्था की स्थिति को रोकने के लिए कर्फ्यू लगा दिया।
फायरिंग को पूर्वोत्तर राज्य में हाल के दिनों में सबसे घातक घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। इसने एक बार फिर विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा) पर बहस को तेज कर दिया है। आम लोगों के साथ-साथ कुछ राजनेताओं ने इसे रद्द करने की मांग की है। नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से अफस्पा को हटाने का अनुरोध किया है क्योंकि यह ‘भारत की छवि पर एक काला धब्बा’ है।
6 दिसंबर, 2021 को मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा कि वह ओटिंग गांव में हुई हत्याओं से बहुत दुखी हैं और उन्होंने केंद्र सरकार से अफस्पा को हटाने की मांग की है। एआईएमआईएम अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस नेता प्रद्युत बोरदोलोई ने भी विवादास्पद कानून पर सवाल उठाए हैं। रायजर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई ने भी हत्याओं की निंदा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच करनी चाहिए और इसे ‘आतंकवादी कृत्य’ घोषित करना चाहिए।
सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा), 1958 भारतीय संसद का एक अधिनियम है जो भारतीय सेना को “अशांत क्षेत्रों” में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है। अशांत क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1976 के अनुसार एक बार ‘अशांत’ घोषित होने के बाद क्षेत्र को कम से कम तीन महीने तक यथास्थिति बनाए रखनी होती है। ऐसा ही एक अधिनियम 11 सितंबर, 1958 को पारित किया गया था, जो उस समय असम के हिस्से नागा हिल्स पर लागू था। बाद में यह भारत के उत्तर पूर्व में अन्य सात राज्यों में लागू हो गया। वर्तमान में, यह असम, मणिपुर, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग, चांगलांग और तिरप जिलों में लागू है। इस तरह का एक और अधिनियम 1983 में पारित हुआ और पंजाब और चंडीगढ़ में लागू हुआ। इसे अस्तित्व में आने के लगभग 14 साल बाद 1997 में वापस ले लिया गया। 1990 में पारित एक अधिनियम जम्मू और कश्मीर पर लागू किया गया और यह तब से लागू है।
1952 में नागा नेशनल काउंसिल (एनएनसी) ने बताया कि उसने एक “स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत संग्रह” किया, जिसमें लगभग 99 प्रतिशत नगाओं ने ‘स्वतंत्र संप्रभु नागा राष्ट्र’ के लिए मतदान किया। 1952 के पहले आम चुनाव का बहिष्कार किया गया था जो बाद में सरकारी स्कूलों और अधिकारियों के बहिष्कार तक बढ़ा दिया गया था। 1953 में असम सरकार ने नगा हिल्स में असम मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर (स्वायत्त जिला) अधिनियम लागू किया और स्थिति से निपटने के लिए विद्रोहियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई बढ़ा दी। जब स्थिति बिगड़ गई, असम ने नगा हिल्स में असम राइफल्स को तैनात किया और असम अशांत क्षेत्र अधिनियम 1955 को अधिनियमित किया, जिससे अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र राज्य पुलिस को उग्रवाद से निपटने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया गया। लेकिन दोनों समूह नगा विद्रोह को नियंत्रित नहीं कर सके और विद्रोही नगा राष्ट्रवादी परिषद (एनएनसी) ने 1956 में एक समानांतर सरकार “नगालैंड की संघीय सरकार” का गठन किया। सशस्त्र बल (असम और मणिपुर) विशेष शक्ति अध्यादेश 1958 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद द्वारा 22 मई, 1958 को प्रख्यापित किया गया था। बाद में इसे 11 सितंबर, 1958 को सशस्त्र बल (असम और मणिपुर) विशेष अधिकार अधिनियम, 1958 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
अफस्पा के क्षेत्रीय दायरे का विस्तार सात पूर्वोत्तर राज्यों – असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा तक भी हुआ। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि अफस्पा का इस्तेमाल एक दमनकारी कानून के रूप में ज्यादा हुआ है। इस कानून के तहत सशस्त्र बलों को बेलगाम शक्तियां दे दी ग। इसीलिए बेजा इस्तेमाल तो बढ़ना ही था। इस विशेष कानून को बनाने के पीछे मूल भावना तो यह थी कि अशांत क्षेत्रों में उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए इसका सहारा लिया जाएगा। इसीलिए सशस्त्र बलों को खुल कर सारे अधिकार दिए गए। अफस्पा के तहत सशस्त्र बलों को बिना अनुमति किसी भी घर की तलाशी लेने, किसी को गिरफ्तार कर लेने और यहां तक कि कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर गोली चला देने जैसे अधिकार हासिल हैं। अगर सशस्त्र बलों की कार्रवाई के विरोध में लोग हिंसा करते हैं और उस सूरत में सशस्त्र बलों की गोली से लोग मारे जाते हैं तब भी गोली चलाने वाले बलों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की इजाजत यह कानून नहीं देता। इसीलिए अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं जब निर्दोष नागरिक सशस्त्र बलों की ज्यादती का शिकार होते रहे हैं। याद किया जाना चाहिए कि मणिपुर में वर्ष 2000 में असम राइफल्स के जवानों ने दस निर्दोष लोगों को मार डाला था। उसके बाद मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने इस कानून को खत्म करने की मांग को लेकर सोलह साल तक अनशन किया।
अफस्पा मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है 1991 में जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति को अपनी दूसरी आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत की, यूएनएचआरसी के सदस्यों ने इस अधिनियम की वैधता के बारे में विभिन्न प्रश्न पूछे। उन्होंने देश के कानून के तहत अधिनियम की संवैधानिकता पर सवाल उठाया और पूछा कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय घोषणापत्र के अनुच्छेद 4 के आलोक में इसे कैसे उचित ठहराया जा सकता है। 23 मार्च 2009 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त नवनेथेम पिल्ले ने भारत से अफस्पा को निरस्त करने के लिए कहा। उन्होंने कानून को “दिनांकित और औपनिवेशिक युग का कानून कहा जो समकालीन अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का उल्लंघन करता है।”
31 मार्च, 2012 को संयुक्त राष्ट्र ने भारत से इस अधिनियम को रद्द करने के लिए कहा, यह कहते हुए कि लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने “राज्य के दुरुपयोग, उत्पीड़न और भेदभाव के उपकरण” के रूप में इस अधिनियम की आलोचना की है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अफस्पा की आड़ में सैनिकों द्वारा की गई किसी भी मुठभेड़ की उचित जांच होनी चाहिए। “इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीड़ित एक आम व्यक्ति था या आतंकवादी, न ही इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमलावर एक सामान्य व्यक्ति था या विशेष। कानून दोनों के लिए समान है और दोनों पर समान रूप से लागू होता है,” सर्वोच्च न्यायालय ने कहा।
(दिनकर कुमार द सेंटिनेल के पूर्व संपादक हैं और आजकल गुवाहाटी में रहते हैं।)