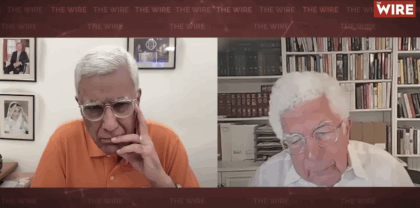विचारधारा का सवाल सभ्यता पर विचार करने वाले के मन में कभी-न-कभी जरूर उठता है। यह मानने में कठिनाई हो सकती है कि विचारधारा का अपना अस्तित्व होता है और उसे व्यक्ति की निरपेक्षता में रहकर समझा जा सकता है। यह एक बुनियादी बात है। इस में थोड़ी स्पष्टता की जरूरत है। विचार व्यक्ति के दिमाग में उत्पन्न होता है। यह उसके अपने दिमाग तक ही सीमित रह जाये तो वह सिर्फ ज्ञान, सही अर्थ में थोथा ज्ञान होता है। थोथा कहना कोई अपमानजनक या उपहासजनक नहीं है। कहने का आशय इतना ही है कि सीमित अर्थ में थोथा थोड़ी-बहुत प्राकृतिक भिन्नता के साथ अपने ही जैसे के पुनरुत्पादन की प्रक्रिया में भाग लेने के अयोग्य होता है, भाग नहीं लेता है। वैसे लोक का प्रचलित अनुभव है, ‘थोथा चना, बाजे घना’!
भाव और विचार एक साथ उत्पन्न होते हैं। तार्किकता भाव की अनिवार्य शर्त नहीं होती है। तार्किकता विचार की अनिवार्य शर्त होती है। कई बार भाव भी विचार का बाना धरकर पेश होता है और विचार भी भाव की तरह पेश होता है। मनुष्य के मन की यह स्वाभाविक प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। विचार को भाव से अलग करना या कह लें, तर्क को अतर्क से अलग करना होता है। शुद्ध विचार या शुद्धता के विचार से बाहर व्यावहारिक ढंग से सोचने पर भी मुश्किल तब होती है जब कोई अपने विचार को उसी विचार की ऐतिहासिक या व्यावहारिक क्रमिकता से जोड़ना चाहता है। ऐसे प्रयास को उस विचार पर वर्चस्व जमाये ‘पंडितों’ का विरोध झेलना पड़ता है। यह तो तुलसीदास को भी मानना पड़ गया कि गाल बजानेवालों को ही ‘पंडित’ माना जाता है।
तात्पर्य यह है कि विचार का प्रवाह तो लोकमन में जारी रहता है, विचार पर वर्चस्व कायम रखनेवाले ‘पंडितों’ के मन में नहीं। लोकमन में प्रवहमान विचार से ग्रहण करना और फिर उसे परिष्कृत कर लोकमन में डाल देना ज्ञान को विचारधारा में बदलना होता है, कह सकते हैं गंगाजल से गंगा की पूजा। यहां, ‘पंडितों’ के सुझाये अंध लोकवादी रुझान से बचने की पूरी कोशिश है। लोकमन से विचार प्रवाह से ग्रहण करना और उसे ज्यों-का-त्यों लोकमन में डाल देना अंध लोकवाद का शिकार होना है। जो गंगाजल से गंगा की पूजा करते हैं वे गंगा जल को उठाकर सीधे गंगा में नहीं डाल देते हैं, मन-ही-मन मंत्र जपते हैं फिर डालते हैं। यह मंत्र जाप ही उनकी परिष्कार प्रक्रिया है! अब है तो है, गंगा कितनी परिष्कृत है, दुनिया जानती है।
लोकमन में विचार की बुद्धिमत्ता के साथ भावुक सांद्रता भी मिली होती है। लोकमन की भावुक सांद्रता से विचार की बुद्धिमत्ता को अलग करके फिर से लोकमन में उसे डाल देना ही ज्ञान को विचारधारा में बदलना हो सकता है। किसी भी विचारधारा के रास्ते का सब से बड़ी बाधा खड़ी करती है, ‘दलीय निष्ठा’। ‘दलीय निष्ठा’ केवल राजनीति में ही नहीं गुल खिलाती है, वैचारिकी के परिसर में भी एक-से-एक गुल खिलाती रहती है।
यह वैचारिकी की ‘दलीय निष्ठा’ ही है कि विचारधारा की बात उठते ही उसे, कम-से-कम हिंदी में मार्क्सवाद या वाम विचार के पक्ष या विपक्ष से जोड़ कर शुरू किया जाता है। यहां इस प्रवृत्ति से बचने की यथा-संभव कोशिश की जायेगी। यह नहीं है कि इस बचने में मार्क्सवाद या वाम विचार के पक्ष या विपक्ष से परहेज है। बल्कि वह जरूरी है, उस पर फिर कभी अलग से इसे समझने की कोशिश की जा सकती है। यहां इतना ही कि लोकमन से ‘जीवंत लेन-देन’ में कोताही ने अंततः इसे जोरदार बनने से रोक दिया।
भारत, और जब भारत कहता हूं तो उसे स्पष्ट कारणों से मोटे तौर पर वृहत्तर हिंदी-समाज का ही अर्थ लिया जाना उचित है, हलांकि इस में शामिल पूरा भारत विचार है। असल में यह भी है कि जिन पीड़ाओं से परेशान हो कर यह लिखने की कोशिश कर रहा हूं उन पीड़ाओं से यह वृहत्तर हिंदी-समाज ही सब से अधिक परेशान है। पूरे भारत पर पड़ रहे इसके प्रभाव से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।
आज-कल हिंदी-समाज इलाके में सनातन और सनातन धर्म की बहुत चर्चा है। तो बात यहां से शुरू की जा सकती है। संदर्भ महाभारत से लिया जा सकता है। महाभारत के शांतिपर्व में कहा गया है, “न यस्य कूटं कपटं न माया न च मत्सरः। विषये भूमि पालस्य तस्य धर्मः सनातनः।।” कूटनीति, कपट, माया तथा ईर्ष्या से सर्वथा मुक्त रहकर जीवनयापन ही सनातन धर्म का पालन होता है। धर्म का एक अर्थ गुण है।
यह उल्लेख करना जरूरी है कि मातृत्व एक सत्य है और पितृत्व एक विश्वास है। मातृ सत्तात्मक से पितृ सत्तात्मक में सत्ता का सत्ता का हस्तांतरण सामाजिक व्यवस्था की नाभिक केंद्रीयता में सत्य की जगह विश्वास को प्राथमिकता एवं प्रतिबद्धता हासिल होती गई। सामाजिक व्यवस्था की नाभिक केंद्रीयता से सत्य का विस्थापन और विश्वास संस्थापन पहली प्रति-क्रांति थी। इस प्रति-क्रांति ने सनातन को खंडित कर दिया। भले ही वंदना मातृभूमि की करें लेकिन आचरण में पितृभूमि का वर्चस्व बनाने का सारा कूट उद्यम होता रहा। विडंबना है कि जो जितनी जोर से मातृभूमि की जय बोलता है वह उस से अधिक तत्परता से पितृ सत्तात्मक व्यवस्था के वर्चस्व के लिए प्रतिबद्ध होता है।
मुंडक उपनिषद से हमने ‘सत्यमेव जयते’ का पाठ लिया और अपने लोकतंत्र के राज-चिह्न पर अंकित कर लिया। मुंडक उपनिषद में उल्लिखित है- “सत्यमेव जयते नानृतंसत्येन पन्था विततो देवयानः। येना क्रमंत्यृषयो ह्याप्तकामो यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्॥” सत्य की जय होती है, अनृत (मिथ्या) की नहीं। लेकिन पितृ सत्तात्मक की कूटनीतिक प्रक्रिया में सत्य तो स्वयं विश्वास से विस्थापित हो गया था! विश्वास कब ‘नृत’ है, कब ‘अनृत’, यानी कब सत्य सरीखा है कब झूठ सरीखा कहना बड़ा मुश्किल होता है।
महात्मा बुद्ध ने अपने विचारों को ‘आर्य सत्य’ कहा; चार आर्य सत्य तो विश्वविख्यात हैं। आर्य का एक अर्थ श्रेष्ठ भी होता है। महात्मा बुद्ध के वैचारिक संघर्ष का एक अंश लगभग अलक्षित रह गया, वह यह कि बुद्ध विचार मातृ सत्तात्मक व्यवस्था की प्राण-प्रतिष्ठा के लिए संघर्षशील था। पितृ सत्तात्मक आक्रमण से बचने-बचाने के लिए उन्होंने ‘स्त्री के स्थान’ के संदर्भ में रणनीतिक मुद्रा अख्तियार किया होगा।
इस रणनीतिक मुद्रा को पितृ सत्तात्मक विचार ने अपनी कूटनीतिक शैली में उलटे बुद्ध विचार पर ही ‘स्त्री विरोधी’ होने के रूप में प्रचलित कर दिया। बहरहाल, यह अधिक सघन शोध का विषय है। कहने का आशय यह है कि मातृ सत्तात्मक के पितृ सत्तात्मक से या कहें सत्य के विश्वास से विस्थापन की ‘प्रति क्रांति’ ने “सनातन” को खंडित कर दिया। कूटनीति, कपट, माया तथा ईर्ष्या से सर्वथा मुक्त रहकर जीवनयापन ही सनातन धर्म का पालन होता है, जिन शक्तियों ने सनातन धर्म के पालन के पथ को कांटों से भर दिया, वे ही इसका गुणगान करते हुए अपनी कारगुजारियों को अंजाम देते रहे।
कम-से-कम भारत में विचारधारा की किसी भी बात को बौद्ध दर्शन या बुद्ध विचार से शुरू न करना मुझे तो वैचारिक अपराध-सरीखा ही लगता है। यह मानकर चलना चाहिए कि बुद्ध विचार का संबंध भारत की सामाजिक राजनीति से भी है, इतिहास और धर्म से भी है। भारत के इतिहास में ब्राह्मणवाद और बुद्ध विचार के संघर्ष पर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने तात्विक रूप से तो विचार किया ही है।
हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण आलोचक आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी बुद्ध विचार के लोक में घुल-मिलकर ‘विलुप्त’ हो जाने की बात कही है। इस घुलने-मिलने से हिंदी-समाज के लोकमन पर बहुत गहरा असर पड़ा। में विचार की दो संबद्ध धाराएं स्पष्ट दिखती हैं, पीड़ाओं से परेशान लोगों की मुक्ति और आत्मीयता से अधिकार का आग्रह। दिक्कत यह हुई कि आत्मीयता से अधिकार की प्रक्रिया के अंतर्गत आत्मीयता को विषाक्त हितैषिता से बदलकर अधिकार को कृपा का अधीनस्थ बना दिया गया। विचार में आंतरिक कूटनीति व्यवहार में आंतरिक टूटनीति को क्रियान्वित करती है।
सनातन मूल्य को बुद्ध विचार और जैन उपदेश ने संरक्षित किया, ये परस्पर संबद्ध (Interlinked और Interlaced) मूल्य थे, सत्य अहिंसा अस्तेय और अपरिग्रह। इसकी विस्तृत व्याख्याएं फिर कभी, लेकिन यहां अस्तेय और अपरिग्रह के अर्थ संकेत आवश्यक है। अस्तेय का अर्थ लोक दृष्टि से बचाकर ‘बहुत कुछ’ पर कब्जा कर लेना और अपरिग्रह का मतलब है अपनी जरूरत से ‘बहुत अधिक’ पर ‘सार्वजनिक नीति’ के माध्यम से अपना कब्जा बना लेना, कब्जा बनाये रखना। महात्मा गांधी ने अपने राजनीति उपकरण के रूप में सत्य और अहिंसा पर अधिक जोर दिया और यह आज विचार में अधिक प्रचलित है, व्यवहार में हरे, हरे! सत्य अहिंसा अस्तेय और अपरिग्रह परस्पर संबद्ध (Interlinked और Interlaced) मूल्य हैं, ये साथ-साथ चलते हैं, किसी एक के भी कमजोर पड़ने या खंडित होने का असर सब पर पड़ता है।
संपत्ति (सीमित रूप में आर्थिक) व्यक्ति का गुण (Property) नहीं है, जैसे आग का गुण या धर्म है ताप। संपत्ति का अस्तित्व व्यक्ति के अस्तित्व से भिन्न होता है। सवाल उठता है, फिर संपत्ति किसका गुण है? सभ्यता में यह एक बहुत बड़ा और नाभिक सवाल है। इसी के जवाब की तलाश में विचारधारा का महत्व है। सत्ता और उदारता में संबंध को समझना भी जरूरी है। उदारता, रामकथा में वर्णित वह ‘मैनाक’ है जिस पर आरूढ़ होकर सत्ता अपने ‘भ्रमास्त्र’ का निशाना साधती है; प्रसंग तुलसीदास के रामचरितमानस से, ‘जलनिधि रघुपति दूत बिचारी। तैं मैनाक होहि श्रमहारी।।’
विल्फ्रेडो पेरेटो ने भले ही 1900 ई के आस-पास अपने ”80/20 के नियम” को स्पष्टता से सूत्रबद्ध किया हो, सभ्यता ने इसकी व्यावहारिकता को बहुत पहले ही अपना लिया थ। पेरेटो अनुकूलता (Pareto optimality) में सुविधा यह है कि सिद्धांत को लागू करने में उपयोगिता की कोई पारस्परिक तुलना की आवश्यकता नहीं होती है; इसलिए यह वरीयताओं की ताकत से जुड़ी समस्याओं से तत्काल बचा ले जाता है। इस से यथा-स्थिति बनी रहती है और यह पेरेटो अनुकूलता असंतोष को बदलाव की तरफ बढ़ने से रोक लेती है।
शोषण के सामाजिक चक्र को तोड़ने की आकांक्षा को लेकर चलनेवाली किसी भी विचारधारा की सामाजिक स्वीकृति को दुरूह बना देती है। इसमें सामाजिक स्वचलन की इतनी ताकत होती है कि ’कुछ नहीं करना’ भी कुछ करने का एक बेहतर तरीका हो जाता है। यह रोजगार का तरीका नहीं हो सकता है। किसी की भी उत्प्रेरणा से ‘सेल्फी’ खिंचवाना तो रोजगार नहीं हो सकता है न! सत्ता और उदारता के बीच के संबंध का रहस्य खुल रहा है, ‘मैनाक’ का इनकार प्रकट हो रहा है।
पेरेटो अनुकूलता (Pareto optimality) की स्थिति फेल करती जा रही है तो बदलाव की ठहर-सी विचारधारा की भी सुगबुगाहट बढ़ रही है। एक अर्थ में विचारधारा की समाप्ति के बाद विचारधारा की नई सुगबुगाहट का यह दौर विचारधारा के व्यक्ति, समूह, संगठन आदि की चकबंदी से मुक्ति का संगीत बुन रहा है। मुक्ति को विच्छिन्नता समझने की भूल करने से आयासपूर्वक बचना चाहिए।
‘रोजगार’ इक्कीसवीं सदी की जनाकांक्षा का बीज शब्द है। रोजगार का सवाल इतना बड़ा है कि इसने स्वतंत्रता की जन्मजात मानवीय आकांक्षा को भी पूरी तरह से आच्छादित कर लिया है, इस आच्छादन में अच्छा कुछ भी नहीं है। विराटता की उद्दंडता के विरुद्ध मनुष्य की लघुता की सहकारी और समवायी विनम्रता की स्वतंत्रता का उपकरण है लोकतंत्र। बड़े लोगों के बड़प्पन को सहयोगिता नहीं, प्रतियोगिता पसंद है। पीड़ाओं से परेशान ‘लघुओं’ की पारस्परिक सहयोगिता में अनेक के प्रति सह-अस्तित्व का स्वागतबोध होता है।
मुश्किल यह है कि प्रतियोगिता के लिए भी एक नहीं अनेक की जरूरत तो होती है, लेकिन ‘बड़ों’ की पारस्परिक प्रतियोगिता में ‘आत्मीयता से अधिकार’ की उद्दंडता में अनेक के प्रति सह-अस्तित्व का कोई स्वागतबोध नहीं होता है। यहां भाव होता है, “एकोअहं, द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति”! यहां, ‘एकोअहं’ की चमकदार और लकदक आकांक्षा की परपीड़कता (Sadistic) की मंत्रणाएं सक्रिय रहती है।
प्रसंगवश, क्या कर रहा है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI), कहने की जरूरत नहीं है। कहने का आशय यह है कि रोजगार की आकांक्षा का सम्मान आज की विचारधारा का मूल प्रस्थान बिंदु हो सकता है। निर्विचार के भ्रामक प्रस्ताव को विचारधारा ही निरस्त कर सकती है, इसलिए है विचारधारा की तलाश।
पिछले कुछ सालों से एक समांतर आभासी दुनिया हमेशा आस-पास मंडराती रही है। महसूस किया जा सकता है सभ्यता के एक अंश के विभिन्न जीवन-स्तर तेजी से सिमटकर सुगम होने का भ्रम अब टूटने लगा है। अब फिजिटल (Phygital =Physical+Digital) की मांग बढ़ती जा रही है। राजमार्गों के चौड़े होते जाने से पगडंडियों के अधिकाधिक संकीर्ण होते जाने का रहस्य अब खुल रहा है। जनसाधारण के बीच भ्रम-मुक्त संवाद की जरूरतें बढ़ रही है।
भाषा समेत संवाद के संसाधनों के मूल चरित्र में अर्थ के बहकावों और भटकावों का पूर्ण विन्यास अब टूट रहा है। इस सब के नेपथ्य में विचारधारा की नई सुगबुगाहटों को महसूस किया जा सकता है। रोजगार सरीखे मुद्दों पर कॉरपोरेट और लोकतंत्र का भीड़ंत निर्णायक दौर में है। ‘लोकतंत्र’ और ‘लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय’ सरीखे सवाल के मृगछल में बदल दिये जाने का दौर अपने ’मकाम’ और मकतल के करीब पर पहुंच रहा है। कहना न होगा कि ‘लोकतंत्र’ और ‘न्याय’ सभ्यता में संतुलन कायम रखनेवाले कारक हैं।
भारत में 2024 का आम चुनाव इस दृष्टि से अतिमहत्वपूर्ण है। वैसे साल 2024 में भारत में ही नहीं कई देशों में, लगभग 70 देशों में, आम चुनाव होना है। सामग्रिक रूप से देखा जाये तो इन देशों के मतदाताओं के निर्णय से विश्व का भविष्य नई करवट लेता हुआ दिख रहा है। भारत आबादी और मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सब से बड़ा देश है। भारत के मतदाताओं का निर्णय निश्चित रूप से वैश्विक राजनीति को भी बहुत ही प्रभावित करेगा, इसलिए पूरी दुनिया के सकारात्मक लोग आशा भरी निगाह से भारत के चुनाव और उस से निकलने वाले नतीजों को इंतजार में व्याकुल नजर से देख रहे होंगे। ‘दलीय निष्ठा’ से बाहर भारत के मतदाताओं का निर्णय क्या होगा इस पर निगाह है दुनिया की, सभ्यता में संतुलन को बचाये रखने के लिए फिलहाल लक्ष्य लोकतंत्र को बचाना है।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा संपन्न हुई। लेकिन, सभ्यता की यात्रा जारी है, कि मंजिल अभी नहीं आई है। सामने 2024 का आम चुनाव है, सोच-समझकर फैसला कीजिए।
(प्रफुल्ल कोलख्यान स्वतंत्र लेखक और टिप्पणीकार हैं)