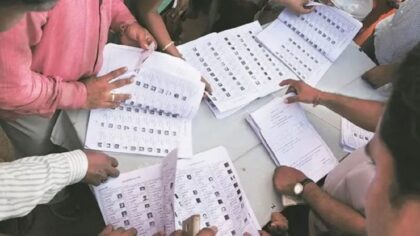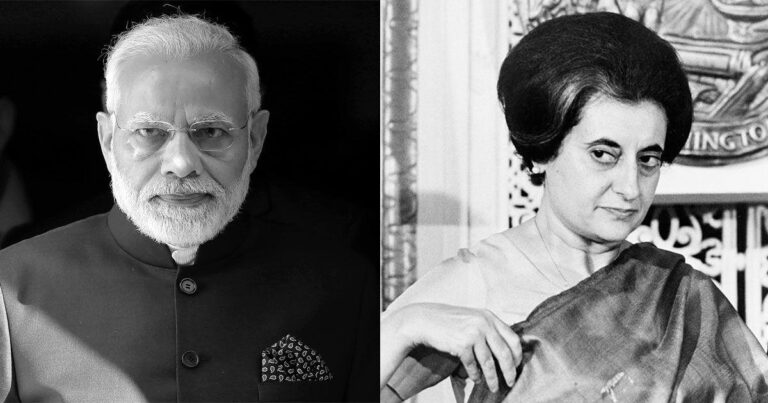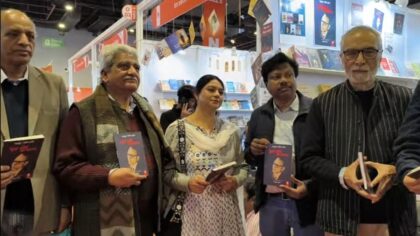इतिहास में अक्सर शासकों ने विरोध और असहमति को देशद्रोह के रूप में देखा है ताकि वे अपने शासन को बनाए रख सकें और किसी भी प्रकार की चुनौती को कुचल सकें। प्राचीन राजतंत्रों से लेकर आधुनिक तानाशाही व्यवस्थाओं तक, शासकों ने राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक विरोध को अपराध करार दिया और असहमत लोगों को “राज्य के शत्रु” घोषित किया। यह रणनीति न केवल विरोधियों को खत्म करने के लिए अपनाई गई, बल्कि जनता में भय पैदा करने और उनकी आज्ञाकारिता सुनिश्चित करने के लिए भी इस्तेमाल हुई।
देशद्रोह के रूप में विरोध का दमन एक ऐतिहासिक प्रवृत्ति रही है, जिसने शासन, मानवाधिकारों और क्रांतियों के विकास को प्रभावित किया है। यह लेख विभिन्न कालखंडों और क्षेत्रों के ऐतिहासिक उदाहरणों के माध्यम से दर्शाता है कि शासकों ने विरोध को कुचलने के लिए देशद्रोह के आरोपों का कैसे उपयोग किया।
ईश्वरीय शासन और निरंकुश सत्ता
प्राचीन रोम: राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों का दमन
प्राचीन रोम में राजनीतिक असहमति को अक्सर “देशद्रोह” (maiestas) माना जाता था। रोमन गणराज्य में सुधारवादी नेता टिबेरियस और गयुस ग्राकस (द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व) को गरीबों के लिए भूमि सुधार करने के प्रयास में मार दिया गया। शासक वर्ग ने उन्हें गणराज्य के लिए खतरा बताया और उनके समर्थकों को भी बेरहमी से कुचल दिया।
रोमन साम्राज्य के दौरान, सम्राट नीरो और टिबेरियस ने किसी भी विरोध को अपराध घोषित कर दिया और आलोचकों को देशद्रोही करार दिया। सम्राट नीरो के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में लुसियस पिसो का मामला यह दिखाता है कि शासक किस प्रकार राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को समाप्त करने के लिए देशद्रोह के आरोपों का उपयोग करते थे।
प्राचीन चीन: कानूनी कठोरता और विचारों पर नियंत्रण
प्राचीन चीन में शासकों ने असहमति को “स्वर्गीय आदेश” (Mandate of Heaven) के खिलाफ चुनौती के रूप में देखा। क़िन वंश (221–206 ईसा पूर्व) के सम्राट क़िन शी हुआंग ने अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए पुस्तकों को जलाने और विद्वानों को मारने का आदेश दिया। हान वंश (206 ईसा पूर्व–220 ईस्वी) ने बाद में कन्फ्यूशियस विचारधारा को अपनाया, लेकिन विरोध प्रदर्शनों को देशद्रोह मानकर उनका दमन जारी रखा।
मध्ययुगीन और पुनर्जागरण काल: धार्मिक और राजनीतिक दमन
धर्माधिकार (इंक्विज़िशन): ईशनिंदा को देशद्रोह मानना
कैथोलिक चर्च और यूरोपीय शासकों ने धार्मिक असहमति को दबाने के लिए देशद्रोह कानूनों का उपयोग किया। स्पेनिश इंक्विज़िशन (1478–1834) के दौरान प्रोटेस्टेंटों, यहूदियों और चर्च की नीतियों पर सवाल उठाने वालों को यातनाएं दी गईं। वैज्ञानिक जियोर्दानो ब्रूनो (1600 में जीवित जला दिया गया) और गैलीलियो गैलिली (1633 में चर्च के समक्ष अपने विचार वापस लेने के लिए मजबूर) जैसे विद्वानों को भी इसी दमन का शिकार बनाया गया।
अंग्रेजी राजशाही: सुधारकों के खिलाफ देशद्रोह कानून
अंग्रेजी शासकों ने राजनीतिक और धार्मिक विरोध को कुचलने के लिए देशद्रोह के आरोपों का सहारा लिया। राजा हेनरी अष्टम (1491–1547) ने सर थॉमस मोर को इसलिए मरवा दिया क्योंकि उन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड में राजा की सर्वोच्चता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसी तरह, महारानी एलिज़ाबेथ प्रथम (1533–1603) ने कैथोलिक विद्रोहों को दबाने के लिए देशद्रोह कानूनों का इस्तेमाल किया।
3. क्रांति का युग: विरोध को देशद्रोह बताकर स्वतंत्रता की लड़ाई का दमन
अमेरिकी क्रांति (1775–1783)
ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी क्रांतिकारियों को देशद्रोही करार दिया। जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन और जॉन एडम्स को ब्रिटिश सरकार ने “विद्रोही” कहा। अगर अमेरिकी क्रांति विफल हो जाती, तो इन नेताओं को देशद्रोह के लिए मृत्युदंड दिया जाता।
फ्रांसीसी क्रांति (1789–1799)
फ्रांस में राजा लुई सोलहवें और उनकी सरकार ने शुरुआती क्रांतिकारियों को देशद्रोही मानकर उन्हें मृत्युदंड दिया। जब जैकोबिन नेता रॉब्सपियर सत्ता में आए, तो उन्होंने भी अपने विरोधियों के खिलाफ वही नीति अपनाई और “आतंक का शासन” (Reign of Terror) के दौरान हजारों लोगों को गिलोटिन पर चढ़ा दिया।
हैती क्रांति (1791–1804)
जब हैती में दासों ने फ्रांसीसी शासन के खिलाफ विद्रोह किया, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने उनके नेता तुसैं लूवर्त्युर को देशद्रोही घोषित कर दिया और उन्हें कैद में डाल दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई।
19वीं और 20वीं शताब्दी: राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद और अधिनायकवाद
उपनिवेशी दमन और स्वतंत्रता संग्राम
19वीं और 20वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासकों ने स्वतंत्रता आंदोलनों को देशद्रोही करार दिया।
भारत में ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह (1931 में फांसी) और महात्मा गांधी (कई बार जेल में डाला) को राजद्रोही करार दिया।
दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को रंगभेद विरोधी संघर्ष के लिए 27 साल तक जेल में रखा गया।
अल्जीरिया में फ्रांस ने अल्जीरियाई स्वतंत्रता संग्राम को क्रूरता से दबाया।
अधिनायकवादी शासन की पूर्ण नियंत्रण वाली नीति
तानाशाह शासकों ने अपने विरोधियों को देशद्रोही बताकर सत्ता कायम रखी।
नाज़ी जर्मनी (1933–1945) में हिटलर ने राजनीतिक विरोधियों को मरवा दिया।
सोवियत संघ (1917–1991) में स्टालिन ने “महान शुद्धिकरण” (1936–1938) में लाखों लोगों को मारा।
माओ जेडोंग के चीन में सांस्कृतिक क्रांति (1966–1976) के दौरान असंतुष्टों को “विरोधी क्रांतिकारी” बताकर कुचला गया।
लोकतंत्रों और अधिनायकवादी राज्यों में विरोध का दमन
आज भी कई सरकारें विरोध को देशद्रोह मानकर दमन करती हैं:
अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को निगरानी में रखा गया।
अरब स्प्रिंग (2010–2012) में मिस्र, सीरिया और लीबिया की सरकारों ने विरोधियों को देशद्रोही करार देकर कुचल दिया।
रूस (2022) में यूक्रेन युद्ध का विरोध करने वालों को “राजद्रोही” कहकर गिरफ्तार किया गया।
अन्ततः
इतिहास में जहां-तहां यह सुबूत बिखरा पड़ा है कि शासकों ने अपनी सत्ता बचाने के लिए विरोध और असहमति को देशद्रोह मानकर दमन किया है। हालांकि, कई बार इतिहास ने उन लोगों को नायक के रूप में स्वीकार किया, जिन्हें कभी “देशद्रोही” कहा गया था। आज भी यह संघर्ष जारी है, जो मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के लिए अनवरत लड़ाई का द्योतक है।
(उपेंद्र चौधरी वरिष्ठ पत्रकार और डाक्यूमेंटरी निर्माता हैं।)