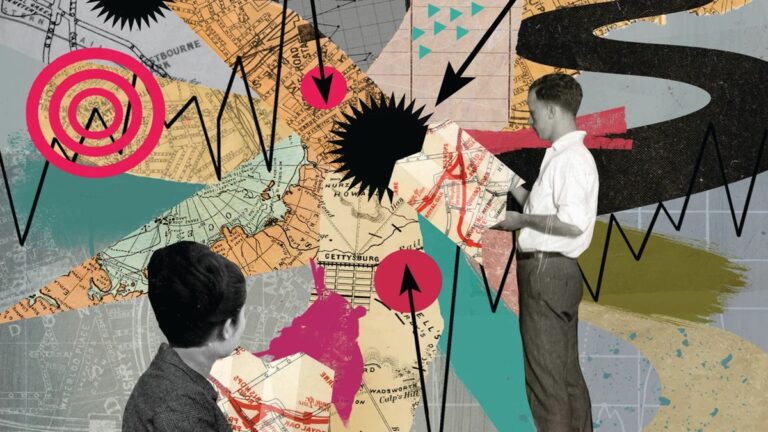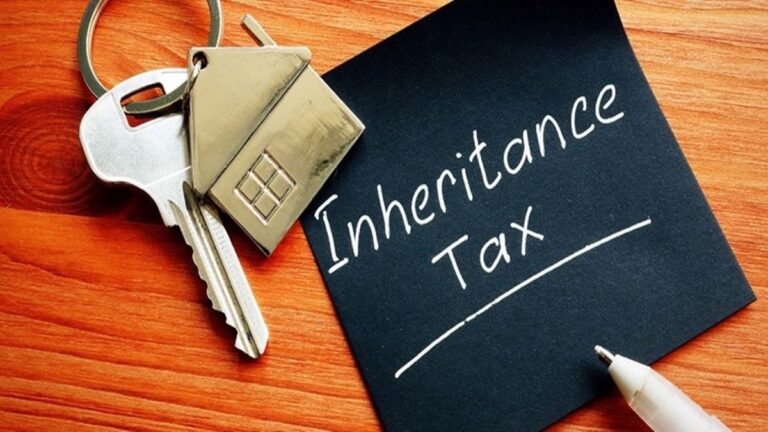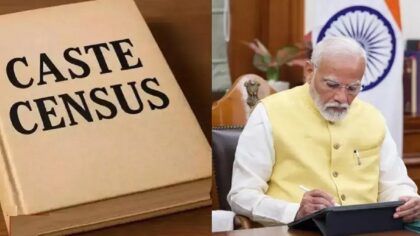सत्ताधारी खेमे का कोरस, जिसमें कंसल्टिंग फर्मों से लेकर वित्तीय मीडिया तक शामिल हैं, मांग कर रहा है कि घरेलू उपभोग को बढ़ावा दिया जाए ताकि भारत की गिरती आर्थिक विकास दर को संभाला जा सके। इस कोरस में सबसे हालिया जोड़ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का है, जिसने अपनी ताज़ा बुलेटिन में उपभोग बढ़ाने की सलाह दी है ताकि अर्थव्यवस्था में निवेशकों की कमज़ोर होती ‘एनिमल स्पिरिट’ को पुनर्जनन किया जा सके।
इस चिंता को लेकर दो बिंदुओं पर ध्यान देना ज़रूरी है। पहला, भारत की विकास दर, जिसके लिए पहले भविष्यवाणी की गई थी कि 2024-25 में यह 7% रहेगी, अब अनुमानित रूप से केवल 0.5% कम यानी 6.5% रहने की बात कही जा रही है। इतनी मामूली कमी से इतनी हलचल मचाने की ज़रूरत नहीं है। 6.5% की विकास दर हर दृष्टिकोण से उच्च मानी जाएगी और इसे ‘एनिमल स्पिरिट’ के कमज़ोर होने का संकेत नहीं माना जा सकता, जिससे सत्ता प्रतिष्ठान के अर्थशास्त्रियों को कोई गंभीर चिंता हो। ऐसी चिंता यह दर्शाती है कि विकास दर की गणना, जो सामान्य GDP की अवधारणा पर आधारित है (जो स्वयं में दोषपूर्ण है), अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकती है।
दूसरा, जैसा कि RBI ने स्वयं स्पष्ट किया है, इसकी चिंता शहरी मध्यवर्ग के उपभोग को लेकर है, न कि मेहनतकश जनसमुदाय के उपभोग को लेकर। जिस उपभोग को बढ़ाने की बात की जा रही है, वह शहरी मध्यवर्ग का है। यह निष्कर्ष निम्नलिखित तथ्यों से निकलता है: यदि मेहनतकश गरीबों के उपभोग को बढ़ाकर कुल मांग बढ़ाने का इरादा होता, तो इसका एक स्पष्ट रास्ता होता कि सभी की मज़दूरी, बिना किसी भेदभाव के, बढ़ा दी जाए। यह कानूनी रूप से न्यूनतम मज़दूरी दर को बढ़ाकर किया जा सकता है।
लेकिन इस दिशा में कोई बात नहीं हो रही है। इसके विपरीत, लार्सन एंड टुब्रो ने मांग की है-और किसी अन्य औद्योगिक घराने के प्रमुख ने इस पर असहमति नहीं जताई है-कि काम के घंटे बढ़ाकर प्रति सप्ताह 90 घंटे कर दिए जाएँ। इसका परिणाम यह होगा कि भारत के कारखाने नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप जैसे बन जाएँगे, जहाँ लोग काम करते-करते मर जाया करते थे। उनका यह तर्क कि “घर पर बैठकर अपनी औरतों को देखने की बजाय काम करने से मज़दूरों की स्थिति बेहतर होगी” और “आराम की बजाय काम उनके जीवन को बेहतर बनाएगा,” नाज़ी कैंपों के प्रवेश द्वार पर लिखे हिटलर के कुख्यात नारे, “काम मनुष्य को स्वतंत्र बनाता है,” से भयावह रूप से मिलता-जुलता है।
स्पष्ट है कि भारत का सत्ता प्रतिष्ठान मेहनतकश जनता का उपभोग बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है। जहाँ तक शहरी मध्यवर्ग की बात है, उसके उपभोग को बढ़ाने के लिए खाद्यान्न मुद्रास्फीति को कम करने की बात की जा रही है। खाद्यान्न मुद्रास्फीति को निश्चित रूप से कम करना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि इसका कुल मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आखिरकार, खाद्यान्न मुद्रास्फीति से लाभान्वित होने वाले भी उपभोक्ता ही हैं। क्या खाद्यान्न मुद्रास्फीति बढ़ने से शहरी मध्यवर्ग में उपभोग की मांग में होने वाली कमी, उस वर्ग के उपभोग में होने वाली वृद्धि से अधिक है, जो खाद्यान्न कीमतों के बढ़ने से लाभान्वित होता है?
खाद्यान्न कीमतों के बढ़ने से लाभान्वित होने वाले वर्ग की बचत दर, शहरी मध्यवर्ग की तुलना में, जो इससे नुकसान उठाता है, ज़रूरी नहीं कि अधिक हो। खाद्यान्न मुद्रास्फीति उस तरह से खाद्यान्न उपभोग को कम नहीं करती, जैसा कि RBI या कुछ अन्य लोग सोचते हैं। यह मेहनतकशों की मांग को निचोड़कर उपभोग की मांग को कम करती है (जो अपनी आय का बहुत कम हिस्सा बचा पाते हैं), न कि अनिवार्य रूप से शहरी मध्यवर्ग को निचोड़कर। लेकिन शहरी मध्यवर्ग, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होने वाले वर्ग की तुलना में, एकाधिकार पूँजी द्वारा उत्पादित वस्तुओं का अधिक उपभोग करता है। यही कारण है कि शहरी मध्यवर्ग की आय पर इतना अधिक ध्यान दिया जा रहा है।
लेकिन बात को और आगे बढ़ाएँ। एक नवउदारवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें खुला व्यापार होता है, में विकास का मुख्य उत्प्रेरक आमतौर पर निर्यात होता है। कभी-कभी संपत्ति की कीमतों में बुलबुले बन सकते हैं, जो असामान्य रूप से उच्च उपभोग को जन्म देते हैं और विकास को कुछ गति दे सकते हैं। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में, यह निर्यात मांग में वृद्धि ही है जो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करती है। इसका मतलब है कि जो मांग की जा रही है, वह निर्यात आधारित विकास के बजाय उपभोग आधारित आर्थिक विकास है, जिसका अर्थ मूलतः घरेलू बाजार आधारित विकास है।
प्रश्न यह है कि क्या यह नवउदारवादी सीमाओं के भीतर संभव है? मध्यवर्ग को आसान शर्तों पर अधिक ऋण उपलब्ध कराने से उसका उपभोग कुछ समय के लिए बढ़ सकता है, लेकिन जल्द ही यह कम हो जाएगा, क्योंकि उपभोक्ताओं पर कर्ज का बोझ बढ़ता जाएगा और वे और अधिक कर्ज लेने से बचना चाहेंगे। इसी तरह, यदि खाद्यान्न मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पा लिया जाए, तो उपभोग में अस्थायी वृद्धि हो सकती है, लेकिन विकास की गति को बनाए रखने के लिए उपभोग में निरंतर वृद्धि नहीं हो सकती।
यह सोचा जा सकता है कि यदि उपभोग बढ़ रहा है और इसके परिणामस्वरूप आय भी बढ़ रही है, तो यह प्रक्रिया अनवरत जारी रहेगी। लेकिन यदि किसी दौर में उपभोग किसी कारण से गिर जाता है, तो यह नीचे की ओर जाने का रुझान शुरू हो जाता है, और इसे रोकने वाला कोई नहीं होता। उपभोग आधारित विकास को लगातार बनाए रखने के लिए इसे किसी बाहरी स्वायत्त शक्ति द्वारा संचालित करना होगा। सरकारी खर्च के माध्यम से उपभोक्ताओं को दी जाने वाली क्रय शक्ति ही वह स्वायत्त शक्ति हो सकती है।
ऐसा होने के लिए सरकारी खर्च में बड़ी छलाँग ज़रूरी है, भले ही वह इस रूप में हो कि सरकार जनता को नकद हस्तांतरण करे, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़े। लेकिन सरकारी खर्च में यह छलाँग तभी संभव है, जब सरकार या तो अपना राजकोषीय घाटा बढ़ाए या उन वर्गों पर कर बढ़ाए, जो अपनी आय का बड़ा हिस्सा बचत करते हैं। केवल ऐसी स्थिति में ही उपभोग बढ़ सकता है।
यदि कर केवल उन वर्गों पर बढ़ाया जाता है, जो अपनी अधिकांश आय का उपभोग कर लेते हैं, तो मान लीजिए, उनसे वसूला गया 100 रुपये का कर उनके उपभोग को 100 रुपये कम कर देता है। यदि यह 100 रुपये उन्हें नकद हस्तांतरण के रूप में वापस दे दिया जाता है, तो उपभोग फिर से 100 रुपये बढ़ जाता है। इस स्थिति में कुल उपभोग में कोई वृद्धि नहीं होती, और न ही उपभोग आधारित विकास होता है।
उपभोग आधारित विकास के लिए ऐसी राजकोषीय नीति की ज़रूरत है, जो अतिरिक्त संसाधन जुटाए-चाहे वह अमीरों पर कर लगाकर हो (जो अपनी आय का बड़ा हिस्सा बचत करते हैं) या राजकोषीय घाटा बढ़ाकर। लेकिन नवउदारवादी व्यवस्था में ये दोनों विकल्प संभव नहीं हैं। राजकोषीय घाटा बढ़ाना संभव नहीं है, क्योंकि यह वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन कानून का उल्लंघन होगा, जो GDP के एक निश्चित प्रतिशत से अधिक घाटे को अनुमति नहीं देता। अमीरों पर कर-चाहे संपत्ति कर के रूप में हो या उनके लाभ पर-लगाने से पूँजी का पलायन होगा, जो नवउदारवादी ढांचे में विकास को प्रभावित करेगा।
वास्तव में, उत्पादक पूँजी के पलायन से पहले वित्तीय पूँजी बड़े पैमाने पर पलायन कर जाएगी, जिससे देश संकट में पड़ सकता है। एक संभावना कृषि विकास को प्रोत्साहित करने की है, जिससे किसानों की आय बढ़े और परिणामस्वरूप उपभोग में वृद्धि हो। उपभोग आधारित, और इसीलिए घरेलू बाजार आधारित विकास का असली औचित्य कृषि आधारित विकास में ही निहित है।
लेकिन इसके लिए सरकार को कृषि-समर्थक नीतियों की ज़रूरत है, न कि किसानों की कीमत पर कॉर्पोरेट और कृषि-व्यवसाय को बढ़ावा देने वाली नीतियों की, जैसा कि वर्तमान में नवउदारवादी नीतियों के तहत हो रहा है। कॉर्पोरेट कृषि को बढ़ावा देने से किसानों की आय बढ़ने के बजाय कम होती है, जिससे उपभोग को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता।
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि निर्यात आधारित विकास से उपभोग आधारित विकास की ओर संक्रमण नवउदारवादी ढांचे में संभव नहीं है। चीन एकमात्र ऐसा देश है, जिसने निर्यात-निर्भरता से उपभोग आधारित विकास को अपना मुख्य आधार बनाने में सफलता हासिल की है। लेकिन चीन नवउदारवादी नीतियों से बंधा नहीं है।
यह ऐसा देश नहीं है, जहाँ सरकारी नीतियों की स्वायत्तता वैश्विक वित्तीय पूँजी की नीतियों की गुलाम हो। इसका कारण यह है कि यह वैश्विक पूँजी के सीमा-पार आवागमन के लिए खुला नहीं है और इसे ऐसा करने की बाध्यता भी नहीं है, क्योंकि इसके पास हमेशा व्यापार और चालू खाता अधिशेष रहता है।
लेकिन भारत और तीसरी दुनिया के अन्य देश एक अलग श्रेणी में हैं। वे न केवल वैश्विक वित्तीय पूँजी के लिए खुले हैं, बल्कि इसके लिए मजबूर भी हैं। अधिकांश देश अपने व्यापार संतुलन को संभाल नहीं पाएँगे, जब तक कि बाहरी वित्तीय पूँजी न आए, और जब तक वे व्यापार पर नियंत्रण न करें और सीमा-पार अनियंत्रित व्यापार को अनुमति दें।
RBI और सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े अर्थशास्त्री इस तरह बात करते हैं, जैसे भारत सरकार आर्थिक नीतियों को बनाने में पूरी तरह स्वायत्त है। लेकिन यह नवउदारवादी अर्थव्यवस्था के कार्य करने के तरीके के बारे में उनकी समझ के पूर्ण अभाव को ही दर्शाता है।
(पीपुल्स डेमोक्रेसी से साभार, अनुवाद: लाल बहादुर सिंह)