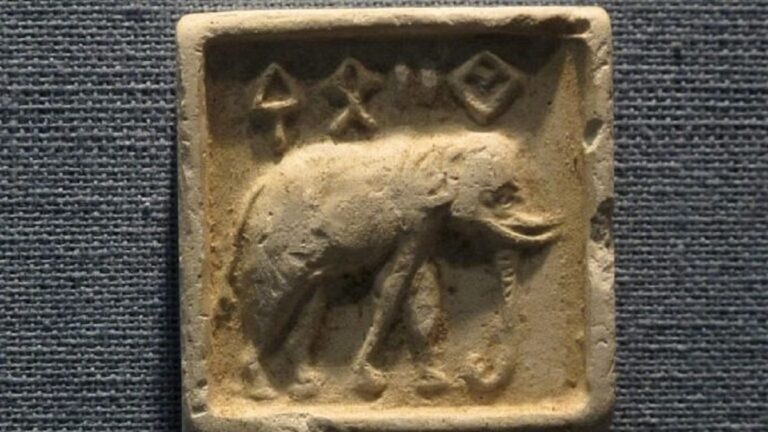भारत में अगस्त महीना का अतिरिक्त महत्व का होता है। 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में हुई वीभत्स घटना के प्रतिवाद में ‘न्याय चाहिए – न्याय चाहिए’ के उद्घोष के साथ आंदोलन चल रहा है। मुख्य मीडिया में राजनीतिक दल के प्रवक्ता आरोप-प्रत्यारोप में सूप-चलनी के खेल में लगे हुए हैं।
प्रतिवाद और प्रतिरोध पश्चिम बंगाल के नागरिक समाज का प्रखर औजार रहा है। पश्चिम बंगाल के लोगों के जीवन में और इसलिए पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी भिन्न तरह की भावुकता की अधिकता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
जाहिर है कि प्रतिवाद और प्रतिरोध का सिलसिला अभी लंबे समय तक चलता रहेगा। ऐसे में न्याय के लिए किये जानेवाले संघर्ष कब राजनीतिक दल सत्ता बताने-पाने के संघर्ष में बदल देते हैं ‘न्याय चाहिए’ की गुहार लगाती जनता को पता ही नहीं चलता है। न्याय के लिए किये जानेवाले संघर्ष को भावुकता की गिरफ्त में फंसने से बचने की बौद्धिक कोशिश करनी ही चाहिए।
कहना न होगा कि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रत्यक्ष प्रतीक होते हैं। उन से जुड़े साधारण-असाधारण सदस्य के अपराध के लिए पूरे दल को जवाबदेह बनाकर राजनीतिक-अग्रता हासिल करने की प्रवृत्ति अंततः लोकतंत्र को ही क्षतिग्रस्त कर देती है। यौन हिंसा की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। इन घटनाओं पर मीडिया में अ-नियंत्रित और अमर्यादित बयान से चर्चा के सभी भागीदार को बचना चाहिए।
खासकर, यौन हिंसा की घटना पर राजनीतिक प्रवक्ताओं की बयान-बहादुरी से सामाजिक वातावरण और अधिक विषाक्त हो जाता है। बात यह है कि बयान-बहादुरी के किसी-न-किसी पक्ष का ऐसा रुख सामने आने लगता है जो शर्मनाक और भ्रामक होता है। इसके बहुत सारे ऐसे मानसिक प्रभाव होते हैं जिससे समाज के सभी संवर्गों के सदस्यों को बचना-बचाना चाहिए।
न्याय की धारणा को एकांगी नहीं बनाया जाना चाहिए न बनाया जा सकता है। रोजी-रोजगार के लिए किये जानेवाले, न्यूनतम-समर्थन (MSP) जैसे मुद्दों पर किये जानेवाले संघर्ष का लक्ष्य भी मूल रूप से न्याय के लिए किया जानेवाला संघर्ष ही होता है। राजनीतिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया ऊपर से एक भले ही दिखती हो लेकिन अंदर से इन के अर्थ भिन्न होते हैं, इनके लक्ष्य भिन्न होते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं का परस्पर सहयोगी होना सामाजिक शुभ को सुनिश्चित करता है, इनमें परस्पर विरोध हितनाशी और एक दूसरे का एवजी बन जाना भ्रामक होता है।
धरना-प्रदर्शन-आंदोलन तो लोकतंत्र और राजनीति की सामान्य प्रक्रिया है। दोनों के लक्ष्य भिन्न होते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का लक्ष्य वास्तविक अर्थ में नागरिक अधिकार और न्याय प्राप्त करना होता है, वहीं राजनीतिक प्रक्रिया का लक्ष्य सत्ता अधिकार और शक्ति प्राप्त करना होता है। जिन्हें लोकतंत्र की सामान्य प्रक्रिया से परहेज है उनका मिजाज लोकतंत्र के माफिक नहीं है।
जनता और नागरिकों के साथ ‘राजनीति’ करनेवाले नेताओं को यह समझना होगा कि वे ‘कुछ भी फेंककर’ नहीं निकल सकते हैं। देश के लोगों का रोजगार मांगना किसी ‘विदेशी षड़यंत्र’ का हिस्सा नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बयान-बहादुरी में लोकतंत्र की सारी सीमाएं लांघते रहे हैं।
यह सच है कि किसी राष्ट्र के जीवन में दस साल का महत्व बहुत नहीं होता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि व्यक्ति के जीवन-स्तर में बेहतरी-बदतरी के लिए दस साल का महत्व बहुत होता है। डॉ राममनोहर लोहिया ने कहा था कि ‘जिंदा कौमें’ पांच साल तक इंतजार नहीं करती हैं।
बड़े सम्मान के साथ कहना जरूरी है कि भारत की ‘जिंदा कौमों’ ने दस साल तक इंतजार ही नहीं किया बल्कि, दस साल तक झूठ को सीने से लगाये मृत-आशा को जिलाने के लिए अपनी जिंदगी का धुआं-धुआं कर लिया।
पूरी दुनिया के बारे में क्या कहा जाये! भारत में सामान्य तौर पर मर्दवादी रुझान खतरनाक हद तक बढ़ता गया है। राज्य व्यवस्था और समाज व्यवस्था के पितृसत्तात्मक होने और उसमें मर्दवादी रुझान के बढ़ने का निकृष्ट असर भी लोकतंत्र को बदसूरत बना रहा है। राजनीतिक विश्लेषण में महिला वोटों के निर्णायक असर के होने की बात कही-सुनी जाती है। महिला वोटों पर महिलाओं कि विशिष्ट स्थितियों का कितना पर कितना प्रभाव पड़ता है, कहना मुश्किल है।
किसी महिला के हाथ में राज्य व्यवस्था होने से व्यवस्था का मर्दवादी रुझान कम नहीं होता है। कहा जा सकता है कि महिला के हाथ में वोट की ताकत होने से भी राजनीति के मर्दवादी रुझान में कोई कमी नहीं होती है। क्योंकि यह सत्ता का नहीं, व्यवस्था और शासन के मिजाज का मामला है।
इंदिरा गांधी के हाथ में बरसों सत्ता रही, खुद सोनिया गांधी का भी सत्ता पर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पर प्रभाव रहा, जयललिता और मायावती देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहीं, ममता बनर्जी कई सालों से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं लेकिन इस से व्यवस्था पर उनके स्त्री होने से कोई पठनीय प्रभाव नहीं पड़ा है।
9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई वीभत्स घटना के परिप्रेक्ष्य हो रहे प्रतिवाद और प्रतिरोध को एक ओर रखकर भी देखा जाये, तो भी कहा जा सकता है कि उनके मुख्यमंत्री रहते पश्चिम बंगाल की राजनीति में मर्दवादी रुझान बिल्कुल कम नहीं हुआ है।
जन-आक्रोश और जन-आंदोलन के बीच के अंतर और अंतर्विरोध को समझना जरूरी है। कुछ इतिहास से कुछ वर्तमान से सीखने की जरूरत है, यकीनन ‘शुद्ध राजनीति’ के लोगों को किसी ‘सीख’ की जरूरत नहीं है। क्या पता, नागरिक समाज को हो!
थोड़ा इतिहास के आईने में झांकने की कोशिश करें! क्रिप्स मिशन के निष्फल हो जाने के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए तीसरा बड़ा आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ और ‘अंग्रेजों भारत छोड़ो’ की राजनीतिक लहर भारत के लोगों के मन में उठने लगी। हालांकि महात्मा गांधी को तुरत गिरफ्तार कर लिया गया।
इसके बावजूद देश भर के युवा कार्यकर्ता ने राजनीतिक आंदोलन की जोत मध्यम न पड़ने दी। कांग्रेस में भूमिगत प्रतिरोध की गतिविधि के लिए कांग्रेस में सक्रिय समाजवादी सदस्य जिनमें जयप्रकाश नारायण की भूमिका को याद किया जाता है; ‘भूमिका’ को कभी-कभी याद करता है लेकिन ‘सीख’ को अकसर भूल जाता है!
कुछ दिन के बाद भारत में प्रांतीय विधान मंडलों के लिए नए सिरे से चुनाव 1946 की शुरुआत में कराए गए। सामान्य सीटों पर तो कांग्रेस को उल्लेखनीय सफलता मिली लेकिन मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत मिल गया। मतलब साफ-साफ समझा जा सकता है कि धार्मिक आधार पर राजनीतिक ध्रुवीकरण हो चुका था।
इसके कुछ ही महीनों के बाद 1946 में ही कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन का लक्ष्य था सीमित स्वायत्तता के साथ भारत के लोगों को संघात्मक व्यवस्था के लिए सहमत करवाना। कैबिनेट मिशन 1946 योजना निष्फल हो गई।
16 अगस्त 1946 का दिन पाकिस्तान बनाने के समर्थन में ‘डायरेक्ट एक्शन’ यानी ‘सीधी कार्रवाई की घोषणा कर दी गई। इसके बाद कोलकाता से शुरू होकर बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत और पंजाब तक हिंदू-मुसलमान के बीच खूनी संघर्ष फैल गया।
संवेदनशीलता और भावुकता में अंतर होता है। शुद्ध संवेदनशीलता का शुरू बुद्धिमत्ता से कभी भी विच्छेद नहीं होता है। संवेदनशीलता और बुद्धिमत्ता मनुष्य के अस्तित्व के मानस के अनिवार्य पहलू हैं। इनमें से किसी एक की भी अशुद्धता दोनों को अशुद्ध कर देती है। संवेदनशीलता से बुद्धिमत्ता के पूर्ण विच्छेद और निषेध से कोरी भावुकता या गलदश्रु भावुकता का जन्म होता है।
आंदोलन की शुरुआत में भावुकता जरूर काम आती है, लेकिन कोरी भावुकता से कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। हक और न्याय के लिए किया गया जानेवाला आंदोलन भी सिर्फ भावुकता से सफल नहीं हो सकता है।
‘न्याय चाहिए – न्याय चाहिए’ की गुहार को हर-बार बुद्धिमान शासक भावुकता से जोड़ने और बुद्धिमत्ता से तोड़ने का प्रयास करता है और अपनी चालाकी में सफल हो जाता है। ‘जोड़ने-तोड़ने’ की राजनीति, कभी-कभी ही नहीं, अकसर खतरे के निशान के पार चली जाती है।
भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने संवेदनशीलता के साथ निष्कंप बुद्धिमत्ता का ऐसा अटूट संयोग बनाये रखा कि ब्रिटिश हुकूमत चकित रह जाया करती थी। संविधान निर्माताओं ने भी अपनी भावुकता को नियंत्रित रखा और बुद्धिमानी से काम लिया। संवेदनशीलता और बुद्धिमत्ता के जुड़ाव और भावुकता के निषेध नहीं, नियंत्रित के महत्व को समझा।
बुद्धिमत्ता के पूर्ण विच्छेद और निषेध से निकली उन्मादी और उपद्रवी भावुकता से समग्र जीवन-व्यवस्था तहस-नहस हो जाती है। कहना न होगा कि राम मंदिर आंदोलन के दौर में बुद्धिमत्ता का पूर्ण विच्छेद और निषेध करते हुए उन्मादी और उपद्रवी भावुकता को सत्ता की राजनीति से जोड़ने की रणनीति से भारतीय जनता पार्टी ने काम लेना शुरू कर दिया था।
जरूरी प्रसंग के रूप में याद किया जा सकता है कि राजीव गांधी के शासन-काल में भारत की राजनीति को उन्मादी और उपद्रवी भावुकता ने अपनी चपेट में ले लिया। दो उदाहरण का उल्लेख ही काफी है। शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उलट देना और राम मंदिर का ताला खुलवा देना।
राजीव गांधी को प्राप्त अपराजेय बहुमत का उन्मादी और उपद्रवी भावुकता की चपेट में आने से बच नहीं पाने के कारण भारत की राजनीति का बुद्धिमत्ता से विच्छिन्न हो गया था। इस विच्छिन्नता के बहु-आयामी नतीजे का सामना भारत की राजनीति और लोकतंत्र को लंबे समय से करना पड़ रहा है। दो सीट पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक साहस बढ़ता गया। धीरे-धीरे इसका प्रभाव और इसकी गति तेज होती गई।
पिछले दस साल से अपने बहुमत के जोर पर ‘एक अकेले के भारी पड़ने’ के औद्धत्य में ‘चार सौ के पार’ की घोषणा तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई। यह अलग बात है कि 2024 के आम चुनाव के नतीजा ने ‘एक अकेले के भारी पड़ने’ के मुहावरे के मुकाबले में ‘अकेला चना भांड़ नहीं फोड़ता’ की दीनता का मुहावरा भारतीय जनता पार्टी के औद्धत्य के सामने रख दिया!
‘चार सौ के पार’ की घोषणा भले ही ‘दो सौ चालीस’ में सिमट गई हो, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और जनता दल यूनाइटेड के अनिवार्य समर्थन से ही सही लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने का ‘गौरव’ तो नरेंद्र मोदी को हासिल हो ही गया!
यह अलग बात है कि लोकतंत्र में ‘गौरव’ के ‘रौरव’ में बदलते बहुत देर नहीं लगती है! मुश्किल से पांव पीछे करनेवाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार अपने फैसले से पीछे हटने का परिदृश्य आम होता जा रहा है। कहने का आशय यह है कि एक बात जरूर गांठ बांधकर रख लेनी चाहिए कि कठिन समय में कोरी भावुक सांद्रता नहीं, निष्कंप बुद्धिमत्ता ही काम आती है।
औपनिवेशिक भारत में कैबिनेट मिशन की विफलता और आजाद भारत में शाह बानो मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को उलट देना और राम मंदिर का ताला खुलवा देना दो ऐसी घटनाएं हैं जिसके चलते भारत की आजादी की आकांक्षा खंडित हो गई और धर्म आधारित राजनीति का ‘महा-द्वार’ खुल गया।
महात्मा गांधी अपने बारे में कहते थे, ‘हां मैं हिंदू हूं। मैं एक ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध और यहूदी भी हूं।’ वे अपनी नागरिकता को भारतीय और जाति को गुजराती मानते थे। बंगाल में जाति का मतलब आज भी जातीयता के अर्थ में ही लिया जाता है।
भारतीय जनता पार्टी के पिछले दस साल के शासन की घातक ‘उपलब्धि’ राजनीति के इस ‘महा-द्वार’ में प्रवेश करने की कुछ अनिवार्य शर्तें स्थापित कर देना है। ये ‘शर्तें’ हैं, सामाजिक और आर्थिक न्याय के सवाल को ‘सम्मान’ के साथ लोकतांत्रिक विवेक की ‘गठरी’ को बाहर रखना। महात्मा गांधी की तरह यह कहने के दुस्साहस से बचना कि ‘हां मैं हिंदू हूं। मैं एक ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध और यहूदी भी हूं।’
यह कम बड़े राजनीतिक साहस की बात नहीं है कि अपनी बुद्धिमानी से काम लेते हुए इंडिया अलायंस गठबंधन के माथे पर न्याय और लोकतांत्रिक विवेक की गठरी लादे हुए और यह कहते हुए कि ‘हां मैं हिंदू हूं। मैं एक ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध और यहूदी भी हूं और मेरे साथ हैं विषमता के दंश से छटपटाते, सामाजिक और आर्थिक अन्याय का शिकार बने आम भारतीय जन’।
‘न्याय योद्धा’ राहुल गांधी भारत की सत्ता राजनीति के ‘महा-द्वार’ में प्रवेश करने की कोशिश में निरंतर लगे हुए हैं। इस कोशिश में निहित राजनीतिक नुकसान के आशंका की परवाह किये बिना लगे हुए हैं।
भावुकता परिचालित जन-आक्रोश और बुद्धिमत्ता संपन्न जन-आंदोलन के अंतर को ध्यान में रखते हुए भारत के लोगों को व्यापक जन-हित के मुद्दों पर बड़े जन-आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए; जन-हित के मुद्दों को विचार-बुद्धिहीन भावुक राजनीति की हितनाशी रणनीति से बचते हुए ही यह तैयारी सार्थक हो सकती है। ‘न्याय चाहिए’ जरूर, साथ-साथ न्याय को समझना भी चाहिए!
(प्रफुल्ल कोलख्यान स्वतंत्र लेखक और टिप्पणीकार हैं)