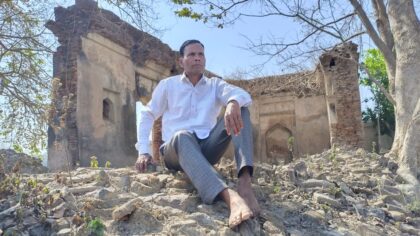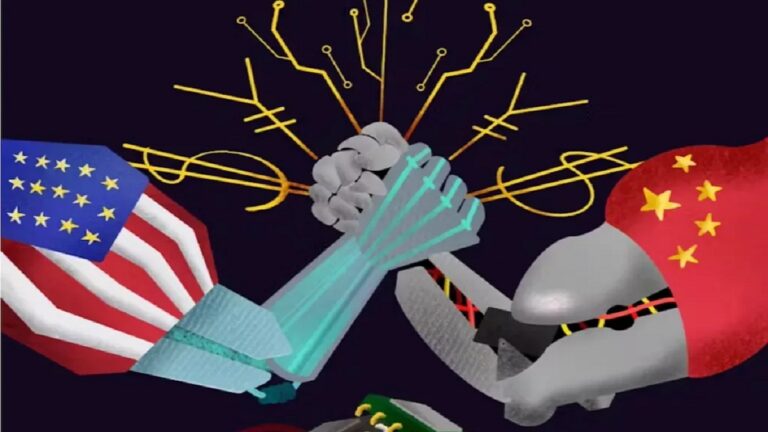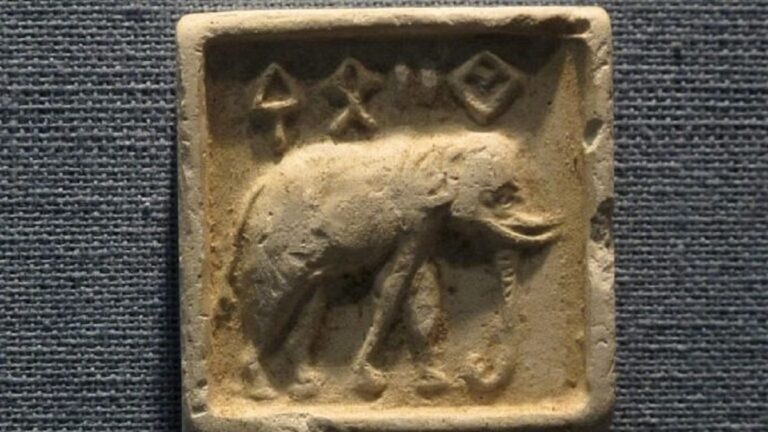संसद में बीते सत्र के दौरान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि विकास परियोजनाओं के लिए पिछले 10 सालों में, 2014-24 के बीच 1,734 वर्ग किमी जंगल खत्म हुए हैं। पर्यावरण के बढ़ते संकट के दौर में इस तरह का बयान चौंकाने वाला था। चूंकि यह आंकड़ा सरकार बता रही थी, तब आप इसकी भयावहता का अनुमान लगे सकते हैं। हालांकि उन्होंने राज्य सभा में यह भी बताया कि 2011 की तुलना में 2021 में 21,762 वर्ग किमी जंगल क्षेत्र विकसित किया गया।
उन्होंने अपने बयान में कुछ और बातों को जोड़ा है जिसे पढ़ने के साथ ही और स्पष्टता आ सकेगीः ‘‘जब भी केंद्र की ओर से जंगली क्षेत्र के गैर-जंगल कार्य के उद्देश्य से प्रयोग में लाने को मान्यता दी जाती है तब पूरक के तौर पर जंगल लगाने और उस भूमि की वर्तमान मूल्य को उसके उपयोगकर्ता से लिया जाता है, जैसा कि इसके लिए प्रावधान बनाया गया है। इसके अलावा कुछ अनुपूरक तरीके भी अख्तियार किये जाते हैं, जैसे भूमि और नमी के संरक्षण का कार्य, जल-जमाव क्षेत्र और उसकी सफाई का कार्य और वन्यजीवन प्रबंधन योजनाएं इससे जुड़ी है और ये जरूरत के अनुरूप इसका हिस्सा होती हैं।’’
यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि जंगल लगाना और जंगल काटने के बीच काफी फर्क है। यहां पर्यावरण मंत्री का जो दूसरा बयान है वह अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम जंगल, पहाड़, नदी, झरना, झील और वन्य-जीवन के बारे में बात करते हैं तो उसके साथ न सिर्फ उसकी भौगोलिक स्थितियां जुड़ी होती हैं, उसके साथ मुनष्य के जीवन की परिस्थितियां भी जुड़ी होती हैं। पेड़ लगाना जंगल रोपना नहीं होता है।
एक प्रसिद्ध कहावत है पेड़ गिनने से हम जंगल को नहीं जान सकते। जंगल भूगोल और जीवन की परिस्थितिकी का हिस्सा है। मसलन, खेत और उसका उत्पादन उसकी परिस्थिति का अभिन्न हिस्सा है। उसके उत्पादन की बढ़ोत्तरी के लिए अतिरिक्त हस्तक्षेप और निवेश उसे एक सीमा से अधिक दूरी तक नहीं ले जा सकते। ऐसा करने पर भूमि का क्षरण, पानी का संचय या भूगर्भ जल के दोहन की स्थिति में उसमें तेजी से गिरावट जैसे परिणाम आयेंगे। इसी तरह से अधिक रसायन का प्रयोग अंततः भूमि के अपक्षय और सामान्य पर्यावरणीय जीवन, जिसमें कीट-पतंगों, पक्षियों से लेकर पारम्परिक पौधों के नुकसान होने और यहां तक की उसके खत्म होने के रूप में संकट सामाने आता है। पंजाब और कुछ हद तक अब हरियाणा में हम इसकी स्थिति देख सकते हैं।
जंगल खुद भी उत्पादन का एक हिस्सा होते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कोई जंगल नहीं है जो मनुष्य के बसवाट और उसकी जीवन पद्धतियों का हिस्सा नहीं हैं। चाहे वे अमेजन के जंगल हों या भारत का अबूझमाड़ कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ का सुदूर जंगल में बसा गांव हो। एक देश की संकल्पना में जंगल उस देश की पर्यावरण का भी अंग बन जाता है। और उसकी भूमिका जंगल के भीतर चल रही जिंदगी से अधिक महत्वपूर्ण हो उठती है। खासकर, पूंजीवाद की मार से तप रही धरती जब और गर्म होती जा रही है और अंटार्टिका की बर्फ पिघलने लगी है तब इन जंगलों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है।
हाल ही में हुए अध्ययन बता रहे हैं कि पेड़ लगाना एक बेहद जरूरी कार्य है। लेकिन, पेड़ की भूमिका जंगल के संदर्भ में बहुत कम होती है। मीथेन और कार्बन डाईआक्साइड जैसी गैस के प्रभावों को खत्म करने के लिए जिस तरह के पर्यावरण की जरूरत होती है वह जंगलों से हासिल होती है। पेड़ एक चुनाव की प्रक्रिया में रोपे जाते हैं जबकि जंगल अपनी भू-परिस्थितियों में बहुविध किस्मों के साथ विकसित होते हैं। इसमें निश्चित ही हस्तक्षेप किया जा सकता है। और पर्यावरण के अध्ययन के आधार पर इसकी विविधता को बढ़ाया जा सकता है; लेकिन इसकी संरचना गुणात्मक तौर पर भिन्न होती है। यह जल संचयन और मौसम के चक्रों के साथ खुद को व्यवस्थित करती है। इसका अपना वन्य जीवन होता है, जिसमें विविध तरह के जीव और पक्षियों के लिए जगह मिलती है और वे इस वन्य जीवन और पौधों, पेड़ों को विकसित करने सहायक की भूमिका में होते हैं।
दक्षिण अमेरीका में अमेजन के जंगलों में हस्तक्षेप ने, खासकर ब्राजील की ओर से की गई अंधाधुंध कटाई ने न सिर्फ अमेजन जैसी नदी को नाले में बदल देने की ओर ले गई, इस जंगल से लगे अन्य कई देश इससे पैदा हुई विभीषिका में फंस गई। भारत में जंगलों और नदियों के बर्बाद करने का इतिहास उपनिवेशिक दौर से जारी है। अंग्रेजों ने न सिर्फ हिमालय क्षेत्र के जंगलों को बर्बाद करने में आगे रहे, वहां के पर्यावरण में कुछ ऐसे पेड़ों को वहां लगाया जिसका नुकसान आज भी जारी है।
पश्चिमी घाट पर उनके द्वारा किया गया हस्तक्षेप कभी भी ठीक नहीं किया गया और उसका असर हमें प्राणघातक भूस्खलन में दिख रहा है। उन्होंने अरावली क्षेत्र, खासकर दिल्ली और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर मैक्सिकन बबूल लगाकर यहां की पर्यावरण विविधता पर गहरा असर डाला। लेकिन, 1947 के बाद विकास की विशाल परियोजनाओं का असर सबसे अधिक मध्यभारत के राज्यों पर हुआ है।
इन इलाकों में सिर्फ जंगल, भूमि, नदी, उत्पादन आदि ही प्रभावित नहीं हुआ। इन इलाकों में बसने वाली जनजातियों को उनके अस्तित्व के संकट तक पहुंचा दिया। इन जंगल क्षेत्रों को विकास के नाम पर जिस तरह अधिग्रहित किया गया और वहां की जनजातीय समूहों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया गया वह भारत के इतिहास की अभूतपूर्व घटनाएं हैं। यह अभियान और उन जनजातीय समूह के लोगों का मारा जाना आज भी जारी है।
जंगल और मनुष्य के बीच एक चिरस्थाई संघर्ष है। ऑस्कर जीतने वाली वृत्तचित्र ‘द एलीफैंट व्हीस्पर’ में इस संघर्ष के चित्रण मनुष्य और जंगल के बीच के रिश्तों की ऐसी गहराई में ले जाता है जिसकी परतों में लाखों साल का इतिहास छुपा है। एक परिवार एक घायल हाथी के बच्चे को पालता है और उस बच्चे को जंगल का हिस्सा बनाता है। जब पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव राज्य सभा को बता रहे थे कि वह जंगल की नमी, जल जमाव और संरक्षण आदि पर ध्यान दे रहे हैं तब वे उन तकनीकी बातों का उल्लेख कर रहे थे, जो जंगल के लिए एक जरूरी हिस्सा होते हैं।
जबकि सच्चाई इससे कहीं बहुत दूर है। खुद दिल्ली के भीतर जंगल क्षेत्र कम हो रहे हैं और अवैध कटाई को लेकर न्यायालय में विवाद अभी भी जारी है। इस शहर से गुजरने वाली दो नदियां महज नाले में तब्दील हो चुकी हैं। देश की राजधानी से जितना दूर जाईए, सरकारी दस्तावेजों के दावे और हकीकत के बीच का फासला उतना ही बढ़ता जाता है। वन्यरोपण के दावे और सच के बीच का फासला हमारे पर्यावरण के संकट में दिख रहा है। इसे आंकड़ों से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
(अंजनी कुमार स्वतंत्र पत्रकार और लेखक हैं)