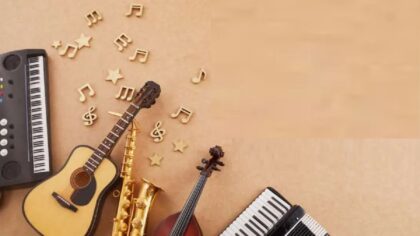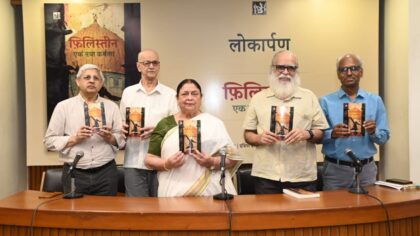दुनिया कहां-से-कहां पहुंच गई। दुनिया की समस्या से भारत की समस्या को कुछ भिन्न प्रकार से देखने-दिखाने की कोशिश में कुछ दिनों से तेजी लाई जा रही है। इस तेजी का बहुत गहरा संबंध हिंदुत्व के राजनीतिक एजेंडा से है। बार-बार भारत को इन मुद्दों के उलझावों में डालकर विपन्न कर दिया जाता है। भारत को विपन्नता में डालने का यह खेल बहुत ही स्पष्टता के साथ संपन्नता के सपनों का माया-जाल बिछाकर खेला जाता है। वर्तमान में हकदारी के सवाल को लोगों के दिमाग से बाहर निकालने के लिए कल्पित इतिहास का पोथा खोज निकाला जाता है। कल्पित भविष्य की रोशनी में कल्पित इतिहास का पन्ना खोला जाता है।
हकदारी का सवाल समाज और व्यवस्था की वर्तमान स्थिति से जुड़ा होता है। जीवन की समस्याओं का हल न तो इतिहास में हासिल किया जा सकता है, न वर्तमान की समस्याओं के किसी आकर्षक हल का भविष्य में मिलने का ही इंतजार किया जा सकता है। हकदारी के सवाल के कोलाहल और कलह से बाहर रहने के लिए नाजायज समस्याओं का अंबार लगा दिया जाता है। इस अंबार के तले जीवन की असली समस्याएं दबा दी जाती हैं। इसलिए, असली समस्याओं पर गौर करना चाहिए। समस्याएं कई हैं। इन समस्याओं पर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैधानिक और राजनीतिक संदर्भों में इन समस्याओं पर नजर दौड़ाने की कोशिश की जानी चाहिए।
ऐतिहासिक रूप से भारत बहुत पुराना, भौगोलिक विविधताओं, सामाजिक बहुलताओं, व्यवहारों, विविध मान्यताओं, अनेक जीवंत दार्शनिक धाराओं, बहुस्तरीय आंतरिक विभाजनों के साथ जीवनयापन करनेवाला देश रहा है। इतना ही नहीं भारत में आगंतुकों, आक्रांताओं के असंख्य जत्थों को भारत के विशाल प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मानजनक ढंग से रचने-बसने की जमीन और घुलने-मिलने का नैसर्गिक अवसर मिला। इन ऐतिहासिक परिस्थिति में भारतीय जीवन की जटिलताओं, चोटिलताओं, उलझावों के साथ भारत की अपेक्षाकृत स्थाई समस्याओं के कारण और तात्कालिक समाधान विकसित होते रहे हैं।
धर्म और मनुष्य का साथ बहुत पुराना है। भारत में आये विभिन्न जत्थों के पास भी आस्था और विश्वास का अपना आधार था। इन जत्थों के लोग समय के साथ भारत के धर्म-समूह का सदस्य बने। प्रारंभ में अपने अस्तित्व की रक्षा करते हुए और बाद में अपने अस्तित्व को समाहित करते हुए इन आगंतुकों के आस्था और विश्वास पहले से प्रवाहित धार्मिक धाराओं में दूध-मिसरी की तरह घुलते-मिलते चले गये। ऐसा नहीं है कि इस घुलने-मिलने में कोई घमासान हुआ ही नहीं! लेकिन हर-बार यहां के पहले से सक्रिय और आगंतुकों के विचारकों, दार्शनिकों ने मिलकर सह-अस्तित्व और सहिष्णुता की उदात्त और उच्चतर भावना ने घुलने-मिलने की संभावना को सच किया। इस तरह से मिलने-जुलने और घुलने-मिलने से भारत की संस्कृति की गंगा-जमुनी संस्कृति बनती रही।
गंगा-जमुनी संस्कृति की भाव-धारा में सक्रिय बुद्धिमत्ता इन आगंतुकों के आक्रमण के जख्मों को दुरुस्त करने में तत्परता के साथ लगी रही। हालांकि उन जख्मों के निशान एकदम से लुप्त नहीं हो गये लेकिन वक्त ने जख्मों के उन निशानों को बहुत हद तक गुप्त जरूर कर दिया। इस्लाम का मामला थोड़ा भिन्न है। इस्लाम के आगमन की परिस्थिति भिन्नता के कुछ कारण भारत में पहले से चले आ रहे बौद्ध-ब्राह्मण संघर्ष और इस्लाम में जगह पाये राजनीतिक मिजाज से भी जुड़े हैं। इन परिस्थितियों पर थोड़ा ठहरकर विचार किया जाना चाहिए।
भारत की गंगा-जमुनी संस्कृति विभिन्न आगंतुकों के दूध मिसरी की तरह घुलने-मिलने से बनी है। भारत की संस्कृति पर नजर डालते समय कवि-गुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर की काव्य-वाणी के मर्म पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए : हेथाय आर्य, हेथाय अनार्य, हेथाय द्राविड़-चीन, शक-हूण-दल, पठान-मोगल एके देहे होलो लीन।
अपने उद्भव के सौ साल के अंदर इस्लाम भारत के संपर्क में आया। गैरबराबरी से जूझती आबादी के लिए इस्लाम में सबसे बड़ा आकर्षण इस के बराबरी के सिद्धांत और व्यवहार में था। इस्लाम के आगमन का स्वागत गैर-बराबरी से परेशान भारत में बहुत अ-स्वाभाविक नहीं था। इस्लाम में दार्शनिक बहस के लिए अधिक आग्रह नहीं होता है। भारत के जीवन के उच्च सोपान पर दार्शनिक विचार-विमर्श का आग्रह और प्रभाव चला आ रहा था। इस्लाम का जब भारत से संपर्क विकसित हुआ तब तक भारत की संस्कृति में ‘आध्यात्मिक वर्चस्व’ का भाव था। भारत के संपर्क में आये इस्लाम को माननेवालों के एक बड़े अंश में ‘सत्ता वर्चस्व’ की प्रवृत्ति की जड़ जम चुकी थी।
‘आध्यात्मिक वर्चस्व’ और ‘सत्ता वर्चस्व’ की इन प्रवृत्तियों का प्रभाव समाज पर भी स्वाभाविक रूप से पड़ा। सामाजिक प्रभाव से उत्पन्न राजनीतिक द्वंद्व और दोलन को ऐतिहासिक संवेदनशीलता के साथ समझना जरूरी है। यह भारत के इतिहास का बहुत संवेदनशील और कातर प्रसंग है। हालांकि भारत में इस्लाम की उपस्थिति एकहरी नहीं थी, लेकिन भारत के लोगों में मुसलमान की स्मृति आक्रांता रूप ही जीवित रही। शक, हूण आदि विभिन्न आगंतुकों का भी प्रारंभिक रूप आक्रांताओं का ही था। उन्हें दूध-मिसरी की तरह घुलने-मिलने का वक्त मिला। ध्यान में होना चाहिए कि इस्लाम को भारत में दूध-मिसरी की तरह घुलने-मिलने का पर्याप्त वक्त नहीं मिला।
मुहम्मद साहब मूर्ति-पूजा के कट्टर विरोध को अरबों ने स्वीकार नहीं किया और उन लोगों ने मुहम्मद साहब पर आक्रमण कर दिया। नतीजतन, मुहम्मद साहब को मक्का शहर छोड़कर अन्यत्र भागना पड़ा, हिजरत करना पड़ा। इस्लाम में सर्वोच्च ईमान तौहीद है। तौहीद ईश्वर के अलावा किसी अन्य की पूजा को कुफ्र मानता है। कुफ्र का सब से बुरा रूप शिर्क है। शिर्क का सबसे बुरा रूप मूर्तिपूजा है। भारत में सभी तो नहीं, लेकिन बहुत बड़ी आबादी मूर्तिपूजक भी थी। यहां की मूर्तिपूजा पर उन लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले में अधिक तेजी और चुस्ती इसलिए भी आ गई कि मंदिरों में पर्याप्त धन भी जमा थे।
इस्लाम का एक रूप भारत के राजनीतिक रुझानवाले उच्च लोगों में था, जिन्हें इस्लाम के माननेवालों के शासक रूप ने लुभाया। एक रूप गैरबराबरी के शिकार ‘खटकर खानेवालों’ में था, जिन्हें इस्लाम के बराबरीवाले रूप ने तेजी से आकृष्ट किया। कहने की जरूरत नहीं है कि भारत में इस्लाम का स्वीकार और प्रसार सिर्फ तलवार के बल पर नहीं हुआ। हां, राजनीतिक कारण से सिर्फ तलवार की भूमिका को ही याद में बनाये रखने की कोशिश जरूर की जाती रही है।
हालांकि, 1857 तक आते-आते गंगा-जमुनी संस्कृति की आवश्यकता के अनुरूप हिंदू-मुसलमान के बीच समझदारी और एकता विकसित हो चुकी थी। इस समझदारी और एकता से अंग्रेज चकित थे। 1857 में जीत के बाद अंग्रेजों ने इस समझदारी और एकता को तोड़ने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रखा। ज्यों-ज्यों आजादी का आंदोलन का तेज होता गया देश में हिंदू-मुसलमान के बीच सांप्रदायिक दंगों का तूफान आता गया। मामला देश-विभाजन तक पहुंच गया। हिंदू-मुसलमान द्वेष और दंगा के चलते भारतीय संस्कृति की गंगा-जमुनी संस्कृति का बहुमूल्य अंश बहुत बुरे अर्थ में प्रभावित हुआ। अंततः महात्मा गांधी जैसे आजादी के आंदोलन और विचार के प्रकाश-स्तंभ की भी हत्या हो गई।
ऐसे कठिन दौर में भी, आजादी के आंदोलन के दौरान अर्जित मूल्यवान अनुभवों के कारण हमारे पुरखों ने बहुत ही धैर्य से पहले के जख्मों के हर निशान को भुलाकर अपने सपनों का सबूत संविधान में संजो दिया। शांति और सद्भाव के साथ बेहतर नागरिक जीवन की संभावनाओं का भव्य द्वार उन्होंने भारत के लोगों के लिए खोल दिया। यहां तक कि सामाजिक, आर्थिक और नागरिक गैरबराबरी को भी रक्तपात की आशंकाओं में फंसे बिना लोकतांत्रिक तरीके से दूर किये जाने का संवैधानिक प्रावधान किया। इस उम्मीद के साथ कि भारत गैरबराबरी के अपने सदियों पुराने रोग का इलाज बिना किसी कष्टकर चीर-फाड़ की ‘शल्य-क्रिया’ के कर लेने में कामयाब रहेगा।
लेकिन अब हो तो इस उम्मीद के विपरीत ही रहा है। ऐसे लोगों का राजनीतिक वर्चस्व बढ़ता चला गया है जिनके मन में बहुत कठिन घात-प्रतिघात के बीच पुरखों की अर्जित गंगा-जमुनी संस्कृति के भारत के अस्तित्व के साथ जुड़े होने का कोई बोध ही नहीं है। वे सूखे हुए जख्मों के निशान ढूंढ़ कर कुरेदते-कुरेदते खून निकाल देने पर बार-बार आमादा हो जाते हैं। योगी आदित्यनाथ खुद जिस नाथ-परंपरा से आते हैं, वह परंपरा भी इस गंगा-जमुनी संस्कृति के निर्माण की मार्मिक प्रक्रिया का ही प्रसंग है। पता नहीं उन्हें इस बात की कोई परवाह है भी, या बिल्कुल ही नहीं है!
रही नाम-पहचान की बात! भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोगों के माध्यम से एक सवाल बार-बार उछल रहा है कि नाम-पहचान छिपाने की क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए पड़ती है कि नाम-पहचान और निशान के आधार पर चुन-चुनकर निशाना बनाया जाता है। जो देश वोटर लिस्ट से नाम खोज-खोजकर जघन्य कांड किये जाने का साक्षी रहा हो उस देश में नाम-पहचान की संवेदनशीलता पर अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नाम-पहचान की सार्वजनिकता का उत्तम विचार ‘चुनावी चंदा’ बटोरने के समय भी सक्रिय रहा करे तो क्या कहने!
साफ-साफ समझने की जरूरत है कि पुराने मन से नई जिंदगी की समस्याओं का हल नहीं निकाला जा सकता है। भारत के लोगों को, खासकर युवाओं को शांति और सद्भाव के साथ बेहतर और सभ्य नागरिक जीवन का हक है। पचास साल पहले की इमरजेंसी और इसी तरह की अन्य राजनीतिक घटनाओं और कारनामों पर इतिहास को निर्णय लेने दिया जाये। वर्तमान को कोलाहल और कलह से भरने के लिए संसदीय राजनीति में माया-जाल न फैलाया जाये।
भारत अपनी गरीबी और दरिद्रता में भी खुश रह सकता है, बस इसके लोगों के हर तरह की गैरबराबरी से मुक्त होने और बराबरी से जीने के हक को सुनिश्चित किया जाये। कहने की जरूरत नहीं है कि बार-बार माया-जाल पसारने का बहुत बुरा असर मनुष्य के मन पर भी पड़ता है। क्योंकि माया-जाल का गहरा रिश्ता मनुष्य की किसी-न-किसी तरह की अन्य मानसिक जरूरत का भी हिस्सा है। क्या भारत के युवाओं को भयावह मनोरोग की तरफ ठेलने की राजनीतिक प्रक्रिया को रोकने में नागरिक समाज की कोई प्रभावी भूमिका नहीं है! है, निश्चित ही है।
नाम-पहचान और खान-पान की समस्या का समाधान सत्ताधारी दल की विचारधारा के राजनीतिक एजेंडा में नहीं है, भारत! नाम-पहचान और खान-पान की नकली समस्या को अपनी राजनीतिक पूंजी बनानेवाले इसे बनाये रखने में ही दिलचस्पी रखते हैं। गलत इरादों (Malafide Intentions) से किये गये अच्छे प्रयास भी बुरे परिणाम देते हैं। इरादा गलत, तो सब गलत! गलत इरादों के साथ तैयार राजनीतिक दुश्चक्र से भारत को बाहर निकलना ही होगा। भारत की नई जिंदगी के लिए नई राजनीतिक शैली की जरूरत है! नई राजनीतिक शैली की सुगबुगाहट की आवाज आनी शुरू तो हुई है। लेकिन इस नई राजनीतिक शैली के कारगर होने का अभी इंतजार ही है। भारत की जिंदगी को नई जीवन शैली, नई कार्य-शैली के प्रारंभ का इंतजार है। इंतजार भारत के युवाओं को है। इंतजार ठीक, बेसब्र इंतजार भी ठीक। यह भी ठीक है कि उन्हें वह भारत उत्तरजीविता में नहीं मिला जिस पर उनका हक था! तो अब क्या! अब यह कि जितना इंतजार युवाओं को अपने सपने के भारत को पाने का है, उतना ही इंतजार भारत को अपने कर्मठ युवा हाथों का है। इस समय तो भारत के सामने सपनों को, खुली आंखों से फिसलते जा रहे सपनों को, साबूत बचा लेने की चुनौती है।
प्रसंगवश, आंकड़े बताये जा रहे हैं कि आठ करोड़ लोगों को रोजी-रोजगार मिला! इतने पवित्र आंकड़े किस ग्रंथ से निकलते हैं, किस ग्रंथ से! यह इतना ही पवित्र और उत्साहवर्धक आंकड़ा है तो इस बात की छान-बीन करके बताना चाहिए कि रोजगार प्राप्त करनेवालों ने कितना कुल कितना आय अर्जित हुआ यह बताने की कृपा की जाये। यह भी कि उपार्जित आय का क्या हुआ? आठ करोड़ लोगों के उपार्जित आय का कोई योगदान न बचत में दिखता है, न खपत में दिखता है। खैर बड़े अर्थशास्त्रियों को जरूर दिखता होगा! बड़े अर्थशास्त्रियों के हाथ ही तो भविष्य है! साधारण आदमी को क्या पता! देखा जाये बजट कौन-सी कथा बांचता है!
(प्रफुल्ल कोलख्यान स्वतंत्र लेखक और टिप्पणीकार हैं)