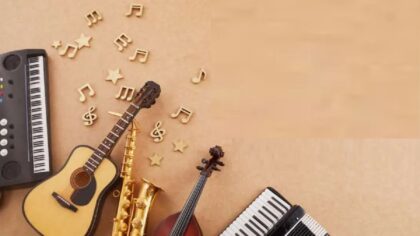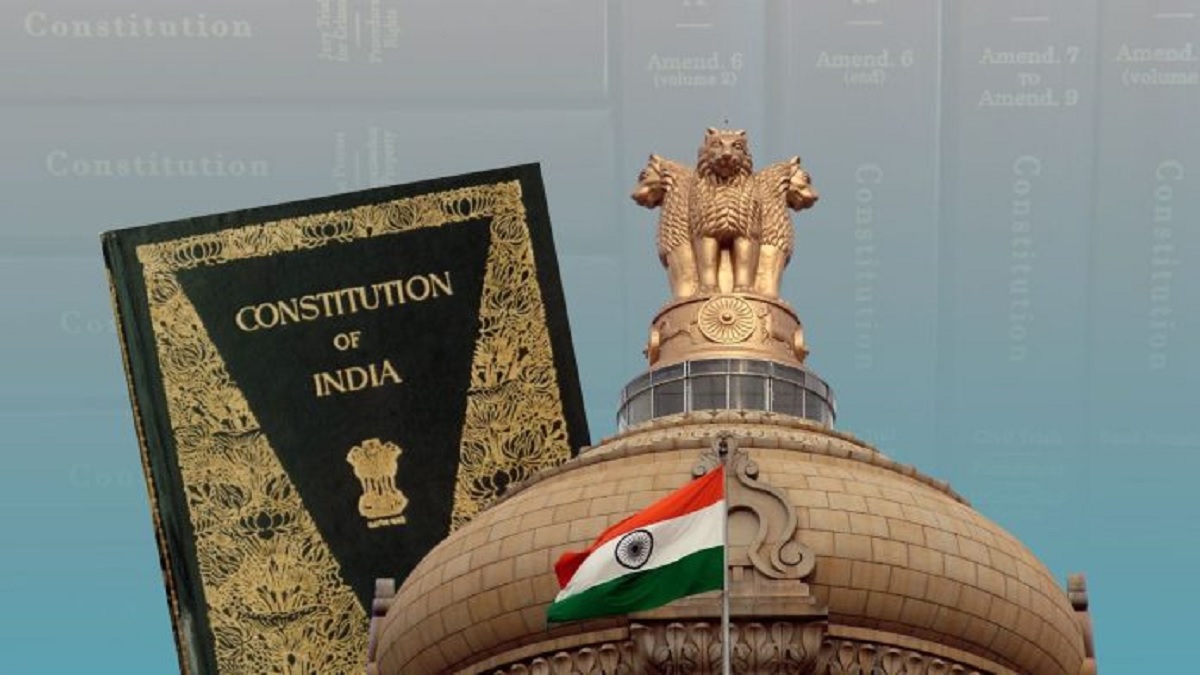यह लोकतंत्र में रस्साकशी का नया दौर है। लोकतंत्र की नई चमक के सामने कुछ देर के लिए ही सही, सत्ताधारी दल का छत्रभंग की स्थिति में पहुंच गई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का तेवर लोकसभा में इतिहास का नया अध्याय खोल रहा था, बहुत दिनों के बाद लगा प्रतिपक्ष बोल रहा है। तथ्य भी मुंह खोल रहा था और तेवर भी बोल रहा था। तथ्य और तेवर के ताल-मेल से कथ्य में पैदा हुई धार ला-जवाब बन गई। सत्ताधारी दल के लोगों के बीच नियमावली की तलाश तेज हो गई। आश्चर्यजनक भाव-भंगिमा के साथ लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो बोलते ही चले गये।
दस साल तक देश के लोगों की मनःस्थिति में ‘असंरक्षण’ का भाव-बोध बैठाने वाले नेता आज लोकसभा के स्पीकर से ‘संरक्षण’ की मांग दुहराते हुए संसदीय दयनीयता स्थिति में पहुंच गये। भारतीय जनता पार्टी की बढ़त और सत्ता पर वर्चस्व के बाद भारत के लोकतंत्र में यह लगभग ‘अ-संभव’ जैसी बन गई स्थिति, सदन के इतिहास की अटूट साक्षी बन गई। यह कम बड़ी बात नहीं है कि नियम-भंग के महारथी को नियम-पुस्तिका की जरूरत पड़ गई। ‘शरणागत’ बनानेवाले लोगों को ‘संरक्षण’ के पनाह में जाने का रास्ता पकड़ने पर मजबूर होना पड़ा। माननीय स्पीकर की भाव-भंगिमा से उन की परेशानी और लाचारी साफ-साफ झलक रही थी।
इसी तरह से राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका भी प्रभावशाली रही। कुल मिलाकर यह कि प्रतिपक्ष की टीम-भावना में गजब का ताल-मेल दिखा और सत्ता का व्यवहार पूरी तरह से अस्त-व्यस्त दिखा। ताल-मेल से ताम-झाम के बिखर जाने का यह याद रखने लायक दृश्य भारत की संसदीय कार्रवाई के इतिहास का हिस्सा बन गया। भारत के लोकतंत्र की संसदीय परिस्थिति में बदलाव लोक-मानस में दर्ज हो गया।
यह ठीक है कि परिवर्तन संसार का अ-परिवर्तनीय नियम है। ‘सब कुछ’ बदलता है, जन भी। जीवन भी। हर बदलाव अपने साथ बदली हुई परिस्थितियों में जरूरतों की नई सूची भी लाता है। परिवर्तन में एक तरह का जोखिम भी होता है। आम तौर पर प्राथमिकताओं और वरीयताओं के क्रमांकन में सामान्य से अ-सामान्य बदलाव से व्यक्ति और समुदाय के हित-साधन की प्रक्रियाओं में भी अंतर आता है। लाभ, अ-लाभ और हानि की नई स्थितियां बन सकती हैं, बल्कि बनती है। परिवर्तन में यथा-स्थिति के टूटने की भरपूर संभावना होती है। स्वाभाविक है कि परिवर्तन में एक तरफ आग्रह, उत्साह, उत्तेजना, उन्माद, आक्रमकता की कोई-न-कोई मात्रा जरूर होती है।
परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न होते ही मनुष्य के मन में डर और आकर्षण एक साथ सक्रिय हो जाता है, कभी-कभी अति-सक्रियता भी देखने में आती है। मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन-भीरुता भी कम नहीं होती है, ऐसे लोगों का आदर्श-वाक्य होता है, ‘जैसे इतना दिन कटा है, वैसे ही बाकी भी कट जाये तो अच्छा।’ जीवन की यह बुनियादी शिक्षा है कि दिन एक तरह से नहीं कटता है। परिवर्तन की प्रक्रिया में कुछ अच्छा भी होता है, कुछ अच्छा नहीं या बुरा भी होता है। दस साल पहले ‘अच्छे दिन’ लाने के आश्वासन के साथ एक बहुत प्रभावी राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हुई थी। अधिकतर लोगों के लिए ‘अच्छे दिन’ का आश्वासन छल ही साबित हुआ, वे ‘पुराने दिन’ के लौट आने के इंतजार में वक्त काट रहे हैं।
‘अच्छे दिन’ में कुछ अच्छा नहीं हुआ तो फिर ‘पुराने दिन’ ही सही। लोकतंत्र के ‘पुराने दिन’ और सत्ताधारी दल के ‘पुराने दिन’ के बावजूद-बोध में तत्त्वगत अंतर है। राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ और जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की वैचारिकी में ‘पुराने दिन’ के प्रति बड़ा मोह होता है। ‘पुराने दिन’ का मतलब वे दिन जब भारत ‘सोने की चिड़िया’ की हुआ करता था! ऐसा कब था? भारतीय जनता पार्टी के समर्थक समूह को दृढ़ विश्वास है ऐसा हुआ था और तब हुआ था जब ‘इस दुनिया’ में इस्लाम का आगमन नहीं हुआ था। जब भारत ‘ऋषि-मुनि-दार्शनिक’ के बीच विमर्श और शास्त्रार्थ हुआ करता था। समाज पर ईश्वर के प्रतिनिधि अवतारी राजाओं का ‘राजसूय यज्ञ’ निर्विघ्न चला करता था।
अर्थात भारत तब ‘सोने की चिड़िया’ था जब कुछ थोड़े लोग विमर्श और शास्त्रार्थ करते रहते थे, यथा-समय ‘राजसूय यज्ञ’ संपन्न होता रहता था। तब था जब, ढेर सारे लोग जीवन के लिए जरूरी उत्पादन के लिए कठोर श्रम के साथ सभ्यता के पन्ने पलटने में रात-दिन लगे रहते थे। विमर्श और शास्त्रार्थ करनेवालों ने इन कामों में लगे लोगों के जन्म ब्रह्मा के चार अंगों से होने के ‘ज्ञान’ से राजा को अवगत करवाते हुए तदनुसार अपनी बनाई वर्ण-व्यवस्था को देव-व्यवस्था बताकर उसके पालन का दायित्व भी राजा को सौंप दिया। ध्यान देने की बात है कि वर्ण-व्यवस्था के पालन का दायित्व राज को सौंपा समाज को नहीं।
ऐसी व्यवस्था जिस में हर किसी को पिछले जन्म में किये कर्म का फल मिले और वह उसी को पाकर संतुष्ट रहे। इसी जन्म में इस जन्म के कर्म के फल की कामना से सर्वथा मुक्त रहे! लक्ष्य यह कि ‘सोने की चिड़िया’ इधर-उधर न भटके बल्कि पिंजरे में सुरक्षित रहे! ‘कैद’ कहना सभ्यता के अनुकूल भाषा की मर्यादा का उल्लंघन है, इसलिए ‘सुरक्षित’ कहना ही अधिक उपयुक्त है! यह सब ठीक से चल रहा था, तभी सारी गड़बड़ी इसलाम के आगमन के कारण पैदा होने लगी।
अब कोई यह पूछे कि जब ‘सब कुछ’ ठीक ही था तो महाभारत क्यों हुआ? राम का रावण से युद्ध क्यों हुआ? धर्म-कथाओं और आख्याओं में उल्लिखित हजार-हजार षड़यंत्र कथाओं का क्या रहस्य है? रहस्य है, लीला! खैर। कुल मिलाकर यह कि ऐश्वर्यशाली ‘पुराने दिन’ का काल्पनिक वैभव हिंदुत्व की राजनीति को बहुत अच्छा और आकर्षक लगता रहा है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त ‘राजनीतिक और सांस्कृतिक समझ’ आम लोगों में विश्वास पैदा करने की कोशिश में लगी रहती है कि वे ‘पुराने दिन’ ही ‘अच्छे दिन’ थे, जो कहीं-न-कहीं खो गये! इस ‘पुराने दिन’ के खो जाने या लौटा नहीं पाने के लिए गांधी-नेहरु जिम्मेवार हैं! उन ‘पुराने दिन’ को फिर से हासिल किया जा सकता है। ‘पुराने दिन’ को हासिल करने के लिए जरूरी है कि ‘सेंगोल’ का कृपा-पात्र बनने के लिए भारत संसद, संविधान, लोकतंत्र मानवता और मानवाधिकार की पछाही बातों की ओछी मानसिकता से मुक्त होकर देवता और देवाधिकार जैसी श्रद्धा और आस्था के साथ उच्च कोटि के ‘आध्यात्मिक सशक्तिकरण’ की राह पकड़ ले!
‘पुराने दिन’ को ‘अच्छे दिन’ बताने और लौटाने के लिए संविधान में बदलाव की कोशिश जरूरी है। यह कोशिश संसद में राजनीतिक बहस के बिना भी, राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ जैसी सांस्कृतिक संस्थाओं की सांस्कृतिक समझ के प्रचार-प्रसार सफल हो सकती है। सवाल उठता है कि ‘सांस्कृतिक समझ’ के पवित्र प्रचार-प्रसार से ही संभव है तो फिर भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलाव की अ-पवित्र राजनीति में क्यों उलझती है? संविधान में बदलाव की अ-पवित्र राजनीति से उलझती इसलिए है कि संविधानवाद की राजनीति उस की सांस्कृतिक समझ के व्यापक प्रचार-प्रसार में बड़ी-बड़ी दुस्तर या अन-उत्तरणीय बाधाएं खड़ी करने में नितांत सक्षम है।
भारत का संविधान वैज्ञानिक मनोभाव की बात कहता है। संविधान के ‘वैज्ञानिक मनोभाव’ और राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ के ‘सांस्कृतिक मनोभाव’ में सीधा टकराव है। इसलिए संविधान की बात करनेवाले सभी के साथ भारतीय जनता पार्टी का सीधा टकराव है, फिर चाहे वे कोई साधारण आदमी हो, कोई विशिष्ट पदधारी व्यक्तित्व या संस्था ही क्यों न हो। जाहिर है कि संविधान से मुकाबला संविधान के माध्यम से करने में कठिनाई ही होती है, इसलिए गैर-संवैधानिक रास्ता अख्तियार करने में भी उसे कोई संकोच नहीं होता है।
कोलकाता उच्च न्यायालय के एक विद्वान जज अभिजीत गंगोपाध्याय सेवा में रहते हुए अपने लंबे समय से सत्ताधारी दल के संपर्क में रहने की बात का उल्लेख करते है। अपने पद से इस्तीफा देते हैं। सत्ताधारी दल में शामिल होते हैं। उनके कांग्रेस में शामिल होने से कैसा राजनीतिक कोहराम मचता उसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। खैर उन्हें टिकट मिलता है, वे सांसद बनने में लग जाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त जस्टिस एमआर शाह अपने सेवा काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुले प्रशंसक रहे हैं। उनके अनुसार अब वे ‘टाइगर शाह’ के नाम से संबोधित किये जाते हैं। उन्हें अपने वक्तव्य के लिए कोई पछतावा नहीं होता है। उन्हें क्या किसी को कोई पछतावा नहीं होता है। उदाहरण ढेर सारे मिल जायेंगे। गनीमत है तो बस इतनी कि जज साहेबान नेता और सांसद बन सकते हैं, लेकिन नेता या सांसद को सीधे-सीधे अब तक जज नहीं बनाया गया है। जो अब तक नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होगा, इस मुगालता के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। भयानक है सोचना कि रास्ता ही रास्ता छोड़ने की गुंजाइश देता है, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो या पैदल चलनेवालों का ‘जनपथ’ ही क्यों न हो! लोभ के महासागर के ज्वार-भाटा में ‘सब कुछ’ तिनके की तरह समा जाता है। और तिनका भी ऐसा कि किसी डूबते हुए के उबरने का झूठा सेहरा भी न बन सके! तो फिर संविधान में बदलाव का मतलब क्या होता है! मतलब तो साफ-साफ समझ में आ सकता है, नहीं क्या!
अपराध को केवल दंड-विधान के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता है। अपराध के कई कारण होते हैं और अपराधी बन जाने की कई परिस्थितियां होती हैं। अपराध और अपराधी के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करनेवाले के दावे चाहे जितने पवित्र हों उन से समाज का कभी भला नहीं हो सकता है, कभी नहीं! आज जीवन में हर तरह के अपराध का वर्चस्व खतरनाक हद तक बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कहना न होगा कि संविधान की रक्षा करनेवालों का संविधान की रक्षा के प्रति दायित्व-बोध या रक्षा के प्रति इरादा का बदल जाना संविधान में बदलाव से कम खतरनाक नहीं होता है!
एक बात तय है कि मतदाता सिर्फ ‘मतदान’ से अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता है। उसके चुने हुए प्रतिनिधि न तो इतने निष्कलुष हैं और न इतने विश्वसनीय हैं, शायद इतने सक्षम भी नहीं हैं कि उनके अकेले के भरोसे भारत के लोग केवल मतदान के माध्यम से संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व सौंपकर निश्चिंत हो सकें! तो फिर रास्ता क्या है? आम लोगों को न ‘अच्छे दिन’ का इंतजार है और न ‘पुराने दिन’ का। इंतजार है तो, बस ‘आनेवाले दिन’ का इंतजार है।
प्रतिकूल चुनावी परिस्थिति में विपक्षी गठबंधन (इंडिया अलायंस) जो कर सकता था किया, आम मतदाताओं ने भी अपनी भूमिका ठीक से ही निभाई। पक्ष-प्रतिपक्ष की संसदीय शक्ति की कार्रवाई तो संसद में हो रही है। ऐसा लगता है कि जानबूझकर सत्ताधारी दल भारत के लोकतंत्र में संसद की भूमिका को ही सीमित करने की फिराक में लग सकती है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रति दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों का रुख उनके प्रति अंततः निष्पक्ष रहेगा ऐसा नहीं लगता है।
पद और शक्ति का कोई भी अहंकार लोकतंत्र के प्रतिकूल ही पड़ता है। संसदीय व्यवस्था में लगातार क्षरण न रुक पाया तो अंततः रण की ही हवा बनने लगेगा। ऐसे में सड़क पर ही भीषण रण होगा। जल-जमीन-जंगल के अधिकार बचाने के लिए रण होगा, संसद में हो तो बेहतर नहीं तो सड़क पर होगा, मगर होगा जरूर। जो भी हो उम्मीद की पतली-सी किरण अब सड़क की तरफ से भी आ रही है। ऐसे में भूखे पेट सोकर ‘सपनों का मजा’ लेने से बेहतर विषमताकारी दीवार के पार नजर दौड़ाकर उभर रही नई सड़क का जायजा लेने का ही रास्ता बचता है। यह ठीक है कि गंगा-जमुनी संस्कृति का जल हमेशा शीतल ही नहीं रहा है, लेकिन लगातार इतना खौलता भी नहीं रहा है।
सत्ता-पक्ष की बौखलाहट का तुमुल कोलाहल लोकतंत्र में शुभ का लक्षण नहीं हो सकता है। जी हां, भारत के आम लोगों को न ‘अच्छे दिन’ का इंतजार है, न ‘पुराने दिन’ का, बस आनेवाले दिन का इंतजार है। पीछे लौटने की कोई बात भी न करे, बस बढ़ते ही चलना है कि मंजिल अभी नहीं आई!
(प्रफुल्ल कोलख्यान स्वतंत्र लेखक और टिप्पणीकार हैं)