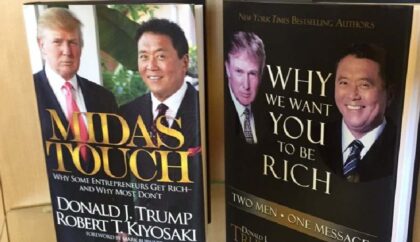दक्षिण भारत इन दिनों दो मुद्दों पर बहुत मुखर है और संसद में गोलबंद हो रहा है। इनमें एक मुद्दा है भाषा यानी तीन भाषा का फ़ार्मूला और दूसरा है परिसीमन का विवाद।
और इसके पीछे वही धारणा है कि उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। भारतीय राजनीति में उसका प्रभाव कम करने की कोशिश है। और इसके कुछ पुख़्ता कारण भी हैं। हम इन्हें बारी-बारी से समझेंगे।
भाषा विवाद
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के तहत हिंदी लागू करना चाहती है। और दक्षिण भारत को लगता है कि यह सीधे तौर पर उनके ऊपर हिंंदी थोपने का मामला है। यही वजह है कि तमिलनाडु और कर्नाटक इस मुद्दे पर मुखर हैं। और संसद में हंगामा है।
आप जानते हैं कि NEP-2020 पहले से ही विवादित है और छात्र संगठनों ने इसका तीखा विरोध किया है, इसी के तहत सरकार तीन भाषा का फ़ार्मूला लाई है। जिसमें हिंदी को लागू करने का सुझाव है।
हालांकि भारत सरकार ने 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही “तीन-भाषा फ़ार्मूला” अपनाया था। इसका उद्देश्य भाषाई संतुलन और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना था। जो कभी नहीं हुआ।
लगभग वही फ़ार्मूला NEP-2020 के तहत है। इसके अनुसार प्रत्येक छात्र को कम से कम तीन भाषाएं सीखनी होती हैं। ये तीन भाषाएं इस प्रकार हैं–
- मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा:
प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होना चाहिए।
यह छात्रों को सहज और प्रभावी रूप से सीखने में मदद करता है।
- हिंदी या कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा:
हिंदी भाषी राज्यों में, हिंदी के अलावा एक दक्षिण भारतीय भाषा (जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम) को पढ़ने पर ज़ोर है।
गैर-हिंदी भाषी राज्यों में, हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में अपनाने का सुझाव है।
- अंग्रेज़ी या कोई अन्य विदेशी भाषा:
अंग्रेज़ी को आमतौर पर तीसरी भाषा के रूप में अपनाया जाता है। कुछ राज्यों में संस्कृत या अन्य शास्त्रीय भाषाएं भी तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जा सकती हैं।
इसी फ़ार्मूले के तहत अब हिंदी को लगभग अनिवार्य करने की कोशिश है और यही दक्षिण भारत के राज्यों की आपत्ति है, क्योंकि हिंदी राज्यों में कभी भी दक्षिण भारत की किसी भाषा को महत्व नहीं दिया।
आपने कब तमिल, तेलुगू को अपनाया जो वे हिंदी को अपनाएंगे?
भाषा का विवाद काफ़ी पुराना है लेकिन स्थिति नहीं बदली है। शायद ही कोई हिंदी भाषी राज्य हो जहां दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर तमिल, तेलुगू, मलयालम या कन्नड़ पढ़ाई जाती हो। यही रवैया बांग्ला और मराठी भाषा को लेकर भी है।
दिल्ली के कुछ केंद्रीय विद्यालयों में इसका विकल्प है लेकिन वो भी बहुत सीमित। और वो भी इसलिए क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है।
हिंदी भाषी राज्यों ने बड़ी चालाकी से हिंदी, अंग्रेज़ी के अलावा तीसरी भाषा के तौर पर संस्कृत को तवज्जो दी। कहीं कहीं संस्कृत के साथ उर्दू का भी विकल्प है। लेकिन अब आमतौर पर संस्कृत ही सभी भाजपा सरकारों की प्राथमिकता में है।
संसद में हंगामा
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार 10 मार्च से शुरू हो गया है। यह 4 अप्रैल तक चलेगा। लेकिन इसके शुरू होते ही पहले दिन वोटर लिस्ट और नई शिक्षा नीति के तहत तीन भाषा फ़ार्मूले को लेकर हंगामा हो गया और लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।
विपक्ष ख़ासतौर पर डीएमके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर ज़ोरदार आपत्ति की है। धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके पर आरोप लगाया कि वे तमिलनाडु के छात्रों के भविष्य के साथ राजनीति कर रहे हैं। प्रधान ने डीएमके को ‘अलोकतांत्रिक’ और ‘असभ्य’ कहा, जिस पर डीएमके सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई। हंगामा बढ़ने पर उन्हें अपने शब्द वापस लेने पड़े।
तमिलनाडु की डीएमके सरकार के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का मानना है कि यह राज्य की भाषाई स्वायत्तता का उल्लंघन है। राज्य सरकार का तर्क है कि हिंदी को अनिवार्य बनाने से तमिल भाषा और संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वे मानते हैं कि यह क़दम भाषाई विविधता के ख़िलाफ़ है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी कन्नड़ भाषा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है और हिंदी को अनिवार्य बनाने के किसी भी प्रयास का विरोध किया है।
परिसीमन (Delimitation) विवाद
भारत में परिसीमन (Delimitation) वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है, ताकि जनसंख्या में हुए परिवर्तनों के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। यह प्रक्रिया जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होती है।
वर्तमान में, परिसीमन को लेकर विवाद इस बात पर है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण कैसे किया जाएगा। दक्षिणी राज्यों, विशेष रूप से तमिलनाडु, ने जनसंख्या नियंत्रण में सफल प्रयास किए हैं, जिससे उनकी जनसंख्या वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम रही है। उन्हें आशंका है कि यदि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण होता है, तो उनकी लोकसभा सीटों की संख्या कम हो सकती है, जिससे उनके राजनीतिक प्रभाव में कमी आ सकती है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है और अन्य राज्यों से समर्थन मांगते हुए कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है और इसे संसद में उठाने की योजना बनाई।
इस विवाद के बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि परिसीमन प्रक्रिया आनुपातिक आधार पर की जाएगी, जिससे सभी राज्यों के साथ न्याय हो सके। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया है कि किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा।
लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि जब आबादी का अनुपात सीट निर्धारण का आधार होगा तो फिर दक्षिण के राज्यों के साथ न्याय कैसे होगा।
परिसीमन का आधार
संविधान में प्रावधान किया गया है कि हर परिसीमन के लिए जनगणना के बाद नए आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा।
भारत में परिसीमन की यह परंपरा 1951 की पहली जनगणना से शुरू हुई, जब संविधान के तहत पहली बार परिसीमन आयोग गठित किया गया था.
आखिरी परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ था, और इसके बाद सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। उस समय भारत की आबादी क़रीब 102 करोड़ थी।
चौथा परिसीमन आयोग 2002 में गठित हुआ और इसकी सिफारिशें 2008 में लागू की गईं। जिसके अनुसार अगला परिसीमन 2026 में होना है। यह नई जनगणना के आधार पर होना था।
भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है। लेकिन आख़िरी जनगणना 2011 में हुई थी। अगली जनगणना 2021 में होनी थी जो अब तक शुरू नहीं हुई।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी क़रीब 121 करोड़ है। जबकि 2023-24 के अनुमान के अनुसार इस समय कुल जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है।
अगर इस आधार पर सीटों का पुनर्वितरण किया जाता है तो दक्षिण के राज्य सबसे ज़्यादा नुकसान में रहेंगे।
दक्षिण भारत के राज्य, जहां प्रजनन दर कम है, सीटों की घटने की आशंका जता रहे हैं, जबकि उत्तर भारत में सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना है।
भारत में इस समय कुल 543 लोकसभा सीटें हैं। यानी हर संसदीय सीट लगभग 18 से 20 लाख की आबादी कवर करती है।
आगामी परिसीमन को लेकर सरकार ने अभी तक स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया है कि प्रति संसदीय सीट आबादी का अनुपात क्या होगा।
लेकिन भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, इसलिए प्रति सीट औसत आबादी बढ़ सकती है।
यदि सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, तो प्रति सीट आबादी का औसत बढ़ जाएगा।
यदि सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है तो प्रति सीट आबादी का अनुपात वर्तमान के करीब या थोड़ा अधिक रह सकता है।
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि लोकसभा सीटों की संख्या को 750 या 800 तक बढ़ाया जा सकता है, ताकि प्रति सीट औसत आबादी करीब 18-20 लाख बनी रहे। शायद यही वजह है कि नई संसद की लोकसभा में 800 से ज़्यादा सदस्यों के बैठने की व्यवस्था बनाई गई है।
लेकिन इन दोनों स्थितियों में दक्षिण भारत का नुक़सान होगा।
अगर 543 ही सीटें रहती हैं तो हर सीट पर आबादी का अनुपात बढ़ जाएगा, तब दक्षिण के राज्यों की सीटों की संख्या जनसंख्या स्थिर रहने की वजह से पहले से भी घट जाएंगी।
और अगर इसी आबादी के अनुपात में सीटें बढ़ाई जाती हैं तो दक्षिण के राज्यों की सीटों की संख्या स्थिर रहेगी और उत्तर भारत की सीटें बढ़ जाएंगी। जो पहले से ही दक्षिण भारत से बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह भी दक्षिण की सीटें घट जाएंगी।
इस समय उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों में लोकसभा सीटों की कुल संख्या: 228 है
जबकि दक्षिण भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मिलाकर लोकसभा सीटों की कुल संख्या: 130 है।
अकेले उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और इसकी वजह जनसंख्या ही है। यूपी जनसंख्या में देश में पहले नंबर पर है। प्रजनन दर भी यहां वर्तमान में भी राष्ट्रीय औसत से ऊपर है।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) 2019-21 के अनुसार यूपी में प्रति महिला प्रजनन दर (Total Fertility Rate – TFR) 2.4 है।
इसी तरह बिहार भी जनसंख्या के मामले में टॉप 3 राज्यों में है। यहां 40 सीटें हैं और यहां की प्रजनन दर देश में सबसे ज़्यादा 3.0 है।
इस तरह देखें तो उत्तर भारत की औसत प्रजनन दर– 2.08 है। जो भारत की कुल प्रजनन दर प्रति महिला 2.0 बच्चे से ज़्यादा है।
जबकि दक्षिण भारत ने जनसंख्या नियंत्रण के सफल प्रयास किए जिसकी वजह से दक्षिण के राज्यों की औसत प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से भी नीचे 1.76 है।
जनसंख्या के आधार पर नए परिसीमन से यह असंतुलन और बढ़ जाएगा। यही वजह है कि दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या बढ़ाने की भी बातें उठी हैं।
इसलिए चाहे वो तीन भाषा फ़ार्मूला हो, जनसंख्या का मुद्दा हो या परिसीमन का मुद्दा दक्षिण भारत की चिंंताओं को दूर करना केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी है। वरना उत्तर–दक्षिण का ये बंटवारा बढ़ता चला जाएगा।
बीजेपी की राजनीति
लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार उत्तर-दक्षिण की इस दूरी को पाटना चाहती है?
फ़िलहाल तो नहीं लगता क्योंकि उसकी पूरी राजनीति उत्तर भारत और “हिंदी-हिंदू-हिंदुस्थान” को केंद्र में रखकर चलती है और तमाम कोशिशों के बाद भी उसे दक्षिण में एंट्री नहीं मिली है। पहले एक कर्नाटक राज्य बीजेपी के कब्ज़े में था, लेकिन 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में वो भी उसके हाथ से चला गया। वहां कांग्रेस की जीत हुई और दक्षिण में प्रवेश का द्वार भी उसके लिए बंद हो गया। हां इस बार कहा जा सकता है कि एनडीए के घटक टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश की सरकार में आए हैं। लेकिन बीजेपी के लिए अभी कोई वैकेंसी नहीं है।
इसे देखकर लगता है कि बीजेपी हिंदी और हिंदुत्व के आधार पर क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने और परिसीमन के आधार पर संसद में दक्षिण का प्रभाव और कम करने की नीति पर काम कर रही है!
इसलिए आने वाले दिनों में यह तकरार, यह विवाद और बढ़ेगा, क्योंकि दक्षिण के महत्वपूर्ण राज्य तमिलनाडु में अगले साल 2026 में चुनाव हैं और बीजेपी अपने लिए संभावना तलाश रही है। हालांकि अभी भी ब्राह्मणवादी हिंदुत्व की राजनीति के आगे द्रविड़ अस्मिता की राजनीति भारी है। यही वजह है कि बीजेपी तमिलनाडु में भी किसी का कंधा तलाश रही है, लेकिन भाषा और परिसीमन के मुद्दे पर तमिलनाडु समेत लगभग पूरे दक्षिण भारत के राज्य फ़िलहाल एकजुट दिखाई दे रहे हैं।
(मुकुल सरल पत्रकार हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)