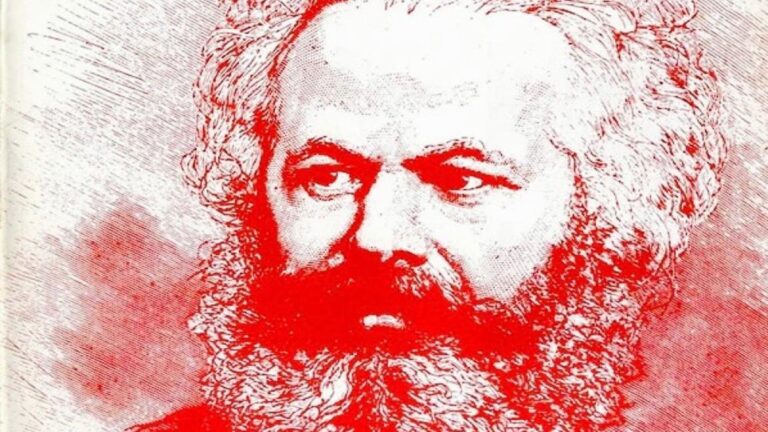चंद्रशेखर आजाद रावण को एक दलित नेता की तरह ही देखा जाता है। इस लोकसभा चुनाव में जब बसपा को, खासकर उत्तर-प्रदेश में एक भी सीट हासिल नहीं हुई, तब एकबारगी सबकी नजर चंद्रशेखर आजाद ‘रावण’ की भारी बहुमत से हुई जीत की ओर गई। आजाद ने उत्तर प्रदेश की नगीना सीट पर 51.19 प्रतिशत वोट हासिल किया। जबकि वहां बसपा को महज 1.33 प्रतिशत वोट ही मिल सका। आजाद ने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा के ओमप्रकाश को डेढ़ लाख से अधिक वोटों से हराया। यहां सपा को 10.22 प्रतिशत वोट मिला।
2019 की लोकसभा के चुनाव के समय में बसपा के गिरीश चंद्र ने भाजपा के यशवंत सिंह को 1.66 लाख वोटों से हराया था। इस बार बसपा की जगह चंद्रशेखर आजाद ‘रावण’ ने लिया और पिछले के मुकाबले थोड़े कम वोट के अंतर पर भाजपा के उम्मीदवार को हरा दिया। इस बार बसपा की जगह आजाद समाज पार्टी के नेता आजाद की इस जीत के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। मुख्य निष्कर्ष तो यही हैः क्या आजाद समाज पार्टी बसपा की जगह ले रही है? क्या चंद्रशेखर आजाद मायावती की जगह ले रहे हैं?
सड़क पर नीला सैलाब
2021 में जब टाइम पत्रिका ने 100 उभरते हुए नेताओं में चंद्रशेखर को जगह दिया तब भारतीय राजनीति में उनकी उपस्थिति को नकार सकना संभव नहीं था। दलित युवाओं के मुखर नेता बनकर उभरे आजाद ने जब दिल्ली में पहली रैली की और तब जंतर-मंतर पर नीला सैलाब उमड़ पड़ा था। वह तनी हुई मूंछों के साथ प्रतिरोध की एक नई इबारत पेश कर रहे थे। वह पेरियार के स्वाभिमान आंदोलन को लगभग 100 साल बाद एक नई शक्ल देने के लिए युवाओं को एक मॉडल दे रहे थे। सफेद पैंट शर्ट पर नीला गमछा और नीला झंडा भारत में 1950 के बाद के दलित आंदोलन का रंग बन चुका है। आजाद ने जब भीम आर्मी का निर्माण किया तब उन्होंने इन्हीं रंगों को अंगीकार किया।
चंद्रशेखर की पढ़ाई देहरादून में हुई थी। उनके पिता वहां स्कूल में अध्यापक थे। यहीं से उन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरा की। उन्होंने छात्र जीवन के शुरूआती दिनों में बसपा की राजनीति नहीं की। वह भाजपा से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य रहे। वहां उन्होंने इस संगठन की मुस्लिम विरोध में सक्रियता को देखा लेकिन दलित समुदाय को लेकर उनकी चुप्पी ने आजाद को इसकी राजनीति से दूर कर दिया। वह दलित समुदाय पर हो रहे उत्पीड़न से बेचैन थे। वह बसपा की अच्छाई और उसकी सीमा को भी परख रहे थे। अंततः 2013 में ‘कुछ कर गुजरने के लिए’ सहारनपुर लौट आये।
उत्तर प्रदेश में इस समय तक भाजपा का उभार तेजी के साथ हो रहा था। इसकी राजनीति अपने सामाजिक और आर्थिक आधार के बल पर एक आक्रामक रुख अपना रही थी। मुस्लिम समुदाय को दलित समुदाय से अलग कर उसके खिलाफ हिंसक ध्रुवीकरण मूलत: बसपा के सामाजिक आधार को ही खत्म करने की ओर ले जा रही थी। इस हिंसक ध्रुवीकरण की राजनीति ने दलित समुदाय पर संगठित हमलों में बढ़ोत्तरी किया। यह हमला दलित और ओबीसी दोनों ही समुदाय के खिलाफ किया गया। खासकर, योगी सरकार बनने के साथ ‘कानून व्यवस्था’ को दुरूस्त करने के नाम एनकाउंटर की बाढ़ आ गई।
इन्हीं राजनीतिक परिस्थितियों में चंद्रशेखर आजाद जब गांवों में साईकिल यात्रा करते हुए युवाओं को आगे आने का आह्वान किया तब उन्हें पुरजोर समर्थन मिला। जब उन्होंने गरकोली गांव के बाहर स्वागत द्वार पर ‘द ग्रेट चमार डा. भीमराव आंबेडकर ग्राम गरकोली वेलकम यू’ का बोर्ड लगाया तब उस इलाके में तहलका मच गया था। आजाद को सामाजिक समर्थन की पुख्ता जमीन तैयार होनी शुरू हो गई थी।
बसपा और सपा की भाजपा के दौर में खतरनाक चुप्पी के बीच आजाद की उठती हुई आवाज दलित युवाओं को आकर्षित कर रही थी और सीमित ही सही, मुलसमान समुदाय में एक उम्मीद जगा रही थी। 2017 में सहारनपुर में कथित तौर पर करणी सेना के हमलों का प्रतिरोध करने में हुई हिंसा का दोषी आजाद को बनाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 2018 में उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धाराएं लगा दी गईं। इस दौरान उन्हें शारीरिक और मानसिक यातना से गुजरना पड़ा। लेकिन, अब वह राष्ट्रीय राजनीति में बहस का एक विषय बन चुके थे। मायावती के नेतृत्व और बसपा की राजनीति को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे थे।
इसके बाद वह सीएए और एनआरसी को लेकर हुए आंदोलन, खासकर दिल्ली में चल रहे आंदोलन में शिरकत कर उन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी स्पष्ट पक्षधरता को सामने रख दिया। वह जब दिल्ली में जामा मस्जिद पर हुई विशाल जुटान के बीच एक नेता के तौर पर प्रकट हुए, तब जो दृश्य बना था वह बहुत समय तक खबर में सनसनी पैदा करता रहा। वह ऊर्जा और साहस से भरे एक युवा नेता की तरह उभरकर सामने आ रहे थे। उन्होंने दिल्ली में ही भीमा कोरेगांव केस में गिरफ्तार लोगों की रिहाई के लिए आयोजित कार्यक्रम में हिस्सेदारी कर साफ कर दिया कि उनकी राजनीति सिर्फ पहचान तक सीमित नहीं है। वह दलित आंदोलन को बहुजन की गणित से निकालकर प्रतिरोध की राजनीति में बदल देने वाले युवा नेता की तरह उभर रहे थे।
जून, 2023 में उन पर सहारनपुर के छुटमलपुर जाते समय जानलेवा हमला किया गया। इस हमले से पहले ही उन्हें जान से मारने की कई धमकियां खुले और छुपे तौर पर मिल चुकी थी। मूलतः यह हमला हिंसक राजनीतिक ध्रुवीकरण की वर्चस्ववादी सामाजिक ध्रुवीकरण का परिणाम थी जो खुद को राष्ट्रवाद के आवरण में पेश कर रहा था। आजाद इसी राजनीति के मुखर विरोधी बनकर उभरे।
आजाद समाज पार्टी (कांशीराम)
यदि आप विकिपीडिया के पेज पर जाएं तब वहां आजाद समाज पार्टी को बसपा से अलग होकर बनी पार्टी की तरह दिखाया गया है। जबकि सच्चाई इसके आस-पास भी नहीं है। यह सच है कि पिछले 15 सालों में बसपा की आलोचना में तेजी दिखाई दी है, और यह आलोचना पार्टी के भीतर और बाहर दोनों तरफ से हो रही है। पार्टी के अंदर की आलोचना में मुख्य जोर मायावती की कार्यपद्धति और उनके व्यक्तिगत व्यवहार को लेकर है। बाहर की आलोचना में एक पक्ष दलित राजनीति में गुणात्मक बदलाव की मांग करता है जबकि दूसरी आलोचना बसपा और कांशीराम की मूल राजनीति पर ही आक्षेप करता है। इस दूसरी आलोचना में ‘पहचान’ की राजनीति के खत्म होने की सैद्धांतिकी और अनुमान का जोर ज्यादा है।
आजाद समाज पार्टी की स्थापना 2020 के मार्च में उस समय हुई है जब बसपा का संसदीय राजनीति में उतार हर तरफ दिखना शुरू हो चुका है। चंद्रशेखर इस पार्टी को बसपा के प्रतिद्वंदी के तौर पर नहीं, बल्कि बसपा की ही राजनीति के पूरक के तौर पर पेश करते हैं। वह बार बार दोहराते हैं कि मान्यवर कांशीराम जी हमारी विचारधारा हैं और मायावती हमारी नेता हैं। हालांकि सैद्धांतिक तौर पर एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी का नेता नहीं हो सकता। दलित राजनीति में ‘व्यवहारवाद’ का यह रूप राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उभर रही नई पार्टी और संगठनों में दिखाई दे रहा है।
चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी को सिर्फ दलित राजनीति तक सीमित रखने के घोर विरोधी हैं। उनका मानना है कि मीडिया ने जानबूझकर दलित आंदोलन को सीमित करके पेश किया। बसपा कभी भी सिर्फ ‘दलित’ की राजनीति नहीं की। बाबा साहेब आंबेडकर भी सिर्फ ‘दलित राजनीति’ की बात नहीं करते। उनके अनुसार पिछले ढाई हजार साल से हम प्रतिरोध की धारा देख रहे हैं। यही प्रतिरोध की धारा हम तक आई है। हम उसका हिस्सा हैं। यह पूरे समाज की मुक्ति की लड़ाई है। (देखेंः द प्रिंट की सान्या ढींगरा और न्यूजलांड्री पर अवधेश कुमार के साथ लिया गया साक्षात्कार)।
आजाद की जीत बसपा की हार नहीं है
चंद्रशेखर आजाद इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं कि उनकी जीत बसपा के हार की शुरूआत है। वह इस बात का भी विरोध करते हैं बसपा भाजपा की ‘बी’ पार्टी है। लेकिन, जब उनसे यह पूछा जाता है कि बसपा के पतन का कारण क्या है तब वह साफ कहते हैं कि वह बसपा के सदस्य नहीं हैं। इस मसले पर वही लोग बोल सकते हैं। यह एक राजनीतिक रणनीति हो सकती है जिससे मायावती के साथ किसी भी टकराहट से बचा जाये। दोनों की राजनीतिक सक्रियता पश्चिमी उत्तर-प्रदेश है। लेकिन, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के इलाकों में काम करने वाली अंबेडकरवाद जन मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी, दोनों की नीति भी यही है। दरअसल वे इस सच्चाई से नहीं मुकरना चाहते कि बसपा ने ही दलित और बहुजन की राजनीति को सामने लाकर समाज के सबसे दमित समुदाय में ‘राजनीतिक चेतना’ को पैदा किया।
नई पार्टियों का उभार इस ‘राजनीतिक चेतना’ को एक नई जमीन देने के उद्देश्य से हुआ है। इस संदर्भ में उनके द्वारा बसपा का स्वीकरण आश्चर्य पैदा नहीं करता है। यह नई दिशा की तलाश में जाने के लिए पुरानी जमीन को न छोड़ने का ही आग्रह है। आजाद के वक्तव्य इन्हीं संदर्भों में हैं। उनके द्वारा विभिन्न जनआंदोलनों में हिस्सेदारी करना और विभिन्न पार्टियों के साथ अपनी शर्तों पर गठजोड़ बनाने का प्रयास पुरानी राजनीतिक जमीन से नये की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति में दिख रहा है। इसी वजह से जो लोग उन्हें दलित राजनीति के चश्में से देख रहे हैं, आजाद की बातों में एक उलझाव भी देख रहे हैं। वे लोग आजाद को बसपा की रणनीति के संदर्भ में व्याख्यायित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वह बसपा से आगे जाने और नये तरह की रणनीति की बात कर रहे हैं, वह इतिहास को भी नये सिरे से देख रहे हैं।
यदि हम आंकड़ों में देखें, तब बसपा का वोट नगीना सीट पर आजाद की ओर जाता दिखता है। पूर्वांचल में यह सपा की ओर गया है। इससे सपा को 12 सीटों का फायदा हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर सपा और राष्ट्रीय लोकदल को फायदा पहुंचा। जिन 13 सीटों पर बसपा ने अंत समय में अपने उम्मीदवार बदले उसमें से 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल किया। लेकिन, यह भी सच है कि वोट के इस बंटवारों से भाजपा ने भी कई सीटों पर आसान जीत हासिल किया। कई अखबारों ने बसपा को भाजपा की हारी सीटों के लिए जिम्मेदार ठहराया। 2014 के मुकाबले उत्तर प्रदेश में बसपा का वोट प्रतिशत 2019 में 19.77 से 19.42 प्रतिशत पर आया था। इस बार यह 9.32 प्रतिशत पर आ गया। इस दस प्रतिशत वोट गिरावट की दिशा फिलहाल भाजपा की ओर जाते हुए नहीं दिखता है। इस संदर्भ में, आजाद का यह कहना ठीक ही है कि बसपा भाजपा की ‘बी’ पार्टी नहीं है।
दरअसल, आजाद बसपा की राजनीति के उतार को उसके सांगठनिक संदर्भों में ही देखते हैं और इस संदर्भ में वह कोई बयान नहीं देना चाहते हैं। नई पार्टी का गठन कर उन्होंने अपनी आलोचना पेश कर दिया है। बसपा अपनी सांगठनिक संरचना में और आगे जाने की स्थिति में नहीं है। इस बात को राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में नये दलित आंदोलनों के उभार में देखा जा सकता है।
बसपा का पतन हो चुका है, यह कथन सच्चाई से दूर है। बसपा की राजनीति और सांगठनिक संरचना संसदीय राजनीति से हो रहे सामाजिक ध्रुवीकरण के संदर्भ में प्रासंगिकता खो रहा है। योगी और मोदी के उभार के पहले बसपा ने सामाजिक ध्रुवीकरण में जिस ब्राह्मण कार्ड को खेला उसके केंद्र में हिंदुत्व की राजनीति ही थी। जैसे-जैसे इसने अपनी जमीन को हिंदुत्व की संरचना से ठोस बनाया और मुस्लिम समुदाय के बहिष्करण को मुकम्मल किया वैसे ही बसपा की ‘ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी आगे बढ़ता जाएगा’ की रणनीति ध्वस्त हो गई। वैसे भी बसपा न तो अपने वोट प्रतिशत में और न ही अपनी सीट के बदौलत बहुमत का कभी भी प्रतिनिधित्व कर सकी। वह एक मजबूत वोट बैंक की तरह थी जिसकी पक्षधरता जीत को काफी हद तक सुनिश्चित करती थी।
बसपा इन्हीं संदर्भों में सत्ता के लिए गठजोड़ की राजनीति में बनी रही। इसकी राजनीति का मुख्य स्वर यही बना रहा। और, इन्हीं कारणों से उसके ऊपर ‘अवसरवाद’ का एक बड़ा सा ठप्पा भी लग गया। बहुमत के दौर में बसपा अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। संसदीय राजनीति में बसपा नेतृत्व के संकट से भी गुजर रही है। जबकि बहुत तेजी से राजनीति एक नया तेवर ले रही है। इस बार बसपा और मायावती का किसी गठबंधन में न जाना उसके वोटरों को रास नहीं आया। उसने पक्ष लिया। हालांकि कुल पक्ष लेने वाले उसके कुल वोटरों का लगभग आधा ही है। अब भी वह बसपा के साथ है। यही कारण है कि आजाद और अन्य उभरते युवा नेता बसपा को भाजपा के साथ जोड़कर नहीं देखते और मायावती को अब भी एक नेता की तरह देखते हैं।
प्रतिरोध ही संघर्ष है
चंद्रशेखर आजाद के साथ पुलिस ने जिस तरह की बर्बरता की और उनके खिलाफ जिस तरह के राजनीतिक बयान दिये गये, खासकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा और जिस तरह के उनके ऊपर केस लगाये गये वह किसी भी उभरते दलित नेता के खिलाफ नहीं लगाये गये। उनके साथ एक अपराधी की तरह व्यवहार किया गया। लेकिन, उन्होंने जिस प्रतिरोध का रास्ता चुना था, उसे उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित फिल्म ‘आर्टिकल 15’ 2019 में आई थी। उस फिल्म का एक किरदार आजाद के साथ मेल खाता हुआ दिखा। बदायूं में हुई एक घटना को केंद्र में बनाई गई इस फिल्म में शुरूआत एक ‘हिंसा’ को प्रदर्शित करने वाली घटना से होता है। इस दृश्य में हिंसा एक प्रतीकात्मक तौर पर आता है लेकिन वार्ता में यही हिंसा आगामी दिनों में दावानल बन जाने का अहसास भी कराती है। फिल्म में इसी की नौबत आती है।
आजाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधान सभा चुनावों में अपने प्रत्याशी उतारते हैं। वह नई उभरती आदिवासी और दलित समुदाय आधार वाली पार्टियों और जन पक्षधर राजनीति करने वालों के साथ गठजोड़ करने का रास्ता बनाते हैं। वह बड़ी पार्टियों के पास तो जाते हैं लेकिन उनके साथ वह अपनी शर्तों के आधार पर गठजोड़ का प्रस्ताव देते हैं। शर्तें नहीं पूरा होने पर साफ तौर पर उनसे अलग हो जाते हैं। वह संसदीय राजनीति में एक रास्ता तलाशते हुए अपनी राजनीति को आगे ले जा रहे हैं।
इस बार जब लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में जब दूसरी यात्रा के नाम में ‘न्याय’ शब्द जोड़ा और इसे आरक्षण का संदर्भ देते हुए सामाजिक न्याय से जोड़ दिया तब सिर्फ भाजपा के लिए ही मुश्किल खड़ा नहीं किया। इसने कांग्रेस नेतृत्व के गठजोड़ को भी एक ठोस आधार दे दिया। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में राहुल गांधी हाथ में संविधान की प्रति लेकर इसके प्रति आसन्न खतरे को लेकर लोगों को चेताना शुरू किया। न्याय और संविधान बसपा और दलित आंदोलन के प्रतीक रहे हैं। जो सीधे डा. आंबेडकर की विरासत के साथ जुड़ता है।
कांग्रेस का दलित आंदोलन के प्रतीकों की ओर आना सिर्फ वोट हासिल करने की ही नीति नहीं थी। उसे यह भी पता है कि हिंदुत्व की राजनीति जिस सवर्णवादी वर्चस्ववादी सामाजिक पृष्ठिभूमि पर खड़ी हो रही है और मुस्लिम समुदाय का बहिष्करण कर रही है उसमें नई जमीन हासिल करने के लिए इसके सिवा और कोई रास्ता भी नहीं है। यही कारण था सिर्फ एक तरफ मोदी ‘घुसपैठियों’ के बारे में भाषण दे रहे थे, वहीं मोहन भागवत ‘आरक्षण’ के मसले पर सफाई दे रहे थे।
भारतीय समाज में दलित, आदिवासी, ओबीसी और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय वे सामाजिक समूह हैं जिनसे भारत की राजनीति में नये तरह के ध्रुवीकरण और समीकरण बनते हैं। भारत का विशाल मजदूर वर्ग का अधिकांश हिस्सा इन्हीं समुदायों से आता है। अधिकतम श्रम और न्यूनतम आय की वजह से इनकी उपस्थिति सार्वजनिक जीवन में होने के बावजूद उनके संगठन की स्थिति बेहद कमजोर रहती है। इसकी वजह से राजनीतिक हस्तक्षेप की क्षमता भी कम रहती है।
पिछले कुछ दशकों से रोजगार के अवसर कम होने और जमीन पर दबाव बढ़ने की वजह से सामाजिक और सांस्कृतिक संकट तेजी से बढ़ा है। भाजपा नेतृत्व की सरकार इन समस्याओं को हल करने की बजाय उन्हें सस्ते दरों या मुफ्त राशन देने की योजनाओं के सहारे उन्हें अपनी राजनीति की ओर खींचने में लगी रही।
यदि हम पिछले 10 सालों का इतिहास देखें, तब हम मजदूरों, ग्रामीण खेतिहरों-मजदूरों के प्रति जिस बर्बरता की नीति को अपनाया गया, दलितों और उनके आंदोलनों के प्रति जिस तरह दमन की नीति अपनाई गई और सनातन के नाम पर मनु की नीति को जिस तरह खुलेआम बढ़ावा दिया गया है, वह बेहद खतरनाक और चुनौतीपूर्ण है। यही कारण है कि सिर्फ दलित आंदोलनों में नये संगठनों का ही उभार नहीं हुआ, कांग्रेस जैसी पार्टी ने भी उसी सामाजिक पृष्ठिभूमि पर खड़े होने की दावेदारी की है। इस दौर में कांग्रेस भी वही नारा दे रही थी जो आजाद अपने साक्षात्कारों में बोल रहे थेः ‘हम अपनी अंतिम सांस तक प्रतिरोध करते रहेंगे’।
आजाद की जीत संसदीय राजनीति में एक दलित राजनीति में एक उम्मीद की तरह देखना उन्हें सीमित करके देखना होगा। आजाद की जीत संसदीय राजनीति में एक नई सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठिभूमि की तलाश है। अब इस रास्तें में सिर्फ वही नहीं हैं। इस राजनीति के कई और राहगीर हैं।
(अंजनी कुमार स्वतंत्र पत्रकार हैं)