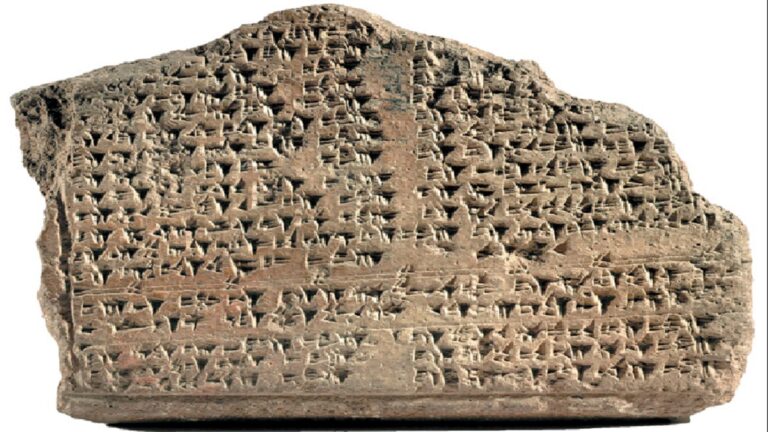29 अप्रैल, 2024 को एक छोटी सी खबर छपीः ‘न्यू-फासिस्ट रैली ने मुसोलिनी की मौत को याद किया’। यह खबर इटली से थी। पूरे यूरोप में फासिस्ट संगठनों के उभार को देखा जा सकता है। इससे जुड़ी खबरें कभी कभार अखबार की सुर्खियां भी बनती हैं। ये खबरें सिर्फ जनवाद और लोकतंत्र के आम मूल्यों के लिए चुनौतियां ही नहीं हैं। ये उन राजनीतिक माहौल को पुख्ता बनाने की ओर ले जा रही हैं जिसमें मजदूर वर्ग और आम जनवादी मूल्यों की आकांक्षा करने वाले समुदायों का अधिकार पूरी तरह छिन जाने का खतरा और गहरा होता जाता है। यदि हम अमेरिका और ब्रिटेन को ही देखें, जहां हाल के दिनों में फिलीस्तिनी लोगों का खत्म करने वाले इजरायली अभियान की आलोचना को वर्तमान सरकारें भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। जबकि वे खुद को लोकतंत्र बचाने वाली पार्टियों में शुमार करती हैं।
उपरोक्त खबर के दो दिन पहले, 27 अप्रैल, 2024 को आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व में गिने जाने वाले राम माधव ने इंडियन एक्सप्रेस में ‘प्रोवाईिंडंग द थैचरिस्ट हेफ्ट’ नाम से एक लेख लिखा। इस लेख का कुछ जमा अर्थ यह था कि थैचरवाद को मजबूत किया जाये जिससे चरम वाम-लिबरल राजनीति को किनारे किया जा सके। वह अपने तर्क में बताते हैं कि भारत में एक मजबूत नेतृत्व से वैश्विक रूढ़िवादी आंदोलन को मजबूती मिलेगी। यहां वह रूढ़िवादी और लिबरल को यूरोपियन, अमेरिकी संदर्भ में प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में इसकी व्याख्या का दायरा फैलता हुआ दिखता है।
यूरोपीय संदर्भ में यह ‘ईश्वर, धर्म, परिवार, राष्ट्र और देशभक्ति’ जैसी शब्दावलियों के सहारे दिखता है जिसका सीधा अर्थ मध्ययुगीन चर्च और राज्य के गठजोड़ से चलने वाली मध्ययुगीन राज्य व्यवस्था है। निश्चित ही, वर्तमान मध्ययुग में नहीं जा सकता तब इसका सीधा अर्थ धर्म और मध्ययुगीन मूल्यों पर आधारित एक ऐसे राज्य का निर्माण जिसमें जनवाद और लोकतंत्र के मूल्यों के लिए कोई जगह नहीं बचती है। राम माधव यूरोपीय और अमरीकी रूढ़िवादी आंदोलन को भारत के बुद्धिजीवियों को नये सिरे से देखने का आग्रह करते हैं और बताते हैं कि भारत की वैचारिकी में यह अपनी जड़ स्थापित कर सकता है और इसमें समाहित हो सकता है। इसके लिए वह भारतीय राष्ट्रवाद के साथ खड़ा होने और इस अवसर को हासिल करने की चुनौती को स्वीकार करने का आग्रह करते हैं।
फासीवाद राष्ट्रवाद के पैराशूट से ही उतरता है। पूंजी का जोर जितना ही बढ़ता है, पूंजीपतियों के बीच उसके मुनाफे के बंटवारे और पूंजी पर अधिक हकदारी का जोर बढ़ता जाता है। मुनाफे के बंटवारे और पूंजी पर अधिक हकदारी, एकाधिकार का सीधा परिणाम न सिर्फ देशों के बीच का विभाजन तेज होता है, वह समाज के भीतर भी उतनी ही तेजी से बंटवारा करता है। वह अपने अंतर्विरोध को मध्यवर्ग और मजदूर वर्ग के सहारे ही निपटाता है और खुद को सुरक्षित बनाये रखता है। वह राष्ट्रवाद को धर्म, ईश्वर, परिवार, परम्परा, संस्कृति, नस्ल, जाति आदि व्यापक निहितार्थों वाले शब्दों को जमीन पर उतरना शुरू करता है और इसे देशभक्ति के रंग में रंगकर सड़कों पर रैलियों और मुहल्लों में कीर्तनों की भरमार कर देता है।
ऐसे में, लोकतंत्र की आम समझ, जिसमें वोट देकर मतों की संख्या के आधार पर नेतृत्व चुनने की प्रक्रिया इन रैलियों और कीर्तनों के तेज झोंकों से डगमगाने लगता है। लोकतंत्र में बहुसंख्या हासिल करना लोकतांत्रिक मूल्यों की एक प्रक्रिया की बजाय, राज्य करने की एक महज एक वैधता हासिल करने की एक प्रक्रिया में बदलता जाता है। इसे अमेरीका में हुए पिछले चुनावों में देखा जा सकता है, जिसमें ट्रंप की भले ही हार हुई, लेकिन उसके तौर तरीकों का असर अब भी वहां बना हुआ है।
दुनिया भर में उभरते फासीवाद का असर भारत में दिख रहा है। यह उभार सिर्फ राजनीति के उस दायरे में ही नहीं है जहां चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों में हम जरूर ही उसके खतरनाक चेहरे को देख सकते हैं। लेकिन, यह अपने उन संगठनों के माध्यम से फैल रहा है, जो चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये समाज और राजनीति के विभिन्न हिस्सों में एक निर्णय करने वाली संस्था की तरह काम कर रहे हैं। ये राज्य की मशीनरी से लेकर सामंतों, गुंडों, दबदबा रखने वाले नेताओं से लेकर गीत, संगीत और सिनेमा तक में नेतृत्वकारी और समन्वयक की भूमिका निभाते हैं। चुनावों और ऐसी ही गतिविधियों के दौरान ये संगठन तेजी से सक्रिय होते हैं और समाज पर प्रभुत्वकारी की तरह छा जाने की ओर बढ़ते हैं।
ऐसे में, उनकी चुनाव लड़ने वाली पार्टी की लोकप्रियता यदि 15 से 20 प्रतिशत के बीच है, तब उपरोक्त संगठनों के माध्यम से यह आसानी से 10 से 15 प्रतिशत की और अधिक बढ़त करने की स्थिति में आ सकती है। निश्चित ही वोट महज एक गणित का खेल नहीं है। लेकिन, पिछले 20 सालों में वोट का गणित कई ऐसे तरीकों से तय होने लगा है, जिसमें वोट की लोकतांत्रिक प्रक्रिया इंजिनिरिंग की गणित की तरह ही तय होने लगा है। और, खुद लोकतंत्र एक महीन धागे पर लटकी एक उम्मीद की तरह ही रह गया है।
लोकसभा चुनाव के अब तक दो चरण पूरे हो चुके हैं। इस चुनाव में वोट की प्रक्रिया के साथ-साथ गैर वोट की वे प्रक्रियाएं भी चल रही हैं, जिससे प्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं। लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था रखने वाले लोग भी कल तक यह कहकर संतोष कर ले रहे थे, कि यदि जनता का चुनाव यही है, तो यह निर्णय सिर माथे पर। लेकिन, सूरत की घटना में जनता की भूमिका ही नदारद हो गई। बहुसंख्या का अर्थ सिर्फ चुनाव में वोट की संख्या ही नहीं है, यह इससे बाहर भी अर्थ रखता है। यह भारतीय लोकतंत्र की एक ऐसी सच्चाई है, जो पहले भी था लेकिन इतना खुले तौर पर नहीं था।
ऐसे में, भारतीय लोकतंत्र की संसदीय राजनीति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरी आस्था रखने वाला हिस्सा, उनकी पार्टी और संगठन एक ऐसे गहन संकट को देख रहे हैं, जिसमें संविधान की मूल संरचना ही खतरे में पड़ गई है। इंडिया गठबंधन में इस चिंता को देखा जा सकता है। लेकिन, भाजपा इस संकट को और बड़े दायरे तक ले जाना चाहती है। वह कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की कई-कई पार्टियों को अर्बन नक्सल के खांचे के साथ जोड़ देना चाहती है। राम माधव अपने लेख में जिसे लेफ्ट-लिबरल नाम देते हैं, मोदी अपने भाषणों में उन्हें अर्बन नक्सल के नाम से पुकारते हैं।
इस चुनाव में हार जीत से बड़ा मसला समाज और राज्य पर उन नियंत्रणकारी संस्थाओं की बढ़ती ताकत का है, जो सत्ता में होने और न होने के बावजूद अधिक मजबूत और निर्णयकारी होती गई हैं। भारतीय समाज में सबसे बड़ा तबका किसान का है। इसमें भूमिहीनों और गरीब की संख्या सर्वाधिक है। किसानों का अधिकांश हिस्सा न तो कोऑपरेटिव के माध्यम से उत्पादन की प्रक्रिया पर न्यूनतम नियंत्रण रखने की स्थिति में रह गया है और न ही अपने संगठनों के बल पर राज्य के साथ अपने हितों को सुरक्षित कर सकने की क्षमता में है। दूसरी ताकत मजदूर वर्ग है। इसका एक छोटा सा हिस्सा संगठित क्षेत्र में है और अधिकांश गैर संगठित क्षेत्र में। दोनों ही हिस्से अपने संगठन और यूनियन में बेहद कमजोर स्थिति में हैं। तीसरा हिस्सा युवा और छात्रों का है जिसमें बेराजगारी चरम पर है और भविष्य की चिंता भयावह स्तर पर पहुंच चुकी है। सामाजिक समुदाय के स्तर पर आदिवासी समुदाय को बड़े पैमाने पर उनके अधिकारों से वंचित कर उन्हें एक ऐसे अस्तित्व के संकट की ओर ठेला जा रहा है जिसमें खुद देश की प्राकृतिक अवस्था ही तबाह होने की ओर बढ़ रही है।
इसी तरह से दलित समुदाय को लगातार सामाजिक तौर पर दमित बनाये रखने का आग्रह समाज को एक हिंसक सरंचना में बदल देने की जुगत में लगा हुआ है। यही स्थिति मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों की भी है। इन सभी समुदायों के बीच लगातार धर्म, ईश्वर, परिवार, परम्परा, आस्था, देशभक्ति जैसे मूल्यों का लगातार प्रचार होने और इसी आधार पर संगठित होने, विभाजनों के दायरे को बढ़ाते हुए एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाने की प्रक्रिया के लगातार मजबूत होते जाने से मजदूर, किसान, छात्र, युवा, दलित जैसी आधुनिक सामाजिक अवधारणाएं लगातार कमजोर होती गई हैं।
भारत के मजदूर वर्ग के सामने सबसे बड़ा संकट खुद को एक मजदूर वर्ग की तरह खड़ा होना है। यदि एक मजदूर अपनी वर्ग चेतना से लैस नहीं है, तब वह समाज का सबसे कमजोर तबका है। यही वह चेतना है जिसके बल पर पर अन्य सारी पहचानों से ऊपर सबसे अधिक उन्नत पहचान सर्वहारा के रूप में सामने आता है और अपने ही जैसी पहचानों के साथ मिलकर एक वैचारिकी और संगठन का निर्माण करता है।
भारत में पिछले 150 सालों में कई आधुनिक बोध से लैस समुदायों और वर्गों का उभार और गठन हुआ। नये मूल्यों और नैतिकताओं को रचा गया। कई सारे आंदोलनों और पार्टियों का गठन हुआ और आज भी इस दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास देखे जा सकते हैं। मजदूर वर्ग को इन सभी प्रयासों के साथ जुड़कर व्यापक पैमाने में संगठित होने के रास्ते पर चलना होगा।
(अंजनी कुमार लेखक और स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)