सत्यशोधक समाज स्थापना दिवस (24 सितंबर, 1873)
पुनर्जागरण को ज्ञानोदय और प्रबोधनकाल के रूप में भी जाना जाता है। इटली में इसका प्रारंभ हुआ था और लगभग तीन सौ वर्षों (14 वीं से 17 वीं सदी) में यह पूरे यूरोप में फैल गया। इसकी शुरुआत यूरोप में धर्म की आलोचना से शुरू होती है। सब कुछ को प्रश्नांकित करना इसकी बुनियाद था। आस्था की जगह तर्क लेता है और ईश्वर की जगह मनुष्य विवेचन-विश्लेषण का केंद्र बनता है। यूरोप का ज्ञानोदय आंदोलन प्राचीन ग्रीक चेतना और आधुनिक विज्ञान के संयोग से निर्मित हुआ था। सच है कि ज्ञानोदय के आंदोलन ने पुनर्जागरण की नींव डाली। ज्ञानोदय आंदोलन ने संपूर्ण विश्व, विशेषकर यूरोप के सोचने-समझने के तरीके और बर्ताव में आमूल-चूल परिवर्तन ला दिया।
इसने कठोर धार्मिक बंधनों को ढीला कर दिया और वैज्ञानिक तरीके से सोचने और देखने के लिए प्रोत्साहित किया। कोपर्निकस से लेकर न्यूटन तक अनके वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक नियमों की खोज की। धार्मिक आस्थाओं को संशयग्रस्त कर दिया। धर्म, ईश्वर और उससे जुड़ी सभी आस्थाएं एवं मान्यताएं प्रश्नों के घेरे में आ गईं। इन प्रश्नों ने मनुष्य की पारंपरिक आस्थाओं को तोड़ दिया और उसके भीतर संशय पैदा कर दिया। इस संशय ने सब कुछ नए सिरे देखने के लिए प्रोत्साहित किया। इसने वैज्ञानिक क्रांतियों के साथ राजनीतिक क्रांतियों की भी पष्ठभूमि तैयार की। वैज्ञानिक आविष्कारों ने नई-नई तकनीक को जन्म दिया, जो बाद में औद्योगिक क्रांति का कारण बना। इस सब कुछ ने आस्था आधारित नजरिए की जगह वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जन्म दिया है। जिसे बाद में मार्क्स ने द्वंद्वात्मक ऐतिहासक भौतिकवाद के रूप में एक मुकम्मल शक्ल दिया। यह दुनिया को देखने का एक वैकल्पिक विश्व दृष्टिकोण बन गया।
भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ ही यहां सीमित स्तर पर ही सही ज्ञानोदय की शुरुआत होती है। यह विरोधाभासी और विडंबनापूर्ण है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य भारत को अपना उपनिवेश बनाता है यानि एक गुलाम देश बनाता है, वही भारत में ज्ञानोदय और पुनर्जागरण का वाहक भी बनता है। कार्ल मार्क्स ने इस दोहरी भूमिका को सही इन शब्दों में रेखांकित किया- “इंग्लैंड ने एक साथ भारत के लिए परस्पर विरोधी दो भूमिकाओं का निर्वहन किया है, एक विध्वंसक और नई चेतना की निर्मिती, एशियाई प्राचीन-समाज व्यवस्था का उन्मूलन और एशिया में पश्चिमी समाज जैसी भौतिक प्रगति की बुनियाद डालना।”
विश्व भर में पुनर्जागरण के केंद्र में तर्क, विवेक और न्याय पर आधारित प्रबुद्ध समाज का निर्माण रहा है। यूरोप में पुनर्जागरण के पुरोधा लोगों ने सामंती श्रेणी क्रम यानी ऊंच-नीच की ईश्वर निर्मित व्यवस्था को चुनौती दी। भारत में सामंती श्रेणी क्रम वर्ण-जाति के व्यवस्था के रूप में सामने आई थी। इसी का हिस्सा ब्राह्मणवादी पितृसत्ता थी। वर्ण-जाति और पितृसत्ता की रक्षक विचारधारा को ही फुले और डॉ. आंबेडकर ने ब्राह्मणवादी विचाधारा कहा। फुले और डॉ. आंबेडकर ने भारतीय सामंतवाद को ब्राह्मणवाद कहा।
यूरोपीय ज्ञानोदय और पुनर्जागरण के अग्रिम पक्ति के चिंतकों, विचारकों,लेखकों और संघर्षशील योद्धाओं में एक थॉमस पेन थे, जिन्होंने भारतीय पुनर्जागरण के सच्चे जनक और पुरोधा जोतिराव फुले के सोचन-समझने के तरीके को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। पश्चिम में जिस तरह और जिस कठोर भाषा में थॉमस पेन ने ईसाई धर्म और बाइबल की कूंपमंडूकताओं और मनुष्य विरोधी मूल्यों की आलोचना की, उससे भी कठोर भाषा में जोतीराव फुले ने हिंदू धर्म के मनुष्य विरोधी चरित्र को उजागर किया। मनुष्य की स्वतंत्रता और उसके द्वारा निर्मित समाज में समानता, ये दो फुले के सबसे बड़े जीवन मूल्य थे। भारतीय पुनर्जागरण का केंद्रीय कार्यभार वर्ण-जाति व्यवस्था और पितृसत्ता के खिलाफ संघर्ष था। जिसके खिलाफ निर्णायक संघर्ष की शुरुआत जातीराव फुले ने की थी।
भारतीय पुनर्जागरण के पुरोधा राजा राममोहन राय, देवेन्द्र नाथ टैगोर, विवेकानंद और दयानंद सरस्वती नहीं, बल्कि जोतिराव फुले, शाहू जी, पेरियार, सावित्रीबाई फुले, ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई हैं। भारतीय पुनर्जागरण का केंद्र बंगाल नहीं, महाराष्ट्र है। भारत में पुनर्जागरण की पहली सच्ची संस्था सत्यशोधक समाज था, क्योंकि बंगाली पुनर्जागरण के पुरोधा लोगों के बरक्स जोतीराव फुले, सावित्री बाई फुले, ताराबाई शिन्दे और डॉ. आंबेडकर ने भारतीय सामंतवाद यानी ब्राह्मणवाद की जड़ वर्ण-जाति और पितृसत्ता को अपने संघर्ष का केंद्र बिन्दु बनाया। महाराष्ट्र के पुनर्जारण की एक बड़ी विशेषता यह है कि यहां पुरुषों के साथ तीन महान महिला व्यक्तित्व भी हैं, जिन्होंने ब्राह्मणवाद यानी सामंतवाद को सीधी चुनौती दी।
इस तथ्य की ओर भी ध्यान देना जरूरी है कि बंगाली या हिंदी भाषी समाज के पुनर्जागरण के पुरोधा कहे जाने वाले लोग द्विज जातियों के हैं, जबकि महाराष्ट्र के पुनर्जागरण के पुरोधा शूद्र-अतिशूद्र जातियों के हैं या महिलाएं हैं।
भारतीय इतिहास को देखने का द्विजवादी नजरिया ही प्रभावी रहा है। यह बात आधुनिक इतिहास के संदर्भ में भी लागू होती है। अकारण नहीं है, पुनर्जारण के असली पुरोधा और संस्थाएं किनारे लगा दिये गये और ब्राह्मणवाद में ही थोड़ा सुधार चाहने वाले पुनर्जागरण के पुरोधा बना दिए गए।
राजा राममोहन राय, देवेन्द्र नाथ टैगोर, विवेकान्द और दयानन्द सरस्वती जाति व्यवस्था और ब्रह्मणवादी पिृतसत्ता के कुपरिणामों से चाहे जितना दु:खी हों,चाहे जितना आंसू बहाएं और उसे दूर करने के लिए जो भी उपाय सुझाएं, लेकिन इन लोगों ने वर्ण-जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को खत्म करने कोई आह्वान नहीं किया। जो इस देश में पुनर्जागरण का केंद्रीय कार्यभार था। बिना वर्ण-जाति और पितृसत्ता के खात्मे के समता आधारित समाज का निर्माण किया ही नहीं जा सकता है और बिना समता के न्याय की स्थापना संभव नहीं है और वर्ण-जाति और पितृसत्ता की मानसिकता के विनाश के बिना भारत में वास्तविक आधुनिकीकरण की शुरूआत नहीं हो सकती थी।
भारत की देशज शोषण-उत्पीड़न और गैर-बराबरी की आर्य-ब्राह्मणवादी व्यवस्था (भारतीय सामंतवाद) को आधुनिक युग में पहली बार चुनौती देने वाले पहले व्यक्तित्व फुले दंपति- जोतीराव फुले और सावित्रीबाई फुले हैं। जिन्होंने सत्य शोधक समाज (1873) के माध्यम से वर्ण-जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को निर्णायक चुनौती दी। कोई पूछ सकता है कि राजाराम मोहन राय और द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज (1828), आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविन्द रानाडे द्वारा स्थापित प्रार्थना (1867) और दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज (1875) जैसे संगठन और इनके संस्थापक व्यक्तित्वों की क्या भूमिका थी? जिन्हें अधिकांश भारतीय इतिहास भारतीय पुनर्जागरण का अगुवा मानते हैं।
इस संदर्भ में जाति का विनाश किताब में डॉ. आंबेडकर की टिप्पणी सटीक है और कहा है कि ये मुख्यत: परिवार सुधार आंदोलन थे। राजाराम मोहनराय, द्वारिका नाथ टैगोर, आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविन्द रानाडे और दयानंद सरस्वती जैसे व्यक्तित्व और इनके द्वारा स्थापित संगठनों ने वर्ण-जाति व्यवस्था और पितृसत्ता को निर्णायक चुनौती देने की जगह इसमें थोड़े- बहुत ऊपरी सुधार की बातें करते थे। जैसे कोई कहता छुआछूत गलत है, कोई कहता था कि सती प्रथा गलत है, कोई कहता कि बाल विवाह गलत है, कोई कहता था कि विधवा विवाह होना चाहिए। कोई कहता था कि जाति खराब है, लेकिन वर्ण-व्यवस्था ठीक है, कोई कहता महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। कोई कहता वेद सही हैं, स्मृतियां (मनुस्मृति आदि) खराब हैं। लेकिन इनमें से कोई भारत में इस सब की जड़ वर्ण-जाति व्यवस्था और पितृसत्ता के खात्मे की बात नहीं करता था और बहुसंख्य समाज शूद्रों (पिछड़ों) अति शूद्रों (दलितों) और महिलाओं की दासता के लिए जिम्मेदार ब्राह्मणवाद (भारतीय सामंतवाद) के खात्मे की बात नहीं करता था और न ही इसको जायज ठहराने वाले ईश्वरों और धर्मग्रंथों को निर्णायक चुनौती देता था।
फुले के नेतृत्व में 24 सितंबर 1973 को स्थापित सत्यशोधक समाज ने समाज सेवा और सामाजिक संघर्ष का रास्ता एक साथ चुना। सबसे पहले उन्होंने हजारों वर्षों से वंचित लोगों के लिए शिक्षा का द्वार खोला। विधवाओं के लिए आश्रम बनवाया, विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अछूतों के लिए अपना पानी का हौज खोला। इस सबके बावजूद वह यह बात अच्छी तरह समझ गए थे कि ब्राह्मणवाद का समूल नाश किए बिना अन्याय, असमानता और ग़ुलामी का अंत होने वाला नहीं है। इसके लिए ही उन्होंने ‘सत्यशोधक समाज’ की स्थापना की। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य वैदिक- पौराणिक मान्यताओं का विरोध करना, शूद्रों-अतिशूद्रों को जातिवादियों की मक्कारी के जाल से मुक्त कराना, वेदो-स्मृतियों और पुराणों द्वारा पोषित जन्मजात ग़ुलामी से छुटकारा दिलाना था।
सत्यशोधक समाज के माध्यम से फुले ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध एक सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की थी। 1890 में जोतीराव फुले के देहांत के बाद सत्यशोधक समाज की अगुवाई की जिम्मेदारी सावित्रीबाई फुले ने उठायी। 1873 में जोतीराव फुले ने गुलामगिरी नामक किताब लिखी। जो एक तरह से सत्यशोधक समाज का घोषणा-पत्र भी था। इस ग्रंथ को लिखने का उद्देश्य बताते हुए वे लिखते हैं कि ‘फिलहाल शूद्र-किसान धर्म और राज्य सम्बन्धी कई कारणों से अत्यन्त विपन्न हालात में पहुँच गया है। उसकी इस हालत के कुछ कारणों की विवेचना करने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई है।’
सत्यशोधक समाज जितना बड़ा समर्थक शूद्रों-अतिशूद्रों की मुक्ति का था, उतना ही बड़ा समर्थक स्त्री-मुक्ति का भी था। सत्यशोधक समाज के संस्थापक जोतीराव फुले ने महिलाओं के बारे में लिखा कि ‘स्त्री-शिक्षा के द्वार पुरुषों ने इसलिए बंद कर रखे थे। ताकि वह मानवीय अधिकारों को समझ न पाए।’ स्त्री मुक्ति की कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, जिसे जोतीराव फुले ने अपने समय में न लड़ी हो। जोतीराव फुले ने सावित्रीबाई के साथ मिलकर अपने परिवार को स्त्री-पुरुष समानता का मूर्त रूप बना दिया और समाज तथा राष्ट्र में समानता कायम करने के लिए संघर्ष में उतर पड़े।
शूद्रों-अतिशूद्रों और महिलाओं के अलावा जिस समुदाय के लिए सत्यशोधक ने सबसे ज़्यादा संघर्ष किया। वह समुदाय किसानों का था। ‘किसान का कोड़ा’ (1883) ग्रंथ में उन्होंने किसानों की दयनीय अवस्था को दुनिया के सामने उजागर किया। उनका कहना था कि किसानों को धर्म के नाम पर भट्ट-ब्राह्मणों का वर्ग, शासन-व्यवस्था के नाम पर विभिन्न पदों पर बैठे अधिकारियों का वर्ग और सेठ-साहूकारों का वर्ग लूटता-खसोटता है। असहाय-सा किसान सबकुछ बर्दाश्त करता है।
जो भी अध्येता भारतीय पुनर्जागरण के इतिहास का ठीक से अध्ययन करेगा वह निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि भारत की पहली सच्ची संस्था जोतीराव फुले द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज था।
(डॉ. सिद्धार्थ जनचौक के सलाहकार संपादक हैं।)







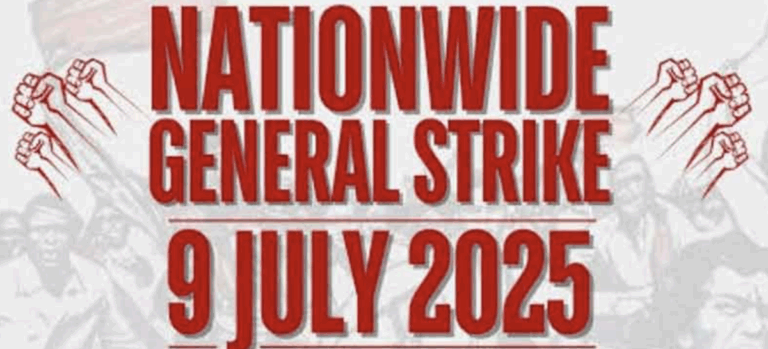






बहुत ही sundar aalekh