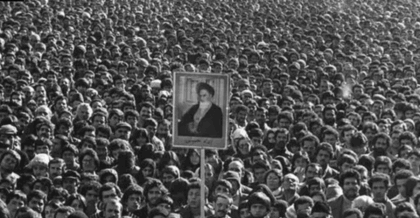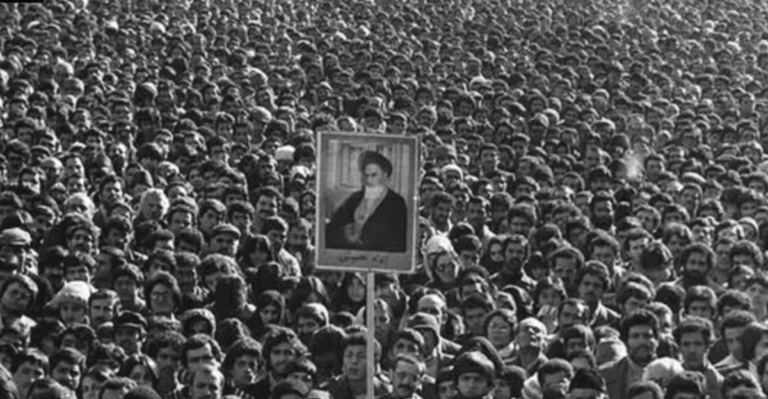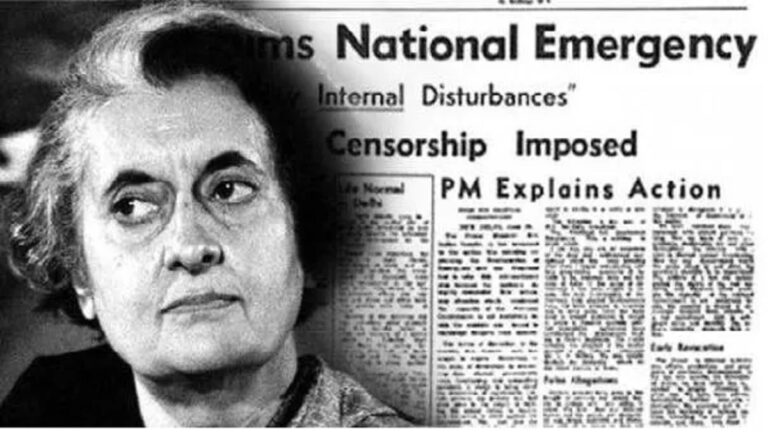दिल्ली। उत्तराखंड के दो जिलों पौड़ी और अल्मोड़ा के बॉर्डर पर रामगंगा नदी के किनारे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया।सोमवार, 4 नवंबर 2024 को सुबह 8:30 बजे उत्तराखंड के मर्चुला के करीब एक बस रामगंगा के पास सड़क से नीचे गिर गई।
बताया जा रहा है कि बस पहले एक चट्टान से टकराई और फिर नीचे गहरे में गिर गई । कुमाऊं डिविजनल कमिश्नर श्री दीपक रावत ने इस घटना में 36 लोगों की मौत की पुष्टि की है।
यह एक बेहद दर्दनाक हादसा था। बताया जा रहा है कि इस घटना में एक परिवार के एक से ज्यादा सदस्यों की भी जान गई है।ऐसी घटना में यह कहकर भी काम चलाया जा सकता है कि- “ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति दे’ और “शोकाकुल परिवार को ऐसी शक्ति मिले कि वे इस दुःख को सहन कर सकें”।
लेकिन इतना भर कह देने से शोकाकुल परिवारों का दुख कम नहीं होने वाला! इनमें से कई लोगों का दुख कम हो सकता था, अगर रामनगर के अस्पताल में इलाज का इंतजाम पूरा-पूरा होता। रामनगर के उस अस्पताल में, जहां घायलों को लेकर पहुंचा गया।
अगर उस अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टर होते, पर्याप्त स्टाफ होता, पर्याप्त दवाइयां होती, टेस्टिंग के साधन पर्याप्त होते, और पैथोलॉजी की पर्याप्त व्यवस्था होती तो कई लोगों की जान बच जाती और कई लोगों का दर्द कम हो जाता है। लेकिन रामनगर के उस अस्पताल में इलाज के नाम पर कुछ भी नहीं था।
इसलिए स्थानीय लोग उस अस्पताल को रेफरल सेंटर कहते हैं। 4 नवंबर की सुबह भी उस अस्पताल में केवल रेफर करने का काम हुआ। किसी को ऋषिकेश भेजा गया और किसी को हल्द्वानी।
नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फ़ोर्स, पुलिस, प्रशासन की टीमों के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही लोकल लोग मदद के लिए पहुंच चुके थे। उन्होंने ही पहले-पहल दुर्घटना ग्रस्त लोगों को निकाला। सबसे पहले वे ही उन्हें रामनगर के अस्पताल तक लेकर आये।
रिपोर्टर को एक लोकल मददगार श्री चांद खान ने रामनगर के अस्पताल का हाल बताते हुए कहा कि अस्पताल में घायलों को बांधने के लिए पट्टी तक नहीं थी। उन्होंने बताया कि घायलों के जख्मों पर दवाई लगाने के बाद रुई के ऊपर पट्टी बांधने की बजाय रुई को टेप से चिपका दिया गया।
चांद खान ने बताया कि ऋषिकेश से जो डॉक्टर आए थे उनका कहना था कि वह घायलों का इलाज वे रामनगर के अस्पताल में ही कर देंगे। लेकिन जब उन्होंने अस्पताल से इक्विपमेंट और सामान की डिमांड की तो उन्हें बताया गया कि जो इक्विपमेंट और सामान वे डॉक्टर मांग रहे हैं, वे तो रामनगर के उसे अस्पताल में हैं ही नहीं।
रामनगर के एक निवासी संजय नेगी ने बताया कि जिन घायलों को फ्रैक्चर था, उन्हें प्लास्टर लगाने की जगह उनकी टूटी हड्डियों को लकड़ी से सहारा दिया गया था। संजय नेगी अन्य लोगों के साथ, पिछले कुछ दिनों से अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं।
उनकी मांग है कि रामनगर के अस्पताल को पीपीपी मॉडल से अलग करके केवल सरकारी अस्पताल बनाया जाए। पीपीपी मॉडल का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यानि सरकारी फंड से मरीज को केवल चारपाई मिल सकती है, बाकी सब खर्चे प्राइवेट होंगे।
पहले से ही धरने पर बैठे हुए लोग चाहते थे कि वे अपनी बात मुख्यमंत्री से कहें। लेकिन रामनगर के अस्पताल में घायलों से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री ने उन लोगों से मिलने से मना कर दिया।
कल्पना कीजिए कि रामनगर के अस्पताल को सरकारी बनाने की लड़ाई लड़ रहे लोग अगर लव-जिहाद जैसे किसी काल्पनिक मामले पर धरने पर बैठे होते तो मुख्यमंत्री का निर्णय क्या होता? क्या वे उन सांप्रदायिक लोगों से मिले बिना चले जाते?
हम जानते हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री के मामले में यह बात ठीक-ठीक कही जा सकती है कि वे उन सांप्रदायिक लोगों से मिले बिना नहीं जाते।
घायलों को पहले मर्चुला से रामनगर लाया गया। मर्चुला से रामनगर के बीच की दूरी 36 किलोमीटर है। रामनगर के अस्पताल में घायलों को सही तरीके से अस्पताल के अंदर ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां न तो कोई स्टाफ था और न ही कोई स्ट्रेचेर आदि ही था। रामनगर के अस्पताल से घायलों को हल्द्वानी के सुशीलादेवी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया।
रामनगर से हल्द्वानी की दूरी 52 किलोमीटर है। जख्मी हालत में घायलों को 52 किलोमीटर का सफर करने के लिए मजबूर किया गया। क्योंकि रामनगर के अस्पताल में बेसिक सुविधाएं भी नहीं थीं।
हल्द्वानी के अस्पताल में पहुंचकर बताया गया कि वहां भी इलाज की व्यवस्था नहीं है। अब मरीजों को ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया गया। हल्द्वानी से ऋषिकेश की दुरी 250 किलोमीटर है।
यानि बुरी तरह से घायल लोगों को पहले 36 किलोमीटर चलवाया गया। वहां से उन्हें 52 किलोमीटर दौड़ाया गया। और उसके बाद भी 250 किलोमीटर दौड़ाया गया। 36 + 52 + 250 = 338 किलोमीटर तक घायलों को बिना इलाज के घुमाया जाता रहा।
उत्तराखंड में आल वेदर सडकें तो बन रही हैं, लेकिन आल इलाज अस्पताल कोई नहीं है। और न ही बनाने की मंशा है। क्योंकि सरकार की नीतियां जनपक्षीय नहीं, पूंजीपति केंद्रित हैं। सरकार को पूंजीपतियों को होटल का व्यापार देना है, लेकिन उत्तराखंड के लोगों को अस्पताल नहीं देना है।
इसलिए आल वेदर रोड पर तो जोर है, लेकिन आल इलाज अस्पतालों पर कोई जोर नहीं है। बल्कि जो अस्पताल पहले से चल रहे थे, उन्हें भी पीपीपी मॉडल पर प्राइवेटाइज करके लोगों की कमजोर जेबों पर हमला किया जा रहा है।
रामनगर वह जगह है जहां उत्तराखंड के पौड़ी और अल्मोड़ा जिले के बहुत बड़े इलाके से लोगों का आना-जाना लगा रहता है।लेकिन इतने बड़े इलाके के लिए कोई काम का अस्पताल नहीं है।
उत्तराखंड के अस्पतालों में रेफर-रेफर का खेल खूब चलता है। मरीजों को रेफर किया जाता हैं। लेकिन उनमें से इलाज कम को ही मिल पाता है।
12 अगस्त, 2022 के उत्तराखंड सरकार के आदेश के अनुसार राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को रेफर करने की अथॉरिटी नहीं है। (इसलिए आयुष्मान कार्ड धारकों को राज्य के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जाकर कोई लाभ नहीं मिलता।)
उत्तराखंड से पलायन की एक बड़ी वजह स्वास्थ्य सुविधाओं की लगभग अनुपस्थिति का होना है। इसलिए शहरों के लोग यहां पिकनिक तो मना सकते हैं, रह नहीं सकते। शिक्षा का न होना, पलायन की दूसरी बड़ी वजह है।
हाल में ही उत्तराखंड में मजबूत भू-कानून के समर्थन में कई रैलियां निकली गई। लेकिन सवाल यह भी है कि बिना अस्पताल और बिना स्कूल-कॉलेज के खाली भू-कानून लेकर उत्तराखंड के लोगों को क्या मिल जाएगा?
2017 से पहले उत्तराखंड में एक ठीक-ठाक भू-कानून था ही! वो भू-कानून उत्तराखंड से पलायन को रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो सका?
सन 2018 में मर्चुला से 40 किलोमीटर ऊपर धुमाकोट के पास एक बस का एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में 48 की मौत हुई थी और 12 घायल हुए थे।
घटनास्थल से जब मरीज को धुमाकोट के अस्पताल में लाया गया तो पता चला कि अस्पताल में खड़ी एंबुलेंस में टायर ही नहीं हैं। उतनी मौतों के बाद भी राज्य और उसके लोगों ने क्या सीखा?
दरअसल ऐसा लगता है कि राज्य की नजर में उत्तराखंड के नागरिकों की जान की कोई कीमत है ही नहीं। राज्य की नजर में उत्तराखंड के नागरिकों की कीमत केवल उस समय दिखाई देती है जब उसे राज्य के नागरिकों को सांप्रदायिक आधार पर बांटना होता है।
और ज्यादातर मौकों पर राज्य के लोगों को भी अपने होने का अहसास तभी होता है जब उनके सामने किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को शत्रु के रूप में खड़ा कर दिया जाता है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, रात-दिन लैंड-जिहाद, लव-जिहाद जैसे झूठे और सांप्रदायिक स्लोगन तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि उन्हें अस्पताल स्कूल-कॉलेज बनाने की जरूरत है।
मैं उत्तराखंड में अपने इलाके के ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं, जो TB तक की दवाई लेने के लिए दिल्ली के अस्पतालों में सिफारिश करने वालों को ढूंढते हैं। मैं उत्तराखंड के ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो बच्चों की पढ़ाई की खातिर दिल्ली में बहुत कम पैसे की नौकरी करते हैं और बहुत ही बुरे हालातों में रहते हैं।
अगर उन लोगों के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था और उनकी दवाई की व्यवस्था उत्तराखंड का राज्य ठीक प्रकार से कर देता, तो उन लोगों के कई दुख कम हो सकते थे।
लेकिन जब राज्य का मुखिया ही राज्य के लोगों को नफरत का पाठ पढ़ रहा हो तो उसे लोगों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य से क्या मतलब हो सकता है!
उत्तराखंड के अलग-अलग इलाकों में झूठ के आधार पर सांप्रदायिक प्रदर्शनों का आयोजन करने वाले असामाजिक लोगों के साथ तो उत्तराखंड के अनेक लोग खड़े दिखते हैं, लेकिन जो लोग उत्तराखंड में स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं, उन्हें उत्तराखंड के लोगों ने अकेला ही छोड़ दिया है।
उत्तराखंड में यह सवाल पूछने वाला कोई नहीं है कि 43 सीटर बस में 60 से 65 लोग क्यों बैठते हैं। वहां के लोगों की ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि उन्हें इस तरह के खतरे मोल लेकर सफर करना पड़ता है। क्यों उत्तराखंड की सार्वजानिक परिवहन व्यवस्था को प्राइवेट ऑपरेटरों की मनमानी के हवाले कर रखा है।
अगर उत्तराखंड में सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था शानदार होती, तो इस तरह के हादसे होने की संभावना बहुत कम होती। लेकिन आप उत्तराखंड में किसी भी दिशा में चले जाइए, आपको सरकारी बस सेवा न के बराबर मिलेगी।
यह भी एक बड़ी वजह है कि प्राइवेट बस ऑपरेटर मनमाने ढंग से सवारियों को भेड़-बकरी की तरह ठूंस कर ले जाते हैं और ऐसा करना कई बार हादसों की वजह बनता है।
यह बात साफ होनी चाहिए कि प्राइवेट ऑपरेटर लोगों की सेवा के लिए बसें नहीं चलाते, बल्कि बसें चलाना उनका व्यवसाय है।लेकिन सरकार लोगों की सेवा के लिए बसें चला सकती है, और सरकारी बसें चलाना भी सेवा की परिभाषा के अंतर्गत आता है।
सवाल ये है कि तरह की घटनाओं को रोकने और जान का नुकसान कम करने में राज्य की तात्कालिक और दूरगामी योजनाएं क्या हो सकती हैं? दूसरा सवाल यह है कि क्या इस तरह की घटनाओं का संबंध, राज्य और केंद्र द्वारा अपनाए गए विकास के मॉडल के साथ भी है?
इस घटना के संदर्भ में राज्य ने कुछ तात्कालिक कदम उठाए हैं। लेकिन राज्यों को कुछ लॉन्ग टर्म नीतियों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। राज्यों को सोचना होगा कि राज्य में खेती किसानी को फायदेमंद कैसे बनाया जाए। खेती किसानी को नुकसान पहुंचा रहे जानवरों से किसान की रक्षा कैसे की जाए?
बंदरों और सुअरों जैसे जानवरों से निपटना, आज की तारीख में कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर राज्य सरकार खेती को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों की नसबंदी करने का कार्यक्रम तेजी से चलाए, तो आने वाले कुछ ही सालों में किसानों को बड़े भारी नुकसानों से बचाया जा सकता है।
ऐसा करके राज्य से हो रहे पलायन पर भी एक हद तक रोक लगाई जा सकती है। उत्तराखंड की सरकार को राज्य में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ताकि राज्य के लोग शिक्षा की तंगी के कारण राज्य के बाहर जाने को मजबूर न हों। लेकिन इसके उलट उत्तराखंड की राज्य सरकार, राज्य में स्कूलों को लगातार बंद करने में लगी हुई है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत तो राज्य में स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया में बहुत तेजी आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 में बताई गयी क्लस्टर स्कूल की संकल्पना को राज्य में तेजी से लागू किया जा रहा है। जिसके कारण पिछले कुछ ही सालों में राज्य के 3000 से ज्यादा है स्कूलों को बंद किया जा रहा है।
जिस राज्य में लोग जंगल के घास पर अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं, उस राज्य की सरकार ने लोगों के बिना मांगे ही, उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड दे दिया है। क्योंकि वर्तमान सरकार को हर बात में हिन्दू-मुसलमान करना बहुत अच्छा लगता है।
सरकार में बैठे लोगों को इस बात का पक्का भरोसा है कि हिंदू-मुसलमान के विभाजनकारी मंत्र का जाप करने भर से ही वे सत्ता की कुर्सी पर काबिज रह सकते हैं।
अगर राज्य के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, जंगल के संसाधनों पर वाजिब हिस्सेदारी, और जंगली जानवरों से सुरक्षा आदि मिल रही होती, तो राज्य के लोग भारी मात्रा में देश के अलग-अलग हिस्सों में कम जाते और हमें राज्य की लचर परिवहन व्यवस्था में कभी-कभी अचानक से भारी भीड़ कम दिखाई देती। और उत्तराखंड के लोग मर्चुला जैसी दुर्घटनाओं का शिकार होने से बच सकते थे।
हमें भीड़ की भीड़, उत्तराखंड में ऊपर चढ़ते और उत्तराखंड से नीचे उतरते हुए इसलिए दिखाई देती है क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार विकास के जिस मॉडल पर काम कर रही है, वह अत्यंत केंद्रीकृत है। वह मॉडल राज्य के लोगों की जरूरत के हिसाब से नहीं, बल्कि कुछ खास लोगों की जरूरत के हिसाब से बनाया गया मॉडल है।
भारत में और राज्य में शहरों का विकास भी अत्यंत केंद्रित है। विकास डी-सेंट्रलाइज्ड नहीं है। यही कारण है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आपको दिल्ली जैसे शहरों में मिलेंगे। लेकिन गांवों, छोटे कस्बों और छोटे शहरों में नहीं मिलेंगे।
विकास के इस मॉडल की वजह से भी तमाम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार की तलाश में, कुछ चुनी हुई जगह की तरफ जाते हैं। लेकिन अपने सांस्कृतिक अनुष्ठानों के लिए उन्हें अपने गांव की ओर लौटना होता है।
क्योंकि ये सांस्कृतिक अनुष्ठान एक ही तारीख में पड़ते हैं, इसलिए भी पहले से कमजोर परिवहन व्यवस्था भीड़ के वजन को सहन नहीं कर पाती और कई बार बुरी तरह से टूट जाती है।
इसलिए जरूरी है कि देश और राज्य में शहरों का विकास, विकेंद्रित तरीके से हो। ताकि लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार जैसी बेसिक जरूरतों की तलाश में अपनी जड़ों से कटकर बहुत दूर न जाना पड़े।
मर्चुला जैसी दुखद घटनाओं पर शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म सॉल्यूशंस के नजरिए से विचार करने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म में आप यह देख सकते हो कि क्या ड्राइवर नशे में था? क्या उस बस का फिटनेस सर्टिफिकेट अपडेटेड था? क्या ड्राइवर के पास जरूरी लाइसेंस था?
क्या ड्राइवर ने डबल ड्यूटी की थी? क्या घायलों को सही इलाज मिल रहा है? क्या मृतकों के परिजनों को राज्य और केंद्र शासित सरकार द्वारा घोषित मुआवजे की राशि समय से मिल रही है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें शॉर्ट-टर्म सॉल्यूशंस के सवाल कह सकते हैं।
लेकिन राज्य और उसके लोगों को कुछ लॉन्ग-टर्म सॉल्यूशंस पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। और उन्हें सोचना होगा कि राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानी, परिवहन व्यवस्था आदि में तेजी से सुधार कैसे किया जाए।
(बीरेंद्र सिंह रावत शिक्षा विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं।)