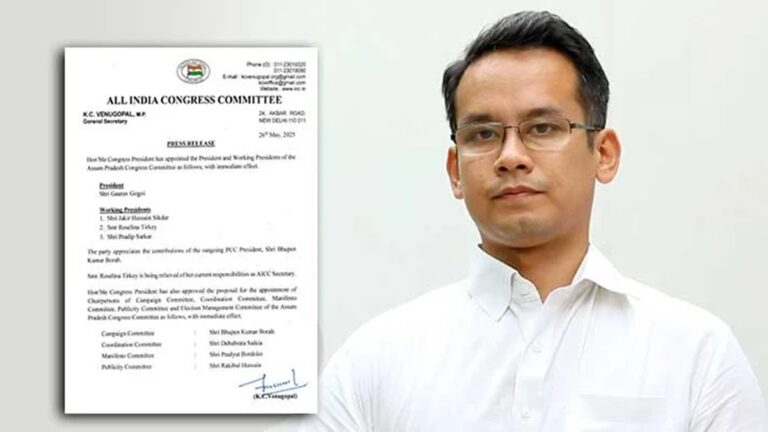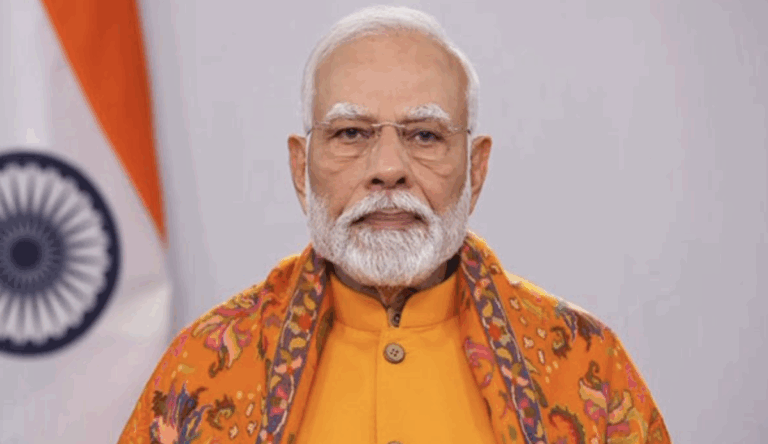‘अखंड भारत’ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सबसे पुराना और प्रिय सपना है, जो भाजपा के सत्ता में आने के बाद से खूब देखा जा रहा है। संघ के मुखिया के भाषण से लेकर स्वयंसेवकों की व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी तक में यह ‘हसीन सपना’ छाया रहता है। हालांकि यह और बात है कि इस सपने को साकार करने का ब्लू प्रिंट किसी के पास नहीं है। हां, जो भारत अभी विद्यमान है उसे खंड-खंड करने के नारे और कार्यक्रम संघ और भाजपा के पास खूब है, जिसके जरिये वे देश के आम आदमी को हलकान किए हुए हैं।
संघ का ऐसा ही एक नारा है- ‘एक राष्ट्र-एक संस्कृति’, जो पिछले दिनों बेंगलुरू में संघ की तीन दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में दोहराया गया। बैठक के बाद संघ के दूसरे नंबर के पदाधिकारी यानी सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि ‘एक राष्ट्र-एक संस्कृति’ की पहल इसलिए की गई थी ताकि देश के लिखित इतिहास की गड़बड़ियों को ठीक किया जा सके और एक सद्भाव वाला भारत बनाया जा सके। संघ की बैठक खत्म होने के एक दिन बाद 24 जनवरी को उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अब समय आ गया है कि ‘एक राष्ट्र-एक संस्कृति’ के विचार को आगे बढ़ाया जाए।
वैसे ‘एक राष्ट्र-एक कुछ भी’, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माथे पर सवार पुराना फितूर है। ‘एक राष्ट्र-एक कर’ यानी जीएसटी से शुरू करके ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’, एक देश-एक राशनकार्ड और ‘एक देश-एक नागरिक संहिता’ तक उनकी सरकार ने ऐसे अनेक नारे उछाले हैं’ यह अलग बात है कि भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में हर नागरिक के लिए सब कुछ एक जैसा करना बिल्कुल नामुमकिन है। जीएसटी से भी कहां एक कर की व्यवस्था बन सकी। जीएसटी में ही पांच किस्म के कर लगते हैं और उसके अलावा कम से कम एक दर्जन किस्म के कर अलग से लगते हैं।
बहरहाल अब ‘एक राष्ट्र-एक संस्कृति’ का शिगूफा उछाल कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस फितूर में शामिल हो गया है। हालांकि संघ का यह फितूर नया नहीं है। कोई नौ साल पहले 2016 में संघ के भाष्यकार एमजी (माधव गोविंद) वैद्य ने ‘एक राष्ट्र-एक संस्कृति’ शीर्षक से एक लेख लिखा था, जिससे इस अवधारणा पर विचार आगे बढ़ा। उन्होंने लिखा था कि देश के लिए एक भाषा या एक धर्म की बजाय एक साझा मूल्य प्रणाली की जरुरत है।
सवाल है कि क्या संघ इस साझा मूल्य प्रणाली को ही एक संस्कृति मानता है? लेकिन इससे बड़ा प्रश्न संस्कृति का है। क्या भारत एक संस्कृति या एक साझा मूल्य प्रणाली वाला देश हो सकता है? हकीकत यह है कि इतिहास में कोई कालखंड ऐसा नहीं रहा है, जब भारत भूमि पर एक साझा मूल्य प्रणाली रही हो। तो फिर अब कैसे यह विचार सामने लाया जा रहा है?
भारत कभी भी एक संस्कृति वाला देश नहीं रहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्बिवेदी ने भारत को अनेक ‘संस्कृतियों का समुच्चय’ कहा है। वे मानते थे कि भारत की सभ्यता का निर्माण कई संस्कृतियों के मेल से हुआ है और ये संस्कृतियां एक दूसरे से भिन्न भी हैं। इसीलिए उन्होंने भारत की सभ्यता को ‘विरूद्धों में सामंजस्य’ साधने वाला कहा है।
इसीलिए जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ‘एक राष्ट्र-एक संस्कृति’ की बात करता है तो हैरानी होती है। संघ भले ही खुद को सांस्कृतिक संगठन बताता हो और अपने को भारतीय संस्कृति का आधिकारिक भाष्यकार भी मानता हो, लेकिन उसे यह समझना अभी बाकी है कि भारत एक संस्कृति वाला देश न तो कभी था और न कभी हो सकता है। संस्कृति और सभ्यता के अंतर को लेकर भी उसकी समझ संदिग्ध मालूम होती है।
पांच हजार साल की भारतीय सभ्यता अगर आज तक अपनी निरंतरता बनाए रख सकी है तो इसकी वजह यही है कि इस दौरान यहां अनेक संस्कृतियां नष्ट हुईं और नई संस्कृतियों का जन्म हुआ लेकिन वे सभ्यता के विशाल समूह का हिस्सा बनी रहीं। वैसे भी भारत जैसे देश में एक संस्कृति की बात कैसे सोची जा सकती है, जहां कोस-कोस पर पानी और दो कोस पर बानी बदलने की बात कही जाती हो।
पानी और बानी बदलने के साथ ही संस्कृति के कई तत्व भी बदलते जाते हैं। भारत में सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां हैं। हर बोली के साथ उसकी अपनी संस्कृति जुड़ी हुई है। हर भाषा और बोली के साथ उसके अपने त्योहार और परंपराएं जुड़ी हुई हैं। यहां तक कि धार्मिक मान्यताएं भी भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से बदल जाती हैं। इस लिहाज से कह सकते है कि संस्कृति एक व्यापक अवधारणा का एक बहुत छोटा हिस्सा है।
भारत में कितनी सामाजिक भिन्नताएं हैं, कितनी परंपराएं हैं, कितनी मान्यताएं और कितने लोक व्यवहार हैं, कितनी भाषाएं और कितनी बोलियां हैं, किस तरह के खान-पान और पहनावे की भिन्नता है, यह सब बातें प्रख्यात समाजशास्त्री एमएन श्रीनिवास या श्यामा चरण दुबे की किताबों को पढ़ कर भी समझा जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया है कि ये सारी भिन्नताएं अलग-अलग संस्कृतियों को जन्म देती हैं।
क्या किसी को यह बताने की जरुरत है विवाह से लेकर अंतिम संस्कार तक की कितनी विधियां इस देश में प्रचलित है? अकेले हिंदू धर्म में कितनी तरह की पूजा पद्धतियां हैं, कितनी तरह की विवाह संस्कृति है और कितनी तरह की अंतिम संस्कार की विधियां है? एमएन श्रीनिवास ने ‘यादों से रचा एक गांव’ में लिखा है कि कर्नाटक में मैसूर के इलाके में हिंदुओं, खास कर सवर्णों में मामा और भांजी या ममेरे और फुफुरे भाई-बहन के बीच विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। क्या उत्तर भारत के किसी राज्य में हिंदू खास कर सवर्ण हिंदू परिवार में इस तरह के विवाह की बात सोची भी जा सकती है?
कर्नाटक के लिंगायत समुदाय में लोगों को मृत्यु के बाद दफनाने का रिवाज है। विवाह और अंतिम संस्कार से अलग अगर पूजा पद्धति की बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर देश के बड़े हिस्से में नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें शुद्ध शाकाहारी खान-पान होता है, जबकि पश्चिम बंगाल में तीन दिन के दुर्गापूजा उत्सव में बलि होती है और वध किए गए पशु का मांस ही देवी का प्रसाद होता है। बलि की यह परंपरा बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और असम जैसे कुछ अन्य राज्यों में भी है। सवाल है कि क्या शाक्त, शैव और वैष्णव परंपराओं को मिला कर एक बनाने की बात की जा सकती है? पिछले कुछ समय से समूचे देश पर जबरदस्ती वैष्णव परम्परा लादने का प्रयास हो रहा है। क्या एक संस्कृति की बहस उसी का हिस्सा है?
बहरहाल, जब हिंदू समुदाय के अंदर ही आप विवाह और अंतिम संस्कार की साझा पद्धति नहीं बना सकते है, खानपान और पहनावे की साझा पद्धति विकसित नहीं कर सकते हैं, पूजा पद्धति को एक जैसा नहीं बना सकते हैं तो यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि जिस देश में दुनिया के लगभग हर धर्म के लोग रहते हैं, उनकी एक जैसी संस्कृति बना दे? देश में मुस्लिम दूसरा बड़ा और ईसाई तीसरा बड़ा धार्मिक समुदाय है। दोनों समुदायों के विभिन्न फिरके भारत में रहते हैं, जिनकी अपनी अलग-अलग मान्यताएं है। उन्हें कैसे एक किया जा सकेगा?
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता बन कर लागू हुई लेकिन आदिवासियों उससे बाहर रखा गया। क्योंकि उनकी संस्कृति बिल्कुल अलग है और ऐसा नहीं है कि देश की समूची आदिवासी आबादी की एक जैसी संस्कृति है। उनके अंदर भी संस्कृतियों की भिन्नता है। हर राज्य में हर अंचल के आदिवासियों के सामाजिक रीति-रिवाज एक दूसरे से भिन्न हैं।
दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रवाद को संस्कृति से जोड़ना चाहता है जो कि एक निहायत अव्यावहारिक और विनाशकारी सोच है। जिस तरह एक संविधान, एक राष्ट्रगान, एक राष्ट्रगीत, एक राष्ट्रीय झंडा आदि बना दिया गया है, उसी तरह एक संस्कृति नहीं बनाई जा सकती। किसी भी उपवन की सुंदरता उसमें खिलने वाले फूलों की विविधता में ही निहित होती है। भारत भी एक ऐसा ही उपवन है जिसमें तरह-तरह की संस्कृति रूपी फूल खिल रहे हैं। यह इसी रूप में रहेगा तो ही इसकी सुंदरता और निरंतरता बनी रह पाएगी, अन्यथा तो इस भारत रूपी एकवचन को बहुवचन होने से कौन रोक सकता है?
(अनिल जैन वरिष्ठ पत्रकार हैं और इंदौर में रहते हैं)