आज़ादी की लड़ाई का समय हिंदोस्तान की तारीख़ का वह कालखंड है, जो अपनी कु़र्बानी, जुनून, वतनपरस्ती, मुल्क के झंडाबरदारों के सब्र, संघर्ष और अंततः आज़ादी पा लेने की कामयाबी के लिए इतिहास में अमर हो गया है। बीसवीं सदी के पहले चार दशकों में मुल्क के लिए कुछ भी कर गुज़रने की जो आबो हवा बह रही थी, वह अकारण नहीं था। उस दौर के हिंदोस्तान में जिस क़द के किरदार मुल्क की रहनुमाई का बीड़ा उठा चुके थे, वह इतने प्रभावशाली थे कि उन्हें देख और सुनकर ही वतन का हर शख़्स देशभक्ति के रस में और राष्ट्र के लिए कुछ भी कर गुज़रने के जुनून में डूब जाता था।
महात्मा गांधी, पं. जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, मौलाना हसरत मोहानी, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद इत्यादि अनेक ऐसे नाम हैं, जो मुल्क के तमाम आम इंसानों को कुछ कर गुज़रने की भावना से स्वयं के किरदारों से स्वतः भर चुके थे। इसका नतीजा यह भी हुआ कि देश का प्रत्येक वर्ग अपने-अपने स्तर पर उस ख़्वाब से दो-चार होने लगा कि आज़ादी के बाद का हिंदोस्तान कैसा होना चाहिए और सिर्फ़ ख़्वाब ही नहीं, अपनी-अपनी क्षमता के हिसाब से वे ख़्वाब में देखे हिंदोस्तान के निर्माण की कोशिशें भी करने लगा। कवि, शायर, लेखक, जन प्रतिनिधि, शिक्षक सभी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में मुल्क को संवारने के मक़सद से जुट गए थे।
पूरे हिंदोस्तान में उस दौर में सिर्फ़ आज़ादी की लड़ाई का जोश ही शिखर पर नहीं था, बल्कि आज़ाद हिंदोस्तान के निर्माण का जुनून भी कमतर नहीं था। ऐसे माहौल में उस समय के हिंदोस्तान के साहित्यकार भी अपने रचनाकर्मों से देश के निर्माण में जुटे हुए थे। उस दौर का हर फ़नकार व साहित्यकार यह कोशिश करने लगा था कि उसके ख़ुद के साहित्य और कला की आने वाले कल में जो सूरत बने, वह हर दृष्टि से विकार रहित हो, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ऐसी कोशिशों और इस तरह की जुनूनी भावनाओं से परिचय कराती हुई एक किताब साहित्य की दुनिया में इन दिनों काफ़ी चर्चा में है।
किताब का नाम ‘रूदाद-ए-अंजुमन’ और इसके प्रस्तुतकर्ता ज़ाहिद ख़ान हैं। वास्तव में यह किताब बीसवीं सदी के चालीस के दशक में ख़ास तौर पर 1946-47 के एक वर्ष की उन बैठकों का ब्यौरा है, जो ‘प्रगतिशील लेखक संघ’ के उर्दू साहित्य के अदीबों द्वारा मुंबई में हर हफ़्ते होती थीं। प्रलेसं उर्दू के मुंबई इकाई के सेक्रेटरी उन दिनों हमीद अख़्तर थे। वे नियमित तौर पर उन बैठकों की रिपोर्ट लिखते थे। हमीद अख़्तर द्वारा लिखा गया यह विवरण उर्दू लिपि में था। जिसका लिप्यंतरण ज़ाहिद ख़ान ने शायर इशरत ग्वालियरी की मदद से हिन्दी में किया है।
इस किताब के सफ़्हे-दर-सफ़्हे गुज़रते हुए उस समय के साहित्यिक सफ़र से रू-ब-रू होने का एहसास बहुत ज़ल्द ही क़ाबिल-ए-तारीफ़ की शक्ल इसलिए ले लेता है कि जब यह अनुभव होना शुरू हो जाता है कि ये अदीब जुनून की किन हदों तक साहित्य को सजाने-संवारने के प्रति समर्पित थे। यह सजाना-संवारना इसलिए बहुत मायने रखता है कि यह सब सिर्फ़ अल्फ़ाज़ों की ख़ूबसूरती और रदीफ़-काफ़िया की दुरुस्ती तक से ही संबंधित नहीं था। सबसे ज़रूरी बात उस वक़्त के साहित्यकार यह मानते थे कि अदब सामाजिक और मानवीय सरोकारों से लबरेज़ होना चाहिए।
किताब में जगह-जगह ऐसे विमर्श, संवाद और टिप्पणियां दर्ज़ हैं, जिनको पढ़कर ज़िंदगी के वे मायने समक्ष में आते हैं, जिनसे इंसान इंसानियत का सबक़ ख़ुद-ब-ख़ुद सीखने लगता है। उदाहरण के लिए ‘‘सरदार जाफ़री, ‘‘दीवार-ओ-दर से आप क्या मुराद रखते हैं?’’ ज़ोए अंसारी, ‘‘शायरी में दीवार-ओ-दर के मानी रुकावट के होते हैं और रुकावट के बाद ही शोरीदा-सर (दीवाना) पैदा होता है, पहले नहीं।’’ (पेज-70) असीम मानवीय क्षमता का इतने कम शब्दों में इतना बेहतरीन वर्णन चमत्कृत करता है।
किताब को पढ़ते-पढ़ते जब यह संवाद सामने आता है कि ‘‘उर्दू शायरी पर हिंदुस्तानी फ़लसफ़ों का बहुत ज़्यादा असर पड़ा। यही चीज़ हिंदुस्तानी तसव्वुरात (विचार) को ईरानी तसव्वुरियत (सोच) से जुदा करती है।’’ (पेज-81), तो पढ़ने वाले का चकित होना, बहुत अप्रत्याशित नहीं होता है। क्योंकि वह तो यह मानता था कि उर्दू, मुसलमानों की भाषा है। और इसकी पैदाइश हिंदुस्तान नहीं कोई और मुल्क है।
इसी सिलसिले में आगे का संवाद है, ‘‘..मीर हसन की मसनवियों को पढ़ने से साफ़ मालूम होता है कि यहां की तहज़ीब का असर उर्दू शायरी पर किस क़दर पड़ा है।.. हमारी शायरी में यूसुफ़-ज़ुलैख़ा के साथ-साथ नल-ओ-दमयंती का भी ज़िक्र आता है, जो बिल्कुल हिंदुस्तानी चीज़ है।’’ (पेज-81, 82) इसी तरह पेज 91 पर दर्ज यह बयान कितना मौजू़अ है, ‘‘मधुसूदन, आख़िर कौन सी चीज़ कहने पर आप आर्टिस्ट को तरक़्क़ीपसंद और कौन सी चीज़ कहने पर रजअत-पसंद (परंपरावादी) कहेंगे।’’
सरदार जाफ़री ने इसका जवाब देते हुए कहा, ‘‘इसका कोई अबदी मेयार (सार्व-कालिक स्तर) नहीं। एक चीज़, एक वक़्त में तरक़्क़ीपसंद और दूसरे वक़्त में रजअत-परस्त हो सकती है।’’
इसी तरह ग़ज़ल क्या है? इसका बेहतरीन विश्लेषण ‘रूदाद-ए-अंजुमन’ में ऐसे दिया गया है, ‘‘ग़ज़ल तो वही है, जिसका हर शे’र, दूसरे शे’र से मुख़्तलिफ़ हो।’’ (पेज-126) उल्लेखनीय है कि यह सब अली सरदार जाफ़री, जोश मलीहाबादी, जोए अंसारी और मजरूह सुल्तानपुरी जैसी वह हस्तियां कह रही हैं, जो ग़ज़ल, नज़्म, या तरक़्क़ीपसंद अदब के आज भी स्तंभ हैं। ‘रूदाद-ए-अंजुमन’ में इस मुद्दे पर भी महत्त्वपूर्ण विश्लेषण है कि क्या प्रगतिशील साहित्य मात्र वामपंथ या वामपंथियों का ही या उनके द्वारा रचा और लिखा गया है?
अक्सर इस तरह की बातें ‘आरोप’ की शक्ल में प्रगतिशील लेखक संघ और उसके साहित्य पर लगाना पिछले कई सालों से एक रवायत सी हो गई है। इस बाबत किताब के कुछ अंश देखने लायक़ हैं। ‘‘ये कहना कि तरक़्क़ीपसंद मुसन्निफ़ीन की तहरीक महज़ कम्युनिस्टों की तहरीक है, बिल्कुल ग़लत है।.. हमारा ही वाहिद (अकेला) अदबी इदारा है, जिसमें मुख़्तलिफ़ सियासी ख़याल और अक़ाएद (विश्वास) के लोग बाज़ मुश्तरका (संयुक्त) मक़ासिद के लिए मुत्तहिद (सहमत) हुए हैं।.. सरमायापरस्ती, ग़ुलामी और जुल्म की मुख़ालफ़त हर अवामी जमाअत के अंदर से की जा सकती है। और यही वो बुनियाद है, जो हम सबको (यानी कि प्रगतिशील विचारधारा के लोगों को) मुत्तहिद (हमराय) करती है।’’ (पेज-145)
इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मानवीय मूल्यों, जीवन के शाश्वत सिद्धांतों का हर समर्थक। और जुल्म-ओ-सितम, नाइंसाफ़ी, फ़िरक़ापरस्ती, ग़रीबी, पाखंड, कट्टरवाद एवं हुकूमत की नाइंसाफ़ी की मुख़ालफ़त करने वाला हर झंडाबरदार यक़ीनन प्रगतिशील या तरक़्क़ीपसंद होगा। इस प्रकार यह कहना कि प्रगतिशील होना, साम्यवादी विचारधारा का होना अनिवार्य है, सरासर ग़लत है।
‘रूदाद-ए-अंजुमन’ वह प्रकाशन है, जिसने आज के पाठकों को साहित्य के शाश्वत मूल्यों से परिचित कराने का सफल प्रयास किया है। सिर्फ़ पाठकों को ही नहीं, साहित्यकारों को भी यह किताब एक राह दिखाती है। महज़ राह दिखाती ही नहीं है, उस पर चलने का शऊर भी बख़्शती है। अली सरदार जाफ़री, ज़ोए अंसारी, ख़्वाजा अहमद अब्बास, सज्जाद ज़हीर, जोश मलीहाबादी, ज़ेडए बुखारी, मजरूह सुल्तानपुरी, अख़्तर-उल-ईमान, मीराजी, मजाज़, कृश्न चंदर, इस्मत चुग़ताई आदि इस पूरी रूदाद के ख़ास साहित्यकार या मुसन्निफ़ीन हैं।
पूरी किताब में अदब की दुनिया के इन्हीं शहंशाहों ने अपने विचारों से अनेक विषयों पर पूरी गंभीरता से विचार किया है। इन सबको पढ़कर यही एहसास होता है कि उस दौर के बाशिंदे, आज़ाद हिंदोस्तान को लेकर कितना फ़िक्रमंद थे और पूरे जुनून से अपनी क़लम को पैना कर रहे थे। हिंदुस्तानी अदब, हर हाल में इंसानी मेयार की रौशनाई से ही लिखा जाना चाहिए।
‘रूदाद-ए-अंजुमन’ मूलतः उर्दू में लिखी गई और वह भी बीसवीं सदी के चालीस के दशक की उर्दू में। उस दौर में उर्दू हिंदोस्तान की वह भाषा थी, जिसे हर हाल में प्राथमिकता ही नहीं दी जाती थी, बल्कि यह अवाम की एक सामान्य भाषा थी। विशेषकर उस इलाके में जिसे आज हम हिन्दी पट्टी कहते हैं। इसलिए इस किताब की उर्दू लिपि निश्चय ही सामान्य नहीं रही होगी। हिन्दी में लिप्यंतरण एक कठिन काम रहा होगा। इसके लिए ज़ाहिद ख़ान को मुबाकरबाद देना लाज़िमी है।
जहां तक भाषा का सवाल है, किताब में कई जगह अरबी-फ़ारसी के कठिन शब्द आए हैं, अनुवादक ने उनका हिन्दी अर्थ प्रत्येक पेज पर उन्हीं शब्दों के साथ दिया है। जिससे उन्हें समझने में परेशानी पेश नहीं आती। ऐसी किताबें निश्चित तौर पर अदब का सरमाया की हैसियत रखती हैं।
किताब : ‘रूदाद-ए-अंजुमन’ (डायरी)
लेखक : हमीद अख़्तर
उर्दू से हिन्दी लिप्यंतरण : ज़ाहिद खान
प्रकाशक : लोकमित्र प्रकाशन नई दिल्ली।
(डॉ.पुनीत कुमार की समीक्षा।)





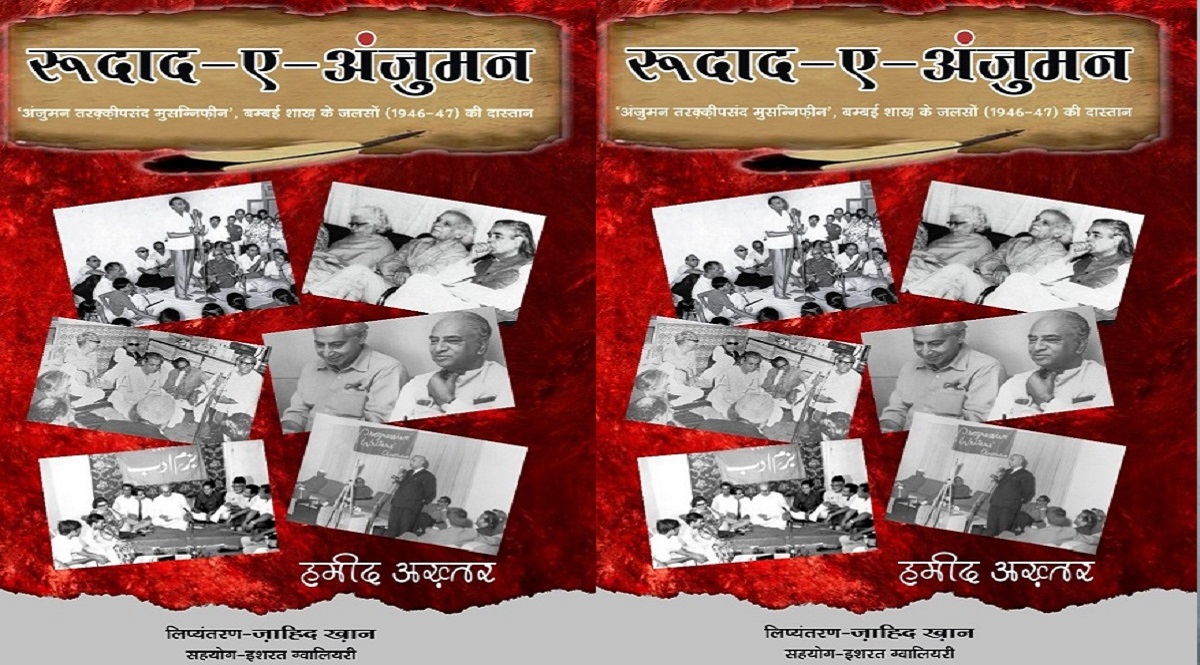
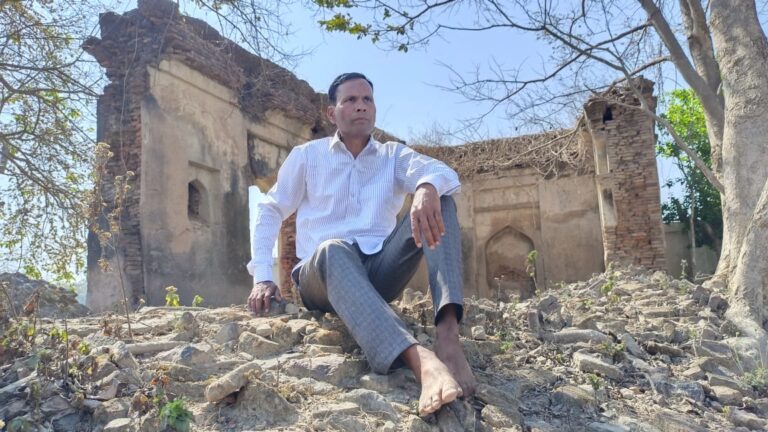

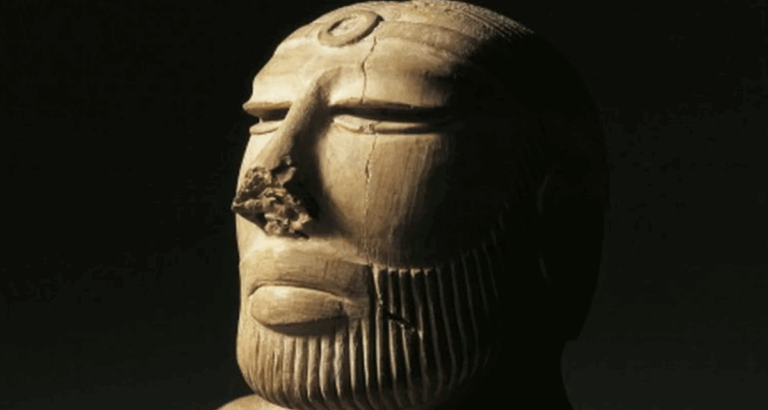





अच्छा विश्लेशण किया आप ने वाक़ई यह किताब बहुत ही अहम है,
इस किताब को पढ़ते हुए आप स्वयं उस दौर में पहुंच जाते हैं ऐसा लगता है जैसे आप भी उन मह्फिलो में शरीक हो, आप साक्षात उस मयारी गुफ़तगू का हिस्सा बन जाते हैं, बयेक वक़्त मुल्की और आलमी म्सायल के साथ साथ उस वक़्त की आदबी सरगर्मियों से भी वाक़िफ होते जाते हैं । इस किताब को पढ़ना यानी अपनी अदबी तारीख से जुड़ना ही है।
इस महत्त्व्पूर्ण दस्तावेज़ को हिन्दी पाठकों में रूबरू करवाने के लिये लेखक ज़ाहिद का बहुत बहुत शुक्रिया।
सुन्दर समीक्षा।