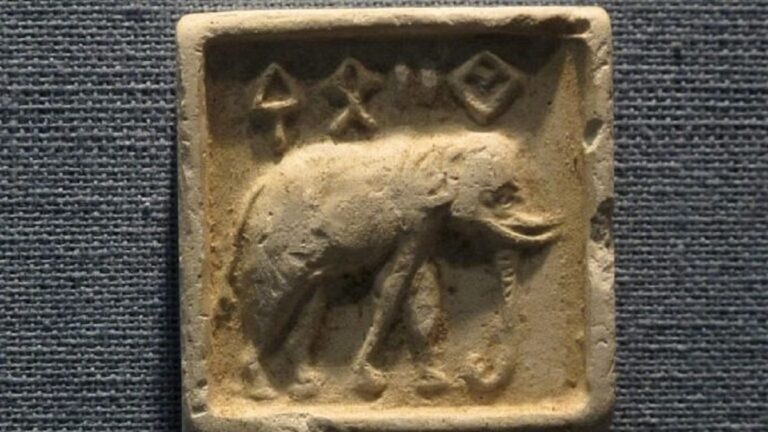पर्यावरण के संदर्भ में ‘परिस्थितिकी’ नाम का एक शब्द आता है, जिसका अर्थ है अपने भौतिक परिवेश के साथ बना और बनाया हुआ संबंध। मानव जीवन केवल दी गई परिस्थितियों में नहीं रहता, बल्कि वह अपने परिवेश को बदलते हुए स्वयं भी निरंतर बदलाव का जीवन जीता है। यही मानव समाज के इतिहास में अभिव्यक्त होता है। यहाँ तक कि उसने जानवरों के इतिहास को भी बदल दिया। नदियों और जलाशयों के साथ उसका प्रभाव अब मौसम तक पर पड़ने लगा है। पर्यावरण इसी बदलती परिस्थितिकी का हिस्सा है, और निश्चित रूप से पर्यावरण इस बदलाव के साथ बदल रहा है।
यह बदलाव निरपेक्ष नहीं है और यह आमतौर पर बेहद प्राकृतिक प्रतीत होता है। हम जिस समाज में रहते हैं, उसकी सर्वोच्च संस्था ‘राज्य’ इस बदलाव को मनुष्य के हित के लिए जारी की गई ‘सर्वसम्मति से बनाई गई नीति’ के तहत लागू करता है। जब इस पर विवाद उठता है, तब बहुसंख्यक धारणा के आधार पर उसे मान्यता दी जाती है। जब यह भी काम नहीं करता, तब राज्य की संप्रभुता और उसकी पवित्रता का हवाला दिया जाता है। लेकिन, जिन हितों के लिए पर्यावरण में बदलाव लाने की नीति बनाई जाती है, उन्हें हरसंभव तरीके से छिपाया जाता है।
यह छिपाने की नीति क्यों अपनाई जाती है? क्योंकि यह धरती सभी मनुष्यों की है। इस परिस्थितिकी और पर्यावरण में सभी हिस्सेदार हैं। इस सामूहिक चेतना को पूंजीवादी चिंतक अक्सर क्लासिक भाषा में ‘बर्बर’, ‘पिछड़ा’, ‘असभ्य’, ‘अराजक’ जैसे नाम देते हैं। पूंजीवाद को मुनाफा चाहिए, जिसकी एक आधारभूत शर्त मेहनतकश लोग हैं और दूसरी उपभोग।
पूंजीवाद परिस्थितिकी में एक मौलिक बदलाव लाता है, जो मालिकाना हक से जुड़ा है। यह एक बड़ी आबादी को शहरों की ओर ठेल देता है और दूसरी ओर इस परिस्थितिकी के उपयोग को मूल्य में बदल देता है। यहीं से मनुष्य का पर्यावरण के साथ अभिन्न रिश्ता टूटता है, और वह एक अजनबीपन भरे रिश्ते में चला जाता है। इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए उसे पैसे का भुगतान करना पड़ता है। यहाँ तक कि साफ धूप और हवा तक से वह वंचित होने लगता है।
भारत दुनिया के शीर्ष पूंजीवादी देशों में नहीं गिना जाता। यह आज भी विकासशील देशों की सूची में शामिल है और कई मानकों में पिछले दशकों की तुलना में और भी पिछड़ गया है। हालाँकि, मोदी सरकार के नेतृत्व में यह दावा जरूर किया जा रहा है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। गाँव की एक कहावत है कि ताड़ के पेड़ के नीचे खड़े होकर उसके फल के गिरने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, और गर्मियों के दिन श्रीफल के पेड़ के नीचे बैठकर कभी आराम नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि ऐसे दावों पर भरोसा करना हानिकारक हो सकता है।
बावजूद इसके, हमारे यहाँ विकास के लिए पूंजीवादी चाहतें प्रबल हैं। इन चाहतों के लिए पूंजीवादी संकटों का हवाला देकर आजकल ग्रीन एनर्जी की बात जोर-शोर से चल रही है। एक तरफ भारत में कोयला और पेट्रोलियम की खपत को कम करने का कोई ठोस रुख नहीं दिख रहा, बल्कि यह बढ़ता ही जा रहा है। पेड़ और जंगल काटने, नदियों और जलाशयों को बर्बाद करने में आज भी कोई कमी नहीं दिख रही।
पूंजीवादी विकास की दौड़ में भारत भले ही पीछे रह गया हो, लेकिन उससे उत्पन्न होने वाले संकटों में यह सबसे अग्रिम पंक्ति में दिखता है। पिछले साल येल विश्वविद्यालय द्वारा पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में कुल 180 देशों की सूची में भारत 176वें स्थान पर था। एक अन्य स्विस कंपनी के वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 74 शहर शामिल थे।
हमें इस संदर्भ में अपने देश की मैन्युफैक्चरिंग उद्योग या अन्य उत्पादक गतिविधियों की सूची देखनी चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि कौन-सी ऐसी पूंजीवादी उत्पादन गतिविधियाँ इन शहरों में चल रही हैं, जिनसे इतना प्रदूषण बढ़ रहा है? भारत में प्रदूषण और पूंजीवादी उत्पादन के बीच सीधा संबंध शायद ही मिले। उदाहरण के लिए, दिल्ली पर्यावरण के मामले में सबसे विवादित शहर रहा। इसमें न्यायपालिका से लेकर विधायिका तक आँकड़े लेकर बैठ गई और इसका दोष किसानों पर डाल दिया गया। यह उद्योगों से उत्पन्न होने वाला प्रदूषण नहीं था।
अशोक गुलाटी और सुवांगी रथ अपने एक लेख ‘ए रिवॉल्यूशन ऑफ क्लीन एनर्जी’ में समस्या की जड़ मुफ्त खाद और बिजली की उपलब्धता बताते हैं, जिसे उनके अनुसार पुनःप्रबंधित किया जा सकता है। वे उत्पादन के पैटर्न को बदलने पर जोर देते हैं। वे बताते हैं कि हरित क्रांति ने उत्पादन में अहम भूमिका निभाई, लेकिन अब उससे भूमि क्षरण में काफी इजाफा हुआ है। उनके लेख में प्रस्तुत आँकड़ों में कोई गलती प्रतीत नहीं होती। वे पहले भी किसान आंदोलन को लेकर लेख लिख चुके हैं और उनका कुल तर्क यही है कि ऐसी उत्पादन व्यवस्था से भारत के समग्र विकास में कोई योगदान नहीं दिख रहा, उल्टे यह भारत की अर्थव्यवस्था पर एक बोझ की तरह है।
यहाँ हम उनके लेख पर हुए वाद-विवाद पर नहीं जा रहे। हम उस तर्क व्यवस्था की ओर देख रहे हैं, जिसे भारत के किसी भी कोने में लागू कर जंगल के इलाकों को काटकर वहाँ खनिज पदार्थों का दोहन किया जाता है या जो इलाके रेतीले हैं, जैसे राजस्थान, या पठारी हैं, जैसे लद्दाख, वहाँ भी यही तर्क लागू किया जाता है। राजस्थान में बड़े-बड़े सौर संयंत्र लगाने की मानो होड़-सी लग गई है। इन परियोजनाओं में कितने पेड़ काटे गए, कितने पानी का उपयोग किया जाता है, और इस तरह की परियोजनाओं से स्थानीय जीवन कितना प्रभावित होता है, इसकी चर्चा ही नहीं की जाती।
सौर पैनल एक निश्चित तापमान पर ही काम करते हैं; उससे अधिक होने पर वे जल सकते हैं। राजस्थान में गर्मियों में औसत से अधिक तापमान रहता है। ऐसे में उन्हें ठंडा रखने के लिए उसी राजस्थान से पानी की आपूर्ति की जाती है। पैनलों को धोने के लिए पानी की अलग व्यवस्था करनी पड़ती है। हाल ही में लद्दाख के चारागाहों को ऐसी परियोजना के लिए अधिग्रहित करने की बात चली, तो वहाँ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और लोग पैदल चलकर दिल्ली तक आए।
प्रदूषण दूर करने वाली कथित ग्रीन एनर्जी का मसला हो या पर्यावरण-अनुकूल खेती का प्रबंधन, यदि पूंजी केंद्र में हो और मनुष्य इसका हिस्सा ही न हो, तो इसके परिणाम पर्यावरण के अनुकूल होना संभव नहीं है। पर्यावरण परिस्थितिकी का हिस्सा है, और मनुष्य इसी परिस्थितिकी का निर्माण करता है। किसानों को इससे बाहर रखकर, उनकी दी गई परिस्थितिकी से अलग रखकर बनाई गई किसी भी नीति से न तो पर्यावरण का भला हो सकता है और न ही उनके जीवन में समृद्धि आ सकती है।
यदि ग्रीन एनर्जी इतनी ही उत्तम और पर्यावरण-अनुकूल है, तो इसमें लोगों की भागीदारी क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? लोगों को उचित दामों पर सौर पैनल और अन्य संसाधन देकर बिजली की माँग पर नियंत्रण किया जा सकता है, जैसा कि पंजाब के संदर्भ में प्रबंधन की बात कही जा रही है। दरअसल, यहाँ बिजली की खपत से अधिक मसला किसानों की खेती की लागत में सरकार की हिस्सेदारी घटाकर उनकी लागत बढ़ाने का है, जिससे खेती उनके लिए बोझ बन जाए और वे खेती से दूर होने लगें।
इससे खेतों पर नजर गड़ाए लोगों के लिए रास्ता साफ हो जाता है। राजस्थान से लेकर लद्दाख जैसी जगहों पर सौर पैनल, और झारखंड जैसी जगहों पर कोयला-पानी आधारित बिजली संयंत्र, पहाड़ों में हाइड्रो प्रोजेक्ट-ये सभी बिजली बनाने और बेचने का बड़ा धंधा हैं। इनका सीधा असर पर्यावरण पर पड़ता है।
पर्यावरण-अनुकूल बिजली उत्पादन की व्यवस्था हो या खेती, सभी जगह उसकी परिस्थितिकी का ध्यान रखे बिना, उसमें मनुष्य की उपस्थिति और भागीदारी के बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है, भले ही वह कथित तौर पर ग्रीन एनर्जी ही हो। पर्यावरण के संदर्भ में की जा रही बातों और नीतियों को मनुष्य की परिस्थितिकी में रखकर देखे बिना न तो उनका मकसद स्पष्ट होता है और न ही उनके पर्यावरण पर पड़ने वाले परिणामों को परखा जा सकता है। आज किसी भी नीति को पर्यावरण के संदर्भ में देखने के साथ-साथ मनुष्य की परिस्थितिकी में परखना भी जरूरी है।
(अंजनी कुमार पत्रकार हैं)