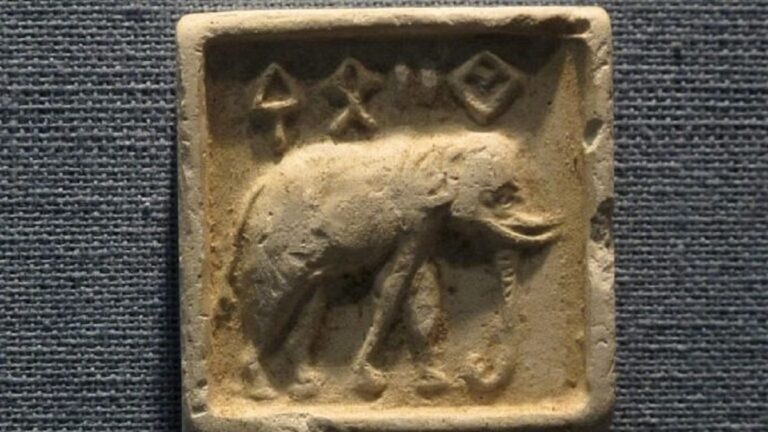नई दिल्ली। कोरोना वायरस का प्रभाव पूरी दुनिया ने महसूस किया जिसके रोकथाम के लिए अलग-अलग राष्ट्रीय सरकारों ने एक ही तरह के समाधान को रेखांकित किया, लॉकडाउन। यह अपने आप में एक आपातकाल था जिसमें लोगों को किसी ख़ास परिधि में बंद कर दिया गया और सरकारों द्वारा उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि यह एक बेहतरीन तरीका है जिसके द्वारा इसे फैलने से रोका जा सकता है।
परन्तु लॉकडाउन के दौरान तीसरी दुनिया में कुछ अलग भी हो रहा था जिसके ऊपर काफी कम लोगों ने गौर किया और वह था प्रत्येक क्षेत्रों का सैन्यीकरण। ख़ास कर यह सैन्यीकरण दो क्षेत्रों में व्यापक रूप से देखने को मिला, खनन क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में जहाँ लोगों ने अपने लोकतान्त्रिक अधिकारों के लिए कई आंदोलन किये हैं। निगरानी क्षेत्र में भी व्यापक वृद्धि देखने को मिलती है। परन्तु क्या सरकारों ने इसे सीधे लागू कर दिया तब इसका जवाब है नहीं। सरकारें किसी भी गैर-संवैधानिक कार्य को करने के लिए एक कानून की मदद लेती हैं। ऐसे ही कानूनों के सन्दर्भ में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 144 जो हमारे विधिक प्रक्रिया में एक औपनिवेशिक निरंतरता का भी प्रतीक है उसपर चर्चा होनी बेहद जरुरी हो जाता है।
2019 में अनुराधा भसीन और गुलाम नबी आज़ाद ने संयुक्त रूप से सर्वोच्च न्यायलय में धारा 144 के सन्दर्भ में एक रिट पेटिशन दायर किया था जिसका मूल सन्दर्भ कानून का दुरुपयोग और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सन्दर्भ में था। इस रिट की सुनवाई हल ही में सुप्रीम कोर्ट ने की जिसमें कोर्ट ने इस कानून की व्यापक व्याख्या करते हुए इसके कई सन्दर्भों को समझते हुए एक व्यापक निर्णय दिया जिसमें न्यायलय ने इस कानून की संवैधानिकता पर बहस न करते हुए केवल उसके प्रयोग पर बात किया है। इसके संवैधानिकता को लेकर पहले ही यह स्थापित कर दिया गया है कि विधि की सम्यक प्रक्रिया द्वारा इस कानून को पास किया गया है तथा इसे सही भी ठहराया गया है।
यह एक कथन नहीं बल्कि किसी भी बुर्जुआ देश की हकीकत है कि स्वतंत्रता और सुरक्षा हमेशा एक विवाद का विषय रहते हैं।परन्तु यह स्थिति ऐसे देशों में ज्यादा भयावह है जिसपर साम्राज्यवाद का सीधा प्रभाव है, जैसे की भारत। सुरक्षा की अपनी एक पूरी राजनितिक अर्थव्यवस्था है जिसे व्यापक रूप से समझने की जरूरत है। हालाँकि हम इस लेख में इस पक्ष पर ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते परन्तु यह समझ लेना बेहद जरुरी है कि आज के समय में पूंजी के प्रसार का एक बहुत बड़ा आधार असुरक्षा का एहसास दिलाना और बाद में सुरक्षा के नाम पर लोगों पर नियंत्रित करना है।
शहरी क्षेत्रों में, जहां लोग अपने मौलिक अधिकारों के लिए लंबे समय से विरोध कर रहे थे, अब वहां दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144 के माध्यम से आवाज़ को दबाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले में इस बात पर चिंता व्यक्त की कि धारा 144 का उपयोग अनिश्चितकालीन और व्यापक रूप से मौलिक अधिकारों को सीमित करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है। बड़े क्षेत्रों में लागू किए गए आदेश, जो आबादी के व्यापक हिस्से को प्रभावित करते हैं, को किसी आसन्न खतरे के विशिष्ट साक्ष्यों के साथ उचित ठहराना चाहिए। अनुराधा भसीन के फैसले में आनुपातिकता के परीक्षण (Test of Proportionality) पर जोर दिया गया। धारा 144 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को किसी विशिष्ट खतरे या समस्या का समाधान करने के लिए “सबसे कम प्रतिबंधात्मक” उपाय होना चाहिए। उदाहरण के लिए, लंबे समय तक बिना पुनर्मूल्यांकन के लगाए गए प्रतिबंध अनुपातहीन माने गए।
विश्वविद्यालय जैसे स्थान, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, या अन्य प्रमुख विश्वविद्यालय, अब राज्य द्वारा विरोध की आवाज़ को दबाने के लिए लक्षित किए जा रहे हैं। अगर हम पीछे जाकर देखें तो विश्वविद्यालय परिसरों का सैन्यीकरण और पुलिसिंग कोरोना महामारी से पहले इतना सामान्य नहीं था। लेकिन कोरोना के बाद, राज्य ने असुरक्षा और पुलिसिंग की झूठी जगह बनाई और डर का एक माहौल खड़ा कर दिया।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 “नुकसान या खतरे की आशंका” के तात्कालिक मामलों से संबंधित है। यह धारा एक मजिस्ट्रेट को यह आदेश जारी करने का अधिकार देती है कि सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका वाले मामलों में तत्काल कार्रवाई की जा सके। इस धारा का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक पहलू धारा 144(3) है, जो विधायिका को यह ताकत देती है कि वह एक बार में ही सभी आवाज़ों को शांत कर सके। इसमें कहा गया है कि, “इस धारा के तहत आदेश किसी विशेष व्यक्ति, किसी स्थान पर रहने वाले लोगों या क्षेत्र में रहने वाले लोगों, या किसी विशेष स्थान पर जाने वाले लोगों के लिए जारी किया जा सकता है।”
उमाकांत यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में माननीय अदालत ने कहा कि इस धारा का उद्देश्य दंडात्मक नहीं बल्कि निवारक कार्रवाई है। अनुराधा भसीन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 144 के आदेश जारी करने में पारदर्शिता की कमी की आलोचना करते हुए कार्यपालिका को निर्देश के तौर पर यह बताया है कि धारा 144 प्रताड़ना का एक तंत्र नहीं है बल्कि विकट परिस्थिति में प्रयोग की जाने वाली मशीनरी है जहाँ सच में व्यवस्था में बाधा आ रही हो. परन्तु अगर धारा 144 के उपयोग से स्पष्ट हो जाता है की हर एक सरकार ने अपने विरोधियों को चुप करने के लिए और ‘राइट तो प्रोटेस्ट’ को कुचलने के लिए इसका प्रयोग किया है . 144 के आदेश का सार्वजनिक रूप से न दिखाया जाना प्राकृतिक न्याय की अवधारणा का उल्लंघन है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निष्पक्षता और पारदर्शिता से मुक्त होना चाहिए। पक्षों को अपनी बात रखने के समान अवसर दिए जाने चाहिए और अदालत द्वारा लिए गए सभी कारणों और निर्णयों की जानकारी संबंधित पक्षों को दी जानी चाहिए।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि मजिस्ट्रेट को धारा 144 लागू करने से पहले वस्तुनिष्ठ सामग्री (objective material) पर भरोसा करना चाहिए और ऐसे आदेश की आवश्यकता को लिखित रूप में न्यायोचित ठहराना चाहिए। “शांति भंग होने की आशंका” जैसे व्यापक और अस्पष्ट औचित्य, बिना ठोस आधार के, अमान्य हैं। कानून की व्याख्या पर जोर देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने आनुपातिकता (proportionality) के प्रमुख सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित किया। धारा 144 का उपयोग केवल आपात स्थितियों के लिए है और इसे अनिश्चितकाल तक जारी नहीं रखा जा सकता। आदेशों में एक स्पष्ट समय सीमा होनी चाहिए और उनकी नियमित समीक्षा होनी चाहिए। प्रभावित पक्षों को धारा 144 के आदेशों के खिलाफ न्यायिक समीक्षा का अधिकार है।
न्यायपालिका ने लगातार यह माना है कि इस प्रावधान का दुरुपयोग सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संवैधानिक संतुलन को कमजोर करता है। यह धारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता के सबसे अधिक दुरुपयोग और राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले प्रावधानों में से एक है, जिसे नीति-आधारित विफलताओं को छिपाने और बड़े पैमाने पर जनता की आवाज़ को दबाने के लिए एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया है। मधु लिमाये, एक समाजवादी, को भी इस अधिनियम के तहत लक्षित किया गया था। यह एक ऐतिहासिक मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 144 एक निवारक और अस्थायी उपाय है, न कि एक दंडात्मक उपकरण। इसका उपयोग सावधानीपूर्वक सीमित होना चाहिए।
आपातकाल के दौरान, कई कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। लेकिन वर्तमान समय में स्थितियाँ पूरी तरह से अलग और असंगत रूप से अनुचित हैं। निवारक हिरासत (Preventive Detention), पब्लिक सेफ्टी एक्ट, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (Official Secrets Act), और धारा 144 जैसे प्रावधान औपनिवेशिक विरासत हैं, जिन्हें हम अभी भी अपने कंधों पर ढो रहे हैं। एन. रवि का इस विषय पर विचार यह है कि हर शासक वर्ग, जिसने विशाल जनता पर शासन किया और उनका दमन किया, उन्होंने पुराने समाज के उपकरणों को नए स्वरूप में उपयोग किया।
बीजेपी सरकार का मुख्य नारा “स्वदेशी” है, जिसमें आपराधिक कानून में नए संशोधन शामिल हैं। जब इस बिल को संसद में प्रस्तुत किया गया, तो हमारे गृह मंत्री ने गर्व से कहा कि हम औपनिवेशिक कानूनी व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनकी वास्तविक मंशा काफी अलग और छिपी हुई है।
‘कानून और व्यवस्था’ और ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ के बीच अंतर कार्यपालिका को एक अलग दिशा में ले जाने के लिए महत्वपूर्ण पहलू है। अदालत ने कई मामलों में, जिनमें मधु लिमाये बनाम उप-मंडल मजिस्ट्रेट भी शामिल है, यह स्पष्ट किया कि धारा-144 सीआरपीसी का उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था के मुद्दों को संबोधित करना है और केवल साधारण कानून और व्यवस्था की समस्याओं के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रावधान का उपयोग विरोध को दबाने या वैध सभा को रोकने के लिए करना असंवैधानिक है। फीस वृद्धि में कटौती की मांग न तो सार्वजनिक व्यवस्था का मामला है और न ही यह कानून और व्यवस्था की स्थिति है।
आपात प्रावधानों के बीच ऐसी प्रक्रियाएँ ऑस्टिन के सुप्त विचारों (dormant dreams of Austin) को जीवंत करती हैं, जो एक सकारात्मकतावादी (positivist) थे और जिन्हें पूरी दुनिया में बुर्जुआ वर्ग द्वारा सराहा गया है, ताकि राजनीति और अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रतिमानों में संप्रभुता की विचारधारा का समर्थन किया जा सके। इस एकतरफा दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है।
(निशांत आनंद कानून के छात्र हैं)