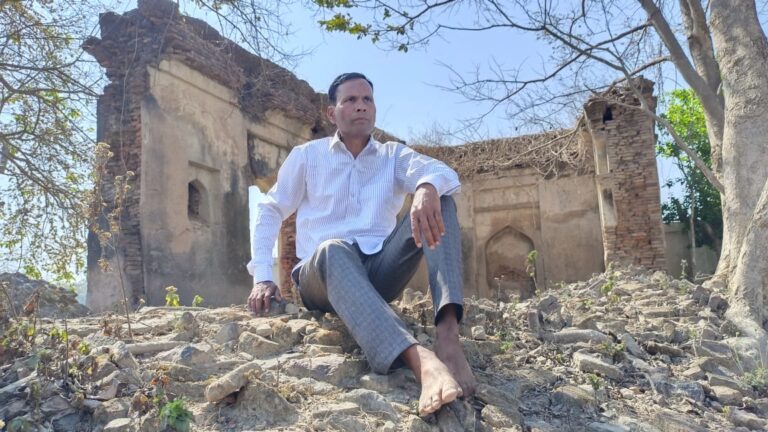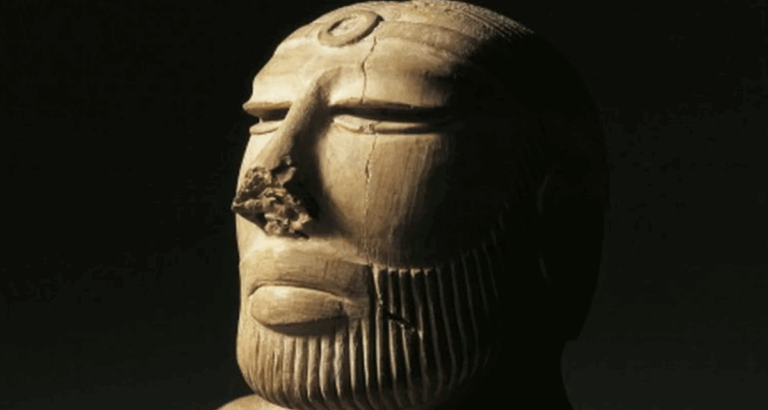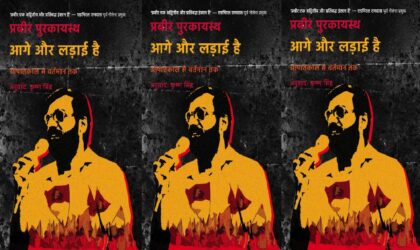बिला-शक, सुरजीत पातर (14 जनवरी 1945-11 मई 2024) हिन्दी साहित्य की दुनिया में समकालनीन पंजाबी कविता की पहचान बन गए थे। पिछले तीस सालों से मंगलेश डबराल जैसे हिन्दी के कई अग्रगण्य कवियों से उनके आत्मीय संबंधों का पता भी चलता है। भारतीय भाषाओं को दिए जाने वाले सरस्वती सम्मान (2009) जैसे कुछ पुरस्कारों से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। हिन्दी सहित भारतीय भाषाओं के मंचों पर उन्हें बार-बार समादृत किया जाता रहा था। भारतीय कविता के किसी भी समारोह में पंजाबी कविता का प्रतिनिधित्व करने वाले वे एक स्वाभाविक नाम रहे हैं।
हिन्दी में उनकी लोकप्रिय और सर्वमान्य छवि के निर्माण का अध्ययन करना दिलचस्प होगा। मूलभूत रूप से, वे ग़ज़लों और गीतों के रचनाकार रहे हैं। इनका हिन्दी अनुवाद असंभव नहीं तो कठिन ज़रूर बना रहता है। उनका समस्त काव्य-साहित्य भी अभी हिन्दी में अनुवादित नहीं हुआ है। 1980 के आसपास प्रकाशित पहल का तेरहवां अंक पंजाबी कविता पर फोकस था। इस अंक में लाल सिंह दिल, सुरजीत पातर, पाश, हरभजन हलवारवी, दर्शन खटकड़ जैसे कई युवा और प्रतिभावान पंजाबी कवियों की ढेर सी रचनाएं काफ़ी सुरुचिपूर्ण तरीक़े से छपी थीं। कहा जा सकता है कि हिन्दी पाठकीय अभिरुचि में उनके बड़े प्रवेश का वह सिंहद्वार था।
बाद के सालों में, हिन्दी काव्य प्रेमियों ने पाश को अपना नायक-कवि बना लिया। हिन्दी में पाश की अद्भुत प्रभावशीलता भी अध्ययन का विषय है। एक ऐसे वातावरण में सुरजीत पातर ने हिन्दी, भारतीय और वैश्विक मंच पर अपनी जगह बनाई, जबकि पाश हिन्दी में एक सजीव उपस्थिति की तरह बने रहे और हैं। जहां पाश की अभूतपूर्व पाठकीयता में उनकी दैहिक अनुपस्थिति का योगदान रहा होगा; वहां पातर के प्रति उमड़े प्रेम में उनकी दैहिक पहुंच ने अपनी भूमिका निभाई होगी। अपनी कविता में ही नहीं, अपने दैनंदिन स्वभाव में भी वे कोमलता, संवेदनशीलता, प्रेम, सामीप्य और मृदुभाषिता का अनुकरणीय उदाहरण थे।
एक प्रकार से, पातर को पाश का काव्यात्मक विलोम कहा जा सकता है। तरलता, सौन्दर्यपूर्ण भाषा, करुणापूर्ण गेयता और दार्शनिक अंदाज़ उनके काव्य और व्यक्तित्व का अभिन्न अंग थे। लगता है कि हिन्दी काव्य-ग्राह्यता में पाश जैसे आक्रामक और पातर जैसे विनम्र दोनों तरह के मिजाज़ पाने की आकांक्षा रही है। यह भी गौरतलब है कि सुरजीत पातर कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में पंजाबी के प्रोफ़ेसर थे। इस वृत्ति ने भी उनके व्यवहार में एक अतिरिक्त सामंजस्यपूर्णता और संतुलन को पैदा किया होगा। इस पृष्ठभूमि के साथ, उनमें एक वास्तविक सहजता और किसानी स्वभाव का संस्पर्श भी जुड़ा था।
पंजाबी के अधिकतर साहित्यकर्मियों की यह विशेषता रहती है। आप उनमें ठेठ ग्रामीण भाषा व्यवहार, देसीपन और दुविधारहित सहयोग भावना को देख सकते हैं। इसलिए सुरजीत पातर में प्रथम दर्जे की काव्य-रचना के साथ एक अपनापे और निर्बाध ताल्लुक़ का माहौल बना रहता था। इसीलिए मानवोचित व्यवहार के निरंतर क्षीणता के दौर में, उनके खोने की उदासी कहीं अधिक घनीभूत और विस्तृत है।
यह महत्वपूर्ण है कि हिन्दी कविता के मौजूदा प्रभावी संसार में छंदबद्ध रचना और उसका गेय पाठ लगभग बेदख़ल या द्वितीयक क्षेत्र का है। बावजूद इसके, इन्हीं विशेषताओं से युक्त सुरजीत पातर और उनका काव्य हिन्दी में अभिनंदनीय हो गया। पातर का कला-बोध उच्चतम श्रेणी का रहा है। हिन्दी की मुख्य आलोचनात्मक आंख कविता में सूक्ष्म व्यवहार को तरजीह देती रही है। पातर इस कसौटी पर फिट बैठते थे। यह भी जोड़ा जा सकता है कि उनकी शायरी के भीतर की मानवीयता और करुणा हिन्दी के उस काव्य-रुझान के अनुकूल थी जो सोवियत संघ के विघटन के उत्तर-काल में विकसित हुआ।
कविता के प्रकट वैचारिक चेहरे की जगह उसके इंसानी चेहरे की ओर रुख किया गया। अवधारणात्मक बड़बोलेपन और उत्साही नारेबाजी को निरुत्साहित किया गया। ये बातें कहीं आटे में नमक जैसी हो गयीं। कविता में मुखर राजनीतिक स्वर की जगह पर, दैनंदिन जीवन के विविध प्रसंगों और स्थानीय अनुभूतियों के बीच से, कवि सामाजिक सत्य को एक निजी भाषा में प्रकट करता नज़र आता है। एक नयी काव्य-ज़ुबान का विकास किया गया जो युगीन और अधिक समावेशी थी।
हिन्दी कविता के हाल के परिदृश्य में विनोद कुमार शुक्ल और मंगलेश डबराल इसके बेहतरीन उदाहरण कहे जा सकते हैं। इन सालों की हिन्दी कविता के इस चेहरे को उत्तर-सोवियतकालीन पूर्वी यूरोप की कविता के साथ जोड़ कर देखा जा सकता है। मिरोस्लाव होलुब (चेक गणराज्य, 1923-1998) और विस्लावा शिम्बोर्स्का (पोलेंड, 1923-2012) के नाम उल्लेख के तौर पर लिए जा सकते हैं। अपने कुल अर्थों में, सुरजीत पातर की कविता को हिन्दी कविता के इस नए स्वरूप की संगति में पढ़ा जा सकता है।
अवतार सिंह पाश (1950-1988) और लाल सिंह दिल (1943-2007) सामाजिक आंदोलनों के प्रमुख कवि बने। सुरजीत पातर आंदोलनों के बीच से उपजी व्यथा, उदासी, समझ और अधिक व्यवहारिक जीवन-बोध के कवि के तौर पर विकसित हुए। कविता के इस नए मार्ग की विषय-वस्तु ने भी शायद उनकी पाठकीयता और स्वीकार्यता को बढ़ावा दिया। पातर की काव्य-उपलब्धि छंद, गेयता और मर्मांतक भावों के कारण साहित्यिक परंपरा से जुड़े मन को भी भा जाती है। पातर जिस प्रकार की कविता लिखते थे, उसका श्रोता या पाठक पर बहुत लंबे समय तक असर रह सकता है: जैसे देर रात को सुनी गई किसी उचाट धुन का। यह बताने योग्य है कि पंजाबी जगत में उनकी काव्य-पंक्तियाँ और ग़ज़लों के शेर अलग-अलग अवसरों पर अक़्सर उद्धृत किए जाते रहे हैं।
पंजाबी के साथ हिन्दी में भी सुरजीत पातर की कमी को देर तक महसूस किया जाता रहेगा। वर्तमान में हम एक ऐसे काव्य-पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जहां काव्य-श्रेष्ठता किसी व्यक्तिगत प्रतिभा या एक कविता में पूरी तरह से अंतर्भूत नहीं हो पा रही है। न हिन्दी में, न पंजाबी में। अच्छे, चमक वाले कवियों की कमी नहीं है। पर, वहां पूरे युग या पूरे इतिहास की काव्य-आवश्यकता किसी एक कवि में संग्रहीत नज़र नहीं आती है। टुकड़ों में बिखरी है। उसे पूर्णता में तब्दील करने की कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं दिखती है। दूसरी ओर, पाठकों का एक बड़ा वर्ग अभी भी काव्य-विराटता की तलाश करता है। संभवत: पातर जैसे कवि उस अपेक्षा को पूरा करते हैं। ऐसे माहौल में, यह ग़ौरतलब होगा कि आने वाले सालों में पंजाबी संसार किन नये कवियों के नामों को हिन्दी साहित्यिक समाज को सौंपता है।
सुरजीत पातर अपनी रचनाशीलता में जिस क्लासिकी भव्यता को छूते रहते थे, वह अब कोई खो गई चीज़ जैसी लगती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस कारण से उन्हें आने वाले समय में भी ढूंढा जाता रहेगा। अन्य शब्दों में, यह भी कहा जा सकता है कि सुरजीत पातर उन पाठकों या श्रोताओं के कवि थे जो कुछ ढूंढते रहते हैं। इस वक़्त तो, व्यक्ति और कवि सुरजीत पातर के साथ हमारे संबंधों का एक लम्बा अध्याय अचानक-से बंद हो गया है।
(सत्यपाल सहगल का यह लेख समयांतर के जून 2024 अंक में प्रकाशित)