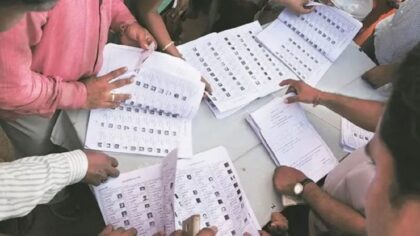डॉनल्ड ट्रंप ने सचमुच अगर यह सोचा होगा कि उनके राष्ट्रपति बनने के साथ ही अमेरिका के फिर से “महान बनने” की शुरुआत हो जाएगी, तो अब उन्हें यह जरूर अहसास हो रहा होगा कि वे एक बड़ी गलतफहमी का शिकार थे। बल्कि वह दिन बहुत दूर नहीं है, जब उन्हें यह अहसास होगा कि उनके आक्रामक रुख एवं मर्यादाविहीन तौर-तरीकों ने दुनिया में अमेरिकी रुतबे के ह्रास की रफ्तार और तेज कर दी है।
अमेरिका लगभग छह दशक तक दुनिया की प्रमुख एवं चुनौतीविहीन शक्ति के रूप में मौजूद रहा। उसके बाद ह्रास के लक्षण उभरने के बावजूद तकरीबन दो दशक और वह अपने रुतबे को कमोबेश बनाए रखने में कामयाब रहा। मगर 21वीं सदी के तीसरे दशक में वस्तुगत स्थितियों में हुए बदलाव से अप्रभावित रहना उसके लिए नामुमकिन होने लगा। कोरोना महामारी, यूक्रेन युद्ध, और गज़ा में अमेरिकी संरक्षण में इजराइली मानव संहार ने उसकी आर्थिक एवं सैनिक शक्ति की सीमाओं को और स्पष्ट कर दिया। साथ ही उसकी ये छवि भी नष्ट हुई कि वह दुनिया में किन्हीं अच्छाइयों का प्रतिनिधि और संरक्षक है।
इतिहास का तजुर्बा है कि किसी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय सत्ता के टिकाऊ होने के लिए जितनी अनिवार्यता हार्ड पॉवर की होती है, उतना ही सॉफ्ट पॉवर भी जरूरी होता है। अमेरिकी रुतबे का आधार उसका सर्व-प्रमुख आर्थिक महाशक्ति होना और सैनिक ताकत में बेजोड़ होना था। यह उसका हार्ड पॉवर था। मगर इसके साथ ही अपने प्रचार तंत्र से अमेरिका विश्व जनमत के दिमाग में यह बैठा सकने में भी वह कामयाब था कि वह ना सिर्फ लोकतंत्र, मानव अधिकारों और सामाजिक- सांस्कृतिक खुलेपन का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि वह इन मूल्यों का संरक्षक भी है। यह अमेरिका का सॉफ्ट पॉवर था।
आज दुनिया में आम नैरेटिव अमेरिका के ह्रास का बना है, तो उसके पीछे वजह उसके इन दोनों पॉवर में लगी सेंध है। बेशक, इसके लिए डॉनल्ड ट्रंप दोषी नहीं हैं। बल्कि हकीकत तो यह है कि ट्रंप (या ट्रंपिज्म) उस ह्रास की लंबी परिघटना से पैदा हुई परिस्थितियों का परिणाम हैं। आर्थिक, सैनिक, एवं देश की नैतिक सत्ता ह्रास के कारण अमेरिकी आवाम के बड़े हिस्से में वो असंतोष फैला, जिसके परिणामस्वरूप ट्रंप का ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ का नारा इस हद तक लोकप्रिय हो पाया। इस नारे ने उन लोगों को आकर्षित किया, जिन्हें यह महसूस होता था कि अमेरिका की ‘महानता’ के वे दिन चले गए, जब देश में सुख-समृद्धि फैली थी और दुनिया में उनके देश का सिक्का चलता था।
अब इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि उन पुराने ‘अच्छे’ दिनों को लौटाने के जिस नेता पर अमेरिकी आवाम ने भरोसा किया, वह अमेरिका के क्षय को और गति देने का माध्यम बन गया है। अपने दूसरे कार्यकाल के लिए ह्वाइट हाउस में ट्रंप के आए अभी बमुश्किल ढाई महीने हुए हैँ। बेशक, किसी नेता के योगदान के मूल्यांकन के लिहाज से यह बहुत छोटी अवधि है। इसके बावजूद कुछ चीजें और दिशा इतनी स्पष्ट हो चुकी हैं कि उनके मद्देनजर कम-से-कम फ़ौरी निष्कर्ष तो निकाले ही जा सकते हैं।
इस दौर में क्या हुआ है, इसे कुछ खास बिंदुओं पर गौर करते हुए समझा जा सकता है। इनमें पहला मुद्दा व्यापार युद्ध का है, जिसका प्रमुख पहलू टैरिफ वॉर (आयात शुल्क युद्ध) है। गौर करने की बात है कि ट्रंप का टैरिफ वॉर उन देशों के मामले में अधिक प्रासंगिक नहीं है, जिन्हें अमेरिका अपना शत्रु या प्रतिद्वंद्वी मानता है। उन देशों के खिलाफ तो अमेरिकी प्रतिबंधों और उच्च आयात शुल्क लगाने का सिलसिला अब काफी पुराना हो चुका है। इसलिए ट्रंप के नए टैरिफ वॉर से रूस, ईरान, उत्तर कोरिया या वेनेजुएला जैसे देशों पर तो कम ही प्रभाव पड़ेगा। चीन पर भी सीमित असर ही होगा, क्योंकि उसके खिलाफ अमेरिका व्यापार और तकनीकी युद्ध ट्रंप के पहले कार्यकाल से लेकर लगातार आगे बढ़ा है और इस वजह से चीन ने कुछ खास तैयारियां कर रखी हैँ।
ट्रंप का टैरिफ वॉर मसल में अमेरिका के सहयोगी, दोस्त या उन देशों के लिए कहर लेकर आया है, जिनसे उसके रिश्ते अच्छे रहे हैं। दुनिया में मौजूदा उथल-पुथल उन देशों से अधिकतम वसूली करने के ट्रंप के नजरिए से पैदा हुई है। ट्रंप प्रशासन के रुख ने उनमें से ज्यादातर देशों को जवाबी कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। इन देशों में उफान मारती भावनाओं की बेहतर अभिव्यक्ति कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कॉर्नी के इन शब्दों में हुई- ‘अमेरिका के साथ आर्थिक एकीकरण को गहरा तथा सुरक्षा एवं सैनिक संबंधों को मजबूत करने के आधार पर हमारा पुराना रिश्ता टिका था। लेकिन अब वह समाप्त हो गया है।’
कभी सोचना कठिन था, लेकिन यह आज की हकीकत है कि कनाडा के अलावा यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, मेक्सिको आदि देश अमेरिका को जवाब देने की बात कर रहे हैं। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) ने 31 मार्च को अमेरिकी व्यापार के रास्ते में विभिन्न देशों में खड़ी कई गईं टैरिफ एवं नॉन टैरिफ बाधाओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने जो कहा, उस पर ध्यान दीजिएः ‘रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया को लेकर तीन चिंताएं जताई गई हैं। एक है हमारी नई सौदेबाजी संहिता, दूसरा है दवा उद्योग, एवं तीसरा जैव-सुरक्षा है। लेकिन इन मुद्दों पर कोई बातचीत संभव नहीं है। कम-से-कम मेरे सत्ता में रहते हुए तो ऐसा नहीं होगा।’
दक्षिण कोरिया के उद्योग मंत्री ने कहा कि स्थिति का निकट विश्लेषण करते हुए उचित जवाब दिया जाएगा। और क्या अभी हाल के वर्षों तक यह सोचना संभव था कि जापान और दक्षिण कोरिया अमेरिका के खिलाफ चीन के साथ मिल कर मोर्चाबंदी करेंगे? मगर इतनी खबर तो पुष्ट है कि तीनों देशों के व्यापार मंत्रियों ने टैरिफ वॉर के मद्देनजर आपस में राय-मशविरा किया है।
उधर यूरोपियन यूनियन से खबर आई कि वहां अमेरिकी व्यापार युद्ध का मुकाबला करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है। यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उरसुला वॉन डेर लियेन ने कहा- ‘अमेरिका से हम मजबूत रुख रखते हुए बात करेंगे। हमारे पास भी बहुत सारे पत्ते हैं। व्यापार से लेकर टेक्नोलॉजी तक हमारे पास बड़ा बाजार है। वैसे शक्ति दृढ़ जवाबी कदम उठाने के संकल्प से निर्मित होती है। हम हर विकल्प को आजमाएंगे।’
(https://www.politico.eu/article/eu-tariffs-counter-strike-big-tech-us-banks-donald-trump/)
ऐसी सख्त भाषा उन देशों में बोली गई है, जो अपनी सुरक्षा और विदेश नीति के लिए काफी हद तक अमेरिका पर निर्भर रहते आए हैं। लेकिन आज वे आंख मूंद कर अमेरिकी फरमान का पालन करने को तैयार नहीं हैं। क्या यह अमेरिकी रुतबे में गिरावट का सबूत नहीं है? क्या इससे यह जाहिर नहीं होता कि ट्रंप काल में अमेरिका किस तरह अलग-थलग पड़ता चला जा रहा है?
और नजर अमेरिका के प्रतिद्वंद्वी देशों की ओर ले जाएं, तब तो ह्रास की कहानी और स्पष्ट हो जाती है। ट्रंप ने सत्ता में आते ही पनामा नहर पर खास निशाना साधा। आरोप लगाया कि पनामा ने नहर को चीन के हाथों सौंप दिया है। असलियत यह है कि हांगकांग की कंपनी हचिंसन के पास पनामा नहर पर स्थित बंदरगाह के संचालन का ठेका है। ट्रंप प्रशासन ने दबाव बनाया, तो हचिंसन ने यह ठेका अमेरिकी कंपनी ब्लैकरॉक को बेचने का सौदा कर लिया। इसे ट्रंप की बड़ी जीत के रूप में देखा गया।
लेकिन वह कहानी का सिर्फ एक अध्याय था। अगला अध्याय बीजिंग में लिखा गया। चीन सरकार ने इस सौदे की समीक्षा का एलान किया और इसके अमल पर रोक लगा दी। समीक्षा इस आधार पर की जा रही है कि क्या सौदा निष्पक्ष तरीके से हुआ और क्या इससे चीन के राष्ट्रीय हित पर आंच आएगी? सार यह कि चीन ने अमेरिका की मंशा पर फिलहाल पानी फेर दिया है। जाहिर है, चीन कहीं से ट्रंप या अमेरिका से भयभीत नजर नहीं आया है। इसकी अनेक दूसरी मिसालें भी हैं।
वैसे निगाह टकराव के अन्य क्षेत्रों की ओर ले जाएं, तो वहां से भी वही संकेत मिलता है कि प्रतिद्वंद्वी या शत्रु देश ट्रंप की आक्रामकता से तनिक भी नहीं डरे हैं। बल्कि ट्रंप ने उन देशों के करीब आने की प्रक्रिया और तेज कर दी है।
ट्रंप ने ईरान को संदेश भेजा कि वह बातचीत की मेज पर आए, अपने परमाणु कार्यक्रम पर नया समझौता करे, वरना अमेरिका उस पर हमला बोल देगा। ईरान ने इस प्रस्ताव को दो टूक ठुकरा दिया। कहा धमकी और दबाव में वह कोई बातचीत नहीं करेगा। इससे खफा ट्रंप ने ईरान पर बमबारी की धमकी दी है। मगर खबर है कि वैसा होने पर जवाब देने की ईरान ने अपनी तैयारियां की हैं। इस बीच रूस की तरफ से आई ये चेतावनी महत्त्वपूर्ण है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने का दुस्साहस ना करे- इसके बहुत भयानक परिणाम होंगे।
ट्रंप का वादा था कि राष्ट्रपति बनने के 24 घंटों के अंदर वे यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे। इसके लिए उन्होंने हाथ-पांव भी खूब मारे हैं। हर तरकीब अपनाई है। लेकिन नतीजा क्या है, यह पिछले हफ्ते खुद उनके बयानों से जाहिर हुआ। ट्रंप ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन युद्धविराम के लिए उनकी बात नहीं मान रहे हैं और इससे वे बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने धमकी दी कि वे रूस पर और सख्त प्रतिबंध लागू कर सकते हैं। जिस टीवी इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही, उसी में उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदीमीर जेलेन्स्की अपने देश के खनिज पदार्थों को अमेरिका को देने के अपने वादे से मुकर रहे हैं। ट्रंप ने धमकी दी कि ऐसा करके जेलेन्स्की अपने लिए बड़ी मुश्किलों को न्योता दे रहे हैँ।
एक अन्य मोर्चा फिलस्तीन के गजा में लड़ाई का है। बेशक, यह ट्रंप की सफलता थी कि ह्वाइट हाउस में प्रवेश के पहले ही उन्होंने वहां युद्धविराम लागू करवा दिया। मगर इजराइल वो युद्धविराम अब तोड़ चुका है और रोजमर्रा के स्तर पर वहां मानव संहार में जुटा हुआ है। उधर इस समस्या के हल के लिए जो सुझाव ट्रंप ने पेश किए, उसे अरब एवं मुस्लिम देश ठुकरा चुके हैं। उनमें वे देश भी शामिल हैं, जिनकी छवि अमेरिका का अधीनस्थ होने की है। गौरतलब है कि गजा में मानव संहार को संरक्षण देना अमेरिकी सॉफ्ट पॉवर के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ है।
ट्रंप का एक और एजेंडा डेनमार्ग के स्वशासी क्षेत्र ग्रीनलैंड पर कब्जे का है। इसे आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने उप-राष्ट्रपति जे.डी. वांस को ग्रीनलैंड भेजा भी। मगर बात कहीं आगे नहीं बढ़ी। ना तो डेनमार्क अमेरिकी मंशा को स्वीकार कर रहा है, ना ग्रीनलैंड के लोग इसके लिए तैयार हैं। ग्रीनलैंड में चुनाव के बाद नई गठबंधन सरकार बनी है। वहां के नए प्रधानमंत्री ने एलान किया है कि अमेरिकी दबाव के खिलाफ ग्रीनलैंड एकजुट रहेगा।
तो प्रश्न है कि ट्रंप की सुन कौन रहा है?
संभवतः भारत या ऐसे कुछ देश अपवाद हो सकते हैं, जहां ट्रंप के एजेंडे का जवाब देने की बात लोगों के मन में आई तक नहीं है। मगर बाकी दुनिया में ट्रंप को हर जगह ठोकर खानी पड़ रही है। बहरहाल, इसे ट्रंप को ठोकर के रूप में देखना परिदृश्य को संकुचित करना होगा। नेता की हैसियत देश की ताकत से बनती है। ट्रंप के एजेंडे को आज अगर अमेरिका के सहयोगी रहे देश भी भाव नहीं दे रहे हैं, तो उसका कारण परिदृश्य में आया मूलभूत परिवर्तन है। यह अमेरिका के हार्ड एवं सॉफ्ट पॉवर में आई गिरावट का संकेत है। यह दुनिया बदले शक्ति संतुलन का नतीजा है। ट्रंप का योगदान बस इतना है कि जो सूरत बन चुकी थी, उन्होंने उसे दुनिया के सामने ला दिया है।
(सत्येंद्र रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिल्ली में रहते हैं)