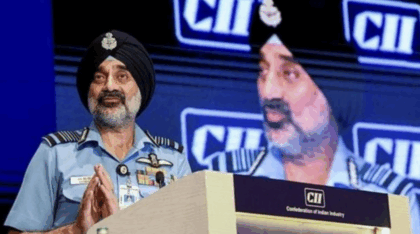हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राजनीतिक विशेषज्ञ और विश्लेषक के साथ साधारण लोगों को भी भरपूर चौंकाया है। राजनीतिक दलों के लिए तो इन नतीजों में राजनीतिक संदेश है ही, समतामूलक समाज व्यवस्था के आग्रही नागरिक समाज के लिए भी इस में कुछ गंभीर संदेश है।
क्या हैं वे संदेश? संदेश और संकेत पढ़ने-समझने के लिए राजनीतिक पृष्ठ-भूमि को याद किया जाना जरूरी है।
लोकसभा 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट गई थी। 543 के सदन में बहुमत का जादुई आंकड़ा 272 है।
यह ठीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा नहीं हासिल कर पाई, लेकिन यह कोई बहुत ही छोटी संख्या भी नहीं है। बहुमत भले न मिली हो, लेकिन संसद में सबसे बड़ा दल तो वह अब भी बनी ही हुई है।
भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक के फैसले के पहले ही नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की बैठक में अपने प्रधानमंत्री बनाये जाने का समर्थन तो जुटा ही लिया।
लगातार दो बार भारतीय जनता पार्टी को मिले पूर्ण बहुमत के साथ और तीसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के घटक दल के समर्थन के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गये।
मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के नेता एन चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के समर्थन पर सरकार चल रही है।
‘पलटू राम’ के नाम से अभिहित किये जानेवाले नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) से बाहर हो गये थे।
उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को छोड़ा है।
उन्होंने विपक्षी गठबंधन बनाने की राजनीतिक पहल की। विपक्षी गठबंधन (इंडिया अलायंस) बन भी गया। इंडिया अलायंस के अघोषित संयोजक के रूप में उन्होंने कारगर भूमिका भी निभाई। लेकिन बीच में वे इंडिया अलायंस में असहज महसूस करने लगे।
जिस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और दुस्साशन को उखाड़ फेंकने के लिए वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) से बाहर हुए थे, उसी के शासन को मजबूत बनाने की भूमिका निभाने वे एनडीए में शामिल हो गये! बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी को ‘अकेले दम’ बहुमत नहीं मिला।
सरकार बनाने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के पास जरूरी संख्या थी। ‘अकेले दम’ पर न सही लेकिन तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में नरेंद्र मोदी सफल हो गये। यह कोई कम बड़ी बात नहीं है।
भारत के संसदीय इतिहास में यह दूसरा ही मौका है कि कोई नेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। इसके पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला था।
सहयोगियों के बल पर चल रही सरकार को ‘कमजोर’ सरकार माना जाने लगा। इस सरकार की ‘कमजोरी’ दिखने भी लगी। भारत में सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार बनने-चलने का यह कोई पहला अवसर नहीं है। सहयोगी दलों की सरकार को ‘मजबूर सरकार’ कहा जाता रहा है।
माननीय कांशीराम तो लोकतांत्रिक दृष्टि से ‘मजबूर सरकार’ को ‘मजबूत सरकार’ से बेहतर मानते थे। नरेंद्र मोदी ने सरकार तो बना ली, लेकिन ‘अकेले दम’ पर सरकार बनाने-चलाने को अभ्यासी नरेंद्र मोदी के गुरूर के लिए यह बड़ा भावनात्मक झटका था।
राम मंदिर बनाने के दंभ, खुद के अवतारी होने के भ्रम पसार कर राजनीति के अंतर्गत ‘अब की बार, चार सौ पार’ के नारे के साथ चुनाव में उतरने के कारण भी यह झटका भावनात्मक रूप से बड़ा बन गया।
भारत की संसदीय राजनीति में भावनात्मक और नैतिक झटकों का क्या महत्व हो सकता है; भावनाएं वैसे भी बहुत अस्थिर होती हैं और नैतिकता को संविधान से बाहर निकालकर किसी अन्य संदर्भ-ग्रंथ का हिस्सा बना दिया गया है। फिलहाल, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार चल रही है।
भारतीय जनता पार्टी कोई सामान्य पार्टी नहीं है। यह राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ की गढ़ी राजनीतिक पार्टी है। महात्मा गांधी जैसे नेता की हत्या की आरोपी रह चुकी है। यह आरोप निराधार नहीं था।
राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ की विचारधारा भारत की आजादी के आंदोलन के विचारधारात्मक मूल्यों से न केवल भिन्न, बल्कि बिल्कुल विपरीत रही है। भारत के संविधान में मुख्य रूप से आजादी के आंदोलन के दौरान अर्जित मूल्य-बोध और नैतिक-दृष्टि को स्वाभाविक तौर पर जगह मिली।
इस मूल्य-बोध के सिर्फ नैतिक-दृष्टि का बनाव भारतीय अनुभवों से न बनकर दुनिया भर के अनुभवों के सहयोजन-संयोजन और सम्मानजनक समायोजन से बना था।
भारतीय अनुभव में भी उन तत्वों को जगह मिली थी, जिन का मौलिक संबंध बौद्ध संदर्भ से था। ये वही बौद्ध संदर्भ हैं जिनका संघर्ष शोषण एवं भेद-भावमूलक वर्ण-व्यवस्था पर आधारित समाज व्यवस्था अंतर्गत सामंतवाद और पुरोहितवाद के पारस्परिक समर्थन से खड़ी आडंबर-प्रधान धार्मिक संरचना से था।
इतिहास में इसे मोटे तौर पर ब्राह्मण-बौद्ध संघर्ष के रूप में समझा जाता है। एक बात यह ध्यान रखना जरूरी है कि जीवन में, इसलिए धर्म में भी कुछ हद तक सामंती स्वभाव, भेद-भाव, पुरोहिती लक्षण, शोषण, आडंबर आदि के लिए थोड़ी-बहुत जगह का बने रहना भिन्न बात है।
और उस जगह के बने रहने के औचित्य प्रतिपादन का सिद्धांत बनाना और अपनाना बिल्कुल भिन्न बात है। इस भिन्नता और विरोधिता पर नजर बनाये रखना जरूरी है, बल्कि बहुत जरूरी है।
असल में हिंदुत्व का लगाव हिंदू धर्म की मान्यताओं या धार्मिक आचरणों में न के बराबर है। हिंदुत्व का एक-निष्ठ लगाव हिंदू की राजनीतिक सत्ता से है।
हिंदू की राजनीतिक सत्ता का आशय क्या है? साफ-साफ कहा जाये तो हिंदू की राजनीतिक सत्ता का आशय वर्ण-व्यवस्था के राजनीतिक समर्थन और जो वर्ण-व्यवस्था के बाहर ठहरते हैं उनके राजनीतिक विरोध का है; बहिष्करण की हद तक का विरोध। शायद ही इसका कोई अन्य आशय हो।
बौद्ध, जैन, सिख, सरना (आदिवासी) आदि धर्म को माननेवाले भी वर्ण-व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन हिंदुत्व की राजनीति की ‘पितृ-भूमि’ और ‘पुण्य भूमि’ की अवधारणा के अनुसार भी बौद्ध, जैन, सिख, सरना आदि की ‘पितृ-भूमि’ और ‘पुण्य भूमि’ भारत ही है।
वह भारत जहां संवैधानिक लोकतंत्र है। बौद्ध, जैन, सिख, सरना आदि के बारे में हिंदुत्व की राजनीति के लिए कोई सीधी और साफ तौर पर दिख जानेवाली विभाजक रेखा खींचना चुनावी राजनीति के अनिवार्य नुकसान का कारण बन सकता है। सीधी और दिखनेवाली न सही, वक्र और गुप्त विभाजक रेखाएं तो खींची ही रहती है।
समतामूलक समाज व्यवस्था के किसी भी रूप का कोई भी पक्षधर, चाहे वह हिंदुत्व की राजनीति के संदर्भ से ‘हिंदू’ ही क्यों न हो, वर्ण-व्यवस्था पर आधारित भेद-भावमूलक समाज व्यवस्था के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता है।
बौद्ध-धर्म और बौद्ध-दर्शन वर्चस्ववादी हिंदुत्व की राजनीति का सबसे बड़ा अवरोध है, इसलिए ऐतिहासिक रूप से ‘बौद्ध विचार’ के साथ जो संघर्ष ‘ब्राह्मण विचार’ का रहा है, वही संघर्ष अब संविधान-सम्मत शासन और हिंदुत्व की राजनीति के संघर्ष के रूप में सतह पर है।
हिंदुत्व की राजनीति भारत के हर पराभव के लिए बौद्ध-विचार पर दोष मढ़ती आई है। समझ में आने लायक बात है कि क्यों अशोक, आंबेडकर बौद्ध-धर्म का रास्ता लेते हैं, पूरा-का-पूरा संत साहित्य बौद्ध-विचार और बौद्ध-मूल्य-बोध से ओतप्रोत रहा है।
व्यक्ति की कई आदिम प्रवृत्तियां मानव समुदाय और सभ्यता की संरचना के प्रतिकूल होती हैं। आदिम प्रवृत्तियों का व्यक्ति के मौलिक स्वभाव से समूल नाश संभव नहीं होता है। इस अर्थ में व्यक्ति और सभ्यता की संरचना में एक टकराव बना रहता है।
सवाल सिर्फ सभ्यता विरोधी आदिम प्रवृत्तियों के आधार पर कुछ व्यक्तियों के समूह के संगठित प्रयास और सभ्यता के पक्ष में व्यक्तियों या समूह के विरुद्ध कुछ व्यक्तियों या समूह के संगठित प्रयास में संतुलन का है।
इन दोनों ही पक्ष के प्रयासों में संतुलन का संघर्ष जारी रहता है। वर्ण-व्यवस्था में वर्चस्ववादी सामाजिक-समूह का पक्ष ब्राह्मणवाद रचता है और इस ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ बौद्ध विचार शुरू से संघर्षशील रहा है।
ध्यान रखने की बात यह है कि आदिम प्रवृत्तियों से पूर्ण मुक्त कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। महत्वपूर्ण है आदिम प्रवृत्तियों पर नियंत्रण की प्रभावी मात्रा जिससे व्यक्ति की चारित्रिक विशिष्टताएं प्रभावित और परिभाषित होती हैं।
राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ का विचारधारात्मक लगाव वर्ण-व्यवस्था आधारित समाज व्यवस्था से ही रहा है, आज भी है। राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ के विचारधारात्मक लगाव के प्रति राई-रत्ती सम्मान भारत के संविधान में नहीं है।
संविधान परिषद की सभाओं में इन मुद्दों पर बहुत गंभीर चर्चा हुई थी। संविधान परिषद की सभाओं में विचार-विमर्श के प्रयोग और विवेक-पूर्ण पराक्रम को बिना किसी पूर्व-आग्रह के देखा जाये तो मोटे तौर पर तीन श्रेणियां बन सकती हैं।
पहली श्रेणी, वह जो बहुत पुरानी शैली इस्लाम और मुसलमान के आगमन के पहले ब्राह्मण युग की समाज व्यवस्था की तरफ बढ़ना चाहते थे। उनके अनुसार यही वह समय था जब भारत ‘सोने की चिड़िया’ था।
दूसरी श्रेणी, वह जो बौद्ध मूल्य-बोध के आधार पर सामाजिक संरचना का पुनर्गठन चाहते थे। उनके अनुसार समतामूलक मानवतावादी समाज व्यवस्था को इसी पुनर्गठन के माध्यम से हासिल किया जा सकता है।
तीसरी श्रेणी वह, जो ब्राह्मण-बौद्ध दोनों के सार्थक मूल्य-बोध को आत्मसात कर उनसे आगे निकलते हुए आधुनिक, समतामूलक और प्रगतिशील समाज व्यवस्था कायम करना चाहते थे।
बन रही नई विश्व-व्यवस्था में यह तीसरी श्रेणी सब से अधिक उपयुक्त थी। बन रही इस नई विश्व-व्यवस्था की तरफ हल्का इशारा करना यहां जरूरी है।
भारत की आजादी के आंदोलन के दौर की चार बड़ी घटनाओं को संदर्भ में लेने से उस बन रही नई विश्व-व्यवस्था की झलक जरूर दिख सकती है।
औद्योगिक क्रांति, सोवियत संघ का अस्तित्व में आना, फासीवाद की जकड़न और दो-दो विश्व-युद्ध का होना। हां। निश्चित ही, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना और संबंधित विश्व संस्थाओं को भी बन रही नई विश्व व्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक मानने से इनकार नहीं किया जा सकता है।
आजादी के आंदोलन के प्रतीक महात्मा गांधी जिस नैतिक-लोकतंत्र की बात करते थे। उस नैतिक-लोकतंत्र की तात्विक अवधारणा पहली श्रेणी के अधिक निकट थी।
इस नैतिक-लोकतंत्र के मूल में यह विश्वास सक्रिय था कि शोषण करनेवाला शोषित होनेवाले की सहन सीमा का उल्लंघन न करे। शोषक को चाहिए कि शोषण के वक्त ईश्वर का ध्यान रखे और ‘आध्यात्मिक चेतना’ को जागृत रखे।
तदनुसार, शोषण की पीड़ा का एहसास अपने अंदर भी जिंदा रखे और शोषित के पक्ष में हृदय परिवर्तन की नैतिकता तक बढ़ने की कोशिश करे। दूसरी ओर शोषित अपनी सहन सीमा को बढ़ाने के लिए ईश्वर की प्रार्थना करे और ‘आध्यात्मिक शक्ति की अनुभूति’ के सहारे शोषक या शोषण के प्रति बिना किसी आक्रोश के ईश्वरीय न्याय पर भरोसा रखे।
दुख के कारणों को समाप्त करने के लिए नहीं, दुख सहने की शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करे! इस अवधारणा में शोषण, शोषक, शोषित के संबंध और व्यवहार का नैतिक आधार ईश्वर, ईश्वरीय न्याय और ‘आध्यात्मिक चेतना’ के संदर्भ से परिभाषित है। इस अवधारणा में कहीं-न-कहीं ‘इस लोक’ से अधिक ‘उस लोक’ की चिंता रहती है।
इस विचार में दूसरों की दी हुई पीड़ा और आत्म-पीड़न को अध्यात्म से जोड़ने की आकांक्षा साफ-साफ पढ़ी जा सकती है। वापस ली जा चुकी किसी किताब में ‘मैला ढोनेवालों की ‘आध्यात्मिक अनुभूति’ में ‘कर्म-योग’ का रहस्य ढूंढने के दुस्साहस को याद किया जा सकता है।
महात्मा गांधी की ‘वैचारिक आत्मा’ राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ की विचारधारा के अधिक करीब थी, लेकिन उनका ‘राजनीतिक शरीर’ कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ था। राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ की विचारधारा से प्रभावित लोगों ने महात्मा गांधी के ‘उस राजनीतिक शरीर’ की तो हत्या कर दी, लेकिन वे महात्मा गांधी की ‘वैचारिक आत्मा’ को न अपना सके।
महात्मा गांधी और बाबासाहेब के ऐतिहासिक तर्क-वितर्क में उनके विचारों के दृष्टि-कोण और राजनीतिक रास्ते की रैखिकता की पहचान की जा सकती है।
पहली श्रेणी के आग्रह में अधिक वैचारिक कट्टरता थी। कट्टरता और प्रतिबद्धता में जहर और दवा का अंतर होता है। दूसरी और तीसरी श्रेणी में वैचारिक कट्टरता नहीं थी, हां प्रतिबद्धता जरूर थी। इन दोनों श्रेणियों में संवाद और समझौता का रास्ता खुला था।
संविधान परिषद की सभाओं में फैसला बहुमत के बहुसंख्यक दबाव से नहीं तर्क-वितर्क की ताकत से होता था। इस मामले में किसी भी अर्थ में कोई कहीं एक-आध अपवाद खोज ही सकता है।
संविधान परिषद में सिर्फ राजनीतिक दलों प्रतिनिधि ही शामिल नहीं थे, राज-रजवाड़ों के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि भी शामिल थे, जिनमें कई शास्त्रज्ञ पंडित भी थे।
औद्योगिक क्रांति के साथ नगर केंद्रीक उत्पादन और विपणन का दौर शुरू हो गया। ब्रिटिश राज में ग्राम-उद्योग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। बड़ी-बड़ी मशीनों और बड़े-बड़े उत्पादन केंद्र का जमाना सामने था।
जाहिर है कि औपनिवेशिक शासन से मुक्त होने के साथ ही भारत के सामने द्वंद्व था! पुरानी और नई जीवन शैली का द्वंद्व! हमारे पुरखों ने पुरानी शैली के जीवंत तत्वों को संजोकर नई जीवन शैली की राह पर कदम बढ़ाने का फैसला किया।
संविधान परिषद ने भरसक कोशिश की कि ऐसे संवैधानिक प्रावधान किये जा सकें कि भारत की विभिन्न संस्कृतियों के अंतर्विरोधों को यथार्थ की धरातल पर उतारकर उनके बीच समरस-सामंजस्य और सहिष्णु संबंध संविधान के दायरे में समा जाये।
ऐसा प्रयास करते समय हमारे पुरखों को इस बात का भरपूर एहसास था कि संवैधानिक प्रावधानों का तब तक कोई सार्थक और उत्साहवर्धक नतीजा नहीं निकल सकता है, जब तक कि संवैधानिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र का समर्थन न हासिल हो जाये।
लोकतंत्र एक जीवनयापन शैली के रूप में तभी कारगर हो सकता है जब संवेदनशील तरीके से संविधान का प्रावधान सामाजिक आचरण का स्वाभाविक आग्रह बन जाये। संविधान के प्रावधान शासन की कथनी भर है, करनी को सरकार के आचरण में लक्षित होना चाहिए।
कथनी और करनी में अंतर, यानी मन वचन आचरण की भिन्नता और विरुद्धता हमारी समस्याओं के मूल में पहले से ही रही है। इस तरह की भिन्नता और विरुद्धता के चलते कई भारी विपत्तियों से भारत के लोकतंत्र का सामना होता रहा है।
एक विपत्ति है, ‘पुराने भारत देश’ और ‘आधुनिक भारत राष्ट्र’ में सामंजस्य विकसित न हो पाना! ‘देश’ अपनी सामाजिक मान्यताओं, रीति-रिवाजों के अनुसार चलता रहा संविधान और कानून की बात जमीन ही नहीं पकड़ पाई; ‘राष्ट्र’ बेखबर बना रहा।
यहां इस कठोर और कटु यथार्थ को याद करना ही होगा कि ‘मान्यताओं और रीति-रिवाजों’ में वास्तविक तात्पर्य-पूर्ण भेद-भावमूलक समाज व्यवस्था का, लगभग बेरोक-टोक, जारी रहना।
बाबासाहेब को इस स्थिति का अनुमान था। उनकी चिंताओं को यहां याद किया जा सकता है; अच्छे से अच्छा संविधान बुरे हाथ में पड़कर बुरा बन जा सकता है और यह कि राजनीति में हम समान वोट-शक्ति पर चलते रहेंगे और साथ ही समाज में भेद-भावमूलक समाज व्यवस्था और विषमतामूलक अर्थ-नीति पर भी चलते रहेंगे।
शासन, समाज और कारोबार में बहुत अंतर्विरोध और अंतर्घात हमारे राष्ट्रीय चरित्र को विष-वृक्ष के रूप में विकसित कर देगा।
यह सच है कि गांवों को एक बदबूदार संकीर्णता का गड्ढा और अज्ञान, अंधविश्वास, संकुचित दृष्टिकोण और सांप्रदायिकता की अंधेरी गुफा कहने के चलते संविधान परिषद की सभा में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का भारी विरोध हुआ।
विरोध के बावजूद गांव की इस यथार्थ स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता था। विरोध करनेवालों का कहना था कि संविधान की संरचना ‘उल्टे पिरामिड’ की नहीं, ‘सीधे पिरामिड’ की तरह हो। यह बात बाबासाहेब भी समझते थे कि सिर्फ गांव का यथार्थ ही सच नहीं है, बल्कि गांव भी सच है।
स्वायत्त शासन के रूप में पंचायती व्यवस्था की संवैधानिक आकांक्षा को महत्व दिया गया, लेकिन इसे ठीक-ठीक लागू करना संभव न हो सका तो इसके अन्य कारणों में से कुछ वह कारण भी जरूर चिह्नित किये जा सकते हैं, जिनका इशारा बाबासाहेब ने संविधान परिषद की सभा में किया था।
राजीव गांधी ने उस दिशा में जो प्रयास किया वह भी पूर्ण रूप से कारगर साबित नहीं हुआ। यह सच है कि कांग्रेस इस दिशा में अपने-आप कोई बड़ी पहल नहीं कर सकी। सफलता की ओर बढ़ते संघर्ष के दौरान थकान का असर सफलता के बाद होता है; कई बार यह असर सफलता की बड़े हिस्से को निष्फल भी बना देता है।
यह समझ में आने लायक बात है कि कांग्रेस की विभिन्न सरकारों ने संविधान के कई लोक कल्याणकरी प्रावधानों को लागू करने कि दिशा में वैसा प्रयास नहीं किया जैसे प्रयास की उम्मीद कांग्रेस से थी। गैर-कांग्रेसवाद का आह्वान करनेवाले डॉ राममनोहर लोहिया के नेतृत्व में समाजवादी आंदोलन की लंबी कतार खड़ी हो गई।
विचारधारात्मक कारणों के अलावा भी समाजवादी दलों के बिखरावों के कई कारण रहे हैं। सत्ता की राजनीति में समाजवादी आंदोलन को बनाये रखकर भी समाजवादी नेता विचारधारात्मक लक्ष्य को प्राथमिकता देते हुए अपनी राजनीति से समाजवादी कार्रवाई को आगे बढ़ाने से वे लगातार चूकते रहे।
वैसे यहां केवल समाजवादी आंदोलन के ‘फिनिश्ड प्रोडक्ट’ नीतीश कुमार की ही बात नहीं की जा रही है। लेकिन करनेवाले ऐसा कर ही सकते हैं।
कम्युनिस्ट आंदोलन का रिश्ता कांग्रेस के साथ बनता-बिगड़ता रहा लेकिन दोनों एक दूसरे के ‘राजनीतिक इस्तेमाल’ की स्थिति को बचाये रखने के प्रति सदैव चौकस और सावधान बने रहे। यह मानने में बड़ी कोई संकोच नहीं चाहिए कि कांग्रेस के साथ रिश्ते के सवाल ने कम्युनिस्ट आंदोलन को कम नहीं उलझाया।
यह भी मानना होगा कि रणनीतिक और राजनीतिक मामलों में बार-बार के उलझावों के बावजूद, यहां तक कि विचारधारात्मक मजबूती और दृढ़ता के कारण बिखरावों के बावजूद कम्युनिस्ट पार्टियों में दृष्टि और दिशा का अंतर नहीं पनपा है, हां गति और प्राथमिकताओं में गंभीर मतभेद जरूर है।
प्रसंगवश, क्या अकारण है कि इलेक्ट्रॉल बांड या भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी या उससे जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति पर आरोप की कोई अंगुली नहीं उठी! क्या बिल्कुल ही अकारण है कि स्त्री-विरोधी अपराधों में वाम मनोभाव के लोगों को अपवाद स्वरूप ही शामिल देखा जाता है।
कांग्रेस के संस्करण की विभिन्न पार्टियों, समाजवादी धारा की पार्टियों, बहुजन राजनीति की पार्टियों और कम्युनिस्ट पार्टियों की राजनीतिक और सांगठनिक चेतना में जितना भी फर्क हो भेद-भाव मुक्त जाति-वर्ण-धर्म निरपेक्ष समाज व्यवस्था को हासिल करने की आकांक्षा में कोई मौलिक फर्क नहीं है, हां अपनी-अपनी सामाजिक-राजनीतिक पृष्ठ-भूमि के कारण तेजी और तीखेपन में जरूर फर्क है।
इस अर्थ में भारतीय जनता पार्टी इन सभी पार्टियों से भिन्न दृष्टि और दिशा की राजनीतिक पार्टी है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ की विचारधारात्मक पृष्ठ-भूमि के कारण हिंदुत्व की राजनीति से जुड़ी शिव सेना भी भारतीय जनता पार्टी से भिन्न मिजाज की राजनीतिक पार्टी रही है।
राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ की पृष्ठ-भूमि के अलावा अन्य कारणों की अनदेखी नहीं की जा रही है, लेकिन यहां इतना ही प्रयोज्य है।
राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपनी विचारधारा के राजनीतिक रुख को छिपाया नहीं। इनकी राजनीति का कमाल यह है कि रुख बदले बिना, रवैया बदल लेने में इनका कोई मुकाबला नहीं है।
रुख की अपरिवर्तनीयता यानी विचारधारा के अचल-तत्व और रवैया की परिवर्तनीयता यानी विचारधारा के चल-तत्व में अभंग ताल-मेल भारतीय जनता पार्टी की स्थाई रणनीति का हिस्सा है।
आजादी के आंदोलन के दौरान भी राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ की विचारधारा पुरानी समाज व्यवस्था और जीवन शैली की तरफ ‘भारत राष्ट्र’ को हांककर ले जाने की कोशिश करती थी। राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ की संस्कृति की समझ (Cultural Competence) यही है।
भारत में मुसलमानों के आगमन के पहले के ब्राह्मण युग की समाज व्यवस्था को हासिल करना, हिंदू राष्ट्र को हासिल करना, राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ की राजनीति के सांस्कृतिक-राष्ट्रवाद का स्पष्ट लक्ष्य है। क्योंकि उनके अनुसार जब वह समाज व्यवस्था थी, तब भारत ‘सोने की चिड़िया’ हुआ करता था।
राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी भली-भांति जानते हैं कि उनकी राह में रोड़े तो कई हैं, लेकिन पहाड़ तो कांग्रेस का ढीला-ढाला राजनीतिक संगठन और कांग्रेसी चेतना ही है।
वे यह भी जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर कई ऐसे महानुभाव हैं जिनकी चेतना कांग्रेसी नहीं है! हालांकि, ‘सत्ता सुख’ के अलावा अन्य कारणों से भी वे कांग्रेस के साथ बने रहे हैं।
भारत की चुनावी राजनीति में असमानतामूलक समाज व्यवस्था की पैरवी करनेवाली अकेली पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी का दल और दर्शन दोनों पूंजीवाद को बहुत तरह से अपने अनुकूल लगता है। भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में बने रहना उनके लिए कई तरह से लाभप्रद है।
जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में भारत के पूंजीवादियों को वह पार्टी मिल गई है, जो नेहरू की तरह से समाजवाद के साथ झूला नहीं झूलती है; बल्कि उन के हित-साधन के लिए समाजवाद को झूला झुला सकती है।
जाहिर है कि पूंजीवाद के प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी में अपना प्रतिनिधि खोजेंगे। उन्हें विश्वास है कि किसी भी कारण से भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से बाहर होने पर वे विवशता में अपना प्रतिनिधि कांग्रेस या अन्य पार्टियों में भी ढूंढ़ लेंगे।
जाहिर है कि उनकी प्राथमिकता तय है। दुनिया भर में पूंजीवाद के समर्थक सरकार चलाते हैं, लेकिन दुनिया की शायद ही कोई राजनीतिक पार्टी जन-हित के मामलों में अपना रुख और रवैया भारतीय जनता पार्टी जैसी रखती होगी।
पहला जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में हुआ। आज कांग्रेस पर सभी हमलावर हो रहे हैं। कांग्रेस खुद भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में ‘हार की समीक्षा’ कर रही है। ‘न्याय योद्धा’ राहुल गांधी कांग्रेस की ‘हार की समीक्षा’ करते हुए चुनावी तंत्र के साथ-साथ कांग्रेस के अंदर भी हार के कारणों की तलाश कर रहे हैं।
चुनावी तंत्र सहित कांग्रेस के बाहर व्याप्त कारणों को चिह्नित करना बहुत मुश्किल नहीं भी हो, साबित करना थोड़ा मुश्किल तो जरूर होगा। हां, कांग्रेस के अंदर चिह्नित हार के कारणों को किस तरह से निष्पक्ष होकर निष्क्रिय करते हैं, यह देखने की बात है।
नागरिक समाज को भी नागरिक कारणों से कांग्रेस की ‘हार की समीक्षा’ करनी चाहिए। इस समीक्षा के दौरान कांग्रेस को हुई राजनीतिक क्षति को विश्लेषित करते हुए भारत के लोकतंत्र को होनेवाली क्षति को चिह्नित करना अधिक जरूरी है। क्योंकि लोकतंत्र में चुनावी हार-जीत अंततः जन-हित से जुड़ा मामला भी होता है।
यह बात साफ-साफ कहना जरूरी है कि गैर-कांग्रेसवाद की बची हुई किसी भी प्रेरणा का कोई भी अंश यदि कांग्रेस की हार में अपनी जीत देखता है तो वह हिंदुत्व की राजनीति के ही पक्ष में खड़ा साबित होने की अनिवार्यता से खुद को बचा नहीं सकता है।
भारत के लोकतंत्र को सभ्य समाज के अनुकूल समतामूलक समाज व्यवस्था के पक्ष में टिकाये रखकर की जाननेवाली राजनीति और भारत के लोकतंत्र को भेद-भावमूलक समाज व्यवस्था के पक्ष में ले जाननेवाली राजनीति में से किसी एक राजनीति को चिह्नित करने और चुनने की चुनौती का सामना नागरिक समाज को बिना हकलाये करना है।
मूल संघर्ष इन्हीं दो किस्म की राजनीति के बीच है, तो समझ में आने लायक बात यह है कि नकारात्मक ध्रुवीकरण का मुकाबला सकारात्मक ध्रुवीकरण से ही किया जा सकता है।
यह मानते हुए भी कि सभ्य और बेहतर जीवन की दृष्टि से ध्रुवीकरण में सर्वस्तरीय नकारात्मकता होती है, होती ही है। इस समय सकारात्मक उद्देश्य के साथ राजनीतिक ध्रुवीकरण के अलावा कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। निवेदन यह कि नागरिक समाज के सामने कठिन चुनौती है।
सभ्य और बेहतर जीवन की सामाजिक समस्याओं के राजनीतिक समाधान का दायित्व राजनीतिक दलों पर है। सामान्य राजनीतिक परिस्थिति में चुनावी हार-जीत को लोकतंत्र की जीत-हार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
लेकिन क्या यह सामान्य राजनीतिक परिस्थिति है? आखिर क्या है, कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब?
(प्रफुल्ल कोलख्यान स्वतंत्र लेखक और टिप्पणीकार हैं)