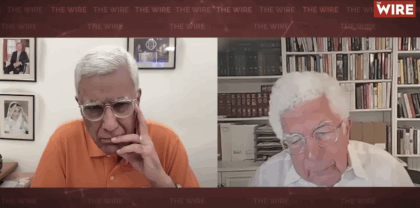भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर्ड हो जायेंगे। रिटायरमेंट के पहले 20 अक्तूबर 2024 को अपने पैतृक गांव कन्हेरसर, पुणे में आयोजित सम्मान समारोह में उन्होंने भाग लिया। रिटायरमेंट का समय आदमी को भावुक कर ही देता है। स्वाभाविक है कि मुख्य न्यायाधीश भी भावुक हुए हो गये होंगे।
जिन्हें जीवन में न्यायालयों में न्यायिक कार्रवाइयों को नजदीक से देखने-सुनने का मौका नहीं मिला, उन्होंने भी कहीं-न-कहीं यह जरूर सुना होगा कि ‘अदालतों में भावुकता का कोई मोल नहीं होता है। अदालतें सबूत पर गौर करती हैं, भावनाओं पर नहीं।’
खबर है कि मुख्य न्यायाधीश ने अपने सम्मान समारोह में कहा कि राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद विवाद के समाधान के लिए आस्था और विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने यह भी कहा कि आस्था और विश्वास हो, तो भगवान हमेशा कोई-न-कोई रास्ता निकाल लेते हैं। बड़े लोगों की बड़ी बात, बड़े लोगों की भावुकता बड़ी। भावुकता के फैसले बड़े!
गरीब लोग तो जीवन भर भात-रोटी के लिए ही भावुक होते रहते हैं। रोजी-रोटी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। जी, समाधान! समझदार लोगों का कहना है कि प्रार्थना से समाधान बड़े लोगों को मिलता है। बड़े लोगों की प्रार्थना भी बड़ी होती है, आरती भी बड़ी होती है।
राम भी उनके गणेश भी उनके! जरूरी नहीं कि हर किसी को प्रार्थना से समाधान मिल ही जाये। समझदार लोगों का दिल से मानना है कि समाधान का मिलना-नहीं-मिलना तो पिछले जन्म के किये अच्छे-बुरे पर निर्भर करता है। इसलिए हर हाल में संतोष ही सबसे बड़ा आश्वासन होता है।
संतोष भी ऐसा कि असंतोष में जनमे विरोध और विद्रोह की हर गलत खयाली को पैदा होते ही नमक चटा दे। यह मानकर संतोष कर लेने पर सब ठीक, लेकिन संतोष की शक्ति के कम होते ही मन दोफांस में पड़कर तितर-बितर हो जाता है।
लोकतंत्र है तो मन तितर-बितर हो ही जाता है। क्योंकि लोकतंत्र गरीब के मन में भी ‘राजा’ का मनोरथ भर देता है; ‘मन मति रंक मनोरथ राऊ।’ असंतोष को बढ़ावा देनेवाले, भड़काने वाले भी तो लोकतंत्र में कम नहीं होते हैं।
मन नैतिक दोफांस में पड़ गया है। कह नहीं सकता संविधान की शपथ लेकर ईश्वर के विश्वस्त होने और ईश्वर की शपथ लेकर संविधान के विश्वस्त होने में क्या फर्क है! ईश्वर के न्याय पर ‘कोई सवाल’ किये बिना विचार करना प्रासंगिक है। समझदार लोगों का मानना है कि किसी ‘सवाल पर विचार’ करने को प्रचलन से बाहर किया जा चुका है।
अब सवाल किये बिना विचार करना फायदा का सौदा है। कुछ लोग फायदा की चिंता किये बिना सवाल तो खूब करते हैं लेकिन विचार राई-रत्ती नहीं करते। जिस सवाल पर इस समय विचार नहीं किया जा सकेगा उस पर समय विचार करेगा। अभी तो बस इतना ही कि जैसे इतने दिन चला है, वैसे ही आगे भी चलता रहे तो गनीमत।
‘हम भारत के लोगों’ की आदत में शामिल है, प्रार्थना करते-करते सो जाना और प्रार्थना करते-करते उठने की कोशिश में अपना जीवन काट लेना! फिलहाल तो यह कि नागरिक विवेक के दोफांस से बाहर निकलना एक चुनौती है। इस चुनौती के केंद्र में कुछ सवाल हैं।
ये सवाल सामान्य नैतिकता से संबंधित हैं; न्यायिक नैतिकता से भी संबंधित हैं। अपने नागरिक होने की समझ को परिभाषित करने के लिए नहीं, मान लीजिए समझने के लिए यह कहा जा सकता है कि नैतिकता व्यवहार के विवेक का व्याकरण है।
पूरी दुनिया में जो कलह और कोलाहल मचा हुआ है उसके कारण को भी समझने की जरूरत है। इसके पीछे केवल राजनीतिक कारण नहीं है, बल्कि राजनीतिक कारण के अलावा भी ‘बहुत कुछ’ है। यह ‘बहुत कुछ’ क्या है, इसे इस समय समझना कठिन है, मगर जरूरी है। लेकिन समझना कौन चाहता है! और क्यों चाहता है!
सभ्य और बेहतर सामाजिक और नागरिक जीवन मनुष्य का जन्म-प्राप्त हक है। यह मनुष्य का जन्म-प्राप्त हक ही नहीं है, बल्कि उसकी मौलिक आकांक्षा भी है। आदर और प्यार पाना भी मौलिक आकांक्षा ही है। इस समय सारी मौलिकताएं स्थगित हैं।
जब ईश्वर से किये गये प्रार्थना की प्रतिध्वनि पर ही ‘सब कुछ’ निर्भर करता है तो फिर न्यायालय को मंदिर मानने के बदले मंदिर को ही न्यायालय माना जाना चाहिए।
अपनी-अपनी आस्था और अपने-अपने विश्वास के मंदिर! न्यायालय, न्यायालय भी अपने-अपने! अपने-अपने ईश्वर के प्रति समर्पित होना और ईश्वर को आत्मार्पित करना ही काफी होना चाहिए था।
लेकिन आजादी के आंदोलन की मंशा के अनुसार ‘हम भारत के लोगों’ ने संविधान के प्रति समर्पित होने और संविधान को आत्मार्पित करने का गौरव हासिल किया था।
गांव के घर-परिवारी लोग सोये-सोये कहा करते थे, जागते रहो! जागते-जागते सोटा करो! चोर के डर से वे भी जागते रहने की कोशिश में लगे रहते थे, जिनके घर में चैन और जीवन में मुंह के अलावा चुराने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था।
मुंह तो खैर वे खुद चुरा लिया करते थे! अपना मुंह तो वे आज भी चुराते रहते हैं। बस चैन को बचाने के लिए चैन से सोते हुए भी जागते रहो, कहा करते थे।
घर-परिवारी लोगों को पता था कि प्रार्थना के बल पर निश्चिंत होना अपने को गफलत में डालना है। वे जानते थे कि सोने के पहले जिस ईश्वर की प्रार्थना वे किया करते हैं, उसी ईश्वर की प्रार्थना चोरी के लिए निकलने के पहले ‘चोर’ भी किया करता है। ईश्वर कभी इन की सुनते हैं, कभी उनकी!
साधु-असाधु में भेद करना ईश्वर की संस्कृति की शोभा के अनुकूल नहीं होता है! वहां भेद-भाव के दूसरे आधार हैं। जहां तर्क स्थगित हो जाता है, वहां प्रार्थना काम आती है। इस पर सोचना गुनाह है कि आखिर तर्क स्थगित हो क्यों जाते हैं? तर्क के स्थगन से न्याय-अन्याय का भेद समाप्त हो जाता है और बचता है एक भरोसा, एक विश्वास, ‘होइहि सोइ जो राम रचि राखा’।
न्याय का लक्ष्य क्या होता है! अन्याय के कारणों का निवारण या असंतोष के कारणों का निराकरण! न्याय का लक्ष्य यदि नैतिक समाज के बनने में योगदान करने का होता है तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संरचना में निहित अंतर्विरोध के चलते निरंतर उत्पन्न होते रहनेवाले अन्याय पर भी न्याय को निश्चित ही गौर करना चाहिए। भारत की न्याय-व्यवस्था राज्य का उपकरण है या नागरिक समाज का उपकरण है?
सीधा सवाल यह हो सकता है कि न्याय की शक्ति का स्रोत कहां है? भारत के संविधान में निहित ‘शक्ति के पृथक्करण’ के सिद्धांत का मतलब तो यही हो सकता है कि ‘संवैधानिक शक्ति के स्रोत’ अनेक हैं। भारत में न्याय-व्यवस्था की शक्ति का स्रोत संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत ‘हम भारत के लोगों’ में है।
‘हम भारत के लोगों’ के अस्तित्व की अभिव्यक्ति संसद सरकार के माध्यम से होती है। इस अर्थ में भारत की ‘शक्तियां’ सरकार में सिमट जाती है। न्याय के स्रोत ‘हम भारत के लोगों’ का मुंह बंद तो ‘हम भारत के लोगों’ की सारी ‘शक्तियां’ सरकार की ‘गर्म मुट्ठी’ में सीमित!
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संरचना में निहित अंतर्विरोधों से उत्पन्न होनेवाले अन्याय को समाप्त करने के लिए अंतर्विरोधों की संवेदनशीलता को समझना और शांत करना अनिवार्य और उपयुक्त उपाय हो सकता है।
इस तरह के उपायों के लागू होने के लिए संस्थागत न्याय से आगे के प्रयासों की जरूरत होती है। आगे के प्रयासों के रास्ते को पहले की तुलना में बहुत संकीर्ण बना दिया गया है।
पिछले दिनों ‘अच्छे दिन’ की तलाश में ‘हम भारत के लोगों’ ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दिया। समर्थन ‘अच्छे दिन’ के लिए था। ‘अच्छे दिन’ को परिभाषित करना या उस के अर्थ को ठीक-ठीक समझना और उसका सामना करने में आनेवाली मुसीबतों का अनुमान ‘हम भारत के लोगों’ को बिल्कुल नहीं था।
जनादेश देनेवाले ‘हम भारत के लोगों’ के ‘अच्छे दिन’ का मतलब कुछ और था और जनादेश हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी का ‘अच्छे दिन’ का मतलब कुछ और ही था! जनादेश देने वाले ‘हम भारत के लोगों’ के लिए ‘अच्छे दिन’ का मतलब हाथ खाली और जनादेश हासिल करनेवाले के लिए ‘अच्छे दिन’ का मतलब साबित हुआ, ‘मुट्ठी गर्म’! मुसीबत यह कि हाथ खाली और मुट्ठी गर्म!
मुसीबतों की जड़ कहां है? राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ का गठन 27 सितंबर 1925 को हुआ। वह समय आजादी के आंदोलन का जबरदस्त दौर था। वह कांग्रेस और महात्मा गांधी की सघन सक्रियता का दौर था। ‘आजादी’ और ‘आंदोलन’ दोनों के प्रति कांग्रेस और महात्मा गांधी से भिन्न रुख, रवैया और नजरिया के कारण राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ का गठन किया गया था।
राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ के नजरिये से सहमत लोगों का आजादी के आंदोलन में ना-भागीदारी या भिन्न-भागीदारी का अपना नजरिया भी बिल्कुल भिन्न ही था।
पूरी राजनीतिक परिस्थिति को लेकर राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ का अपना संतोष-असंतोष था। उन दिनों देश ‘विभाजन की विभीषिका’ और आजादी की प्राप्ति के बाद की चुनौतियों से जूझ रहा था।
उन्हीं परिस्थितियों में बने राजनीतिक माहौल में महात्मा गांधी की हत्या हो गई। जाहिर है कि संविधान के बनने की प्रक्रिया और संविधान के प्रति भी उन का नजरिया भिन्न ही था। संविधान के लागू हो जाने के बाद भी उनकी भिन्नताएं बनी रहीं। आज भी बनी हुई हैं।
भारत के पहले आम चुनाव (25 अक्तूबर 1951 से 21 फरवरी 1952) के समय अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्तूबर 1951 को हुई। राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ अपने को सांस्कृतिक संगठन मानता है। जबकि राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ ने अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना एक राजनीतिक दल के रूप में स्वीकृत की।
1977 में इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष के समय 1977 में अखिल भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया।
अंततः भारी राजनीतिक उठा-पटक के बाद 1980 में अखिल भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के रूप में जनता पार्टी से बाहर निकल आई। इस पूरे घटना क्रम में स्वाभाविक ढंग से राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ की राजनीतिक पार्टी के ही रूप में भारतीय जनता पार्टी की पहचान बनी रही है। स्वाभाविक ही है कि भारतीय जनता पार्टी की पहचान आज भी यही है।
जनता पार्टी के घटक दल के रूप में 1977 से 1980 तक और बाद में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सबसे बड़े घटक दल के नेता अटल विहारी बाजपेयी 13 दिन के लिए 16 मई 1996 से 1 जून 1996, 8 महीने के लिए 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 और फिर वापस 13 अक्टूबर 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे।
बीच में 2004 से 2014 तक कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की सरकार रही।
2014 से 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अकेले दम पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के घटक दलों के समर्थन से नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हुए और अब भी बने हुए हैं।
राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ संस्कृति की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। दोनों मिलकर ‘संस्कृति की राजनीति’ करते हैं। इस ‘संस्कृति की राजनीति’ के चलते भारत की ‘लोकतांत्रिक राजनीति की संस्कृति’ के मूल चरित्र में बहुत ही विपरीत बदलाव आ गया।
भारत की ‘लोकतांत्रिक राजनीति की संस्कृति’ अतीत के अंतर्विरोधों से बाहर निकलकर भविष्योन्मुखी, कल्याणकारी, समावेशी, भेद-भावमुक्त मुक्त, समाजवादी लोकतंत्र के लिए लोकतांत्रिक राजनीति को प्रतिबद्ध करती थी। यह सच है कि ‘लोकतांत्रिक राजनीति की संस्कृति’ अपनी प्रतिबद्धता के निभाव में बुरी तरह से फेल होती रही है।
लेकिन सच यह भी है कि उसने अपनी प्रतिबद्धता को कभी बोझ समझकर फेंकने का इरादा कभी नहीं किया। लेकिन ‘संस्कृति की राजनीति’ ने कभी उस प्रतिबद्धता को ‘दिल से’ अपनाया ही नहीं, निभाने की तो बात ही क्या!
किसी कल्पित अतीत में भारत के ‘सोने की चिड़िया’ के वर्तमान में फुर्र हो जाने का ‘संस्कृति की राजनीति’ को जबरदस्त अफसोस रहा है। अपने अफसोस को अफवाह बनाकर फैलाने की कवायद में ‘संस्कृति की राजनीति’ की सारी शक्ति, इधर दस साल से लगी रही है।
सत्ता में आते ही ‘संस्कृति की राजनीति’ का चाल-चरित-चेहरा सब का असली रूप बहुत तेजी से सामने आने लग गया।
सत्ता में आने के बाद अतीतोन्मुखी दृष्टि, लाभार्थी योजना, ‘हिंदू-हित’ के लिए ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब का प्रयास’ की भ्रामक वाग्मिता (Misleading Rhetoric) की शक्ति-प्रदर्शी घोषणा में कांग्रेस-मुक्त भारत का नारा लगाते हुए ‘संस्कृति की राजनीति’ ‘शक्ति की राजनीति’ के मद में दनदनाती रही।
‘कांग्रेस-मुक्त भारत’ के मतलब में कहीं-न-कहीं भविष्योन्मुखी, कल्याणकारी, समावेशी, भेद-भावमुक्त मुक्त समाजवादी लोकतंत्र की प्रतिबद्धता से मुक्त होने का अंतर्निहित भाव पूरी उग्रता से काम करने लगा।
ऐसा राजनीतिक माहौल कि भारत के नब्बे प्रतिशत सामग्रिक भूगोल पर दस प्रतिशत कब्जा की तार्किकता की वैधता बनाने में ‘सभी’ लग गये! फिर कहें, राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के ‘सांस्कृतिक सोच’ में अतीत का जबरदस्त आकर्षण रहा है।
कहना न होगा कि कांग्रेस को भी अपने अतीत का मोह अकसर उसे आत्म-मुग्ध कर दिया करता है। अतीत की महानताओं का मोह किसी को भी संकीर्ण और भविष्य विमुख बनाकर आत्म-मुग्धता के दलदल में डाल देता है। आत्म-मुग्धता की इस मनःस्थिति और राजनीतिक उपलब्धि के मुंह में 2024 के आम चुनाव ने लगाम डाल दिया है।
भयावह विपरीत राजनीतिक परिस्थिति और संघर्ष के असमान बना दिये गये अवसर में चुनाव संपन्न होने के बावजूद 2024 के आम चुनाव के परिणाम ने ‘चुनावी तानाशाही’ को 240 पर समेट दिया।
चुनाव के माध्यम से ‘चुनावी तानाशाही’ के पैर में पैजनिया डालना लोकतांत्रिक राजनीति की चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत मुश्किल था लेकिन लोकतंत्र की संभावनाओं के लिए उतना ही मुनासिब भी था; यह काम हुआ। ‘इस काम का हो जाना’ मान लेने में, सच पूछा जाये तो थोड़ा सच है तो भ्रम भी कम नहीं है।
मुश्किल और मुनासिब काम हो जाने के बाद जिस राजनीतिक स्फूर्ति का संचार होना चाहिए था, उस राजनीतिक स्फूर्ति में दिख रही शिथिलता बहुत डरावनी है। उम्मीद संवैधानिक स्फूर्ति की भी थी।
नीति और नैतिकता की परवाह किये बिना रिटायरमेंट के मुहाने पर आकर मुख्य न्यायाधीश डॉ धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने जिस ‘निश्छल भाव’ से न्याय-निर्णय के सुझाव और समाधान के लिए ईश्वर के समक्ष प्रार्थना की बात कही है, उस में संवैधानिक स्फूर्ति का अभाव और भ्रम का प्रभाव तो दिखता ही है।
इस देश में करोड़ों परीक्षार्थी प्रार्थना करते हैं, पेपर लीक हो जाता है या फेल कर जाते हैं। चुनाव के दौरान जन-प्रतिनिधित्व का दायित्व हासिल करने के लिए लाखों प्रत्याशी जनता के पास पहुंचने के पहले प्रार्थना करते हैं, कुछ जीत जाते हैं। कुछ नहीं जीत पाते हैं। रोगी अस्पताल में प्रार्थना करते हैं। कुछ बच पाते हैं, कुछ नहीं बच पाते हैं।
06 दिसंबर 1992 का दिन! प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव भी पूजा और प्रार्थना ही कर रहे थे, यानी समाधान के लिए ईश्वर से संवाद! गोली लगने के ठीक पहले बापू प्रार्थना ही कर रहे थे। बापू ने प्राण त्यागने के पहले ‘हे राम’ कहा था। सुना है कि गोली दागने के पहले दागनेवाले ने भी प्रार्थना की थी! भगवान जानें किस भगवान की प्रार्थना की थी!
यह देश राम भरोसे तो रहा ही है। अब उनके भरोसे भी है, जो ‘राम का लाये हैं’। किसी को क्या आपत्ति हो सकती है! प्रार्थना करना, न करना सब का संवैधानिक हक है। ईश्वर के नाम पर संविधान की शपथ लेना भी हक है।
जो हक साधारण जनता को है, वह हक असाधारण न्यायमूर्तियों को भी है। लेकिन न्याय-नैतिकता और संवैधानिक नीति की परवाह किये बिना संवैधानिक लोकतंत्र के ईश-तंत्र में बदले जाने के भ्रम प्रसार का हक! क्या पता!
जब समाधान ईश्वर से ही प्राप्त होना है, तो फिर न्याय-व्यवस्था का इतना ताम-झाम का मतलब क्या है, यह पूछने का हक भी कहीं-न-कहीं होना चाहिए, होगा ही! यह मुल्क सबकी भलाई के लिए ईश्वर के सामने हमेशा से प्रार्थना करता आया है।
आजादी के आंदोलन के दौरान कांग्रेस के बारे में ‘कई लोग’ हिकारत से कहते थे कि कांग्रेस प्रार्थना और पिटीशन की पार्टी है। प्रार्थना पर तो इस देश को पहले से ही बहुत भरोसा रहा है।
सवाल यह है कि अब, साधारण नागरिक पिटीशन पर भरोसा करे या प्रार्थना पर भरोसा करे! इस सवाल और इस तरह के सवालों से उत्पन्न होनेवाली समस्याओं का समाधान प्रार्थना से मिल सकता है या पिटीशन से! कौन बता सकता है।
(प्रफुल्ल कोलख्यान स्वतंत्र लेखक और टिप्पणीकार हैं)