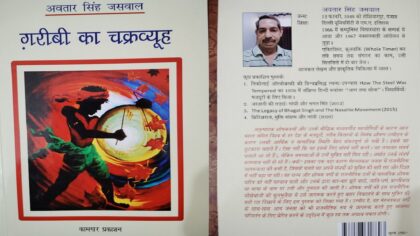बयान कभी-कभी महज़ अल्फ़ाज़ नहीं होते, बल्कि वो आईना होते हैं, जिसमें किसी शख़्स की नीयत, सियासत और सोच की परछाइयां साफ़ नज़र आती हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का वह बयान, जिसमें उन्होंने देश की सबसे मुक़द्दस और संवैधानिक संस्था- सर्वोच्च न्यायालय को ही देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति के लिए ज़िम्मेदार ठहरा दिया, न सिर्फ़ सियासी बेहयाई की इंतिहा है, बल्कि भारत की न्यायिक गरिमा और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सीधा हमला है। यह वह ज़हर है जो अब धीरे-धीरे भाषणों से निकलकर व्यवस्था की शिराओं में घोला जा रहा है।
यह बयान सिर्फ़ किसी एक सांसद की ज़ुबान से निकला अनर्गल आरोप नहीं है, बल्कि यह एक मुकम्मल मानसिकता का आईना है- एक ऐसी सोच जो हर उस संस्था को बेदख़ल करना चाहती है, जो संविधान, इंसाफ़ और जवाबदेही की बुनियाद पर खड़ी है। सवाल यह नहीं कि किसने कहा, सवाल यह है कि किस पर कहा गया- और कितना कुछ बिना कहे कह दिया गया।
जिस देश में अदालतों को इंसाफ़ का आख़िरी मरकज़ माना जाता है, जहां सुप्रीम कोर्ट सिर्फ़ फ़ैसले नहीं सुनाता बल्कि संविधान की आत्मा की हिफ़ाज़त करता है- वहां अगर संसद के भीतर बैठा कोई जनप्रतिनिधि सुप्रीम कोर्ट को ही गृहयुद्ध जैसी स्थिति का ज़िम्मेदार ठहराने लगे, तो यह महज़ शब्दों की लापरवाही नहीं, बल्कि लोकतंत्र की बुनियादों को हिलाने वाली साज़िश है।
क्या यह बयान न्यायालय की अवमानना नहीं है?
क्या यह सीधा-सीधा मुख्य न्यायाधीश और पूरी न्यायपालिका की नीयत पर सवाल नहीं उठाता?
क्या यह वह पल नहीं है जब सर्वोच्च न्यायालय को अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज़ उठानी चाहिए- एक मुक़दमा नहीं, एक इबारत, जो यह साबित कर दे कि इंसाफ़ की दीवारें इतनी कमज़ोर नहीं होतीं?
निशिकांत दुबे पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं- कई गंभीर धाराओं में। वे स्वयं न्यायपालिका के कटघरे में खड़े हैं। और अब वही व्यक्ति न्यायपालिका को कठघरे में खड़ा कर रहा है। यह किसी एक संस्था का नहीं, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे का अपमान है। और यह अपमान सहना, केवल चुप रहना- न सिर्फ़ दुर्भाग्य होगा, बल्कि ख़तरे की घंटी भी।
बीजेपी अगर इस बयान से किनारा कर भी ले, तो सवाल उसकी चुप्पी का रहेगा। क्या यह खामोशी सहमति की हमआहंगी नहीं है? क्या यह सत्ता की ऐसी साज़िश नहीं है जिसमें हर वो आवाज़ जो संविधान की हिफ़ाज़त करती है, मुनाफ़िक़ी और हमला दोनों की ज़द में है?
आज देश को एक फ़ैसला लेना होगा।
क्या वह उस संविधान के साथ खड़ा होगा जो करोड़ों भारतीयों की उम्मीद, हिफ़ाज़त और पहचान है? या वह उन आवाज़ों को जगह देगा जो संविधान को रौंदकर अपनी सत्ता की सीढ़ियां मज़बूत करना चाहते हैं?
क्योंकि यह लड़ाई किसी एक इंसान, एक पार्टी या एक अदालत की नहीं है। यह लड़ाई भारत के लोकतांत्रिक वजूद की है। यह लड़ाई उस भरोसे की है जो करोड़ों लोगों ने संविधान की किताब में देखा था। और यह लड़ाई अब सिर्फ़ अदालतों की नहीं, बल्कि हर जागरूक नागरिक की है।
अगर आज अदालतें चुप रहीं, तो कल अदालतें नहीं रहेंगी।
और जब अदालतें नहीं रहेंगी, तो इंसाफ़ भी सिर्फ़ किताबों में रह जाएगा- और मुल्क अपनी ही परछाईं से डरने लगेगा।
अब वक़्त है कि अदालत अपनी गरिमा के लिए खड़ी हो। अब वक़्त है कि हम सब लोकतंत्र के उस आईने को बचाने के लिए आवाज़ उठाएं, जिसे सियासत की उंगलियां रोज़ खरोंच रही हैं।
(जौवाद हसन स्वतंत्र पत्रकार हैं।)