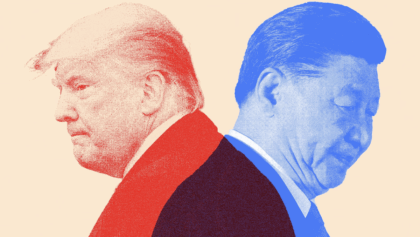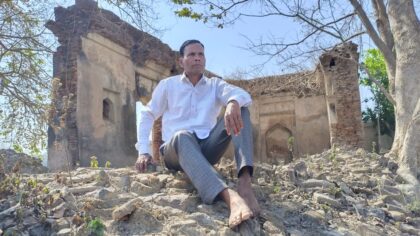यूरोपियन यूनियन (ईयू) के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए भारत की वार्ता में गैर-व्यापार बाधाओं का कांटा फंस गया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दो टूक कहा है कि ईयू के कार्बन बॉर्डर एडस्टमेंट मेकेनिज्म (सीआरबीएम) और जंगल कटाई संबंधी विनियमन के कारण व्यापार वार्ता आगे नहीं बढ़ पा रही है। गोयल ने कहा कि ‘आत्म-सम्मान रखने वाला कोई देश’ ऐसी गैर-व्यापार रुकावटों को स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने कुछ स्टील उत्पादों से संरक्षण संबंधी ईयू के नियमों को भी ‘अतार्किक’ बताया।
कुछ समय पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी कहा था कि सीबीआरएम एकतरफा और मनमाना है, जिस पर अमल होने के बाद ईयू के लिए भारत के निर्यात में बाधा आएगी।
इसी तरह ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार की वार्ता में भी कुछ पेंच फंसे हुए हैं। बताया जाता है कि ब्रिटेन भारतीय कर्मियों के लिए अपना बाजार उतना खोलने को तैयार नहीं है, जितना भारत चाहता है। जबकि ब्रिटेन की पूर्व ऋषि सुनक सरकार के एक मंत्री कहा था कि भारत इस समझौते के तहत सिर्फ लाभ चाहता है, वह कोई रियायत नहीं देना चाहता।
इन दोनों उदाहरणों से पहली नजर में यह संकेत ग्रहण किया जा सकता है कि भारत सरकार मुक्त व्यापार समझौते तो चाहती है, लेकिन ऐसा करते समय वह देश के हितों की रक्षा के लिए जागरूक भी है! मगर गंभीर पड़ताल करने पर कहानी कुछ और सामने आती है।
गोयल ने ताजा टिप्पणी फेडरेशन ऑफ यूरोपियन बिजनेस इन इंडिया के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए की। उसी मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए गोयल ने कहा कि भारत कभी भी ‘बंदूक के साये में बातचीत’ नहीं करेगा। वह व्यापार वार्ता के लिए अनुकूल समय का इंतजार करेगा। ये बात उन्होंने तब कही, जब उनका ध्यान इस ओर दिलाया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत सहित अनेक देशों पर reciprocal टैरिफ 90 दिन के लिए टाल दिया है। यानी इस समयसीमा के भीतर भारत को अमेरिका से द्विपक्षीय व्यापार वार्ता पूरी करनी होगी।
भारतीय मीडिया में गोयल की इन टिप्पणियों को अमेरिका और ईयू के लिए सख्त संदेश बताया गया है।
मगर इसे किस बात का संकेत समझा जाए? क्या भारत ने आखिरकार मन बना लिया है कि अमेरिका के गैर-टैरिफ शर्तों पर वह समझौता नहीं करेगा? या, देश में भारत के रुख को लेकर बढ़ रही व्यग्रता को शांत करने के लिए वाणिज्य मंत्री ने एक फ़ौरी टिप्पणी की है?
भारत के व्यापार विशेषज्ञों में अब यह समझ गहरा चुकी है कि अमेरिका का मकसद सिर्फ टैरिफ कम करवाना नहीं है। ऐसा होता, तो ईयू पर 20 फीसदी reciprocal टैरिफ लगाने का एलान ट्रंप नहीं करते। ईयू में अमेरिकी वस्तुओं पर औसत टैरिफ दो प्रतिशत से भी कम है। ईयू ने इसे शून्य कर देने की पेशकश की थी। मगर उसे ठुकराते हुए ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ लगा दिया। टैरिफ की गणना करते समय कथित गैर-टैरिफ रुकावटों, करेंसी मैनुपुलेशन (मुद्रा की कीमत में हेरफेर), आंतरिक सब्सिडी और अपनी अर्थव्यवस्था के संवेदनशील क्षेत्रों को किसी देश में मिले संरक्षण का आकलन भी उसने किया। इसीलिए भारत पर 26 प्रतिशत reciprocal टैरिफ लगाया गया, जबकि भारत में अमेरिकी आयात पर औसत टैरिफ 17.5 फीसदी है।
इस बारे में पुष्ट खबरें हैं कि द्विपक्षीय व्यापार वार्ता (बीटीए) में अमेरिका ने ‘गैर-टैरिफ रुकावट’ से संबंधित उपरोक्त मुद्दों को भी एंजेडे पर रखा है। इन पर समझौता करने से भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों को बेहद नुकसान का अंदेशा है। ये आशंका इतनी गहरी है कि थिंक टैंक- ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरई)- ने सरकार को सलाह दी है कि अमेरिका से मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता में बने रहने के अपने रुख पर फिर से विचार करे।
जीटीआरआई ने सलाह दी है कि भारत 90 फीसदी औद्योगिक निर्यात पर टैरिफ घटा कर शून्य करने का प्रस्ताव भले अमेरिका के सामने रख दे, लेकिन संवेदनशील क्षेत्रों और कथित गैर-टैरिफ मुद्दों पर रियायत ना दे। ऐसा करने से कृषि, औषधि उद्योग, ऑटोमोबिल सेक्टर आदि के बुनियादी हितों पर चोट पहुंचेगी। जीटीआरआई के आकलन से सहज ही सहमत हुआ जा सकता है। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने भारत के सामने जो मांगें रखी हैं, उनमें शामिल हैः
- किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के सिस्टम को कमजोर करना
- अमेरिका के कृषि उत्पादों पर टैरिफ घटाना
- जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) खाद्यों की अनुमति देना
- पेटेंट कानून में बदलाव करना, ताकि अमेरिकी दवा कंपनियां भारतीय बाजार में मनचाही पैठ बना सकें
- अमेरिका की ई-कॉमर्स कंपनियों को भारत में निर्बाध बिक्री की इजाजत देना
जीटीआरआई ने कहा है- “कृषि उत्पादों पर टैरिफ घटाने से करोड़ों किसानों की आजीविका पर खराब असर पड़ेगा। कारों पर शुल्क घटाने से ओटोमोबिल सेक्टर में भारत की एक तिहाई उत्पादक क्षमता पर फर्क पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका से ऐसा समझौता 1990 के दशक में किया था, जिससे उसकी कार इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। उस उदाहरण से हमें सबक लेना चाहिए।”
क्या यह उम्मीद की जाए कि भारत का सरकार कोई मंत्री इस बारे में देश को आश्वस्त करेगा? क्या अमेरिका के संदर्भ में ऐसे बयान की अपेक्षा की जाए कि उपरोक्त शर्तों को ‘आत्म-सम्मान रखने वाला’ कोई देश स्वीकार नहीं कर सकता?
ये साफ हो चुका है कि ट्रंप प्रशासन की नीति इंच ऑफर करने वाले देशों से किलोमीटर हथिया लेने की है। दुर्भाग्य से भारत सरकार ने आरंभ में इंच समर्पित करने की पेशकश कर बेवजह कमजोरी का संकेत दे दिया। बहरहाल, अभी भी समय है, जब वह उस गलती को सुधार ले। विशेषज्ञ इस पर एकमत हैं कि नई परिस्थितियों में व्यापार के वैकल्पिक बाजार ढूंढना भारत का लक्ष्य होना चाहिए।
जीटीआरआई का सुझाव है कि अमेरिका को एकतरफा रियायतें देने के बजाय
- भारत को केमिकल्स, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में चीन के साथ मिल कर प्रोडक्ट वैल्यू चेन बनाने का प्रयास करना चाहिए।
- रूस और चीन जैसे देशों के साथ व्यापक भागीदारी कायम करने पर उसे विचार करना चाहिए
- ईयू, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए उसे वार्ता करनी चाहिए।
अच्छी बात है कि भारत पहले से ईयू और ब्रिटेन के साथ ऐसी पहल कर चुका है। बेशक, उनमें से किसी देश के साथ समझौते में “आत्म-सम्मान” की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, मगर सबको यह अवश्य ध्यान में रखना होगा कि भारत का “आत्म-सम्मान” सबसे ज्यादा अमेरिका से चल रही वार्ता में ही दांव पर लगा है।
असल मुद्दा यह है कि भारत को किसी भी अन्य देश के सामने कमजोर मुद्रा में क्यों दिखना चाहिए? ऐसा नहीं होता, अगर भारत ने घरेलू बाजार को सशक्त एवं विस्तृत करने पर ध्यान दिया होता। भविष्य में भी “आत्म-सम्मान” से जीने की स्थिति तभी बनेगी, जब ऐसा किया जाएगा।
(सत्येंद्र रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिल्ली में रहते हैं)