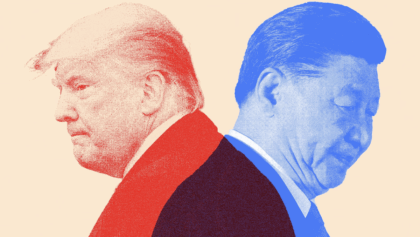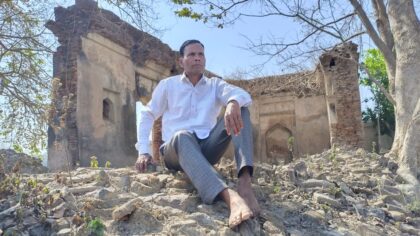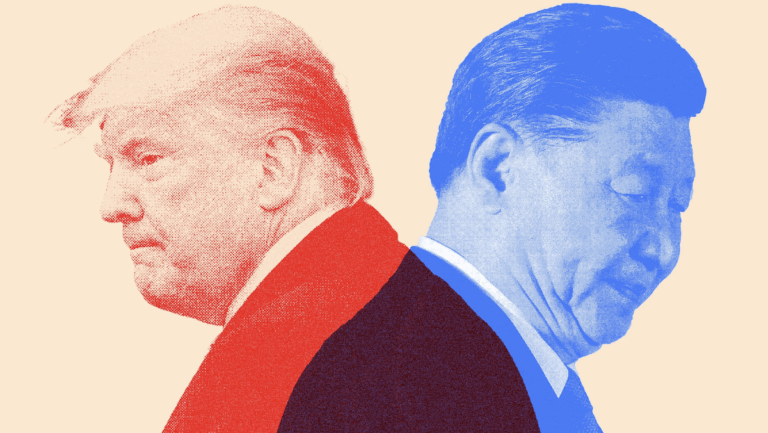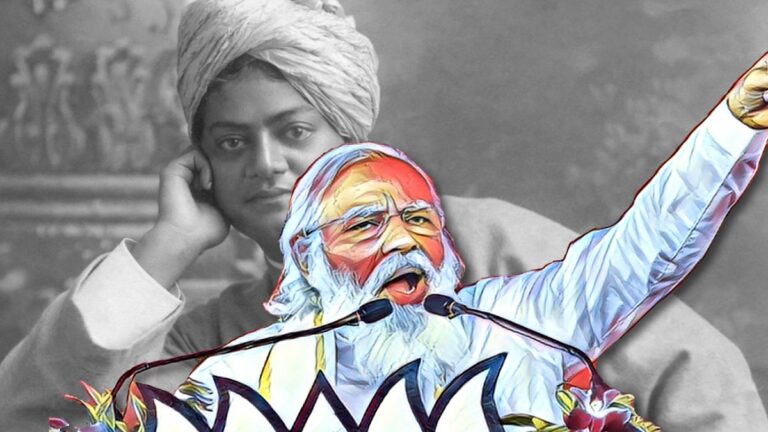गैर-भाजपा दलों की मुश्किल यह है कि वे जितनी राजनीतिक पूंजी कमाते हैं, जल्द ही उससे ज्यादा खर्च कर डालते हैं। नतीजा यह होता है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए जो ‘राजनीतिक’ या वैचारिक ताकत चाहिए, उसे वे बना नहीं पाते। इसके बाद उनके लिए राजनीति का मतलब जोड़-घटाव बन जाता है। मगर दिक्कत यह है कि यह जोड़-घटाव भी वे गलत अंकगणित के साथ करते हैं। उससे ठोस जमीनी प्रश्नों का जो हल निकलता है, उसका गलत होना लाजिमी ही है।
कमाई से ज्यादा राजनीतिक पूंजी खर्च करने की मिसाल देखनी हो, तो हाल की तीन घटनाओं पर गौर किया जा सकता हैः
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी बहुचर्चित भारत जोड़ो यात्रा से यह संदेश देने की कोशिश की कि वे भाजपा/आरएसएस से लड़ाई के सही संदर्भ को समझते हैं। यह एक वैचारिक और भारत के सपने या सोच से जुड़ी लड़ाई है। राहुल गांधी ने यह संकल्प भी जताया कि वे इस ल़ड़ाई को इसी संदर्भ में लड़ने को तैयार हैं।
लेकिन कर्नाटक का चुनाव आते-आते उनकी पार्टी ने असल में क्या किया? तमाम वैचारिक आग्रहों को ताक पर रख कर वह ऐसे समीकरण बनाने में जुट गई, जिससे लिंगायत समुदाय के कुछ वोट उसे भी मिल सकें। इसके लिए मौजूदा बोम्मई सरकार में मंत्री रहे जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावड़ी को ना सिर्फ कांग्रेस में शामिल किया गया, बल्कि उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट भी दे दिया गया।
अब प्रश्न है कि क्या शेट्टार और सावड़ी सचमुच उस विचारधारा से असहमत हो गए हैं, जिसके खिलाफ संघर्ष के लिए राहुल गांधी ने चार हजार किलोमीटर की पदयात्रा की थी?
हकीकत यह है कि दोनों नेताओं (और उन जैसे कई और नेताओं) ने भाजपा सिर्फ इसलिए छोड़ी, क्योंकि भाजपा ने अपने चुनावी गणित के तहत उन्हें टिकट नहीं दिया। ये नेता उसी सरकार का हिस्सा रहे, जिसे कांग्रेस ’40 परसेंट सरकार’ कह रही है। इन नेताओं ने उस कथित 40 परसेंट कल्चर पर कभी एतराज नहीं जताया।
कर्नाटक में पिछले दो-तीन साल में उग्र सांप्रदायिकता का नजारा देखने को मिला है। हिजाब पर पाबंदी की बहुचर्चित घटना इसी दौर में वहां हुई है। शेट्टार, सावड़ी और टिकट ना मिलने के असंतोष के कारण भाजपा छोड़ कांग्रेस में आने वाले उन जैसे नेताओं को इस राजनीति पर भी कोई एतराज नहीं रहा (और ना ही अब भी होगा)। मुद्दा वही है कि क्या कांग्रेस सचमुच ऐसा सोचती है कि ऐसे लोगों को साथ लेकर वह उस आइडिया और इंडिया को वापस लोकप्रिय बना सकेगी, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अस्तित्व में आई थी?
अब दूसरी मिसाल पर गौर करते हैं। तमिलनाडु की डीएमके नेतृत्व वाली सरकार ने अपनी छवि भारत के संघीय ढांचे की रक्षा और सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध सरकार के रूप में बनाने की कोशिश की है। इसके लिए अभी हाल में उसने सामाजिक न्याय सम्मेलन भी आयोजित किया। हालांकि इस सम्मेलन में जिस तरह के नेताओं और अन्य लोगों को बुलाया गया, उससे इस आयोजन पर कई सवाल उठे थे, फिर यह समझा गया था कि इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठाना अपने-आप में सही दिशा में एक पहल है।
लेकिन उसी सरकार ने पिछले हफ्ते एक कानून पारित कराया, जिसके तहत राज्य में कंपनियों को कर्मचारियों से 12 घंटे तक काम लेने की इजाजत दे दी गई। कुछ सहयोगी दलों और ट्रेड यूनियनों के जोरदार विरोध के कारण फिलहाल इस श्रमिक विरोधी कानून के अमल पर रोक दिया गया है। लेकिन इससे पहल से एम के स्टालिन की सरकार और पार्टी की कॉरपोरेट समर्थक की जो छवि बनी है, उससे मुक्त होना उनके लिए आसान नहीं होगा।
इससे यह सवाल भी उठा है कि जब श्रमिक वर्ग के हितों का असल मुद्दा सामने आता है, तो भारतीय संसदीय राजनीति में शामिल सभी प्रमुख पार्टियों का एक जैसा नजरिया और वर्ग चरित्र क्यों सामने आ जाता है?
अब तीसरी मिसाल पर ध्यान दें। गैर-भाजपा दलों की तरफ से गुजरे वर्षों में यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि भाजपा सरकारें rule of law (कानून के राज) को खत्म कर रही हैं। वे सांप्रदायिक हिंसा की वकालत या उसे आयोजित करने वाले लोगों को संरक्षण देती हैं। उधर जिन लोगों को केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के पहले दंगों या जघन्य सांप्रदायिक हिंसा के आरोप में सजा हुई थी, उन्हें अब सरकारी फैसले के तहत जेल से रिहा किया जा रहा है। गुजरात दंगों के सिलसिले में हुए बिलकीस बानो बलात्कार कांड के अपराधियों को जेल से छोड़ने के गुजरात सरकार के फैसले से जन समुदाय के एक बड़े हिस्से में व्यग्रता पैदा हुई थी।
अब बिहार में जो हुआ है, उस पर गौर कीजिए। नीतीश कुमार-तेजस्वी यादव की सरकार ने हत्या के आरोप में सजायाफ्ता आनंद मोहन को रिहा करने के लिए नियमों में ऐसे बदलाव किए, जिससे 26 अन्य अपराधियों को भी जेल से छोड़ने का रास्ता साफ हो गया। आखिर आनंद मोहन से नीतीश-तेजस्वी सरकार का यह लगाव किस आधार पर है? क्या यह सीधे तौर पर एक जाति विशेष का चुनावी समर्थन पाने के मकसद से उठाया गया कदम नहीं है?
मुद्दा यह है कि आनंद मोहन की रिहाई का समर्थन करने या इस पर चुप रहने वाली पार्टियां बिलकिस बानो के बलात्कारियों की रिहाई का विरोध किस मुंह और तर्क से कर सकती हैं? क्या बिहार सरकार ने भी rule of law का वैसा ही अनादर नहीं किया है, जैसा करने का इल्जाम भाजपा पर है? यहां यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि बिहार सरकार में कांग्रेस भी शामिल है और उस सरकार को सीपीआई (एमएल) लिबरेशन का समर्थन प्राप्त है।
ये तीन सिर्फ ताजा घटनाएं हैं। अगर अतीत में जाकर देखें, तो वैसे अनेक मामले मिलेंगे, जो गैर-भाजपा दलों की राजनीतिक पूंजी के खजाने में सेंध लगाते हैं। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अतीत का बहुत सारा बोझ इन दलों और उनके नेताओं के साथ जुड़ा रहा है, जिस कारण उनके लिए जनता के एक बड़े हिस्से में विश्वसनीयता हासिल करना आज भी एक बड़ी चुनौती है।
अगर इस पूरे संदर्भ या पृष्ठभूमि को ध्यान में रखा जाए, तो यह समझने में अधिक आसानी हो सकती है कि आखिर देखते-देखते भाजपा/आरएसएस इस देश की प्रमुख शक्ति और उनकी विचारधारा सबसे लोकप्रिय विचारधारा कैसे बन गई? कांग्रेस और अन्य कथित धर्मनिरपेक्ष दलों ने गुजरे दशकों में राजनीतिक पूंजी बनाई, लेकिन साथ ही अवसरवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद आदि में संलग्न होने के कारण वे अपनी पूंजी गंवाते भी रहे। अपने को नुकसान पुहंचाने वाला जो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया, वो यह था कि उनकी ‘राजनीति’ (POLITICS) क्या है, यह समझना लोगों के लिए मुश्किल होता चला गया।
अपने को अराजनीतिक बनाने की उनकी प्रवृत्ति इस हद तक पहुंची कि 2004 में जब कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए बना, तो सरकार के समाजोन्मुख कार्यक्रम तय करने के लिए यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को गैर-राजनीतिक बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को लेकर राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनानी पड़ी। इस तरह कांग्रेस और यूपीए में शामिल अन्य दलों ने सोच-विचार का काम आउटसोर्स कर दिया।
इसके विपरीत भाजपा/आरएसएस अपनी विचारधारा (भले उसे दूसरे लोग समाज और देश के लिए कितना ही खतरनाक समझते हों) का प्रचार और प्रयोग करने में जुटे रहे हैं। इसके जरिए जन समर्थन जुटाने और जनमत को असल मुद्दों से भटकाए रखने की उन्होंने ऐसी क्षमता दिखाई है कि देश के पूंजीपति वर्ग को उनमें अपना सबसे मजबूत हित-रक्षक नजर आने लगा है। आज पूंजीपति/शासक वर्ग का पूरा दांव भाजपा पर लगा हुआ है।
ऐसे में उसे सिर्फ स्पष्ट और संकल्पबद्ध वैचारिक राजनीति के जरिए ही चुनौती दी जा सकती है। इस राजनीति को जनता में स्वीकार्य बनाने के लिए लोगों के बीच रह कर प्रयोग करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। लेकिन यह बात ज्यादातर गैर-विपक्षी दल और नेता समझते भी हैं, इस बात के कोई संकेत नहीं हैं।
ऐसे में विपक्ष का कुल जमा-खर्च घाटे में बना हुआ है, तो उसमें कोई हैरत की बात नहीं है। राजनीतिक पूंजी के घाटे में चल रही पार्टियों का आपसी गठजोड़ कभी कारगर नहीं होता है। इसलिए 2024 में व्यापक विपक्षी गठबंधन बनने की बातें असल में भ्रामक हैं। नीतीश कुमार जैसे अविश्वसनीय नेता अगर ऐसे गठबंधन के प्रमुख सूत्रधार बनते दिखते हैं, तो यह घाटा कुछ और बढ़ ही जाता है।
वैसे भी जिस अंकगणितीय समझ के आधार पर ऐसे प्रस्तावित गठबंधनों से उम्मीद जोड़ी जाती है, वोटों के अर्थ में उसका कोई ठोस हिसाब अभी तक किसी ने पेश नहीं किया है। सिर्फ अतीत में कांग्रेस विरोधी हुए कुछ प्रयोगों के स्मृतिमोह में ऐसे प्रयासों से ऊंची उम्मीदें जोड़ी जाती हैं। लेकिन ऐसी उम्मीदों का धराशायी होना एक स्वाभाविक परिणाम होता है।
(सत्येंद्र रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं।)