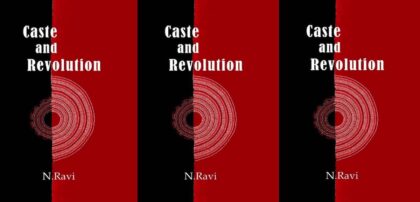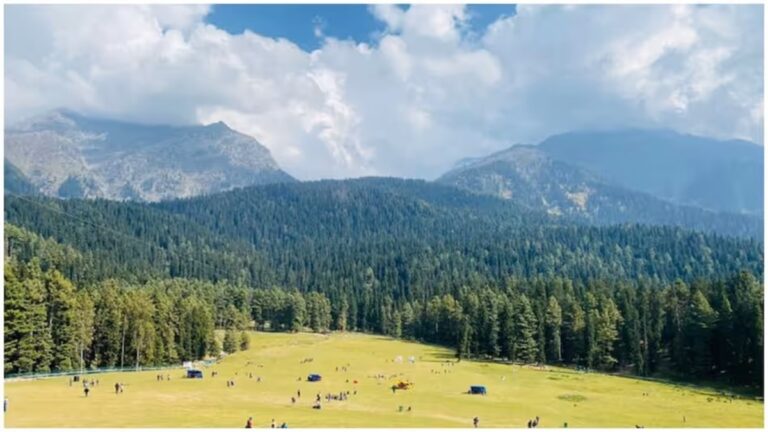इतिहास गवाह है कि शताब्दियों से मानव, सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए निरंतर भटकता रहा है और इसी कारण दुनिया में कई युद्ध, क्रांति, बगावत, विद्रोह हुये हैं जिसके कारण अनेक बार सत्ता परिवर्तन हुए हैं। अगर भारत की बात की जाये तो हमारा भारतीय समाज पहले वर्ण व्यवस्था आधारित था जो धीरे-धीरे बदलकर जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गया। असमानता, अलगाववाद, क्षेत्रवाद, रूढ़िवादिता समाज में पूरी तरह व्याप्त थी। यह सामंती दौर था जहां गरीब, दलित, आदिवासी, महिलाओं और विकल अंग व्यक्तियों को न्याय नहीं मिलता था।
आजादी के बाद यदि विश्व के हमारे सबसे बड़े लोकतंत्र पर नजर डालें तो कुछ परिवर्तन अवश्य हुआ है लेकिन अभी भी समाज का बड़ा हिस्सा मुख्यतः गरीब, अशिक्षित, निर्बल, दलित और दमित समुदाय न्याय की तलाश में भटकता नजर आता है। अदालतों में विचाराधीन मुकदमों को देखा जाये जो कोई साढ़े पांच करोड़ की संख्या है जिसका निपटारा कब तक हो पायेगा कह पाना मुश्किल है। मुकदमों का यह पिरामिड देशवासियों के लिए चिंता और भय का कारण है।
यूं अदालती फैसलों में पांच-छह वर्ष का समय लगना तो सामान्य-सी बात है, पर यदि बीस-तीस साल में भी निपटारा न हो तो आम लोगों के लिए यह किसी नारकीय त्रासदी से कम नहीं है। वैसे तो न्याय का मौलिक सिद्धांत यह है कि ‘न्याय में विलंब होने का मतलब न्याय को नकारना है’। विडम्बना यह कि देश की अदालतों में जब करोड़ों मामलों में नित्य न्याय नकारा जा रहा हो तो आम आदमी को न्याय सुलभ हो पाना मृग मरीचिका जैसा ही है।
वस्तुत: अदालतों में त्वरित निर्णय न हो पाने के लिए प्रशासनिक कार्यप्रणाली ही ज्यादा दोषी है जो अंग्रेजी शासन की देन है। उसमें व्यवहारिक परिवर्तन आज तक नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हों, देश के विधि मंत्री हों या अन्य, लंबित मुकदमों के अंबार को देखकर चिंता में डूब जाते हैं, लेकिन किसी को हल नजर नहीं आता है। उधर सुप्रीम कोर्ट, अदालतों में जजों की कमी का रोना रोता है।
पूर्व कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मार्च में राज्यसभा में बताया था कि देश के अंदर हाईकोर्ट के जजों के लगभग 30 प्रतिशत पद खाली हैं। उच्च न्यायालयों में 1,114 जजों की स्वीकृत संख्या है और वर्तमान में 780 पद भरे हुए हैं जबकि 334 पद खाली हैं। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालयों में 334 पदों के लिए हाईकोर्ट कॉलेजियम की 118 सिफारिशें चरणों में हैं। जबकि सरकार को अभी तक 216 वेकेंसी के लिए सिफारिशें नहीं मिली हैं।
जजों की कार्य कुशलता के संबंध में उड़ीसा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस बिलाई नाज ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के लिए कई जज फौजदारी मामले डील करने में अक्षम हैं। 1998 की फौजदारी अपीलें बंबई उच्च न्यायालय में इसलिए विचाराधीन पड़ी हैं क्योंकि कोई जज प्रकरण का अध्ययन करने में दिलचस्पी नहीं लेता। पदों की कमी और रिक्त पदों को भरे जाने में विलंब ऐसी समस्याएं हैं, जिनका निराकरण जल्दी होना चाहिए किंतु यहां भी यथावत शिथिलता देखी जा सकती है।
समाचार-पत्रों और टीवी के सर्वव्यापी अस्तित्व के बावजूद नोटिस तामील के लिए उनका सहारा नहीं लिया जाता। नोटिस तामील होने में अत्यधिक वक्त जाया होता है। आवश्यकता इस बात की है कि कानूनों में तत्संबंधी सुधार कर जमानत और अपीलों की चेन में कटौती की जाए और रोज पेशियां बढ़ाने पर बंदिश लगाई जाए।
यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि दलित अत्याचार संबंधी कानून को कभी ठीक से लागू ही नहीं किया गया। दलित अत्याचार के मामले जल्दी निपटाने के लिए न तो विशेष अदालतें बनाई गई और न ही पुलिस अधिकारियों को दलितों-आदिवासियों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए कानून के अहम प्रावधानों के बारे में ठीक से अवगत कराने का प्रयास हुआ।
सच्चाई तो यह भी है कि न्यायपालिका की शिथिलता और अकुशलता से अपराध और आतंकवाद को भी बढ़ावा मिलता है। हमारे संविधान में सामाजिक और आर्थिक न्याय की गारंटी समस्त नागरिकों को एवं जीवन जीने की गारंटी प्रत्येक व्यक्ति को दी गई है। सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित के बीच सामान्जस्य स्थापित करना है। इसलिए कल्याणकारी राज्य की कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी।
बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय को ध्यान में रखते हुये समाजवादी व्यवस्था का प्रावधान भी रखा गया। पर राजनीतिक स्वार्थों और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी ने समाजवादी स्वप्न साकार नहीं होने दिया। राजनीतिक और ब्यूरोक्रेट भ्रष्टाचार में लिप्त होते गए। देश में भ्रष्टाचार इतना सर्वव्यापी हो चुका है कि सम्प्रति व्यवस्था का कोई भी कोना उसकी सड़ांध से बचा नहीं है, लेकिन फिर भी उच्च स्तरीय न्यायपालिका कुछ अपवाद छोड़कर सामान्यतया साफ-सुथरी ही कही जाएगी।
मुकदमों के निपटारे में विलंब का एक कारण भ्रष्टाचार भी है। उच्चत्तम न्यायालय और हाईकोर्ट के जजों को हटाने की सांविधानिक प्रक्रिया इतनी जटिल है कि कार्रवाई किया जाना बहुत कठिन होता है। न्यायिक आयोग के गठन का मसला सरकारी झूले में वर्षो से झूल रहा है।
एक पहलू यह भी है कि यदि विगत छह दशकों में राज्य के तीन अंगों अर्थात विधायिका, कार्यपालिका तथा न्याय पालिका के प्रदर्शन पर नजर डाली जाए तो इनमें न्यायपालिका को बेहतर माना जाएगा। अनेक अवसरों पर उसने विधायिका और कार्यपालिका द्वारा संविधान के उल्लंघन को रोका है। उसकी सक्रियता ने जनजीवन में एक नई उम्मीद भी पैदा की लेकिन न्यायालय से पूर्व की न्याय प्रक्रिया किस तरह प्रारम्भ होती है इसे भी देखना आवश्यक है।
उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद-21 में विवक्षित गरिमामयी जीवन की विभिन्न व्याख्याओं से स्पष्ट है कि मानव जीवन पशुवत नहीं है और सम्मान व गरिमा के साथ जीवन यापन करना हमारा अधिकार है और यह मानवाधिकार भी है। लेकिन ऐसा एक स्वस्थ, पारदर्शी, सामाजिक, आर्थिक व प्रशासनिक प्रणाली में ही सम्भव है। लेकिन जिस व्यवस्था के बल पर देश में सुशासन लाने की बात होती रही है वही व्यवस्था कुशासन की नींव बन चुकी है।
सवाल यह है कि आखिर क्या वजह रही कि पुलिस व्यवस्था विफलता और भ्रष्टाचार के कगार पर है। ‘इण्डिया करप्शन एवं ब्राइवरी रिपोर्ट’ के अनुसार भारत में रिश्वत मांगे जाने वाले सरकारी कर्मचारियों में से तीस प्रतिशत की भागीदारी तो मात्र पुलिस तन्त्र की है।
भारत में पुलिस के हस्तक्षेप का दायरा बहुत ही विस्तृत है इसीलिए पुलिस के पास असीमित अधिकार हैं। वह राज्य सत्ता की सबल संस्था है, सत्ता का सशक्त औजार भी है। जाहिर है उसका चरित्र राजसत्ता के चरित्र से अलग नहीं हो सकता। पुलिस द्वारा रिश्वत प्राथिमिकी दर्ज करवाने, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने में कोताही बरतने या मामला न दर्ज करने तथा जांच करते समय सबूतों को नजरदांज करने सम्बन्धी मामलों में ली जाती है। रसूखदारों के दबाव में काम करना तथा अवांछित राजनैतिक हस्तक्षेप को झेलना पुलिस अपना कर्तव्य समझने लगी है।
पुलिस रिफॉर्म और पुनर्संगठन की आवश्यकता कई दशकों से महसूस की जा रही है लेकिन इस पर अमल नहीं किया जाता। केंद्र के गृहमंत्री एवं कानून मंत्री कोई पहल नहीं करते। उनके लिए यह सर्वथा लाभ की स्थिति है कि कानून व्यवस्था राज्यों की जिम्मेदारी है इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों और हरियाणा में दलित अत्याचार की हाल की घटनाएं इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किस तरह बहुसंख्यकों एवं खाप पंचायतों ने ऐसे हमलों की योजना बनाई और उस पर खुलेआम अमल करवाया।
आगजनी तथा हत्याओं में लिप्त अपनी जाति के लोगों को बचाने में खाप पंचायतें आगे आईं। सांप्रदायिक तनाव बनाया गया। दंगे करवाये गए। दलितों को जिंदा जलाया गया। चुनाव और वोट की राजनीति की गयी। प्रायः यह देखा जाता है कि पुलिस एवं प्रशासनिक अमला ऊंची-दबंग जातियों के हितों की हिफाजत करने में लगे रहते हैं। स्वाभाविक तौर पर प्रश्न उठता है कि जब तक समाज के मानस में बदलाव नहीं होगा- जिससे नए किस्म के समाज सुधार एवम सांस्कृतिक आन्दोलनों से क्रियान्वित किया जा सकता है- क्या हमारे लिए सम्भव होगा कि हम जमीनी स्थिति में कोई गुणात्मक प्रभाव कर सकें।
हलांकि पुलिस तन्त्र की स्थापना कानून-व्यवस्था को कायम रखने के लिये की गई थी तथा आज भी सामाजिक सुरक्षा तथा जनजीवन को भयमुक्त एवं सुचारू रूप से चलाना पुलिस तन्त्र का विशुद्ध कर्तव्य है। इस क्षेत्र में पुलिस को पर्याप्त लिखित एवं व्यवहारिक अधिकार भी प्राप्त हैं। भारत के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास, बढ़ती जनसख्या, प्रौद्योगिकी का विकास, अपराधों का सफेद कॉलर होना इन तमाम परिस्थितियों के कारण पुलिस तन्त्र की जबावदेही के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ी है। लेकिन भारतीय समाज में पुलिस की तानाशाहीपूर्ण छवि, जनता के साथ मित्रवत ना होना तथा अपने अधिकारी के दुरुपयोग के कारण वह आरोपो से घिरती चली गई है ।
आज स्थिति यह है कि पुलिस बल समाज के तथा कथित ठेकेदारों, नेताओं तथा सत्ता की कठपुतली बन गया है। समाज का दबा-कुचला वर्ग तो पुलिस के पास जाने से भी डरता है, पुलिस वर्ग को तमाम बुराइयों तथा कुरीतियों ने घेर लिया है। पुलिस में सामान्यतया भ्रष्टाचार और अपराधीकरण के कई मामले हमारे सामने आते रहते है। चूंकि पुलिस के पास सिविल-समाज से दूरियां बनाये रखने और उनके ऊपर असम्यक प्रभाव बनाये रखने की तमाम व्यवहारिक शक्तियां हैं अतः साधारण वर्ग अपनी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता और यदि वह साहस जुटाता भी है तो उसके भयावह परिणाम भी उसे भोगने पड़ते हैं।
कार्यपालिका और न्यायपालिका उसकी कोई मदद नहीं कर पाती क्योंकि उनका आधार तो पुलिस पर ही टिका होता है। ऐसे में सामान्य व्यक्ति को न्याय मिलना बहुत दूर की संभावना ही कही जाएगी। चौथा खंभा कहलाने वाला मीडिया भी अंततः राजनीति के दलदल और मुनाफा कमाने के औजार के रूप में तब्दील हो चुका है। अब वह भी सामान्य व्यक्ति के दुःख दर्द का साझीदार नहीं है।
ऐसी स्थिति में समाज के पास एक सशक्त आंदोलन निर्मित करने के अलावा कोई और विकल्प शेष नहीं बचता है।
(शैलेन्द्र चौहान साहित्यकार हैं और जयपुर में रहते हैं।)