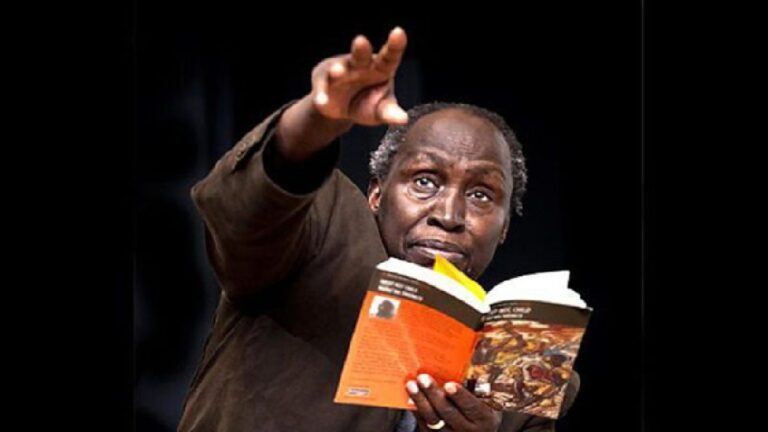जनवरी, 1946 में साहिर लुधियानवी और मैं बंबई पहुंचे, तो हमारी उम्र बिल तर्तीब पच्चीस और बाईस साल थी। ये बर्र-ए-सग़ीर (हिंद उपमहाद्वीप) की जद्दोजहद, आज़ादी का सुनहरा दौर था। और मुल्क के कोने-कोने से आज़ादी के नारे बुलंद हो रहे थे। बंबई शहर रॉयल इंडियन नेवी के जवानों की बग़ावत के नारों से गूंज रहा था। साहिर लुधियानवी का पहला शे’री मजमूआ ‘तल्ख़ियां’ डेढ़-दो बरस पहले शाए हो चुका था। और इसका शुमार नौजवान नस्ल के तरक़्क़ीपसंद शुअरा (शायर या लेखक लोग) में होने लगा था।
मैंने उस वक़्त तक दो-तीन कहानियां लिखी थीं। और दिल-ओ-दिमाग़ पर अदब की तरक़्क़ीपसंद तहरीक का ग़लबा (प्रभुत्व) था। बंबई पहुंचने पर दिल खु़शी से मामूर था। इसीलिए कि आज़ादी से पहले दो-तीन बरस ये शहर उर्दू के सभी तरक़्क़ीपसंद और नामवर अदीबों और शायरों की क़याम-गाह (निवासस्थान) होने का शरफ़ (श्रेय) हासिल कर चुका था।
सय्यद सज्जाद ज़हीर, जोश मलीहाबादी, कृश्न चंदर, इस्मत चुग़ताई, शाहिद लतीफ़, मजाज़, मंटो, मुम्ताज़ हुसैन, सरदार जाफ़री, कैफ़ी आज़मी, मजरूह सुल्तानपुरी, विश्वामित्र ‘आदिल’, नियाज़ हैदर, हाजरा मसरूर, ख़ुदैजा मस्तूर, सफ़दर मीर, इब्राहिम जलीस, प्रेम धवन, मीराजी, ज़ोए अंसारी ग़रज़ कि बर्र-ए-सगीर के चप्पे-चप्पे से अदीब और शायर बंबई आकर आबाद हो गए थे। और मेरे जैसे नौजवान के लिए इससे ज़्यादा खुश वक़्ती की और क्या दलील हो सकती थी कि बंबई में उन सब से मुलाक़ात करने का मौक़े मयस्सर आएंगे।
हमारे बंबई पहुंचने से कोई एक बरस पहले हैदराबाद दक्कन में तरक़्क़ीपसंद मुसन्निफ़ीन का एक ज़बर्दस्त इज्तिमा हो चुका था। साहिर इसमें शरीक हुआ था। इसीलिए वो बंबई में क़ियाम-पज़ीर (ठहरे हुए) अदीबों और शायरों से मिल चुका था। कृश्न चंदर का मील का पत्थर रिपोर्ताज ‘पौदे’ उसी कॉन्फ्रेंस की यादगार था। और शाए होकर मुल्क-गीर (राष्ट्रीय स्तर पर) सतह पर दाद वसूल कर चुका था। इसी रिपोर्ताज के इस एक फ़िक़रे ने ख़ास तौर से बहुत शोहरत हासिल की थी, ‘‘सय्यद सज्जाद ज़हीर शक्ल-ओ-सूरत से चमड़े के सौदागर मालूम होते हैं।’’
चुनांचे बंबई पहुंचने के फ़ौरन ही बाद हम लोग सैंडहर्स्ट रोड पर स्थित कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर पहुंचे। जहां मैं पहली बार बन्ने भाई से मिला। उनके अलावा डॉ. अशरफ़, पीसी जोशी, अली सरदार जाफ़री, कैफ़ी, ज़ोए अंसारी, मोहम्मद मेहदी और मिर्ज़ा अशफ़ाक़ बेग वगैरह से भी मुलाक़ात हुई। ये सभी लोग पार्टी के हफ़्तावार अख़बार ‘क़ौमी जंग’ से मुनसलिक (जुड़े हुए) थे। और उर्दू वाले कहलाते थे।
कुमार मंगलम और उसकी बहन पार्वती भी यहीं मिले। जिनके बारे में बताया गया कि ये दोनों मद्रास के एक करोड़पति ख़ानदान के चश्म-ओ-चिराग़ हैं। और सब कुछ छोड़छाड़ कर बंबई आ गए हैं। बाद में ये दोनों भाई-बहन हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के मेंबर भी बने। कुमार मंगलम बहुत दिनों तक काबीना के रुक्न रहे। पार्वती कोई बीस बरस पहले पार्लियामेंट के एक वफ़्द (शिष्टमंडल) के हमराह लाहौर भी आई थीं। 1947 के बाद दोबारा उससे लाहौर ही में तफ़्सीली मुलाक़ात हुई थी।
बंबई के इन सब दोस्तों और अदीबों-शायरों में बन्ने भाई को बड़ी मुंफ़रिद (विशिष्ट) पोजिशन हासिल थी। वो हैरतअंगेज़ शख़्सियत के मालिक थे। एक क़िस्म की चुम्बकीय ताक़त उनके वुजूद में रची-बसी थी, जो लोगों को अपनी तरफ़ खींचती थी।
बंबई में हमारे हल्क़ा-ए-अहबाब (मित्र-मंडली) में ये बात मशहूर थी कि बन्ने भाई जिस नौजवान के कंधे पर हाथ रख देते हैं, वो कहीं का नहीं रहता। घर-बार, बहन-भाई, बीवी-बच्चों को छोड़कर उन्हीं का हो रहता है। या फिर कम्युनिस्ट पार्टी का कुल वक़्ती रुक्न बन जाता है। हुआ यूं कि उन्होंने हमारे कंधे पर फ़ौरन ही हाथ रख दिया। बंबई शहर के शबिस्तानों (ख़्वाबगाह) और ख़ूबांओं (प्रियतमाओं) से अभी पूरी तरह आशना भी नहीं हुए थे कि उन्होंने अपने साथ में लेकर काम पर लगा दिया था।
सज्जाद ज़हीर मालाबार हिल के बालकेश्वर रोड पर रहते थे। ये सड़क चौपाटी से मालाबार हिल को जाती है। उसी पर कुछ आगे जाकर क़ायदे आज़म रिहाइश पज़ीर (निवास करते) थे। ये उमरा का रिहाइशी इलाक़ा था। जिस मकान में बन्ने भाई का क़याम था, वो उनके किसी अमीर दोस्त की मिल्किय्यत था। जिसने बड़े इसरार के साथ उन्हें वहां रहने पर मजबूर किया था।
ये मकान बंबई के उमरा की रिहाइश-गाहों के दरमियान स्थित ज़रूर था, मगर उसके अंदर कुछ भी नहीं था। कोई पलंग या किसी क़िस्म का फर्नीचर नहीं था। दो-तीन गद्दे, चंद चादरें, डेढ़-दो दर्जन के क़रीब बर्तन और बान के तीन मूंढे जिनमें से एक मुस्तक़िलन (स्थायी तौर पर) बन्ने भाई की स्टडी में रहता था।
वो हमेशा बैठकर अध्ययन करते। यहीं एक मामूली सी मेज़ थी। जिस पर उनकी किताबें, काग़ज़ात और लिखने का सामान रखा रहता था। दिन में वो तक़रीबन तीन घंटे बैठकर अध्ययन करते। इतना ही वक़्त लिखने में इस्तेमाल करते। पार्टी के दफ़्तर में वो तक़रीबन चार-पांच घंटे गुज़ारते। जहां उनकी ज़िम्मेदारी पार्टी के हफ़्तावार अख़बार ‘क़ौमी जंग’ को मुरत्तिब (संपादित) करने तक महदूद थी।
सियासी मज़ामीन वो बिल- उमूम (प्राय:) दफ़्तरी औक़ात (समय) ही में लिखते। घर में अदबी मज़ामीन पर काम करते। वो बहुत पढ़ने वाले शख़्स थे। उर्दू, फ़ारसी के क्लासिकी अदब बिल-ख़ुसूस (ख़ास तौर पर) शुअरा का उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया था। बज़ाहिर वो बहुत कम-गो (कम बोलने वाले) और ख़ामोश इंसान नज़र आते थे। लेकिन बातचीत के दौरान में उनके अध्ययन और अदब से उनकी वाबस्तगी का अंदाज़ा करने में कोई मुश्किल न होती।
उर्दू और फ़ारसी के शुअरा के काम और मुक़ाम के बारे में बाज़ औक़ात लोग उनके साथ घंटों बहस करते। और सुनने वालों को ये फ़ैसला करने में किसी क़िस्म की दुश्वारी न होती कि उन्होंने न सिर्फ़ उन शुअरा का अध्ययन किया है, बल्कि वो उनकी तख़्लीक़ात (लेखन) पर बहुत ग़ौर-ओ-फ़िक्र भी करते रहे हैं।
घर में उस वक़्त बन्ने भाई और उनकी बेगम रज़िया और उनकी तीन बेटियां रहती थीं। नज़मा, उस वक़्त छह साल की थी। नसीम तीन-साढे़ तीन साल की। और तीसरी बहुत छोटी थी। उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं है। उस घर में आने-जाने वालों का हुजूम रहता था। अली सरदार जाफ़री, कैफ़ी आज़मी और मजाज़ तक़रीबन रोज़ाना आने वालों में से थे। जोश ‘शालीमार कंपनी’ से जुड़े हुए थे, जो पूना में थी। वो महीने में दो-एक बार ज़रूर आते। और इस घर में उनके साथ एक निशस्त (बैठक) लाज़िमी होती।
हमारे बंबई पहुंचने के थोड़े ही दिनों बाद कलकत्ता से हिंदू-मुस्लिम फ़सादात की ख़बरें मिलने लगीं। जिनके रद्देअमल के तौर पर बंबई में भी मारामारी शुरू हो गई। और शहर के इलाक़ों में छुरा घौंपने की वारदातें रोज़मर्रा का मामूल बन गईं। बंबई में फ़िरक़ावाराना फ़सादात हमेशा से इसी तरह होते चले आ रहे हैं कि हिंदुओं के इलाक़े में इक्का-दुक्का मुसलमान और मुसलमानों के इलाके़ में कोई अकेला हिंदू छुरे का शिकार कर लिया जाता है। छुरा घौंपने वाला अक्सर वारदात करके किसी गली में गायब हो जाता था। इसी रियायत से इन फ़सादात को मारा-मारी या ‘भुस्का-भुस्की’ का नाम दिया जाता है।
हम उन दिनों वार्डन रोड पर मुक़ीम (ठहरे) थे। ये भी उमरा का पुर-अमन इलाक़ा था। और फ़सादात से बिल्कुल महफ़ूज़। मगर हमें यहां से निकलने बिल-ख़ुसूस सैंडहर्स्ट रोड पर पार्टी के दफ़्तर जाने की इजाज़त नहीं थी। फ़सादात शुरू होने के पन्द्रह रोज़ तक हम वार्डन रोड या मालाबार हिल के सिवा कहीं नहीं गए। जब फ़सादात का ज़ोर कम हुआ और हमें घूमने-फिरने की आज़ादी मिली, तो हम पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे। वहां जाकर मालूम हुआ कि बन्ने भाई इस तमाम अरसे में रोज़ाना मामूल (नियम) के मुताबिक़ दफ़्तर आते रहे।
ये इलाक़ा हिंदुओं बल्कि महासभाईयों का गढ़ था। शहर के किसी भी हिस्से में फ़सादात होते, तो मुसलमान सैंडहर्स्ट रोड और हिंदू भिंडी बाज़ार और मुहम्मद अली रोड का रुख़ न करते। सय्यद सज्जाद ज़हीर को दोस्तों और रफ़ीक़ों (संगी-साथी) ने बहुत समझाने की कोशिश की, कि वो इधर न आएं। मगर वो घर से रोज़ाना मामूल के मुताबिक निकलते और चौपाटी से होते हुए पैदल या ट्राम पर दफ़्तर पहुंच जाते।
उनका कहना था, ‘‘मैं लोगों को हिंदू और मुसलमान के खानों में तक़्सीम नहीं कर सकता। न उन पर बे-एतिमादी (अविश्वास) का इज़हार कर सकता हूं।’’
इस सारे ज़माने में दफ़्तर और घर में लोग उनके बारे में सख़्त फ़िक्रमंद नज़र आते। मगर उन्होंने किसी भी वक़्त किसी क़िस्म की कमज़ोरी का इज़हार नहीं किया। हालांकि सूरत ये थी कि शहर में हिंदुओं के हाथों मुसलमान, और मुसलमानों के हाथों हिंदू क़त्ल हो रहे थे। और सैंडहर्स्ट रोड का कोई गुंडा किसी भी वक़्त सज्जाद ज़हीर के पेट में छुरा घौंप सकता था। मगर उन्होंने उन फ़सादात में अपने मामूलात (दिनचर्या) में कोई फ़र्क नहीं आने दिया। और रोज़ाना दफ़्तर आते रहे।
इंसान की नेकी पर उनका ऐतिमाद (विश्वास) उस हद तक था कि सब कुछ देखते हुए भी अपनी ज़ात की हिफ़ाज़त के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं थे। जिस क़िस्म की ज़िंदगी वो गुज़ार रहे थे, उन्हीं के जैसे लोग उसका हौसला कर सकते थे। वो अगर चाहते तो उनके लिए दुनियावी आसाइशों (सुविधाओं) की कमी नहीं थी। वो सर वज़ीर हसन के बेटे और ऑक्सफोर्ड के तालीमयाफ़्ता थे।
जिस क़िस्म की अमीराना और पुर-आसाइश ज़िंदगी उन्होंने गुज़ारी थी, वो किसी भी आम आदमी को ज़िंदगी भर के लिए नाकारा बना सकती थी, मगर उन्होंने दुनिया को दु:खों से निजात दिलाने, समाजी ग़ैर बराबरी को ख़त्म करने और एक बेहतर दुनिया तामीर करने का इरादा कर रखा था। जिस पर वो ज़िंदगी की आख़िरी सांस तक क़ायम रहे। ये वनवास तो उन्होंने ख़ुद लिया था। अपनी रज़ा (मर्ज़ी) और ख़ुशी के साथ।
सय्यद सज्जाद ज़हीर जैसे लोग रोज़-रोज़ पैदा नहीं होते। बर्र-ए-सग़ीर में तरक़्क़ीपसंद तहरीक के रूह-ए-रवां भी वही थे। उन्होंने बर्र-ए-सग़ीर के अदीबों, शायरों को अदब की सेहतमंदाना रवायात (स्वस्थ्य परंपराओं) की पासदारी (निरीक्षण) का शुऊर (अच्छा-बुरा पहचानने की शक्ति) दिया। वो खु़द नक़्क़ाद, शायर और अदीब थे। ‘लंदन की एक रात’, ‘रौशनाई’, ‘ज़िक्र-ए-हाफ़िज़’, ‘पिघला नीलम’ उनकी हमेशा याद रहने वाली तसनीफ़ात (रचनाएं) हैं।
अगर वो सियासी काम करने की बजाय अदबी काम और तख़्लीक़ी सरगर्मियों पर ज़्यादा तवज्जोह देते, तो शायद उन्हें उर्दू के बहुत बड़े अदीब के तौर पर याद रखा जाता। लेकिन जो काम उन्होंने तन्हा अंजाम दिया, वो मुमकिन है बहुत से इदारे मिलकर भी नहीं कर सकते। और इसके लिए उनका नाम यक़ीनन हमेशा ज़िंदा रहेगा।
(हमीद अख़्तर का लेख, उर्दू से हिंदी लिप्यंतरण- ज़ाहिद ख़ान और इशरत ग्वालियरी)