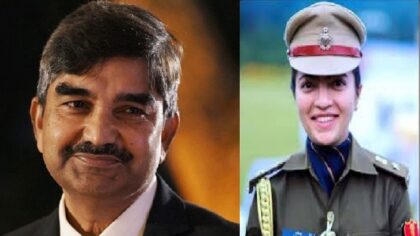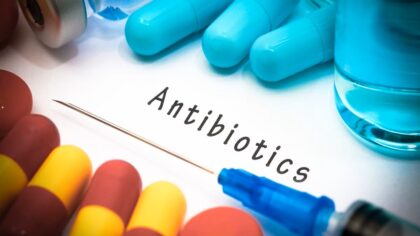अजमेर। पिछले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था वाला देश बना है। केवल आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी इसने दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।
आर्थिक क्षेत्र में मज़बूती का प्रभाव भारत के सामाजिक स्तर पर भी नज़र आने लगा है। लेकिन जिस तेज़ी से भारत में तरक्की हो रही है, उसकी अपेक्षा लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। जिसकी वजह से देश में बेरोज़गारी की दर कम नहीं हो रही है।
देश का कोई राज्य ऐसा नहीं है, जहां बेरोज़गारों की फ़ौज नहीं है। इसका सबसे बुरा प्रभाव देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ रहा है, जहां युवा टेक्निकल स्किल की कमी के कारण रोज़गार की दौर में पिछड़ रहे हैं।
राजस्थान का नाचनबाड़ी गांव भी इन्हीं में एक है, जहां युवा रोज़गार की तलाश में भटक रहे हैं। वह किसी प्रकार मज़दूरी कर परिवार का पेट पाल रहे हैं।
अजमेर से करीब 11 किमी दूर घूघरा पंचायत स्थित इस गांव में लगभग 500 घर हैं, जहां अधिकतर कालबेलिया और बंजारा समुदाय की बहुलता है। जिन्हें सरकार की ओर से अनुसूचित जनजाति समुदाय का दर्जा प्राप्त है।
इस समुदाय के अधिकतर युवाओं के पास रोज़गार का कोई स्थाई साधन नहीं है। वह प्रतिदिन मज़दूरी करने अजमेर जाते हैं। जहां कभी काम मिलता है तो कभी पूरे दिन खाली बैठ कर घर वापस लौट आते हैं।

इस समुदाय की 50 वर्षीय सीता देवी बताती हैं कि उनके दो बेटे हैं। सभी का अपना परिवार है। लेकिन किसी के पास भी रोज़गार का स्थाई साधन नहीं है। वह सभी मज़दूरी करने अजमेर शहर जाते हैं। जहां कभी उन्हें काम मिलता है तो कभी खाली हाथ वापस आ जाते हैं।
पूरे महीने उन्हें 10 से 15 दिन ही काम मिलता है। मिस्त्री के काम में एक दिन में 500 रुपए से अधिक नहीं मिलते हैं। यदि बेलदारी का काम मिला तो 300 रुपए से अधिक नहीं दिए जाते हैं।
इतनी कम आमदनी में एक बड़े परिवार का भरण पोषण करना बहुत मुश्किल होता है। वह कहती हैं कि गांव में शिक्षा के प्रति बहुत अधिक जागरूकता नहीं होने के कारण बच्चे पढ़ाई से भी दूर हो जाते हैं। जो आगे चलकर उनके लिए रोज़गार प्राप्त करने में एक बड़ी रुकावट बन जाती है।
इसी समुदाय की 48 वर्षीय जमना देवी कहती हैं कि जातिगत भेदभाव भी रोज़गार प्राप्त करने में एक बड़ी रुकावट बन जाती है। अक्सर उनके परिवार के पुरुषों को जातिगत भेदभाव के कारण रोज़गार नहीं दिया जाता है। गृह निर्माण के कार्यों से लेकर मज़दूरी के अन्य कामों में भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है।
आय के सीमित साधनों की वजह से परिवार आर्थिक रूप से और भी अधिक कमज़ोर हो जाता है। वह बताती हैं कि उनका बेटा पांचवीं तक पढ़ा हुआ है। इस आधार पर उसे मज़दूरी के अतिरिक्त कहीं भी रोज़गार नहीं मिलता है।
अच्छा रोज़गार प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा की आवश्यकता होती है जबकि अभी भी कालबेलिया समाज में शिक्षा के प्रति पूरी तरह से जागरूकता नहीं आई है।
स्वरोज़गार के संबंध में बात करने पर वह कहती हैं कि कालबेलिया समाज में कोई भी आर्थिक रूप से इतना सशक्त नहीं हैं कि वह खुद का कोई रोज़गार शुरू कर सके और न ही गांव में कोई स्वयं सहायता समूह संचालित है जिससे जुड़कर रोज़गार प्राप्त किया जा सके।
जमना देवी के अनुसार कोरोना काल में कालबेलिया समुदाय को बहुत अधिक आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ा था। गांव में लोगों का रोज़गार चला गया, जिससे परिवार के सामने रोज़ी-रोटी की समस्या खड़ी हो गई थी।
लोगों को घर चलाने के लिए ऊंचे ब्याज दरों पर क़र्ज़ लेना पड़ गया था। इस दौरान उन्हें भी क़र्ज़ लेने पड़े थे और आज भी वह चालीस हज़ार रूपए की कर्ज़दार है। जिसे पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है।
गांव में बंजारा समुदाय की 40 वर्षीय सीमा बताती हैं कि वह और उनके पति कमाने के लिए रोज़ शहर जाते थे। जहां वह दोनों बेलदारी का काम करते थे। लेकिन कुछ सालों से तबीयत ख़राब रहने के कारण अब वह नाचनबाड़ी गांव में घूम-घूम कर सब्ज़ी बेचने का काम करती हैं जबकि पति अभी भी शहर जाते हैं।
वह कहती हैं कि परिवार में 8 सदस्य हैं जबकि घर में उन दोनों के अतिरिक्त कमाने वाला और कोई नहीं है। ऐसे में बहुत मुश्किल से गुज़ारा चल रहा है। सीमा कहती हैं कि गांव में रोज़गार के नाम पर लोग केवल मज़दूरी करना ही जानते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई काम समझ में नहीं आता है।
कुछ युवा आसपास के मार्बल फैक्ट्रियों और चूना भट्टियों में भी काम करते हैं। लेकिन उन्हें बहुत कम मज़दूरी मिलती है। जिससे परिवार का गुज़र बसर बहुत मुश्किल से होता है। वह बताती हैं कि कम आमदनी का प्रभाव बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर ज़्यादा नज़र आता है।
जबकि इस दौरान उन्हें अधिक से अधिक पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है। लेकिन नाममात्र आय वाले घरों में पौष्टिक भोजन का मिलना मुश्किल है। गांव में आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराये जाते हैं, जिससे शारीरिक रूप से उन्हें लाभ मिलता है।
सीमा कहती है कि यदि गांव में ही रोज़गार के साधन उपलब्ध हो जाएं तो कई समस्याओं का निवारण संभव हो सकेगा।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा सोमवार को जारी नवीनतम वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2023 से जून 2024 की अवधि के दौरान बेरोजगारी दर 3.2 प्रतिशत है।
महिलाओं में भी बेरोजगारी दर 2022-23 के 2.9 प्रतिशत की तुलना में 2023-24 के दौरान बढ़कर 3.2 प्रतिशत हो गई है। हालांकि इसी अवधि में पुरुषों की बेरोजगारी दर थोड़ी घटकर 3.3 प्रतिशत की तुलना में 3.2 प्रतिशत हो गई है।
वहीं ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी के दर की बात करें तो यह 2022-23 के दौरान 2.4 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 2.5 प्रतिशत हो गई है। यदि राज्यों के अनुसार बेरोज़गारी की दर देखी जाए तो राजस्थान देश का दूसरा सबसे अधिक बेरोज़गारी वाला राज्य है।
हालांकि केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों की ओर से युवाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।
राजस्थान सरकार की ओर से मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए बैंक से लोन दिया जाता है। इसमें सब्सिडी भी उपलब्ध कराया जाता है।
इस योजना में सरकार द्वारा व्यवसाय के आधार पर 25 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक लोन दिया जाता है। योजना के तहत उपलब्ध कराए जाने वाला लोन बैंकों के माध्यम से दिया जाता है।
इसमें सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है ताकि युवाओं को ऋण चुकता करने में कोई मानसिक दबाव न पड़े। इसके अतिरिक्त इस वर्ष के केंद्रीय बजट में भी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर भी खास फोकस करते हुए रोज़गार सृजन की बात की गई है।
इसके लिए स्किल डेवलपमेंट से लेकर एजुकेशन लोन, अप्रेंटिसशिप के लिए इंसेंटिव, ईपीएफ में अंशदान के साथ पहली नौकरी पाने वालों के लिए सैलरी में योगदान और न्यू पेंशन सिस्टम के लिए योगदान में बढ़ोतरी जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट (आईएचडी) की रिपोर्ट “इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024” के अनुसार भारत में 2021 के दौरान सभी प्रवासियों में से करीब 10.7 फीसदी ने रोजगार कारणों से पलायन किया था। इनके पलायन के लिए बेहतर रोजगार की तलाश और अपने क्षेत्र में अवसरों की कमी जैसे कारक प्रमुख रहे थे।
यह स्थिति बताती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। दरअसल देश के अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार की कमी के कारण लोगों की एक बड़ी संख्या बड़े महानगरों और औद्योगिक इलाकों का रुख करती है।
हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा एक महत्वपूर्ण साधन है। जिसने लोगों को गांव में ही रह कर रोज़गार उपलब्ध कराया है। वहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप भी गांवों में रोज़गार उपलब्ध कराने का सबसे सशक्त माध्यम बन रहा है।

वर्तमान में, देश में लगभग 6.6 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं, जिनसे करीब 70 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 2025 तक लगभग 80 मिलियन परिवारों को इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। देश के सभी राज्य सरकारों द्वारा भी इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है।
इसी वर्ष राजस्थान सरकार ने भी अपने बजट में अगले पांच सालों में दो लाख और एक साल में करीब चालीस हजार नए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने का लक्ष्य रखा है।
सरकार का यह लक्ष्य यकीनन ग्रामीण स्तर पर न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, बल्कि इससे गांवों से होने वाले पलायन को रोकने में भी मदद मिलेगी।
आवश्यकता इस बात की है कि युवाओं और समाज के सभी वर्गों को इससे जोड़ा जाए, उन्हें आसानी से लोन उपलब्ध कराया जाए और इस दिशा में उनका मार्गदर्शन किया जाए।
यदि गांवों तक रोज़गार को पहुंचाया जाए तो न केवल ग्रामीण क्षेत्र आर्थिक रूप से सशक्त होगा, बल्कि शहरों और महानगरों पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा।
(अजमेर से नमीरा बानो की ग्राउंड रिपोर्ट।)