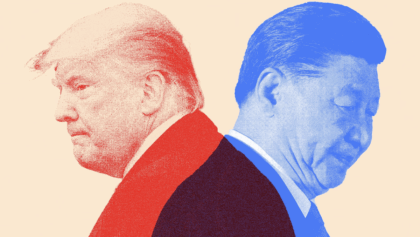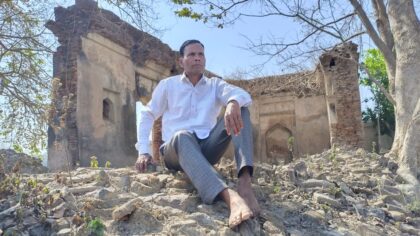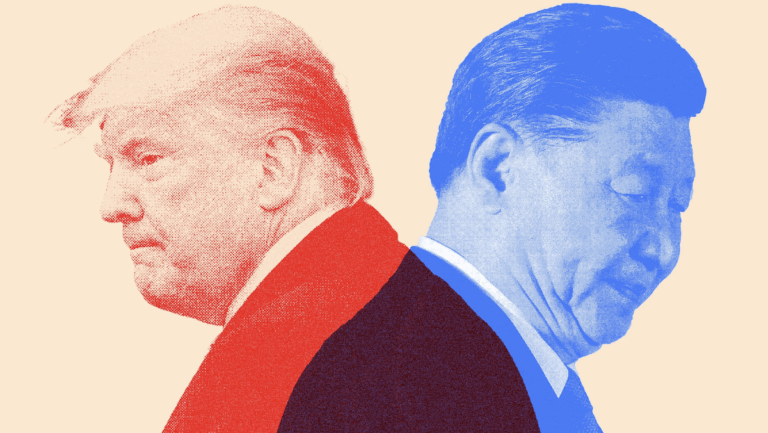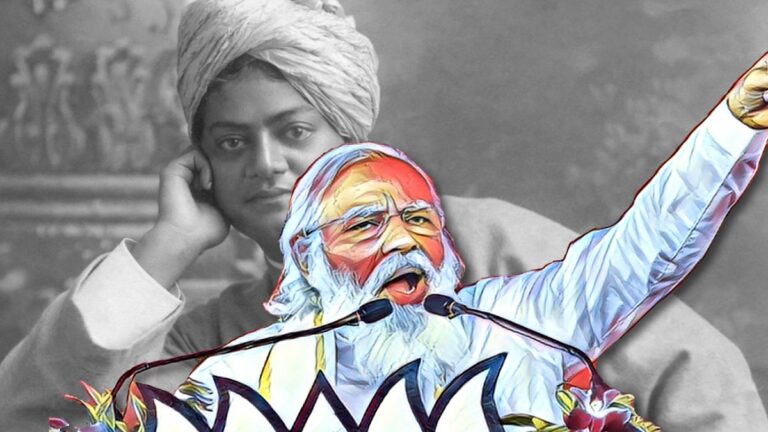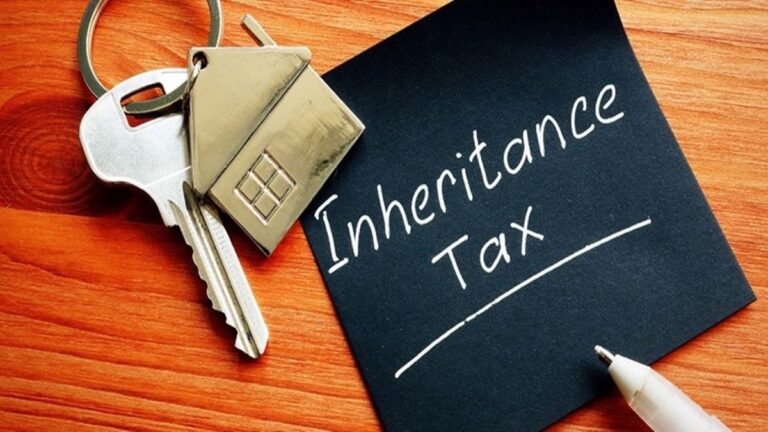एक प्रेक्षक मोंटगोमरी मार्टिन ने भारत से संपदा के इस पलायन की भर्त्सना की। उन्होंने अपनी गणना द्वारा बताया कि 1833 तक तीन दशक में 72.4 करोड़ पाउंड संपदा का दोहन हो चुका था। उन्होंने कहा कि पिछले पचास साल में 840 करोड़ पाउंड संपदा का दोहन हो चुका था। उन्होंने कहा कि, “ऐसे दोहन से अब तक इंग्लैंड भी गरीब हो चुका होता, फिर भारत पर इसका कैसा प्रभाव हुआ होगा इसे समझा जा सकता है जहां मजदूरी बेहद ही कम है।”
1833 में भारत और चीन के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी की इजारेदारी खत्म हो गई। ऐसा उन अंग्रेज उद्योगपतियों के दबाव पर हुआ, जो भारतीय टेक्सटाइल को यूरोपीय बाजारों से हटाने के बाद अब भारत के बाजार पर एकछत्र राज चाहती थी। हालांकि कंपनी 1857 से 59 तक चले महाविद्रोह तक राज करती रही।
ब्रिटेन को भारत का निर्यात घट गया।
भारत के सूती कपड़ा उद्योग को नष्ट करने के बाद, ब्रिटेन से धागे और कपड़े का आयात तेजी से बढ़ गया। और 1840आते आते उसके साथ भारतीय व्यापार घाटे में चला गया। लेकिन दुनियां के और देशों को भारत का निर्यात बढ़ता गया और वह ब्रिटेन से होने वाले नए घाटे से बहुत अधिक था। तो कुल मिलाकर बढ़ता हुआ व्यापारिक निर्यात सरप्लस हमेशा बना रहा।
सोने के आयात को घटाने के बाद भी यह बहुत अधिक था।
जिसे इरफान हबीब शुल्क वसूली कहते हैं,उसकी समस्या को फिलहाल उन देशों को भारत से निर्यात बढ़ाकर पूरा कर लिया गया जिनसे ब्रिटेन का व्यापार घाटे में था। चीन तक अफीम निर्यात को बढ़ाने का अभियान, जहां यह गैर कानूनी था और अफीम युद्ध में इसके बंदरगाहों को जबरदस्ती खोलना, वह इस त्रिकोणीय व्यापार पैटर्न को बढ़ावा देने की प्रक्रिया का ही हिस्सा था।
भारत में स्थानीय किसानों को राज्य एकाधिकार के तहत जबरदस्ती बेहद कम दाम पर अफीम पैदा करने के लिए बाध्य किया गया और उससे चीन के साथ ब्रिटेन का जो व्यापार घाटा था उसे खत्म किया गया।
1800की तुलना में 1820 तक कुल राजस्व संग्रह तीन गुना हो गया। क्योंकि बॉम्बे डेक्कन और मद्रास भू राजस्व बंदोबस्त के तहत आ गए।
उधर नमक और अफीम पर इजारेदारी से और राजस्व आने लगा। संपदा का पलायन बढ़ गया, लेकिन अब यह पहले के ब्रिटेन के साथ सीधे व्यापारिक निर्यात सरप्लस की तुलना में अधिक घुमावदार तरीके से होने लगा। क्योंकि वह सीधा सरप्लस घाटे में बदल गया था। Tribute वसूली की समस्या के समाधान के लिए एक अधिक सामान्य समाधान की जरूरत थी। समाधान 1861 में प्रभाव में आया जब भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी के हाथ में आ गया।
यह सामान्य और प्रभावी था। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत मामलों के सचिव ने भारत के समानों के विदेशी आयातकों को आमंत्रित किया कि वे भारत से आयात के बदले सोना, स्टर्लिंग और अपनी मुद्राएं उनके पास जमा करें। इसके बदले उन्हें विनिमय का एक अधिकारिक बिल दिया जाएगा जो भारत में कैश होने वाले रुपए के समतुल्य होगा।
ये काउंसिल के बिल जिस मूल्य पर बेचे जाते थे, उनकी विनिमय दर समय-समय पर इस तरह adjust की जाती थी कि जिससे कि विदेशी आयातकों को कभी भी भारतीय निर्यातकों को भुगतान में सोना देना कभी भी सस्ता न पड़े, ट्रांसपोर्ट की कीमत जोड़ने के बाद वह मिस्र से आ रहा हो या ऑस्ट्रेलिया से, लंदन के काउंसिल बिल के रास्ते की तुलना में।
विनिमय दर को इस तरह लागू किया जाता था कि वित्तीय सोना का आयात भारत में न पहुंचने पाए।
भारतीय सामानों के विदेशी आयातक
वे किसी निजी भुगतान की तुलना में काउंसिल बिल को ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि वे निश्चिंत हो सकते थे कि बिल का हमेशा सम्मान होगा क्योंकि वह ब्रिटिश सरकार के एक मंत्र द्वारा जारी किया गया था।
काउंसिल बिल केवल रूपए में कैश हो सकते थे। भारत के निर्यातक जो विदेशी आयातकों से काउंसिल बिल पाने के बाद विनिमय बैंक से उसे कैश करा सकते थे। निर्यातक बदले में जिनसे सामान लिए थे उन्हें भुगतान करते थे। इस तरह पुराने संपदा पलायन का मूल चरित्र बरकरार था। उत्पादकों को भुगतान किया जाता था लेकिन अपने निर्यात सरप्लस के लिए नहीं। क्योंकि उन्हें जो भुगतान किया जाता था वह उनसे वसूले गए टैक्स का ही एक हिस्सा होता था।
निर्यात सरप्लस कर राजस्व का ही माल रूप commmodity फार्म था। हालांकि इस आधिकारिक प्रणाली का दायरा कंपनी राज की तुलना में ज्यादा व्यापक था, इस अर्थ में कि पूरी दुनियां से ब्रिटिश भारत की कुल निर्यात सरप्लस की कमाई हड़प ली जा रही थी। आय का आंतरिक पुनर्वितरण भी इस प्रणाली के तहत उत्पादक वर्गों से व्यापारी वर्ग की ओर हो रहा था। कुल माल निर्यात से सरप्लस कमाई 1871 से,1901के बीच भारतीय राजस्व पर इंग्लैंड द्वारा लगाए गए कुल खर्च के समतुल्य था।
यहां यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि council bills के माध्यम से चुकाया गया यह सरप्लस व्यापार में लाभ और सोने के रूप में लाभ का कुल योग है। यह स्पष्ट है कि भारत की निर्यात सरप्लस कमाई में आंतरिक कारकों तथा वैश्विक बाजार की स्थितियों के कारण काफी उतार चढ़ाव होता था। लेकिन इस कमाई का उपयोग करके इंग्लैंड द्वारा स्टर्लिंग खर्च धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था।
1861से शुरू हुए नई व्यवस्था में कंपनी राज की सीधी व्यवस्था के मूल पहलू बने रहे। उपनिवेश के उत्पादकों को उन्हीं से वसूले गए टैक्स से निर्यात सरप्लस का भुगतान किया जाता था। और इसलिए दरअसल उन्हें कुछ नहीं मिलता था। यह दरअसल पूंजीवादी केंद्रों को मिलता था, इससे होने वाली दुनिया भर से कमाई, सोने और विदेशी मुद्रा के रूप में।
भारत के विदेशी निर्यातकों से मिलने वाले सोने का एक छोटा हिस्सा हो सकता है कि आर्थिक नियंत्रण की व्यवस्था से बच जाता हो और भारत पहुंच जाता हो, शायद princely states के बंदरगाहों से होकर। लेकिन पूरी संभावना है कि यह बहुत कम रहता हो और इसकी गणना भी असंभव है। लेकिन भारत के माल निर्यात सरप्लस का दुनियां के भुगतान का बहुत बड़ा हिस्सा सफलता पूर्वक ब्रिटेन द्वारा हड़प लिया जाता था। और वह कभी भी उपनिवेशों के उत्पादकों तक नहीं पहुंचने दिया जाता था, जिन्होंने अपनी मेहनत से उसे कमाया है, चाहे सोने के रूप में या वित्तीय भुगतान के रूप में या विदेशी मुद्रा के रूप में।
न तो औपनिवेशिक सरकार को भारत की उस विदेश से अर्जित कमाई का कोई हिस्सा मिलता था जिसे वह रूपये में बदल सके, जैसा किसी भी संप्रभु देश में होता है। इसके विपरीत, लंदन में बैठा अंग्रेज विदेश मंत्री इंग्लैंड में खर्च हुए या विदेश में खर्च हुए धन के रूप में भारत के बजट के इस हिस्से पर अपना आधिकारिक दावा करता था। यह न सिर्फ आय को कम करने वाला था। बल्कि रूपये की कमी और ब्याज दर को हमेशा ऊंचा बनाए रखने का काम करता था।
गणना में भारत का विशाल और बढ़ता हुआ माल निर्यात सरप्लस बताया जाता था कि वह राज्य द्वारा संचालित अदृश्य खर्चों द्वारा पूरी तरह प्रतिस्ंतुलित हो जाता था। पर यह केवल बार बार होने वाले संपदा के पलायन तक सीमित नहीं था। 1837 से लेकर1900 तक यह पलायन 59.6 करोड़ पाउंड था। 1861से यह काउंसिल बिल से होने लगा। 1947 तक यह 28 अरब पाउंड हो जाता है।
1765 से 1947 तक यह 397 अरब पाउंड हो जाता है। यह 1947 में इंग्लैंड के कुल जीडीपी का 38 गुना है। डॉलर में यह 1.9 ट्रिलियन हो जाता है। यह 1947 में इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा के कुल जीडीपी से ज्यादा है।
हमारा अनुमान कमतर ही है। यह भारत से इंग्लैंड जाने वाले कुल संपदा का एकदम सटीक मूल्यांकन नहीं है। बहरहाल कुल अदृश्य मांग हमेशा भारत के विदेशी मुद्रा अर्जन से, वह चाहे जितना तेज बढ़ रहा हो, अधिक दिखाई जाती थी। इसलिए हमको हमेशा ब्रिटेन का ऋणी बनाए रखना थोपी हुई नीति के तहत था। भारत की विराट विदेशी कमाई न जाने किस जादू से लंदन के विदेश सचिव के कार्यालय में उड़ जाती थी और भारत को हमेशा घाटे में दिखाया जाता था।
सच्चाई यह है कि भारत की अपनी सोने की और निर्यात सरप्लस से होने वाली विदेशी मुद्रा अगर इसे मिल जाती, आंशिक रूप से पूरा नहीं भी, तो वह इतनी अधिक थी कि भारत जापान की 1868 की मैजी क्रांति से पहले ही टेक्नोलॉजी आयात करके बहुत पहले ही आधुनिक औद्योगिक ढांचा बना सकता था। या पूंजी निर्यात कर सकता था और उसे उधार न लेना पड़ता।
1860 और 1870 दशक के कच्चे कपास के भारी उछाल के दौर में भारी विदेशी कमाई से भारतीय रेलवे कई गुना बनाई जा सकती थी। 1860 से 1876 के बीच भारत का निर्यात सरप्लस 13.5 करोड़ पाउंड था, जबकि सिंचाई और रेलवे पर खर्चा मात्र 2.6 करोड़ डॉलर था।
लेकिन क्योंकि भारत का सारा सोना और अर्जित विदेशी मुद्रा इंग्लैंड हड़प लेता था, इसलिए भारत पर रेलवे आदि के लिए लंदन के मुद्रा बाजार से कर्ज लेना थोप दिया जाता था। यह कर्ज निजी कर्ज दाताओं से भारी ब्याज दर पर लेकर औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारत पर थोप दी जाती थी, बिना यह समझे कि रेलवे से कितना लाभ हो रहा है।
भारत की सारी विदेशी कमाई लंदन में अंग्रेज मंत्री (Secretary of State) के खाते में चली जाती थी और फिर accounting में वह सब अदृश्य liability के नाम पर खत्म हो जाती थी। प्रशासनिक खर्च, सेना पर खर्चे, ऋण पर ब्याज आदि। कुल home चार्जेज का केवल 12.7% प्रशासनिक खर्चे थे। स्टर्लिंग में चुकाया जाने वाला कर्ज का ब्याज सबसे बड़ा खर्चा था, होम चार्जेज का करीब आधा।
ऐसा इसलिए नहीं था कि बहुत अधिक निवेश आ रहा था। (पूरे उपमहाद्वीप को कुल ब्रिटिश विदेशी निवेश का शायद 10% मिला होगा।) बल्कि इसलिए कि हर बड़े बाहरी खर्च को पूर्णतः या आंशिक रूप से भारतीय राजस्व से वसूला जाता था और वह भारत के निर्यात सरप्लस से जहां ज्यादा होता था उसे भारत के स्टर्लिंग ऋण में जोड़ दिया जाता था।
इन अतिरिक्त खर्चों में शामिल था, भारतीय सीमाओं के बाहर ब्रिटेन के साम्राज्यवादी युद्ध, 1857 के महासंग्राम के दमन में हुआ खर्च, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज जब खत्म हुआ तो उसके शेयर होल्डर्स को भारतीय बजट से भुगतान, लाल सागर और मॉरिशस से केप टाउन तक टेलीग्राफ लाइन का खर्चा, तमाम देशों में ब्रिटेन के मुकदमों का खर्चा आदि। ये सारी कीमतें जो भारत के तेजी से बढ़ती विदेशी कमाई से हमेशा ज्यादा होती थीं, सब भारत के ऋण में जोड़ दी जाती थी। इसमें 9 गुना छलांग लगी, जब 1857 के महाविद्रोह के दमन के खर्चे को इसमें जोड़ दिया गया।
स्टर्लिंग ऋण 1870 में फिर बढ़कर दोगुना हो गया और 1880 दशक और फिर 1891 में रुपए में ऋण में भारी छलांग लगी जब सरकार ने मौद्रिक सोना रिजर्व जरूरतों के लिए आयात किया। 1901 तक, कुल ऋण 13.5 करोड़ पहुंच गया। जो ब्रिटिश भारत के जीडीपी का पांचवां हिस्सा और इसके वार्षिक निर्यात सरप्लस कमाई का आठ गुना हो गया।
सदी के मोड़ पर, मौद्रिक सोने के 80% को जो भारी भारतीय खर्च पर औसतन किया गया था, उसे लंदन भेज दिया गया। भारत से कई साल तक आते यह भारतीय सोना जिसका वहां की निजी निवेश कंपनियां लंबे समय से इंतजार कर रही थीं, कम ब्याज पर उन्हें ऋण का आधार बना।
क्योंकि ब्रिटेन की सरकार भारत पर थोपी जाने वाली अदृश्य liabilities को नियंत्रित करती थी, वह निर्यात सरप्लस कमाई से अपने हिसाब से उन्हें एडजस्ट करती थी। यह विदेशी कमाई से इसे एडजस्ट करने तक ही सीमित नहीं रहती थी बल्कि जब उसे अतिरिक्त फंड की जरूरत होती थी तो कर्ज भी थोप देती थी। यह समायोजन हमेशा असमान ढंग से होता था। जब भारत की निर्यात सरप्लस कमाई तेजी से बढ़ जाती थी, तो आम पलायन के आइटम्स के साथ बहुत सी नई मांगे उसमें जोड़ दी जाती थी जिससे इस कमाई को ब्रिटेन स्थानांतरित किया जा सके।
1919 में जब निर्यात सरप्लस 11.4 करोड़ पाउंड पर पहुंच गया तो भारत से आयातित 6.7 करोड़ पाउंड नहीं दिया गया और उसे जबरदस्ती भारत का युद्ध में योगदान मान लिया गया।
इसके अलावा तमाम उपहार अंग्रेजों द्वारा खुद को ही सौंप लिए जाते थे। उदाहरण के लिए दस करोड़ पाउंड (जो भारत के कुल वार्षिक बजट से अधिक था ) का उपहार प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड ने ले लिया जिसके बारे में किसी भारतीय को पता नहीं था। अगले साल 4.5 करोड़ का उपहार दे दिया गया, जाहिर है इन दोनों से भारत के कर्ज का बोझ बढ़ गया।
लेकिन जब भारत की विदेशी कमाई गिर जाती थी, वैश्विक मंदी आदि के कारण, तब जो धन लिया जाता था, उसे भारत पर उधार माना जाता था। यहां तक कि महामंदी के सालों में, जब भारत की निर्यात कमाई तेजी से गिर गई, तब भी शुल्क कम नहीं किया गया जिससे थोपे गए ऋण के साथ भारत से सोने का ब्रिटेन की ओर दोहन पलायन भी जारी रहा।
अदृश्य बोझों की ऐसी तिकड़मों के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करती रही कि भारत का करेंट अकाउंट हमेशा घाटे में रहे, इसका व्यापारिक निर्यात चाहे जितना भी अधिक हो।
नौरोजी और दत्त दोनों इस बात को लेकर बेहद सचेत थे कि जब देश के उत्पादकों से वसूले गए धन को पूरी तरह देश के अंदर खर्च नहीं किया जा रहा है, तो इसका एक ही अर्थ है कि उत्पादकों को निचोड़ा जा रहा है।
दत्त ने 1830 में लिखे इस लेख को उद्धृत किया,” ग्रेट ब्रिटेन को दिया जाना वाला tribute हमारी मौजूदा नीति में सबसे आपत्तिजनक चीज है। किसी देश में इकट्ठा किया जाने वाला टैक्स अगर उसी देश में खर्च किया जाता है तो वह बिल्कुल अलग चीज है, उस टैक्स की तुलना में जो दूसरे देश में खर्च किया जाता है। जहां तक राष्ट्रीय उत्पादन पर इसके असर की बात है, तो दूसरे देश को देना उसे समुद्र में फेंक देने के बराबर है।” वे सही थे।
बड़े पैमाने पर सरप्लस बजट से जनता की क्रयशक्ति गिरती जा रही थी। आय की कमी ने उत्पादकों की मूल खाद्यान्न के उपभोग को घटा दिया। इसने खाद्यान्न उत्पादन की जमीन के क्षेत्रफल को घटा दिया, उसे निर्यात उत्पाद के लिए उपलब्ध करा दिया और खाद्यान्न निर्यात को बढ़ा दिया। ब्रिटिश भारत में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन में लगातार होने वाली गिरावट आय में इस गिरावट का सबूत है।
विंगेट के रेखांकन में यह जोड़ा जाना चाहिए कि औपनिवेशिक शासकों के लिए भारतीय बजट में टैक्स राजस्व इंग्लैंड में खर्च के रूप में अलग रख दिए जाते थे, समुद्र में नहीं फेंके जाते थे। जो उससे भारी मात्रा में सामान मुफ्त में ले जाया जाता था और जो उसके उपयोग से अधिक होता था उसका दूसरे देशों को पुनर्निर्यात कर दिया जाता था।
अंग्रेजों के पहले के शासक, जिनमें आक्रांता भी शामिल थे, भी टैक्स वसूलते थे, लेकिन वे घरेलू आबादी का स्थाई हिस्सा बन गए थे और वे सारा सरकारी खजाना देश के अंदर ही खर्च करते थे। वे कर से कोई निर्यात नहीं करते थे, जिससे संपदा का पलायन हो इसलिए ब्रिटिश शासन जैसा उनकी आय में कोई कमी नहीं होती थी।
नौरोजी और दत्त ने बताया कि देश के बाहर तमाम खर्चे हमारे बजट से किए जाते थे क्योंकि हम उपनिवेश थे, इस तरह हमारी सम्पदा का पलायन होता था। वे ब्रिटेन के सीधे फायदे के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। होम चार्जेज भारत में शासन के खर्चे नहीं थे, भारत में काम करने वाले अंग्रेज चाहे वे नागरिक सेवा में हों या सैन्य सेवा में, उन्हें नियमित तनख्वाह भारत के घरेलू बजट खर्च के रूप में दी जाती थी।
छुट्टी और पेंशन भत्ते आदि 1861,से 1934 तक केवल 12.7% थे। होम चार्जेज का 77%से ऊपर उस ऋण के ब्याज पर खर्च होता था जो देश के बाहर उस समय सेना पर खर्च होता था। 10% सरकारी स्टोर की खरीद पर खर्च होता था। भारत के बाहर औपनिवेशिक युद्धों पर खर्च पूर्णतः या आंशिक रूप से भारतीय राजस्व से वसूला जाता था। यह परजीवी पैटर्न विनाशकारी ढंग से 1941से 1946 के बीच भी दोहराया गया जब दक्षिण एशिया में युद्ध का विराट खर्च भारत पर डाल दिया गया। जिसके फलस्वरूप भारत में 30 लाख से अधिक लोगों की भूख से मौत हो गई।
हमने चर्चा किया कि कैसे अंग्रेजों द्वारा उपनिवेशों के सरप्लस के एक हिस्से को हड़प लिया जाता था। जो उपनिवेशों से संपदा का पलायन था। यदि काल्पनिक रूप से मान भी लिया जाय कि ब्रिटिश प्रशासकों व सिपाहियों की पेंशन आदि का खर्चा राजस्व से न वसूला जाता, तो अंग्रेजों द्वारा वसूली के लिए इनकी जगह कुछ दूसरे तरकीबें निकाल ली जातीं। मसलन यह कि रानी के कुछ महलों की मरम्मत के लिए इसे लिया जा रहा है क्योंकि वह यहां की शासक है!
……..समाप्त।
( प्रो प्रभात पटनायक और प्रो उत्सा पटनायक के लंबे लेख का संक्षिप्त भावानुवाद है। साभार Monthly Review, अनुवाद लाल बहादुर सिंह )