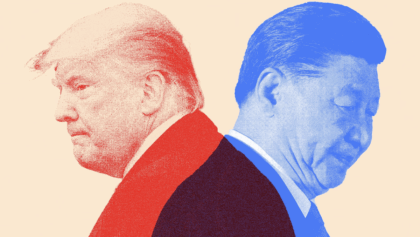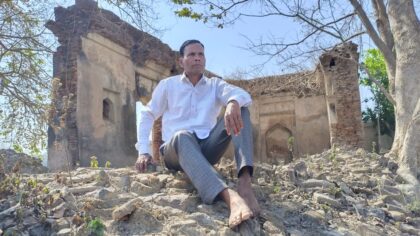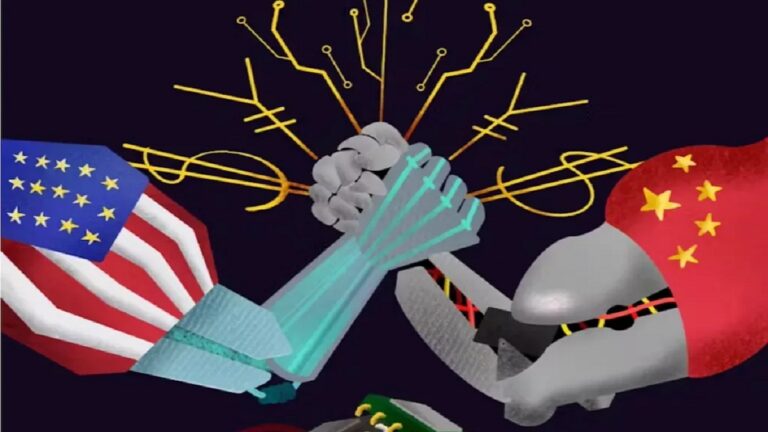2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा (LoC) पर युद्धविराम की पुष्टि केवल दोनों देशों की आपसी बातचीत या क्षेत्रीय कूटनीति का नतीजा भर नहीं है। यह फैसला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदलते भू-राजनीतिक हालात और खासकर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा से गहराई से जुड़ा है। यह लेख इस युद्धविराम को उस वैश्विक राजनीति के संदर्भ में समझने की कोशिश करता है, जिसमें दक्षिण एशिया की रणनीति, अस्थिरता और दोनों देशों की अंतरराष्ट्रीय मजबूरियां शामिल हैं।
भारत-पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से तनाव और सीमित संवाद के बीच झूलते रहे हैं। लेकिन, 2025 में हुआ यह युद्धविराम उस समय आया है, जब पूरी दुनिया दो ध्रुवों, अमेरिका और चीन में बँटती जा रही है। ऐसे में यह फ़ैसला कोई भरोसे पर आधारित पहल नहीं, बल्कि एक मजबूरी है, जो वैश्विक दबावों और रणनीतिक परिस्थितियों के तहत लिया गया है। यह युद्धविराम आपसी समझ से कहीं ज़्यादा अंतरराष्ट्रीय संतुलन बनाए रखने का प्रयास है।
2020 के दशक में अमेरिका और चीन के बीच भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और तेज़ हुई है, जो अब विशेष रूप से एशिया में सैन्य, तकनीकी और आर्थिक मोर्चों पर लड़ाई का रूप ले चुकी है।
पिछले कई सालों में अमेरिका ने भारत से अपने रिश्ते इसलिए मज़बूत किए हैं, क्योंकि वह भारत को चीन का मुक़ाबला करने वाली एक बड़ी शक्ति के रूप में देखता है। सैन्य सहयोग, व्यापार और ‘क्वाड’ जैसे मंचों के ज़रिए अमेरिका ने भारत को अपनी ‘इंडो-पैसिफिक रणनीति’ में प्रमुख भागीदार बनाया है।
दूसरी तरफ़, चीन ने ख़ासकर चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान से अपने संबंध और भी मज़बूत बनाए हैं। चीन ने पाकिस्तान को वित्तीय मदद, बुनियादी ढांचे में निवेश और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक समर्थन देकर अपना स्थायी साथी बनाए रखा है।
इस स्थिति में दक्षिण एशिया एक अप्रत्यक्ष टकराव का मैदान बन गया है, जहाँ छोटे-छोटे संघर्ष और युद्धविराम भी वैश्विक असर रखते हैं।
इस समय पाकिस्तान एक बेहद संवेदनशील दौर से गुज़र रहा है। यह देश एक साथ कई मोर्चों पर गहरे संकट में फंसा हुआ है। आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और आंतरिक सुरक्षा सभी क्षेत्र चुनौतीपूर्ण हो चुके हैं।
आर्थिक रूप से पाकिस्तान की हालत नाज़ुक है। महंगाई दो अंकों में बनी हुई है, विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो चुके हैं और कर्ज़ का बोझ लगातार बढ़ रहा है। IMF से मिले राहत पैकेज और चीन और खाड़ी देशों से आर्थिक मदद के बावजूद देश में संरचनात्मक सुधार नहीं हो सके हैं। बेरोज़गारी बढ़ रही है, उद्योग ठप हैं और मुद्रा अवमूल्यन के कारण आवश्यक वस्तुओं का आयात मुश्किल होता जा रहा है। अर्थव्यवस्था कर्ज़ के जाल में फँस गई है, विकास की गति रुकी हुई है।
राजनीतिक मोर्चे पर, देश में गहरा ध्रुवीकरण है। सेना की भूमिका अब भी नागरिक संस्थानों पर हावी है, जिससे लोकतंत्र कमज़ोर हुआ है। 2024 के आम चुनावों के बाद उत्पन्न विवाद, विपक्षी दलों का असंतोष और बार-बार होने वाले विरोध प्रदर्शन जनता का भरोसा तोड़ रहे हैं। मीडिया पर नियंत्रण और असहमति की आवाज़ों को दबाने से अस्थिरता और बढ़ी है।
कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान की स्थिति अलग-थलग पड़ने जैसी है। चीन के साथ घनिष्ठ संबंध बने ज़रूर हैं, लेकिन पश्चिमी देशों से रिश्तों में खटास आई है। भारत, अफ़ग़ानिस्तान और ईरान के साथ भी तनाव बना हुआ है।
सुरक्षा के मोर्चे पर ख़ैबर पख़्तूनख़्वा और बलूचिस्तान में आतंकवादी हमले अब भी जारी हैं। पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी रणनीति अस्पष्ट और असंगत मानी जा रही है।
कुल मिलाकर, पाकिस्तान एक गहरे संकट के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, जहां से निकलने के लिए उसे आंतरिक सुधार, लोकतांत्रिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सहयोग की सख़्त ज़रूरत है।
ऐसे में पाकिस्तान के लिए 2025 का यह युद्धविराम कई राष्ट्रीय संकटों से निकलने का एक साधन है। उसकी अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है। महंगाई, कर्ज़ और IMF जैसे संगठनों पर निर्भरता बढ़ गई है।
आतंकवाद के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की छवि अब भी संदेह के घेरे में है, हालांकि, वह FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुका है। लेकिन, उसे खाड़ी देशों और पश्चिमी दुनिया से लगातार दबाव मिल रहा है।
चीन चाहता है कि पाकिस्तान के पश्चिमी इलाक़ों, खासकर गिलगिट-बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान में स्थिरता बनी रहे, ताकि उसके निवेश सुरक्षित रह सकें।
इसलिए, पाकिस्तान ने यह युद्धविराम एक कूटनीतिक विराम के रूप में अपनाया है, ताकि अंदरूनी हालात कुछ समय के लिए संभाले जा सकें और अंतरराष्ट्रीय आलोचना से बचा जा सके।
ऐसा भी नहीं है कि भारत की ओर से यह युद्धविराम किसी तरह की कोई नरमी है, बल्कि एक रणनीतिक संयम का संकेत है, जो मौजूदा वैश्विक और क्षेत्रीय हालात को ध्यान में रखकर लिया गया है।
चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) , विशेषकर पूर्वी लद्दाख में पर चल रहे तनाव भारत को एक साथ दो मोर्चों पर युद्ध की आशंका से घेरते हैं।
भारत अपनी वैश्विक आर्थिक और कूटनीतिक स्थिति को मज़बूत करना चाहता है (जैसे G20, I2U2, क्वाड), और युद्ध जैसे हालात उसे इस दिशा से भटका सकते हैं।
पाकिस्तान पर भरोसा न होने के बावजूद, रणनीतिक हलकों में यह समझ है कि अगर नियंत्रण रेखा पर शांति बनी रहे, तो भारत अपने असली प्रतिद्वंद्वी यानी चीन पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।
इसलिए, यह युद्धविराम मिलन नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं को फिर से व्यवस्थित करने की रणनीति है।
चाहे औपचारिक रूप से मध्यस्थता न कर रहे हों, लेकिन चीन और अमेरिका दोनों की दिलचस्पी क्षेत्रीय स्थिरता में है। चीन चाहता है कि पाकिस्तान का पश्चिमी सीमा क्षेत्र शांत रहे, ताकि वह अपना ध्यान ताइवान, दक्षिण चीन सागर और पश्चिमी देशों के साथ आर्थिक तनाव पर केंद्रित कर सके।
अमेरिका को भारत-पाकिस्तान के बीच शांति से यह फ़ायदा है कि भारत अपनी ऊर्जा और संसाधन इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में लगाए और चीन का प्रभाव सीमित कर सके। इसलिए, यह युद्धविराम भले ही दो देशों के बीच हो, लेकिन इसे वैश्विक ताक़तों की मौन सहमति मिली हुई है।
यह सोचना जल्दबाज़ी होगी कि 2025 का युद्धविराम भारत-पाकिस्तान रिश्तों में नए युग की शुरुआत है। कश्मीर, आतंकवाद और विश्वास की कमी जैसे मूल विवाद अब भी जस के तस हैं। इसके अलावा, आतंकी संगठनों या अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाओं के कारण यह युद्धविराम कभी भी टूट सकता है। अभी यह शांति एक अंतरराष्ट्रीय संतुलन पर टिकी अस्थायी स्थिति है, कोई स्थायी समाधान नहीं।
इस तरह, भारत-पाकिस्तान के बीच का यह युद्धविराम दिखाता है कि दक्षिण एशिया की राजनीति अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रह गयी है, बल्कि वैश्विक ताक़तों की चालों से प्रभावित हो रही है। घरेलू राजनीति और पुरानी दुश्मनियां अब भी हैं, लेकिन इस बार युद्ध से बचाव का असली कारण अंतरराष्ट्रीय दबाव और रणनीतिक पुनःसंतुलन है।
जब तक अमेरिका-चीन टकराव बना रहेगा, दक्षिण एशिया की स्थिरता भी उन्हीं ताक़तों के फ़ैसलों पर निर्भर रहेगी। यह युद्धविराम कब तक टिकेगा, यह केवल भारत और पाकिस्तान पर नहीं, बल्कि वॉशिंगटन और बीजिंग की रणनीतियों पर भी निर्भर करेगा।
(उपेंद्र चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हैं।)