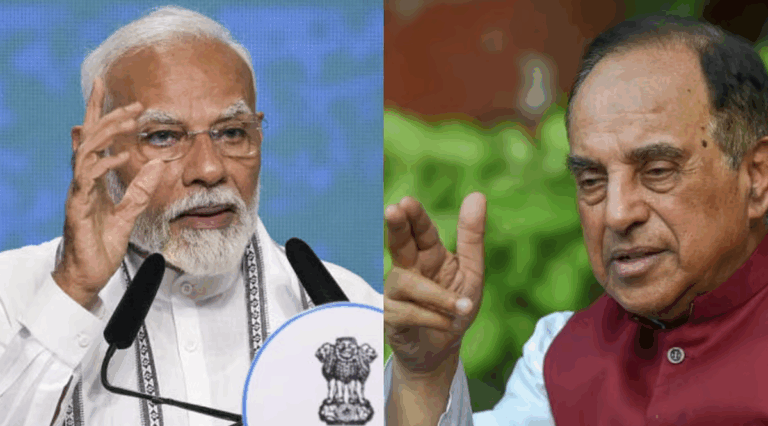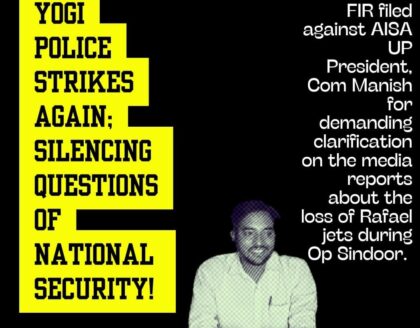एक सरकारी रिपोर्ट के हवाले से देश के कई राज्यों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए छात्रों के कुल पंजीकरण की संख्या को कई मीडिया संस्थानों ने प्रकाशित किया। इसमें पंजीकरण से बाहर रह गए बच्चों की कुल संख्या पिछले सत्र की तुलना में दी गई थी। ये संख्याएँ पिछले कुछ सालों से आमतौर पर बढ़ती दिख रही हैं। कुछ ही राज्य हैं, जिनमें कुछ उतार-चढ़ाव के साथ स्थिति स्थिर है। लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थिति काफी हैरान करने वाली है।
2023-24 में उत्तर प्रदेश में इस स्तर के कुल पंजीकरण की संख्या 1.74 करोड़ थी, जो 2024-25 में घटकर 1.52 करोड़ हो गई। महज एक साल में 21.83 लाख बच्चों का पंजीकरण घट गया। इसकी तुलना में बिहार में पंजीकरण की कमी 6.15 लाख रही। वहाँ बच्चों की संख्या 2023-24 में 1.79 करोड़ थी, जो 2024-25 में 1.73 करोड़ हो गई। कुल 10 राज्य-उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, असम, तमिलनाडु, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और गुजरात-में एक साल में कम हुए पंजीकरण की संख्या लगभग 45 लाख के करीब है।
इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की रिपोर्ट का जिक्र नहीं है। इन आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में पंजीकरण से बाहर रह गए बच्चों की संख्या गुणात्मक रूप से अलग दिख रही है। हालाँकि, कम होते पंजीकरण को लेकर केंद्र की ओर से राज्यों को निर्देश जारी किए गए हैं और इसे सुधारने पर जोर दिया गया है।
यह रिपोर्ट मूलतः पीएम-पोषण योजना के दस्तावेजों का हिस्सा है। पीएम-पोषण योजना मूलतः मध्याह्न भोजन योजना ही है, जिसका नामकरण 2021 में बदल दिया गया। बहरहाल, यहाँ इस योजना पर बात नहीं करनी है। मूल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर बच्चे पंजीकरण से बाहर क्यों रह गए। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की पढ़ाई के लिए शासन-प्रशासन की सक्रियता उनके निर्देशों, कार्यशालाओं, कई स्तरों पर छानबीन और देखरेख आदि के माध्यम से देखी जा सकती है।
पिछले कुछ सालों में गैर-सरकारी संगठनों की मदद से भी प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की कोशिशें देखी जा सकती हैं। लेकिन, यदि पंजीकरण के स्तर पर देखें, तो पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड यह दिखाते हैं कि इसके परिणाम इन सक्रियताओं के एकदम विपरीत हैं। यहाँ जो ड्रॉप-आउट की संख्या दी गई है, वह अन्य राज्यों की तुलना में गुणात्मक रूप से भिन्न है।
यहाँ उत्तर प्रदेश के एक निर्देश की ओर ध्यान देना चाहिए, जिसमें प्राइमरी स्कूल में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु को 6 वर्ष कर दिया गया है। यह अर्हता किस आधार पर तय की गई, इस संबंध में कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। आमतौर पर पाँच साल की उम्र ही पहली कक्षा के लिए दाखिले के लिए पर्याप्त मानी जाती थी। 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों से बाल वाटिका योजना के तहत शिक्षित करने की योजना शुरू की गई है।
इस योजना के नीति-निर्देश में कहा गया है कि इसे निजी क्षेत्र के स्कूलों में भी लागू किया जाएगा। लेकिन, वहाँ तो पहले से ही इस तरह की पढ़ाई की व्यवस्था चल रही है। निजी स्कूलों ने प्री-स्कूल तैयारी के नाम पर प्री-नर्सरी और नर्सरी जैसी श्रेणियाँ बनाकर अपने यहाँ बच्चों के प्राथमिक कक्षा में भर्ती की जमीन तैयार कर ली है। बाल वाटिका योजना को जमीन पर उतारने के लिए आंगनबाड़ी में काम करने वाले लोग ही जिम्मेदार होंगे या नई नियुक्तियाँ की जाएँगी, यह स्पष्ट नहीं है। पिछले साल आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाओं को शिक्षण पद्धतियों से लैस करने के लिए वर्कशॉप की कुछ खबरें अखबारों में जरूर आई थीं।
उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर से जुड़ी कुछ और खबरों पर नजर डालें। पिछले साल 6 फरवरी को फ्री प्रेस जर्नल की खबर के अनुसार, प्रदेश में 85,252 प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षक कम थे। 4 नवंबर, 2024 को हिंदुस्तान टाइम्स ने स्कूलों में बच्चों के कम पंजीकरण को आधार बनाते हुए खबर छापी थी: ‘कम पंजीकरण: पूरे उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राथमिक स्कूलों के बंद होने की संभावना’। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों की ओर से इसका खंडन छपा था।
इस खबर को जमीनी स्तर से जोड़कर पढ़ने से कुछ और बातें खुलती हैं। सरकारी निर्देशों में ये स्कूल बंद नहीं होते। जिन स्कूलों में पंजीकरण कम होता है, उनका पुनरीक्षण आदि कर उन्हें अन्य स्कूलों के साथ ‘मर्ज’ अर्थात् समाहित कर दिया जाता है। इस तरह कम पंजीकरण वाले बच्चे और शिक्षक एक अन्य चल रहे स्कूल के साथ मिला दिए जाते हैं। इस तरह की समाहरण प्रक्रिया तेजी से चल रही है। कुछ स्कूलों के भवन क्षतिग्रस्त और पुराने होने की वजह से भी उन्हें अन्य स्कूलों के साथ समाहित कर दिया गया। कुछ स्कूलों को मॉडल स्कूलों में भी बदला गया है।
उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के पोर्टल, मंत्रियों के बयान और स्वयं मुख्यमंत्री के भाषणों में प्रदेश में शिक्षा का स्तर बहुत तेजी से बेहतर होता हुआ दिखाया जा रहा है। लेकिन, आँकड़े इसके अनुकूल नहीं लगते। हिंदुस्तान टाइम्स की 4 जनवरी, 2024 की एक रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश में कुल पंजीकृत बच्चों की संख्या के 67 जिलों में 70 प्रतिशत से कम हिस्सा ही स्कूल आ रहा था।
कुछ जिलों में तो यह लगभग 60 प्रतिशत के आसपास था। इस संख्या का अनुमान मध्याह्न भोजन योजना के आँकड़ों के आधार पर लगाया गया था। इस संदर्भ में कई सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों को अध्ययन के लिए लगाया गया। इनके अध्ययन के निष्कर्ष क्या थे, अभी तक पता नहीं चला। लेकिन, ड्रॉपआउट की जो संख्या प्रकाशित हुई है, वह समस्या के विकराल होने को जरूर दिखा रही है।
उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था है। लेकिन, पिछले 15 सालों के आँकड़ों को देखें, तो वहाँ पंजीकृत बच्चों की संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है। भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षण व्यवस्था में दिख रही यह बदतर हालत एक बड़े सामाजिक संकट को दर्शा रही है। सर्वशिक्षा अभियान के तहत जब भोजन और शिक्षा को जोड़ा गया था, तब गरीब वर्ग से आने वाले बच्चों को पोषण मुहैया कराना एक लक्ष्य था और दूसरा, उन्हें प्राथमिक स्तर पर शिक्षित करना था।
जिस तेजी से अखिल भारतीय स्तर पर, और खासकर उत्तर प्रदेश में, प्राथमिक स्कूलों को चलाने, शिक्षकों की उपलब्धता और बच्चों के पंजीकरण की समस्या पैदा हुई है, उसका अंतिम परिणाम शिक्षकों की कमी, स्कूलों को बंद करने/समाहित करने और अंततः पंजीकरण में कमी के रूप में देखा जा रहा है। इसे सिर्फ बच्चों के पंजीकरण में कमी के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के समग्र संकट के रूप में देखा जाना चाहिए।
किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था उसकी आर्थिक, सामाजिक और नैतिक आधारशिला होती है। शिक्षा की कमी सिर्फ इन आधारशिलाओं को ही प्रभावित नहीं करती, कई बार ये आधारशिलाएँ ही इस कमी को जन्म देती हैं। सामान्यतः भारत में प्राथमिक शिक्षा को लेकर जो उदासीनता दिखाई गई, उससे एक चक्रीय संकट पैदा हुआ। गरीबी ने इसे और जटिल बना दिया। मध्याह्न भोजन योजना इस चक्र को तोड़ने का एक प्रयास था। यह योजना भी स्कूलों के माध्यम से ही संचालित हो सकती है।
पिछले एक दशक में स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में कमी, शिक्षा मित्रों की व्यवस्था, स्कूलों की घटती संख्या आदि कुछ और नहीं, बल्कि भारत की शिक्षा व्यवस्था के चरमराकर टूटने को ही दिखा रहे हैं। बच्चों की स्कूलों में घटती संख्या सिर्फ शिक्षा की कमी को नहीं दिखा रही, बल्कि यह एक बार फिर हमारे समाज को पीछे की ओर ले जा रही है।
शिक्षा की अनौपचारिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था का अनौपचारिक हिस्सा ही बनाती है, जो भारत में बढ़ता हुआ दिख रहा है। इससे पैदा होने वाली बेरोजगारी समाज को और भी बदतर स्थिति की ओर ले जाती है और इसके परिणामस्वरूप शिक्षा के संकट को और बढ़ा देती है। इस पर जमीनी हकीकत को सामने लाने वाली रिपोर्ट भी एक बड़ी चुनौती है।
कई राज्यों में प्राथमिक शिक्षा के संकट को सामने लाने वाले पत्रकारों को जेल में डाल देने की घटनाएँ हुई हैं। अब इसकी हकीकत स्वयं सरकारी रिपोर्ट में दर्ज हो रही है। इस पर राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप क्या परिणाम लाएँगे, यह देखना बाकी है। पिछले सत्रों में पंजीकरण की गिरावट का सिलसिला अब एक विकराल रूप लेता हुआ दिख रहा है।
(अंजनी कुमार पत्रकार हैं)