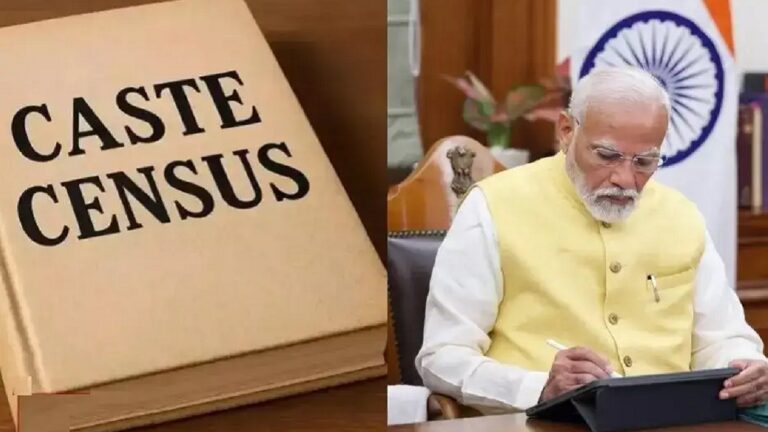25 जून, 1975 को संविधान का सहारा लेकर इस देश के संवैधानिक लोकतंत्र और अवाम के साथ जो किया गया, क्या इन बीते 45 सालों में हमारे समाज और हमारी सियासत ने कोई सबक लिया? क्या आपातकाल यानी इमरजेंसी के उस खतरनाक अनुभव से गुजरने के बावजूद इस देश ने अपने समाज और लोकतंत्र को ज्यादा सुसंगत और सुदृढ़ करने की कोशिश की? हमारे नागरिक और मानवाधिकार आज कितने सुरक्षित और व्यापक हुए हैं? जो होता दिख रहा, वह अप्रिय और निराशाजनक ही नहीं, भयावह है! चौतरफ़ा अंधेरा और आतंक सा है।
इससे बाहर निकलने की रोशनी नहीं दिखती! कोई साफ रास्ता नहीं नज़र आता! अंधेरे और धुंधलके में जो यदा-कदा झलकता है, वह कितना असमर्थ, अप्रभावी और अस्पष्ट है! निम्न-मध्यवर्गीय, किसान-मजदूर, शहरी गरीब और साधारण बेहाल हैं। यथास्थिति के पक्ष में खड़े वर्ण, धर्म और टीवी की बेशुमार ताक़त के बावजूद मध्य वर्ग का एक हिस्सा कभी-कभी कुछ हिलता नज़र आता है। पर परिदृश्य में अब भी एक तरह का सूनापन है।
अन्याय और अनर्थ के इस सबसे तूफानी दौर को लेकर सबसे सक्रिय प्रतिक्रियाएं गैर-दलीय सामाजिक समूहों और छात्र-युवाओं से आ रही हैं। सर्वाधिक उत्पीड़ित भी यही दो समूह हो रहे हैं। कुछ तरक्की-पसंद बौद्धिक और लिबरल्स भी मुखर हैं। दमन की चपेट में वे भी हैं। सोशल मीडिया पर कुछ कोलाहल है। उसमें कुछ सार्थक भी है! छिटपुट प्रयासों और अपवादों को छोड़ दें तो देश और सूबों की सियासत आम तौर पर सहमी सी नजर आती है। ज़्यादातर जगहों पर सन्नाटा, भय या भ्रम है! आजादी के बाद समाज इतना लाचार, इतना बीमार और इतना बेहाल कब था!
हमने इमरजेंसी देखी थी, इसलिए कोई ये कहकर आज के दौर को सहज, स्वाभाविक और सही नहीं ठहरा सकता कि जो कुछ हो रहा है, वह सब संवैधानिक प्रक्रिया और नियम-कानून से ही तो हो रहा है! फिर परेशानी किस बात की? सवाल क्यों? सवाल इसलिए कि इमरजेंसी के दरम्यान लोगों के संवैधानिक अधिकारों को ‘संवैधानिक प्रक्रिया’ के तहत ही निलंबित किया गया था। इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल किया गया था। रातों रात राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी की उद्घोषणा पर हस्ताक्षर भी कराया गया था। कैबिनेट की मंजूरी भी बाद में ले ली गई थी।
आज भी बहुत सारे फैसले किसी मंत्रिमंडलीय बैठक या राष्ट्रपति के अनुमोदन के बगैर ही हो जाते हैं। भाषण में ही पहले उद्घोषणा हो जाती है, बाद में उस पर मंत्रिमंडल की मोहर लगती है। संसद या सर्वदलीय सहमति की बात तो बहुत दूर की रही। कोई नेता जब ‘भगवानों का भी नेता’ हो जाय तो फिर सामूहिक फैसले या संवैधानिक प्रक्रिया की बात का कोई मतलब नहीं रह जाता। इंदिरा गांधी को तब संसद में आज से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत था। उन्होंने एक संवैधानिक प्रावधान का प्रयोग कर संवैधानिक प्रक्रिया और लोकतंत्र को पटरी से उतार दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी और पार्टी में अपनी हैसियत की चिंता थी। 12 जून, 1975 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से वह और उनके निकटस्थ सलाहकार डर गये थे।
श्रीमती गांधी का संसदीय चुनाव ही अवैध घोषित हो गया। बहरहाल, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली। कोर्ट ने फैसला पलटा तो नहीं लेकिन वोटिंग अधिकार के बगैर पद पर बने रहने की छूट दी। तब इंदिरा गांधी के लिए यह भी बड़ी राहत की बात थी। संकट में फंसी इंदिरा गांधी ने इस फैसले का इस्तेमाल करते हुए 25 जून को इमरजेंसी की घोषणा करा दी। दिवंगत पत्रकार कुलदीप नैयर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के ग्रीष्मावकाश की बेंच की तरफ से उक्त फैसला देने वाले जस्टिस वी कृष्ण अय्यर को इस बात का मलाल था कि कहीं उनके फैसले को भारत मे इमरजेंसी लगाए जाने का एक कारण तो नहीं समझा जायेगा। (बियांड द लाइंस, नैयर, 2012 )।
आज क्या हो रहा है? इसे सिर्फ दिल्ली से नहीं देखा जाना चाहिए। गुजरात से दिल्ली, हर महत्वपूर्ण मुकाम और मौके से देखा जाना चाहिए। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में विपक्षी नेताओं और अन्य विरोधियों से निपटने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन कानून (‘मीसा’) नामक कानून काफी कुख्यात हुआ था। एफसीआरए भी तभी आया था, जो सन् 2010 के बाद और भी कठोर कानून बन चुका है। यह कानून एनजीओ और अन्य संस्थाओं के विदेशी फंड पाने के मामलों को देखता है। मोदी-राज में इसे इस कदर कड़ाई के साथ लागू किया गया है कि कुछ धुर दक्षिणपंथी एनजीओ को छोड़कर ज्यादातर की वैध फंडिंग भी बंद हो चुकी है।
इन दिनों यूएपीए और एनएसए जैसे कानूनों के जरिये सत्ता-विरोधियों की गिरफ्तारी का जिस तरह का सिलसिला चल रहा है, वह इमरजेंसी से बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ कम भी नहीं है। एक शादी-शुदा शोध छात्रा जो सीएए-एनआरसी को देश और समाज के लिए अनुचित समझती है, उसे सरकार देश की राजधानी में ‘आतंकवादी’ मानकर यूएपीए जैसे क्रूरतम कानून के तहत उस वक्त गिरफ्तार करती है, जब वह गर्भवती है और देश कोरोना के बढ़ते संक्रमण से सहमा हुआ है। काफी कशमकश के बाद हाल में उस युवा शोध छात्रा सफूरा जरगर को ढेर सारी शर्तों के साथ जमानत मिली है। हां, इमरजेंसी और आज के दौर का एक फर्क जरूर नजर आता है।
इमरजेंसी में तत्कालीन सरकार ने सबसे अधिक विपक्षी नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं या ऐसे युवाओं को गिरफ्तार किया था, जिनमें वह प्रतिरोध की तनिक भी संभावना देख रही थी। अल्पसंख्यक समुदाय भी तरह-तरह से निशाने पर था। आज उससे भी ज्यादा हैं। आज के दौर में विपक्षी नेताओं से ज्यादा सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र-युवा, लेखक-बौद्धिक और पत्रकार सरकार के निशाने पर हैं। ज्यादातर स्थापित विपक्षी नेताओं को मौजूदा सत्ताधारियों ने ‘अनुकूलित’ सा कर लिया है। कुछ डर (सीबीआई-इडी आदि के) के चलते तो कुछ अन्य कारणों से ‘पट’ गए हैं। जो नहीं डरे या नहीं पटे, उनसे सत्ताधारियों को फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं महसूस होता। इसलिए ऐसे विपक्षी भी सत्ता के निशाने पर ज्यादा नहीं हैं।
असल निशाने पर हैं-गैर-वीवीआईपी साधारण लोग! पैटर्न देखिये, कभी कोई मौजूदा या पूर्व संपादक, कभी कोई लेखक-कवि, कोई मानवाधिकार कार्यकर्ता, एडवोकेट या कोई सामाजिक कार्यकर्ता या छात्र-युवा ही मुख्य निशाने पर हैं। आनंद तेलतुंब़ड़े, गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरवर राव, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, मोहम्मद सैफी या सफूरा जरगर, क्या इनमें किसी एक की जिंदगी या पृष्ठभूमि में कुछ भी ऐसा है, जिसे आपराधिक बताने की कोशिश की जाय? देवांगना और नताशा को दिल्ली के दंगों के अभियुक्त के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। इसी क्रम में प्रो. योगेंद्र यादव और हर्षमंदर के नाम भी दिल्ली-पुलिस के आरोपपत्र में शामिल किए गए हैं।
कुछ औरों के भी जोड़े जाते रहेंगे। पर जिन लोगों के विजुअल्स उपलब्ध हैं और पूरी दुनिया में देखे जा चुके हैं, उनके नाम न तो किसी एफआईआर में और न ही किसी आरोपपत्र में हैं। सिर्फ इसलिए कि वे सत्ताधारी दल के नेता हैं या ‘मनुवादी-हिन्दुत्वा बिग्रेड’ के कार्यकर्ता या समर्थक हैं। फेसबुक के सीइओ जकरबर्ग तक अमेरिका में बैठे-बैठे सत्ताधारी दल के ऐसे कुछ नेताओं के आपत्तिजनक बयानों की तरफ संकेत करते हैं। पर दिल्ली पुलिस और सत्ताधारी दल ‘मनुवादी हिन्दुत्वा ब्रिगेड’ के ऐसे किसी सदस्य के हर गुनाह को नजरंदाज कर उन्हें उत्साहित करते नजर आते हैं।
ऐसा इसलिए भी कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से अलग आज का यह निरंकुश दौर किसी एक नेता की कुर्सी बचाने से अभिप्रेरित नहीं है। इसका ज्यादा बड़ा मकसद और ठोस एजेंडा है। दमन, साजिश और जुल्म के सारे हथकंडों के पीछे मौजूदा सत्ताधारियों का सबसे बड़ा एजेंडा है-मौजूदा भारत को एक औपचारिक सेक्युलर-लोकतंत्र से मनुवादी-हिन्दुत्व आधारित भारतीय-राष्ट्रराज्य में तब्दील करना। इस खतरनाक राजनीतिक परियोजना का समाज में पुरजोर प्रतिरोध फिलहाल नहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि हमारे समाज ने इमरजेंसी से कोई सबक नहीं लिया। दूसरा कारण है कि हमारे समाज में लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म की जड़ें भी गहरी नहीं हैं। इन दोनों मूल्यों के लिए भारतीय समाज में सुसंगत और व्यवस्थित ढंग से लंबी लड़ाई भी नहीं हुई है।
दुर्भाग्यवश, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आर्थिक असमानता और सामाजिक भेदभाव से जूझने का एजेंडा उतनी प्रमुखता से नहीं शामिल था। केरल और तमिलनाडु जैसे जिन कुछ प्रदेशों में वह शामिल था, वे आज बेहतर स्थिति में हैं। पर सबसे अधिक आबादी और संसद की सर्वाधिक सीटों वाले हिन्दी भाषी प्रदेशों में समानता और समावेशी समाज के मूल्यों को प्रमुखता नहीं मिली थी। इसलिए यह संयोग नहीं कि आजादी के बाद यूपी-बिहार, मध्यप्रदेश आदि जैसे प्रदेशों में बुनियादी भूमि सुधार, शिक्षा सुधार और स्वास्थ्य सेवा संरचना जैसे मुद्दे शासन का अहम एजेंडा नहीं बने। आज भी नहीं हैं। इससे देश के बड़े क्षेत्र में लोकतंत्र के मूल्यों को बल नहीं मिला। सत्ता-राजनीति मंदिर-मस्जिद, जात-पांत और धर्म-संप्रदाय के इर्द-गिर्द चलती रही।
बहुत सारे समाजशास्त्री और विद्वान आज की परिस्थिति और परिघटना से चकित हैं कि भारत जैसे ‘जीवंत लोकतंत्र’ को क्या हो गया है? निरंकुशता को इतना बल कहां से मिल रहा है? लोकतांत्रिक प्रतिरोध की आवाजें कहां चली गईं? पर इस परिघटना पर मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं! दरअसल, डेमोक्रेसी की ठोस जमीन तैयार हुए बगैर आजादी के बाद हमने सेक्युलर-डेमोक्रेसी ओढ़ ली थी! अब देखना बस इतना है कि ओढ़ी ही यह चादर आज के इन निरंकुश तूफानी-थपेड़ों में कुछ बचती है या चिंदी-चिंदी हो जाती है! यकीकन, आज के दौर में उस पुरानी इमरजेंसी की पुनरावृत्ति नहीं होगी! उससे कुछ अलग होगा, हो रहा है और आगे और भी होगा!
कितने सारे कानून हैं, जो सत्ता से असहमत किसी खास व्यक्ति या किसी आम नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकारों का गला घोंटने और जेल भेजने के लिए काफी हैं। हम देख ही रहे हैं कि यूएपीए और एनएसए समेत न जाने कितने सारे निरंकुश प्रावधानों के जरिए डेमोक्रेसी को पटरी से उतारा गया है। और तो और कोविड-19 से निपटने के लिए ‘एपिडेमिक डिजीज एक्ट1897’ जैसे औपनिवेशिक कानूनों और सन् 2005 के आपदा प्रबंधन कानून के कुछ असंगत प्रावधानों का भी धड़ल्ले से दुरुपयोग किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से लेकर उन पर लाखों रुपये का क्षति-पूर्ति फाइन लगाने जैसे मौजूदा सरकारों के फैसले औपनिवेशिक हुकूमत के निरंकुश कदमों की याद दिलाते हैं।
हम सन् 47 में ‘आजाद’ हुए और सन् 50 में लोकतांत्रिक गणराज्य बन गये। संवैधानिक लोकतंत्र स्थापित! फिर देखिए, इतने बरस बाद आज हम और हमारी डेमोक्रेसी कहां है? तब से अब तक का कैसा रहा है ये सफ़र? क्या ये नहीं लगता हमारे यहां डेमोक्रेसी संविधान के पन्नों, कुछ संरचनाओं और कुछ लोगों तक सीमित रह गई। आम आदमी के पास रह गया है, बस उसके ‘वोट का अधिकार!’ उस पर भी कुछ समय से तरह-तरह की बातें होती रहती हैं जैसे नागरिकता पर होती रहती हैं।
यूरोप और अन्य इलाकों के कई खुशहाल लोकतांत्रिक मुल्कों की तरह हमारी डेमोक्रेसी देश के आम लोगों तक और हमारी जमीन तक क्यों नहीं पहुंची? ऐसा क्यों हुआ? ऐसे तमाम जटिल सवालों का जवाब डॉ बीआर अम्बेडकर के वांग्मय में मिलता है। अगर भारतीय संविधान सभा में दिये उनके 25 नवम्बर, 1949 के भाषण को ध्यान से पढ़ा जाय तो भारत में डेमोक्रेसी के इस क्षरण और हरण की असल कहानी समझी जा सकती है! असल वजह है-हमारे वर्ण-आधारित समाज का सामाजिक और आर्थिक रूप से भयानक तौर पर असमानता-मूलक होना। ऐसे में डेमोक्रेसी कागज पर तो उतर सकती है पर जमीन पर नहीं।
(उर्मिलेश वरिष्ठ पत्रकार हैं और राज्यसभा टीवी के संस्थापक एग्जीक्यूटिव एडिटर रह चुके हैं।)