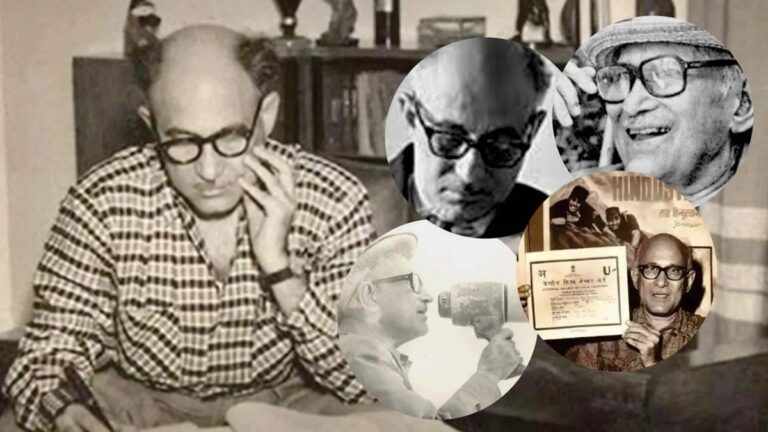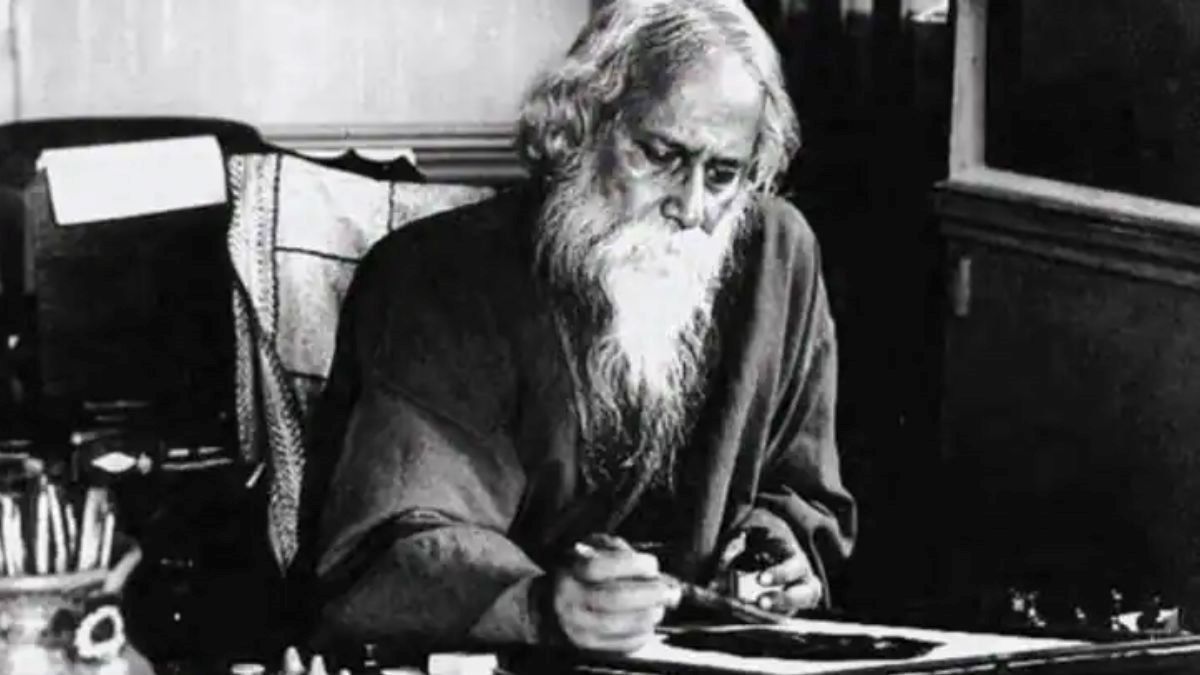सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ़स्पा) एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा की वजह, एक दर्दनाक वाक़या है। नगालैंड में 4 और 5 दिसंबर की दरमियानी रात को सेना की 21 पैरा स्पेशल फोर्स ने आतंकवादी होने के शक में ओटिंग गांव और मोन हेडक्वार्टर में चौदह निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी थी। इस घटना को पैरा स्पेशल फ़ोर्सेज ने ग़लत पहचान का मामला बताया है। बहरहाल इस घटना के बाद से ही राज्य में तनाव की स्थिति निर्मित है।
नगालैंड पुलिस ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए, भारतीय सेना के 21 पैरा विशेष बल के ख़िलाफ़ तिज़ित पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की है। यही नहीं नगालैंड सरकार ने इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। सेना ने भी इस घटना पर अफ़सोस जताते हुए कहा है कि इसकी उच्चतम स्तर पर जांच की जाएगी। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद नगालैंड और मेघालय दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से ‘आर्म्ड फ़ोर्सेज़ स्पेशल पावर एक्ट’ हटाने की मांग की है। इत्तेफ़ाक से दोनों ही जगह बीजेपी गठबंधन की सरकार है।
उत्तर-पूर्व हो या फिर जम्मू-कश्मीर हिंसा और उग्रवाद से प्रभावित इन इलाकों में ‘सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून’, ‘अशांत क्षेत्र कानून’ और ‘जन सुरक्षा’ जैसे कई कानून जो कि शांति बहाल करने के नेक मक़सद से अमल में लाए गए थे, आज इन कानूनों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। इन कानूनों की आड़ में सुरक्षा बल, बेकसूर नागरिकों का उत्पीड़न कर रहे हैं। दोनों ही इलाकों में एएफएसपीए का अभी तलक का तजु़र्बा यह दिखलाता है कि सुरक्षा बलों द्वारा इन कानूनों की धाराओं का ग़लत इस्तेमाल किया जाता रहा है। मानवाधिकार हनन की ढेरों घटनाओं के बावजूद, जिम्मेवार अफ़सरों या सुरक्षाकर्मियों के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने की इजाज़त दिए जाने की मिसाल इन सूबों में बमुश्किल मिलती है।
11 सितंबर, 1958 को अमल में आए ‘सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून’ की लगातार आलोचनाओं के बाद भी सत्ताधारियों द्वारा हमेशा यह कहकर इस कानून का औचित्य ठहराया जाता रहा है कि आतंकवाद पर काबू पाने के लिए यह ज़रूरी है। यदि इसे वापस ले लिया गया, तो आतंकवाद से प्रभावित इलाकों में तैनात किए गए सुरक्षा बलों के मनोबल पर ग़लत असर पड़ेगा। वहीं सेना इन कानूनों की यह कहकर हिमायत करती है कि इन राज्यों में आतंकवाद से लड़ने के लिए उसके पास कुछ विशेष अधिकार होने ज़रूरी हैं। क्योंकि, स्थानीय जनता अक्सर आतंकियों के बहकावे में आ जाती है और पुलिस व स्थानीय अधिकारी भी उनका पूरा सहयोग नहीं करते। सत्ता और सेना की तमाम दलीलें और बचाव अपनी जगह, पर अब सवाल यह उठता है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे कानूनी प्रावधान क्यों रहने चाहिए, जो सुरक्षाकर्मियों को यह आश्वासन दें कि वे बेग़ुनाह लोगों की हत्या करें, मानवाधिकारों का उल्लंघन करें या उनका उत्पीड़न, लेकिन फिर भी वे सज़ा पाने से बचे रहेंगे।
बीते तीन दशक में उत्तर—पूर्वी राज्यों और जम्मू-कश्मीर में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जिसमें बेग़ुनाह नौजवान और बच्चे बिना किसी कसूर के मारे गए। सुरक्षा के नाम पर फ़र्जी मुठभेड़ और मासूमों का भयानक उत्पीड़न हुआ। साल 2013 में ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों की जांच के लिए जस्टिस संतोष हेगड़े की अगुवाई में तीन जजों की एक समिति का गठन किया था। ‘हेगड़े आयोग’ ने कुल 1528 मामलों में से 62 की जांच की। जांच के बाद आयोग का निष्कर्ष था कि 62 में से 15 मामले फ़र्जी मुठभेड़ के हैं। कहने को हमारी हुक़ूमतें जब-तब मानव अधिकारों के उल्लंघन को बर्दाश्त न करने की बातें करती हैं, लेकिन हकीकत में उनका यह तर्ज़-ए-अमल नहीं होता। आम नागरिकों पर ज़्यादती करने वाले हथियारबंद फ़ोर्सेज पर शायद ही कभी कोई कार्यवाही हो पाती है। ‘सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून’ के तहत सुरक्षा बलों को बिना वारंट के किसी भी घर की तलाशी लेने और गिरफ्तार करने से लेकर गोली चलाने तक के अधिकार हैं। यही नहीं, दोषी सुरक्षाकर्मियों के ख़िलाफ़ तब तक न्यायिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती, जब तक केन्द्र इसकी इजाज़त न दे दे।
देश में ‘सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम’ को लागू हुए आज छह दशक से भी ज्यादा हो गए हैं। साल 1958 में जब यह कानून बना, तो इसके पीछे मक़सद नगालैंड के हथियारबंद अलगाववादी आंदोलन से निपटना था। लेकिन एक फ़ौरी मक़सद से बनाए गए इस कानून को बाद में वापिस लेने की बजाय ज़ारी रखा गया। जबकि नगालैंड में फ़िलहाल संघर्ष विराम की स्थिति है और वहां शांति बनी हुई है। नगालैंड ही नहीं, बाद में इसे उत्तर-पूर्व के कई सूबों मसलन असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और ख़ास तौर पर साल 1990 में जम्मू-कश्मीर में सख़्ती से लागू कर दिया गया। यह विवादास्पद कानून अभी भी जम्मू-कश्मीर के अलावा नगालैंड, असम, मणिपुर (इंफ़ाल के सात विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर) और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है। इस विवादास्पद और काले कानून को समाप्त करने की मांग इन सूबों में बरसों से उठती रही है। कानून के ख़िलाफ़ लोग सड़कों पर उतरे, धरना-प्रदर्शन, आंदोलन किए लेकिन सरकार हमेशा इससे बेपरवाह बनी रही।
असम राइफल्स के कुछ जवानों पर मणिपुर की एक नौजवान लड़की के साथ बलात्कार और उसकी हत्या का इल्जाम लगा, तो इस कानून के ख़िलाफ़ उस वक्त पूरे राज्य के लोग सड़कों पर उतर आए। यहां तक कि सेना मुख्यालय के बाहर मणिपुर की महिलाओं ने निर्वस्त्र प्रदर्शन भी किया। उसी जन आंदोलन के चलते तत्कालीन केन्द्र सरकार ने अधिनियम की समीक्षा के लिए एक कमेटी गठित की। कमेटी ने जून, 2005 में सौंपी अपनी रिपोर्ट में ‘सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून’ को ख़त्म करने की सिफ़ारिश की मगर हुआ कुछ नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने ‘अफ्स्पा’ के ख़िलाफ़ डेढ़ दशक से ज्यादा समय तक भूख हड़ताल की। उनकी मांग थी कि ‘सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून’ को मणिपुर से हटाया जाए। इरोम शर्मिला के इस सत्याग्रह ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, लेकिन देश की सरकार की निग़ाह यहां नहीं हुई। उत्तर-पूर्वी राज्यों के लोगों की आकांक्षाओं के जानिब केन्द्र की उपेक्षा का जो नज़रिया पहले था, वह आज भी बिल्कुल नहीं बदला है।
तमाम जांच आयोग, ‘सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून’ को ख़त्म करने के पक्ष में अपनी राय दे चुके हैं। बावजूद इसके केन्द्र सरकार आज भी इस क़ानून को ख़त्म करने के लिए मन नहीं बना पाई है। जब भी इस कानून की समीक्षा या इसे ख़त्म करने की बात उठती है, तो सेना सबसे पहले इसका विरोध करने लगती है। सेना जिस तरह से ‘सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम’ को मुक़द्दस मानते हुए, कानून में किसी भी संशोधन के ख़िलाफ़ है, उसे लोकतंत्र में किसी भी लिहाज से सही नहीं ठहराया जा सकता। बीजेपी के अलावा देश की दीगर सियासी पार्टियां इस कानून में संशोधन या इसे कुछ इलाकों से हटाने की मांग लंबे अरसे से करती रहीं हैं। केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह इस मांग को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखे। परिप्रेक्ष्य यह है कि इस कानून को हटाने या इसमें संशोधन की मांग सिर्फ़ नगालैंड, मेघालय, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर से ही नहीं उठ रही है, बल्कि पूर्वोत्तर के बाकी सूबों में यह मुद्दा बहुत पहले से है। पड़ोसी देश म्यांमार और चीन से चल रहे सीमा विवाद के बीच हो सकता है, इस कानून को एक दम रद्द करना मुश्किल हो, लेकिन फिर भी उन धाराओं में संशोधन क्यों नहीं किया जा सकता, जिनसे सैन्यकर्मियों द्वारा ड्यूटी से इतर किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघनों को संरक्षण दिया जाता है।
उत्तर-पूर्व हो या फिर जम्मू-कश्मीर दोनों ही जगह सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफ़स्पा) का अभी तलक का तजुर्बा हमें यह दिखलाता है कि इस कानून का इस्तेमाल फ़ौज मनचाहे तरीके से करती रही है। कानून में कुछ ऐसी धाराएं हैं, जिनका इस्तेमाल अवाम के हकों को रौंदने में होता है। सर्वोच्च अदालत ने इस कानून पर सवाल उठाते हुए, कई बार सरकार से इस मनमाने और बेलगाम कानून की समीक्षा करने का आदेश दिया है। लेकिन सरकार इन आदेशों पर कोई अमल नहीं करती। हर बार पूर्व के न्यायिक आदेशों की तरह इन्हें बिसरा दिया जाता है। देश की सुरक्षा के लिए सेना हर ज़रूरी कार्यवाही करे, इस बात से भला कौन एतराज़ करेगा। लेकिन कार्यवाही करते वक्त वह स्थानीय नागरिकों के प्रति भी संवेदनशील हो। उनका बिला वजह उत्पीड़न न किया जाए।
शीर्ष अदालत ने साल 2017 में अपने एक अहम फै़सले में कहा था,‘‘अशांत इलाकों में अफ़स्पा के लागू होने के बावजूद सशस्त्र बल और पुलिस ज़्यादा ताक़त का इस्तेमाल नहीं कर सकती है और न ही आपराधिक कार्रवाई से बच सकती है। सुरक्षा बलों के लिए भी क्या करें और क्या न करें ? के नियम हैं। इन्हें तोड़ने को किसी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता।’’ अदालत का यह कहना सही भी है। सरकार हो या फिर सेना, लोकतंत्र में जवाबदेही सभी की बनती है। कोई भी अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकता। कानून की नज़र में आखि़र सब समान हैं।
(जाहिद खान वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और समीक्षक हैं। आप आजकल मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रहते हैं।)