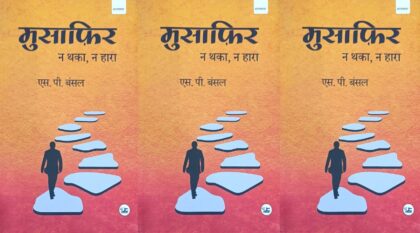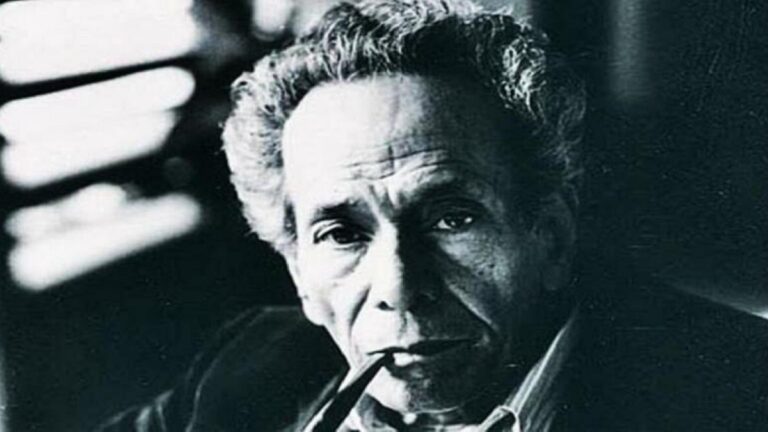सिनेमा की शुरुआत के दौर से ही इस बात को पहचान लिया गया था कि सिनेमा प्रचार का बहुत सशक्त माध्यम हो सकता है। सिनेमा एक दृश्य माध्यम है और इसकी बुनियादी विशेषता यह होती है कि उसमें जीवन को बिल्कुल वैसा ही दिखाया जा सकता है जैसा हम जीवन को जीते हुए अनुभव करते हैं। न केवल अपने जीवन को वरन दूसरों के जीवन को भी। इसका अर्थ यह है कि सिनेमा यथार्थ को अभिव्यक्त ही नहीं करता वरन वह इस माध्यम के द्वारा दर्शकों के मानस में अयथार्थ को यथार्थ समझने का भ्रम भी उत्पन्न कर सकता है। जिन अतिरंजनापूर्ण और अयथार्थ घटनाओं को साहित्यिक और पौराणिक पुस्तकों में पढ़ते हैं उन्हें सिनेमा ठीक उसी रूप में पर्दे पर घटित होता हुआ दिखा सकता है। और दर्शकों में यह भ्रम पैदा कर सकता है कि वह जो देख रहा है वह सचमुच घटित हो रहा है।
अगर हम सिनेमा तकनीक से परिचित हैं तो हम आसानी से पहचान लेते हैं कि जो पर्दे पर देख रहे हैं, वह वास्तविक जीवन में मुमकिन नहीं है। जैसे-जैसे फ़िल्म तकनीक का विकास हुआ है वैसे-वैसे सिनेमा के पर्दे पर बहुत कुछ दिखाया जाना संभव हुआ है जो मनुष्य की कल्पना की उपज है, यथार्थ नहीं है, या जो उस अतीत का हिस्सा रहा है जो बीत चुका है और जिसे वापस नहीं लाया जा सकता। यह सिनेमाई प्रौद्योगिकी का कमाल ही है कि करोड़ों साल पहले के डायनासोर को जिसकी नस्ल ही खत्म हो चुकी है, उन्हें सिनेमा के पर्दे पर जीवित रूप में चलते-फिरते और चिंघाड़ते हुए दिखाया जा सकता है, दिखाया गया है। लेकिन ऐसी अतिरंजनापूर्ण और अयथार्थ घटनाओं को देखते हुए मुमकिन है कि दर्शक उनसे आह्लादित तो हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वह उन्हें वास्तविक ही माने।
सिनेमा यथार्थ को यथार्थ की तरह ही नहीं अयथार्थ को यथार्थ की तरह दृश्यांकित करके दर्शक के मन में अयथार्थ को यथार्थ मानने का यकीन पैदा कर सकता है। वह एक ऐसी कहानी गढ़कर हमारे सामने पेश कर सकता है जिसे हम सच मान बैठें। वह किसी ऐतिहासिक पुरुष की ऐसी छवि निर्मित कर सकता है जो जरूरी नहीं कि उसकी वास्तविक छवि से मेल खाती हो, लेकिन फ़िल्म देखकर हम उसे ठीक वैसा ही मानने लग सकते हैं जैसा उसे दिखाया गया है। इसी तरह वह हमारे अपने आसपास के यथार्थ को जिसके हम स्वयं हिस्सा हैं, सिनेमा इस रूप में दिखा सकता है कि जो पर्दे पर दिखाया जा रहा है उसे ही सच मान लें और स्वयं अपने अनुभवों को अनजाने में असत्य समझने लगें।
सिनेमा का प्रोपेगेंडा के रूप में उपयोग उसकी इसी शक्ति के कारण ही संभव है। यह इसलिए भी संभव होता है कि हमें अपने समय और समाज के प्रति जितना जागरूक होना चाहिए उतने नहीं होते। इसलिए जब सिनेमा के पर्दे पर ऐसी छवियां बारबार हमारे सामने रखी जाती हैं जो पूरी तरह से झूठ पर टिकी होती हैं तो भी हम उसे सच मान लेते हैं। प्रथम विश्वयुद्ध में हार के बाद जब हिटलर की नेशनल सोशलिस्ट पार्टी (नाजी पार्टी) ने जर्मन की जनता के मनोमस्तिष्क में यह बैठा दिया गया कि उसकी पराजय और दुर्दशा का कारण यहूदी हैं और इस झूठ को फैलाने के लिए व्यापक प्रचार किया गया तो धीरे-धीरे जर्मन जनता ने भी मान लिया कि यही सत्य है।
यहूदी समुदाय जर्मन समाज का एक बहुत ही नगण्य सा अल्पसंख्यक समुदाय था, कुल आबादी का एक प्रतिशत से भी कम। लेकिन यहूदी समुदाय के विरुद्ध धुआंधार प्रचार ने जर्मन जनता के मन में यह बैठा दिया कि यहूदी ही हमारी सारी समस्याओं का कारण है और अगर इस बुराई को जर्मन राष्ट्र् से समूल नष्ट कर दिया जाता है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस असत्य के साथ-साथ यह भी प्रचारित किया गया कि जर्मनी को उसका खोया हुआ स्वाभिमान केवल नाजी पार्टी और उसका सर्वोच्च नेता हिटलर ही वापस दिला सकते हैं।
1933 में जब हिटलर जर्मनी का शासक बना तब उसने ऐसे कई फ़िल्में बनवायीं जिनमें यहूदियों की बर्बर और हिंसक छवि पेश की गयी थीं। उसने ऐसे वृत्तचित्र बनवाये जिसमें स्वयं उसकी छवि ‘अतिमानवीय’ नज़र आती थी। जर्मन फ़िल्मकार लेनी रिफ़ेंस्ताल ने कई वृत्तचित्र बनाये जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध वृत्तचित्र था, ‘ट्राइंफ ऑफ दि विल’ (1935) जिसमें नेशनल सोशलिस्ट पार्टी (नाज़ी पार्टी) की छठी कांग्रेस जो न्यूरेम्बर्ग में 1934 में आयोजित हुई थी, उस पर आधारित यह वृत्तचित्र था। लगभग पौने दो घंटे के इस वृत्तचित्र की शुरुआत बादलों के बीच से धरती की ओर आते हुए विमान से होती है जिसमें से हिटलर उतरता दिखाया गया है। लाखों-लाख लोग उसकी प्रतीक्षा करते नज़र आते हैं जिनके चेहरे पर उल्लास का सामूहिक भाव नज़र आता है।
विमान से उतरकर हिटलर का जनता के बीच आना ठीक वैसा ही है जैसे आकाशीय देवता का धरती पर अवतरण होना। इस पूरे वृत्तचित्र में हिटलर की जयजयकार करता हुआ विराट जनसमूह और बारबार हजारों की संख्या में अनुशासनबद्ध होकर परेड करते और हिटलर को सलामी देते सैनिक और अर्धसैनिक बल एक ऐसे शासक की छवि निर्मित करते हैं जिसके पीछे पूरा देश है और जिसका चुनौतीहीन एकमात्र शासक हिटलर है। वृत्तचित्र के आरंभ से लेकर अंत तक हिटलर और जर्मनी को बार-बार एक दूसरे का पर्याय कहा गया है। पार्टी की अग्रिम पंक्ति के नेता बार-बार आकर हिटलर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ‘फ्यूरर आप ही जर्मनी हैं, जब आप कुछ करते हैं तो पूरा देश क्रियाशील हो जाता है’। एक अन्य नेता कहता है, ‘आप विजय की गारंटी है और आप ही शांति की गारंटी है। चूंकि हिटलर ही जर्मनी है इसलिए हिटलर के प्रति निष्ठा ही जर्मनी के प्रति निष्ठा है और हिटलर के लिए संघर्ष ही जर्मनी के लिए संघर्ष है।
वृत्तचित्र की शुरुआत ही इस बात से होती है कि 1933 में यानी जब हिटलर सत्तासीन हुआ तो जर्मनी का मानो पुनर्जन्म हुआ। हिटलर से पहले के चौदह साल यानी प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मनी की हार से लेकर हिटलर के सत्ता में आने के बीच का काल एक राष्ट्र के रूप में जर्मनी की अवमानना और निरादर का काल रहा है। उसे कदम-कदम पर अपमानित किया गया और उस पर ऐसी शर्तें थोपी गयीं जिसने उसके आत्मसम्मान को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। राष्ट्र के रूप में अपने खोये आत्मसम्मान को हिटलर ने दोबारा हासिल करने को अपनी पार्टी का सबसे बड़ा लक्ष्य बनाया। उसने जर्मन नागरिकों में अपमान के इन थोड़े से सालों को भूलकर दो हजार साल के गौरवपूर्ण इतिहास को याद रखने का आह्वान किया। उसने जर्मन नागरिकों के मन में इस मिथ्या धारणा को बैठा दिया कि वे उस आर्य नस्ल के हैं जो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं और जिसे पूरी दुनिया पर शासन करने का अधिकार है।
यहूदियों जैसी ‘निकृष्ट नस्लों’ को समाप्त करना, उन्हें नागरिक अधिकारों से वंचित करना आर्य नस्ल की सुरक्षा और जर्मन राष्ट्र की रक्षा के लिए आवश्यक है। इन बातों का प्रचार करने के लिए सिनेमा की ताकत को हिटलर बहुत अच्छी तरह से जानता था और उसने इस माध्यम का भरपूर उपयोग किया। हिटलर और उसका प्रचार मंत्री जोसेफ गोयबेल्स इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि लगातार किया जाने वाला प्रचार भले ही वह असत्य और अर्धसत्य पर ही क्यों न टिका हो, लोगों को गहरे रूप में प्रभावित कर सकता है। इस मिथ्या प्रचार का ही नतीजा था कि हिटलर के सत्ता में आने के बाद से ही यहूदियों पर तरह-तरह के प्रतिबंध लगाये गये, उनका सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार किया गया। जर्मन जनता ने यहूदियों के खिलाफ हिटलर द्वारा उठाये गये हर कदम का समर्थन इसलिए किया कि पहले से ही उनके दिमागों में भर दिया गया था कि प्रत्येक यहूदी जर्मन राष्ट्र के लिए खतरा है और उसका गुनहगार है और इसलिए उनको किसी भी तरह की सजा दिया जाना न अवैधानिक है और न अनैतिक।
हिटलर और उसके पूरे तंत्र ने शिक्षा में, इतिहास में और ज्ञान-विज्ञान के दूसरे क्षेत्रों में ऐसे बदलाव किये जो उनके राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने में मददगार हों। नाजीवादी शासनतंत्र ने डार्विन के विकासवाद की एक ऐसी विकृत व्याख्या प्रस्तुत की, जिससे वे यह साबित कर सके कि प्राकृतिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल आर्यों की हैं और उन्हें मानवजाति पर और इस पृथ्वी पर शासन करने का अधिकार है। इन अमानुषिक और विकृत धारणाओं में यकीन का ही नतीजा था कि यहूदियों को जर्मन नागरिकों से अलग रखने के लिए उन्हें नज़रबंदी शिविरों में भेज दिया गया। ये ही शिविर यातनागृहों में बदल दिये गये जहां यहूदियों का सामूहिक कत्लेआम किया गया। एक बहुत ही छोटा-सा अल्पसंख्यक सवा पांच लाख आबादी का यहूदी समुदाय जो जर्मनी की कुल आबादी के एक प्रतिशत से भी कम था, को जर्मनी की पराजय और पतन का जिम्मेदार ठहरा दिया गया।
लेकिन दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान यूरोप के जिन देशों पर हिटलर की सेना ने कब्जा किया वहां यहूदियों का कत्लेआम भी किया गया। जर्मनी का पड़ोसी देश पोलेंड जिस पर हिटलर की सेना ने युद्ध के शुरुआती काल में ही कब्जा कर लिया था और जहां तीस लाख यहूदी रहते थे, भयावह नरसंहार के द्वारा उनको खत्म कर दिया गया और युद्धोपरांत यानी 1945 में पोलेंड में केवल 45 हजार यहूदी बच पाये थे। इस तरह पूरे यूरोप में यहूदियों के व्यापक नरसंहार में यूरोप की कुल यहूदी आबादी जो 95 लाख थी, उसमें से 60 लाख यहूदी मार दिये गये। यह नरसंहार ही भयावह नहीं था बल्कि उससे भी ज्यादा भयावह यह सच्चाई थी कि हिटलर के सत्ता में आने के बाद किये गये प्रचार ने जर्मनी की बहुसंख्यक जनता को हिटलर का समर्थक बना दिया। उसके प्रचार अभियान का ही नतीजा था कि जनता हिटलर के युद्धोन्मादी और बर्बर क्रूरताओं के भागीदार भी बन गये थे।
लाखों-लाख यहूदियों को दी जाने वाली यातनाएं इसीलिए संभव हो सकीं क्योंकि उनको क्रियान्वित करने के लिए इंजीनियर, डॉक्टर और दूसरे पेशों से जुड़े शिक्षित और कुशल लोग अपनी सेवायें दे रहे थे। फासीवादी प्रचारतंत्र ने पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना को हिंसक और संवेदनहीन बना दिया था। यातना शिविरों से बहुत पहले से यहूदियों के विरुद्ध हिंसक कार्रवाइयां आरंभ हो चुकी थीं। यहूदियों का आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार किया जाने लगा। उनके घरों और प्रतिष्ठानों पर हमले किये जाने लगे। उनकी भीड़ द्वारा लिचिंग की जाने लगी और जब उन पर हमले हो रहे थे तो जर्मन नागरिक या तो निष्क्रिय बने रहे या उस हिंसक भीड़ का हिस्सा बन गये।
फासीवादी प्रचारतंत्र के इस उदाहरण से यह समझना भूल होगी कि केवल फासीवादी राजसत्ता ही अपने पक्ष में प्रचार के लिए सिनेमा का उपयोग करती है। लेकिन सिनेमा अन्य किसी माध्यम की तुलना में ज्यादा तीव्र और व्यापक असर वाला माध्यम है इसलिए अन्य माध्यमों की तुलना में प्रचार के लिए सिनेमा की उपयोगिता बहुत अधिक बढ़ जाती है। यह अंतर जरूर है कि जहां दक्षिणपंथी राजसत्ताएं सिनेमा के माध्यम से जनता के विभिन्न वर्गों और समुदायों के बीच नफरत और घृणा फैलाने का काम करती हैं, वहीं लोकतांत्रिक और जनपक्षीय सत्ताएं विभिन्न वर्गों और समुदायों के बीच एकता और भाईचारा पैदा करने की कोशिश करती हैं।
एक और अंतर यह होता है कि जनपक्षीय सत्ताएं केवल कथ्य पर ही नहीं उनकी रचनात्मक और कलात्मक प्रस्तुति पर भी ध्यान देती हैं। यह कहना बहुत गलत नहीं है कि हर कला माध्यम जिनमें सिनेमा भी शामिल है, एक तरह का प्रचार ही होती है, लेकिन यह प्रश्न जरूर पैदा होता है कि प्रचार का मकसद क्या है और उसका प्रभाव दर्शकों पर किस तरह का पड़ता है। 1915 में अमरीकी फ़िल्मकार डी डब्ल्यू ग्रिफिथ की मूक श्वेत-श्याम फ़िल्म ‘बर्थ ऑफ ए नेशन’ भी एक प्रचार फ़िल्म थी। इस फ़िल्म में ग्रिफिथ ने अमरीकी गृहयुद्ध को कहानी का विषय बनाया था, लेकिन इस गृहयुद्ध में उसकी सहानुभूति श्वेत समर्थक नस्लवादी समूह ‘कु क्लक्स क्लान’ के प्रति थी जो मानता था कि श्वेत औरतों को अश्वेतों के हमले से बचाने के लिए और अमरीका में श्वेतों के वर्चस्व को बनाये रखने के लिए अफ्रीकी मूल के लोगों को नियंत्रण में रखना जरूरी है और जरूरत हो तो इसके लिए हिंसा का सहारा लेने में भी कुछ गलत नहीं है। इस तरह यह फ़िल्म अश्वेत लोगों के प्रति घृणा और नफ़रत की प्रचारक बन गयी। स्वाभाविक था कि अश्वेत समुदाय इसका विरोध करता और इस पर प्रतिबंध की मांग करता लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गयी। आज भी यह फ़िल्म हॉलीवुड की सबसे खतरनाक नस्लवादी फ़िल्म मानी जाती है, भले ही तकनीकी दृष्टि से यह एक बेहतरीन फ़िल्म कही जा सकती है।
1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद के शुरुआती दशकों में बनी सोवियत फ़िल्मों को भी प्रचार फ़िल्म माना जा सकता है। यहां हम सर्गेइ आइसेंस्टीन की फ़िल्मों का उल्लेख कर सकते हैं। जिस समय आइसेंस्टिन ने फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा वह मूूक सिनेमा का दौर था। सिनेमा की प्रकृति, स्वरूप और प्रक्रिया पर फिल्मकार विचार करने लगे थे। इसी पृष्ठभूमि में आइसेंस्टिन ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया था। 1924 में उन्होंने अपनी पहली पूर्ण कथा फिल्म ‘स्ट्राइक’ का निर्माण किया। इसके एक साल बाद 1925 में उनकी विश्वविख्यात फिल्म ‘दि बेटलशिप पोटेम्किन’ भी प्रदर्शित हुई। इसके दो साल बाद उनकी दूसरी महत्त्वपूर्ण फिल्म ‘अक्टूबर’ प्रदर्शित हुई।
25 अक्टूबर 1917 को हुई बोल्शेविक क्रांति का एक दशक पूरा होने पर यह फिल्म बनायी गयी थी। 1924 से 1927 के बीच की तीन फिल्मों का संबंध क्रांति की पृष्ठभूमि (स्ट्राइक), क्रांति के दौर (दि बेटलशिप पोटेम्किन) और उसकी सफलता (अक्टूबर) की स्थितियों से है। इन्हें बोल्शेविक क्रांति की फिल्म-त्रयी कहा जा सकता है। ‘स्ट्राइक’ फिल्म ज़ारशाही रूस में मजदूरों की विकट स्थिति का चित्रण करती है। अपने शोषण के विरुद्ध जब वे आवाज़ उठाते हैं और संघर्ष करते हैं तो किस तरह उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए सत्ता उत्पीड़न का रास्ता अख्तियार करती है, यही इस फिल्म का विषय है। मजदूरों की हड़तालों और उनके दमन की ही परिणति 1905 की क्रांति में होती है, जिस पर आइसेंस्टिन ने अपनी दूसरी फ़ीचर फिल्म ‘दि बेटलशिप पोटेम्किन’ का निर्माण किया था।
1905 की क्रांति उससे पहले लगातार होेने वाली हड़तालों और जनसंघर्षों की परिणति ही थी। 1905 में इन हड़तालों ने राष्ट्रव्यापी विद्रोह का रूप धारण कर लिया था। कई स्थानों पर सैनिकों ने भी मजदूरों का साथ दिया और इस क्रांतिकारी उभार में शामिल हो गये। इस दौरान सिर्फ हड़तालें ही नहीं हुईं। मजदूरों ने प्रदर्शन और धरने भी दिये। यह सही मायने में एक व्यापक जन आंदोलन था जिसमें मजदूरों और विद्रोही सैनिकों और क्रांतिकारियों ने राजशाही के दमन और उत्पीड़न का जबर्दस्त प्रतिरोध किया। ‘दि बेटलशिप पोटेम्किन’ इसी जनांदोलन, विद्रोह, संघर्ष और उसके दमन की कहानी बताती है। 1905 की क्रांति नाकामयाब हुई। हजारों क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिये गये और उनमें से 1400 को फांसी दे दी गयी।
1905 की असफल क्रांति के बारह साल बाद ही अक्टूबर 1917 में रूस के मजदूरों ने बोल्शेविक क्रांतिकारियों के नेतृत्व में ज़ारशाही को उखाड़ फेंका और ब्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में मेहनतकशों की सरकार स्थापित की। यह एक नये युग की शुरुआत थी। अमरीकी लेखक जाॅन रीड ने क्रांति के दस दिनों का जो विवरण अपनी पुस्तक ‘दस दिन जब दुनिया हिल उठी’ (1919) में प्रस्तुत किया था, उसे ही आधार बनाकर आइसेंस्टिन ने अपनी अतिमहत्त्वाकांक्षी फिल्म ‘अक्टूबर’ का निर्माण किया। ‘दि बेटलशिप पोटेम्किन’ का निर्माण 1905 की क्रांति की याद में उसके बीस साल बाद किया गया था और ‘अक्टूबर’ का निर्माण क्रांति के पहले दशक की समाप्ति पर 1927 में किया गया।
बोल्शेविक क्रांति के एक दशक के अंदर बनी ये तीनों फ़िल्में जो क्रांति के विभिन्न चरणों को सिनेमा के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं, निश्चय ही इन्हें प्रचार फ़िल्म कहा जा सकता है। लेकिन ये फ़िल्में किसी समुदाय, धर्म, नस्ल या राष्ट्र के प्रति नफ़रत पर टिकी नहीं थीं। मज़दूरों और क्रांतिकारियों के संघर्ष को इनके कथानक का विषय बनाया गया था। यहां तक कि जिस जारशाही राजसत्ता के विरुद्ध यह संघर्ष किया गया था, उनका चित्रण करते हुए राजसत्ता क दमन और उत्पीड़न को जरूर चित्रित किया गया था, लेकिन इस चित्रण में सोवियत जनता के साहस और संघर्ष को केंद्र में रखा गया था। अगर हम इन फ़िल्मों की तुलना ‘बर्थ ऑफ ए नेशन’ और हिटलर के दौर में बनी यहूदी विरोधी फ़िल्मों से करें तो इन दो भिन्न तरह की प्रचार फ़िल्मों के अंतर को समझा जा सकता है।
आज हमारा देश कुछ हद तक उन्हीं परिस्थितियों के बीच से गुजर रहा है जो हिटलर के शासन के आरंभिक दौर में जर्मनी गुजर रहा था। 2014 से दिल्ली की केंद्रीय सत्ता पर एक ऐसी पार्टी काबिज है जिसका संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से है। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी और उसका उद्देश्य भारत को एक हिंदू राष्ट्र् बनाना है। वे अपनी राजनीतिक विचारधारा को हिंदुत्व नाम देते हैं। यह विचारधारा उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर से ग्रहण की थी जिन्होंने 1923 में ‘हिंदुत्व’ नामक पुस्तक लिखी थी। आरएसएस ने अपने इस राजनीतिक उद्देश्यों को कभी छुपाया नहीं। इस संगठन के दूसरे सरसंघचालक एम एस गोलवलकर ने अपनी पुस्तक ‘वी ऑर अवर नेशनहुड’ में उन्होंने जो विचार पेश किये उसके पीछे फासीवाद और नाज़ीवाद का प्रभाव भी था। इस पुस्तक में गोलवलकर यह प्रश्न उठाते हैं कि ‘अगर निर्विवाद रूप से हिंदुस्थान हिंदुओं की भूमि है और केवल हिंदुओं ही के फलने-फूलने के लिए है, तो उन सभी लोगों की नियति क्या होनी चाहिए जो इस धरती पर रह रहे हैं, परंतु हिंदू धर्म, नस्ल और संस्कृति से संबंध नहीं रखते’ (गोलवलकर की हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा : एक आलोचनात्मक समीक्षा, शम्सुल इस्लाम, फारोस, नयी दिल्ली, पृ. 199)।
स्वयं द्वारा उठाये इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वे लिखते हैं कि ‘वे सभी जो इस विचार की परिधि से बाहर हैं, राष्ट्रीय जीवन में कोई स्थान नहीं रख सकते। वे राष्ट्र का अंग केवल तभी बन सकते हैं जब अपने विभेदों को पूरी तरह समाप्त कर दें। राष्ट्र का धर्म, इसकी भाषा एवं संस्कृति अपना लें और खुद को पूरी तरह राष्ट्रीय नस्ल में समाहित कर दें। जब तक वे अपने नस्ली, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अंतरों को बनाये रखते हैं, वे केवल विदेशी हो सकते हैं, जो राष्ट्र के प्रति मित्रवत हो सकते हैं या शत्रुवत्त’ (वही, 199)। गोलवलकर की इन बातों का अर्थ यही है कि भारत केवल हिंदुओं का राष्ट्र् है और बाकी सभी धार्मिक और नस्ली समुदाय विदेशी हैं। वे भारत में रह सकते हैं लेकिन जब वे ‘अपने विभेदों को पूरी तरह समाप्त कर दें’ और ‘खुद को पूरी तरह राष्ट्रीय नस्ल में समाहित कर दें’। अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि ‘अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें राष्ट्र के रहमो-करम पर, सभी संहिताओं और परंपराओं से बंधकर केवल एक बाहरी की तरह रहना होगा, जिनको किसी अधिकार या सुविधा की तो छोड़िए, किसी विशेष संरक्षण का भी हक़ नहीं होगा’ (वही, पृ. 201-202)। अगर वे अपने को राष्ट्रीय नस्ल में समाहित नहीं करते हैं तो ‘जब तक राष्ट्रीय नस्ल उन्हें अनुमति दें वे यहां उसकी दया पर रहें और राष्ट्रीरय नस्ल की इच्छा पर यह देश छोड़कर चले जाएं’।
यह संयोग नहीं है कि आरएसएस ने अपनी प्रेरणा फासीवाद और नाजीवाद से ग्रहण की है। इस पुस्तक में गोलवलकर ने अल्पसंख्यकों के प्रति जर्मनी और इटली ने जो रवैया अपनाया, उसकी न केवल प्रशंसा की बल्कि उसे अनुकरणीय भी माना। वे इसी पुस्तक में लिखते हैं, ‘जर्मन नस्ल का गर्व आज चर्चा का विषय बन गया है। नस्ल तथा उसकी संस्कृति की शुद्धता बनाए रखने के लिए देश को सामी नस्लों—यहूदियों—से स्वच्छ करके जर्मनी ने पूरी दुनिया को पूरी तरह स्तब्ध कर दिया है। यहां नस्ल का गौरव अपने सर्वोच्च रूप में अभिव्यक्त हुआ है। जर्मनी ने यह भी दिखा दिया है कि किस तरह नस्लों तथा संस्कृतियों का, जिनकी भिन्नताएं उनकी जड़ों तक जाती हैं, एक एकीकृत समग्रता में घुलना-मिलना लगभग असंभव ही है। यह हिंदुस्थान में हमारे लिए एक अच्छा सबक है कि सीखें और लाभान्वित हों’ (वही, पृ. 189-190)।
आरएसएस से संबद्ध राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी (जिसका पहले नाम भारतीय जनसंघ था) जब-जब सत्ता में आयी है, चाहे राज्यों में या केंद्र में उसने उस दिशा में लगातार कदम उठाये जो आरएसएस की सांप्रदायिक फासीवादी विचारधारा के पक्ष में जाते हैं। लेकिन 2014 में जबसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, हिंदू राष्ट्र बनाने के अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ी है। लेकिन इस काम में सफलता तभी हासिल हो सकती है जब व्यापक हिंदू जनता का समर्थन उसे मिले। इस दिशा में तो आरएसएस और उससे संबद्ध सभी संगठन ज़मीनी स्तर पर हमेशा काम करते रहे हैं लेकिन सत्ता में आने पर वे पूरे सरकारी तंत्र का भी निर्लज्जतापूर्वक अपने लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। इनमें पाठ्यक्रमों में फेरबदल, हिंदुत्वपरस्त सांप्रदायिक इतिहास लेखन और अपनी विचारधारा के प्रचार के लिए मीडिया का इस्तेमाल शामिल हैं।
लेकिन सबसे प्रभावी माध्यम सिनेमा है जिसका 2014 से हिंदुत्व की विचारधारा के प्रचार के लिए लुका-छिपा और कई बार बिल्कुल नग्न रूप में इस्तेमाल होता रहा है। इस आलेख में आगे ऐसी कई फ़िल्मों पर विचार करेंगे। लेकिन उनसे विचार करने से पहले हिंदी सिनेमा की आठवें-नवें दशक की उन फ़िल्मों पर भी गौर करना जरूरी है जिन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं और मूल्यों के कमजोर होते जाने ने विकल्प के रूप में उन गैरलोकतांत्रिक प्रवृत्तियों को बल दिया जो अंतत: देश को फासीवाद की ओर धकेलने में सहायक बनीं। लोकतंत्र के कमजोर होने की आलोचना यदि इस तरह की फ़िल्मों का सकारात्मक पक्ष था, तो इसका नकारात्मक पक्ष यह था कि सिनेमा जन आंदोलनों की बजाय निजी स्तर पर प्रतिशोध को हल के रूप में पेश करने लगा। प्रतिशोध की जो परंपरा ‘जंजीर’ से शुरू हुई वह लगभग तीन दशकों तक हिंदी सिनेमा की मुख्य प्रवृत्ति के रूप में लगातार मजबूत होती गयी। धीरे-धीरे यह प्रतिशोध जो पहले अपराधियों के विरुद्ध था, वह 1990 के दशक से आतंकवाद के विरुद्ध केंद्रित होने लगा और इसका वैचारिक आधार बना अंधराष्ट्रवाद।
इसकी पराकाष्ठा 2008 में प्रदर्शित हिंदी फ़िल्म ‘ए वेडनेस्डे’ में दिखायी देती है जो आतंकवाद के विरुद्ध ‘प्रतिशोधी आतंकवाद’ को जायज ठहराती है और आतंकवाद के विभिन्न रूपों की बजाय केवल इस्लामी आतंकवाद को ही अपने निशाने पर लेती है। इस फ़िल्म को काफी लोकप्रियता प्राप्त हुई और इस तरह की फ़िल्में दर्शकों के बीच इस विचार को लोकप्रिय बनाने में सहायक बनीं कि इस्लामी आतंकवाद ही आतंकवाद है और उसके विरुद्ध उठाया जाने वाला हर कदम चाहे वह कितना ही गैरकानूनी क्यों न हो, जायज है। इस तरह पिछले तीन-चार दशकों से हिंदी सिनेमा अपने दर्शकों को फासीवादी सोच की ओर धकेलती जा रही है और आज हम एक ऐसे मुक़ाम पर पहुंच गये हैं जहां कुछ आतंकवादियों को नहीं पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय को देश का दुश्मन और आतंकवाद का समर्थक बताया जा रहा है। उनका होना ही देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ‘द कश्मीर फाइल्स’ और ‘द केरला स्टोरी’ के माध्यम से भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को ऐसे स्याह रंग में पेश किया गया है जो देश के शत्रुओं के साथ मिलकर बहुसंख्यक हिंदुओं को अपने ही देश में अल्पसंख्यक बनने के लिए मजबूर कर दे और देश का एक बार फिर से विभाजन हो जाये।
इन दोनों फ़िल्मों पर विचार करने से पहले पिछले दो दशकों में बनी उन फ़िल्मों पर भी विचार करने की जरूरत हैं जो भारत के इतिहास और वर्तमान को तथ्यों की बजाय सांप्रदायिक पूर्वाग्रह के साथ तोड़-मरोड़कर पेश करती हैं। मणिरत्नम की फ़िल्म ‘बोंबे’ और ‘रोजा’ में मुसलमान समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह साफ तौर पर देखा जा सकता है। ‘बोंबे’ में सांप्रदायिक दंगों के लिए जहां एक ओर मुसलमानों को गुनहगार बताया गया है तो दूसरी ओर ‘रोजा’ में मुसलमानों को आतंकवादी और स्त्री-विरोधी दिखाया जाता है। इन फिल्मों के ही हिंदू पात्रों से तुलना करने पर दो समुदायों के पक्षपातपूर्ण चित्रण को आसानी से पहचाना जा सकता है।
इतिहास में से ऐसे नायकों को चुना जा रहा है जिन्हें मुस्लिम शासकों के विरुद्ध देशभक्त नायक के रूप में पेश किया जा सके। चाहे वह तान्हा जी हो, या पृथ्वीराज चौहान या चितौड़ की पद्मावती जिसे दिल्ली का मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी हासिल करना चाहता था। यहां संजय लीला भंसाली की फ़िल्म ‘पद्मावत’ का उदाहरण लिया जा सकता है जिन्होंने इस फ़िल्म में अलाउद्दीन खिलजी को एक क्रूर और बर्बर मुस्लिम शासक के रूप में ही पेश नहीं किया, साथ ही फ़िल्म में सती-प्रथा का महिमा-मंडन भी किया गया। फ़िल्म में अलाउद्दीन खिलजी को जिस ढंग से पेश किया गया है, वह ऐतिहासिक अलाउद्दीन से मेल नहीं खाता, वह ‘पदमावत’ महाकाव्य के अलाउद्दीन से भी मेल नहीं खाता। श्याम बेनेगल के धारावाहिक ‘भारतः एक खोज’ के एपिसोड 25 में ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अलाउद्दीन के जीवन और कार्यों से जुड़े प्रसंगों का नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया गया था। उसे देखने से स्पष्ट हो जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो छवि फ़िल्म ‘पद्मावत’ में गढ़ी गयी है, वह पूरी तरह से अनैतिहासिक और काल्पनिक है।
फ़िल्म में अलाउद्दीन खिलजी को बर्बर, हिंसक और व्यभिचारी बताया गया है। जिस तरह उसे अपने नजदीकी लोगों की निर्मम हत्या करते हुए, औरतों को अपनी हवस का शिकार बनातेे हुए दिखाया गया है वह उसके वास्तविक चरित्र से मेल नहीं खाता। लंबे और खुले बाल रखना, क्रूर हँसी हँसना, मांस को जानवरों की तरह खाना, यहां तक कि नाचते और गाते हुए भी शरीर और चेहरे पर क्र्रूर भाव प्रकट करना उसके चरित्र को एक खास सांचे में ढालता है। इसके विपरीत रतनसेन को सुसंस्कृत, सभ्य और शिष्ट आचरण करता हुआ दिखाया गया है। एक ओर खिलजी अपनी पत्नी मेहरुन्निसा के साथ क्रूर ढंग से पेश आता है, उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करता है जबकि रतनसेन पद्मिनी के सम्मान का सदैव ध्यान रखता है।
खिलजी से मेहरुन्निसा भय खाती है जबकि पद्मिनी रतनसेन से प्रेम करती है और पति की सेवा करना ही अपना धर्म समझती है। उसके लिए अपने प्राणों तक की आहूति देने को तैयार हो जाती है। खिलजी के खाने के असभ्य तरीके के विपरीत रतनसेन के यहां जब अलाउद्दीन के सामने चांदी की थाली में भोजन पेश किया जाता है तो ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया है कि वह शाकाहारी भोजन है और जिसे बहुत ही शिष्टाचार के साथ पेश किया गया है। खिलजी और रतनसेन की यह जो भिन्न और विपरीत छवियां पेश की गयी है, उसके पीछे की प्रेरणा विद्वेेषपूर्ण और सांप्रदायिक है। यह उस सांप्रदायिक और सवर्ण हिंदू मानसिकता को पुष्ट करती है जिसके अनुसार हिंदू शाकाहारी होता है, अहिंसक होता है और स्त्री को देवी समझ कर पूजा करता है जबकि मुसलमान मांसाहारी होता है, हिंसक और बर्बर होता है और स्त्री पर अत्याचार करने वाला व्यभिचारी होता है। फ़िल्म के अनुसार खिलजी इसी बर्बर मुस्लिम मानसिकता का प्रतिनिधि है और रतनसेन और पद्मिनी सुसंस्कृत हिंदू मानसिकता का।
फ़िल्म आरंभ से अंत तक राजपूती गौरव का महिमामंडन करती है। उन्हें ऐसी वीर जाति के रूप में पेश किया गया है जो अपने आत्मसम्मान के लिए अपनी जान दे भी सकती है और जान ले भी सकती है। इसी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए राजपूती स्त्रियां सामूहिक आत्मदाह करने से भी नहीं डरती। फ़िल्म के आरंभ में यद्यपि कहा गया है कि फ़िल्म सती प्रथा का समर्थन नहीं करती लेकिन फ़िल्म में जौहर के पूरे कृत्य को जिस विस्तार से धार्मिक परंपरा का पालन करते हुए भव्यता से दिखाया गया है वह शर्मनाक भी है और खतरनाक भी। संजय लीला भंसाली ने जौहर को युद्ध का ही एक रूप बताकर उसका औचित्य सिद्ध करने की कोशिश की है। जबकि यह पितृसत्तात्मक सोच का सर्वाधिक घृणित रूप है जो सतीत्व की रक्षा के नाम पर स्त्री को जबरन हत्या और आत्महत्या की ओर धकेलता है।
इन फ़िल्मों का एक पहलू राष्ट्र्वाद भी है। पृथ्वीराज चौहान हो या तान्हा जी, राजा रत्नसेन हो या कोई अन्य राजपूत और मराठा शासक इन सबको जिन मुस्लिम शासकों से संघर्ष करते हुए दिखाया जाता है उन्हें फ़िल्मों में विदेशी आक्रांता रूप में पेश किया जाता है, भले ही उनकी कई पीढ़ियां हिंदुस्तान में रहती आयी हों। विडंबना तो यह है कि फ़िल्मों में जिस राष्ट्रवाद की जय जयकार की जाती है, वह केवल मुस्लिम शासकों के विरुद्ध ही सक्रिय नज़र आता है यहां तक कि मुसलमानों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए अंग्रेज शासकों की गुलामी को भी जायज ठहराया जाता है।
अक्षय कुमार के नायकत्व वाली फ़िल्म ‘केसरी’ का उदाहरण दिया जा सकता है जहां उन सिख सैनिकों को अफ़गान के मुसलमानों से लड़ते हुए दिखाया गया है जो अपने देश पर हुए अंग्रेज हमलावरों का साहसपूर्ण मुकाबला कर रहे होते हैं। लेकिन भारतीय सैनिक अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले अफ़गान कबीलों का अंग्रेजों की तरफ से मुकाबला करते हैं और फ़िल्म में इन्हें वीर देशभक्त कहा गया है जबकि उनकी हैसियत अंग्रेजी उपनिवेशवाद के गुलामों से ज्यादा नहीं थी। भारत की आज़ादी की लंबी लड़ाई का इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है।
इस दौरान सिनेमा के माध्यम से आधुनिक इतिहास के विकृतिकरण की कई कोशिशें भी सामने आयी हैं और भविष्य में भी आने वाली हैं। ऐसी ही एक कोशिश राजकुमार संतोषी की फ़िल्म ‘गांधी-गोडसे : एक युद्ध’ के माध्यम से सामने आयी है। हिंदी के प्रख्यात कथाकार असग़र वजाहत के नाटक ‘’गोडसे@गांधी.कॉम’ पर आधारित है जिसमें यह कल्पना की गयी है कि यदि गांधीजी गोडसे की गोलियों से न मरे होते तो उनके साथ क्या होता। फ़िल्म जिस तरह प्रस्तुत की गयी है, उससे स्पष्ट है कि पूरी फ़िल्म संघ परिवार के राजनीतिक एजेंडे का जाने-अनजाने अनुसरण करती है। कांग्रेस और नेहरू के प्रति जो नफरत संघ परिवार व्यक्त करता रहा है, फ़िल्म उस नफरत को बढ़ाने में ही योग देती है।
फ़िल्म पूरी दृढ़ता से यह स्थापित करती है कि नाथुराम गोडसे एक साहसी और सच्चा देशभक्त था। गांधी की हत्या उसने जरूर की जिसके लिए उसे माफ कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि गांधी जी ने तो उसे माफ कर दिया था। लेकिन अगर गांधी जिंदा रहते तो नाथुराम गोडसे नेहरू और कांग्रेस से कहीं ज्यादा गांधी के नजदीक होता और शायद उनका प्रिय भी। दरअसल, यह फ़िल्म गांधी को संघ परिवार में समायोजित करने, नेहरू और कांग्रेस को खलनायक बताने और राष्ट्रीय आंदोलन की गौरवशाली परंपरा को बदनाम करने और हिंदुत्ववादी नाथुराम गोडसे को महान देशभक्त और जननायक के रूप में स्थापित करने के संघी अभियान की कोशिश ओर सांप्रदायिक फासीवादी विचारधारा के प्रसार का हथियार बन गयी है।
यह महज संयोग नहीं है कि हिंदू महासभा के नेता और अंग्रेज सरकार से बारबार माफी मांगने वाले और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे के मेंटर विनायक दामोदर सावरकर पर भी शीघ्र ही ‘स्वतंत्र वीर सावरकर’ नामक फ़िल्म रिलीज होने वाली हैं। फ़िल्म के टीजर को देखकर ही पता चल जाता है कि इस फ़िल्म की बुनियाद झूठ पर रखी गयी है। फ़िल्म बताती है कि आजादी की लड़ाई सिर्फ 90 साल यानी 1857 से 1947 के बीच ही चली जबकि यह लड़ाई लगभग दो सौ साल चली 1747 से लेकर 1947 तक। न केवल राजाओं और नवाबों ने बल्कि किसान जनता ने भी कई युद्ध लड़े। संन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, टीपू सुलतान और उनके पिता ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किये थे और अपना बलिदान दिया था। इस टीजर में यह भी कहा गया है कि आज़ादी की लड़ाई कुछ ही लोगों ने लड़ी बाकी सब सत्ता के भूखे थे। यह बात वे ही कह सकते हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया या जिन्होंने इस लड़ाई के साथ विश्वासघात किया।
टीजर में यह भी बताया गया है कि अगर महात्मा गांधी के अहिंसावाद पर देश नहीं चलता तो आजादी 35 साल पहले मिल चुकी होती। यानी कि 1947 में नहीं बल्कि 1912 में। ऐसे झूठ बोलते हुए यह भूल जाते हैं कि महात्मा गांधी 1912 में दक्षिण अफ्रीका में थे और 1915 में वे वापस लौटे थे। 1917 में उन्होंने पहला जनआंदोलन किया था जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। हद तो तब हो गयी कि टीजर में यह भी दावा किया गया है कि सावरकर से सुभाषचंद्र बोस, भगतसिंह और खुदीराम बोस ने प्रेरणा ग्रहण की थी। खुदीराम बोस 1908 में शहीद हो गये थे तब तक सावरकर विदेश से लौटे भी नहीं थे। जिस समय खुदीराम बोस शहीद हुए उस समय उनकी उम्र महज 18 साल थी।
जहां तक भगतसिंह और सुभाषचंद्र बोस का सवाल है, वे सावरकर की सांप्रदायिक राजनीति के घोर विरोधी थे और जब भगतसिंह को फांसी हो रही थी, तब सावरकर ने उनके समर्थन में एक शब्छ तक नहीं कहा। दरअसल सावरकर मौजूदा शासकों के प्रेरणा स्रोत हैं। वे उसी हिंदुत्व में यकीन करते हैं जिसकी अवधारणा सबसे पहले सावरकर ने ही पेश की थी। यह महज संयोग नहीं है कि सावरकर के जन्मदिन पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन की नयी इमारत का उद्घाटन किया था।
1965 में हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान युद्ध के बाद सोवियत संघ के शहर ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था और उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में ही ह्रदयाघात से मौत हो गई थी। उस समय संघ और उनके संगठनों ने इस झूठ को पूरे देश में फैलाया था कि ताशकंद में शास्त्री की मृत्यु दरअसल साजिश के तहत हत्या थी। बिना किसी प्रमाण के यह अफवाह फैलायी गयी और इसी अफवाह को ‘दि ताशकंद फाइल्स’ नाम से विवेकरंजन अग्निहोत्री ने फ़िल्म का रूप दे दिया।
ये फ़िल्में इस बात का प्रमाण है कि मौजूदा सांप्रदायिक राजसत्ता की विचारधारा से प्रेरित होकर कई फ़िल्मकार ऐसी फ़िल्में बना रहे हैं जिनमें भारत के इतिहास को विकृत रूप में पेश किया गया है और इस तरह जनता को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन इनसे भी ज्यादा खतरनाक वे फ़िल्में हैं जो ऐसे संवेदनशील घटनाओं के माध्यम से सामने आयी हैं जो बहुत ही क्रूर और हिंसक रूप में मुस्लिम समुदाय को पेश करती हैं और इस तरह हिंदू जनता के मन में अपने ही पड़ोसी भाइयों के प्रति नफरत और घृणा का प्रचार करती हैं। उनके मन में मिथ्या भय भरा जा रहा है कि उसका पड़ोसी मुसलमान ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है जो मुस्लिम देशों और इस्लामी आतंकवादियों के साथ साजिश करके इस देश को मुस्लिम राष्ट्र् बनाने के अभियान में जुटा है। ये फ़िल्में हैं : ‘दि कश्मीर फाइल्स’ और ‘दि केरला स्टोरी’।
‘दि कश्मीर फाइल्स’ (2022) कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के जबरन पलायन पर बनायी गयी फ़िल्म है। फ़िल्मकार का दावा है कि यह कश्मीरी पंडितों से लिये गये साक्षात्कारों पर आधारित है कि किस तरह कश्मीरी पंडितों की हत्याएं की गयीं और उनको कश्मीर घाटी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र कृष्ण पंडित जिसके माता-पिता इस्लामी आतंकवादियों के द्वारा मारे गये थे, की हत्या के वास्तविक कारणों की खोज करता है और उसे मालूम पड़ता है कि किस तरह घाटी के मुसलमानों के सहयोग और समर्थन से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया गया था।
फ़िल्म 1990 के हालात के इर्द-गिर्द बुनी गयी है और कश्मीर के हालात के लिए कश्मीरी मुसलमानों को कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराती है। फ़िल्म आतंकवादियों के हाथों मारे गये कश्मीरी मुसलमानों का बिल्कुल उल्लेख नहीं करती और न ही वहां तैनात भारतीय सेना के हाथों मारे गये निर्दोष कश्मीरी मुसलमानों की हत्या के बारे में भी चुप रहती है जो कश्मीरी पंडितों की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में मारे गये हैं। इस तरह यह फ़िल्म कश्मीरी पंडितों के पलायन की एकतरफा कहानी कहती है, न कि कश्मीर के यथार्थ को समग्रता में और निष्पक्ष रूप में प्रस्तुत करती है।
इस फ़िल्म को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कश्मीरी मुसलमानों को सांप्रदायिक और राष्ट्रद्रोही के रूप में और पाकिस्तान के समर्थक के रूप में रखती है जबकि सच्चाई यह है कि कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए बहुत से मुसलमान न केवल आगे आये बल्कि इस कारण उनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। कांग्रेस, नेशनल कान्फ्रेंस के बहुत से कार्यकर्ता और नेता दहशतगर्दों के हाथों मारे गये थे। कश्मीर के मौजूदा यथार्थ पर और भी कई फ़िल्में बनी हैं, मसलन, विनोद भारद्वाज की ‘हैदर’ और एजाज़ खान की फ़िल्म ‘हामिद’ का उल्लेख किया जा सकता है जो कश्मीर के अंदरुनी हालात को ज्यादा ईमानदारी और वस्तुपरक ढंग से पेश करती हैं।
दरअसल, ‘दि कश्मीर फाइल्स’ झूठे प्रचार पर आधारित एक सांप्रदायिक दृष्टिकोण की अत्यंत साधारण प्रोपेगेंडा फ़िल्म है जो हिंदुओं को भड़काने का काम करती है। इस फ़िल्म को इतना अधिक महत्व इसलिए मिला क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फ़िल्म को देखने का आह्वान किया और यह दावा किया कि इस फ़िल्म में कश्मीरी पंडितों के बारे में उस सच्चाई को सामने रखा गया है जिसे आज तक देश से छुपाया गया है जबकि इस फ़िल्म में ऐसा कुछ नहीं है जिससे देश की जनता पहले से परिचित नहीं रही हो। इस फ़िल्म को लोकप्रिय बनाने के लिए भाजपा की राज्य सरकारों ने टैक्स माफी से लेकर अपने कर्मचारियों को छुट्टी देकर उन्हें फ़िल्म देखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। लेकिन इस फ़िल्म ने जनता के दिमागों में सांप्रदायिक जहर भरने का ही काम किया। यह फ़िल्म इस हद तक नफरत और घृणा फैलाने वाली थी कि भारत में होने वाले फ़िल्म फेस्टिवल में इसराइल के फ़िल्मकार और जूरी अध्यक्ष नादव लेपिड ने एक वल्गर प्रोपेगेंडा फ़िल्म कहकर इसकी भर्त्सना की थी।
अभी हाल ही में प्रदर्शित फ़िल्म ‘दि केरला स्टोरी’ (2023) ‘दि कश्मीर फाइल्स’ से एक कदम आगे कही जा सकती है, जो पूरी तरह से एक ऐसे मुद्दे पर बनायी गयी है, जो आरएसएस और उससे संबद्ध संगठनों द्वारा फर्जी रूप से प्रचारित किया गया है। वह मुद्दा है, लव जिहाद का। फ़िल्म का दावा है कि केरल राज्य से 32000 हिंदू लड़कियों की ब्रेन वाशिंग करके और मुस्लिम लड़कों के जाल में फंसाकर उन्हें शादी करने के लिए मजबूर किया गया, उनका धर्म परिवर्तन किया गया और बाद में उनके कथित पतियों के साथ सीरिया, यमन आदि इस्लामी देशों में आइएसआइएस जैसे आतंकवादी संगठनों में सेक्स स्लेव के रूप में भेज दिया गया। इन बतीस हजार औरतों का आज कुछ भी पता नहीं है। उनके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता।
जब बतीस हजार की संख्या को कोर्ट में चुनौती दी गयी तो फ़िल्म के निर्माता और निर्देशक ने बताया कि यह सरकारी आंकड़ा है लेकिन जब यह कहा गया कि केरल सरकार ने कभी भी यह आंकड़ा नहीं पेश किया केवल पूर्व मुख्यमंत्री ऑमन चंडी ने वे आंकड़े जरूर पेश किये थे जिसमें हिंदू, मुसलमान और ईसाई धर्मावलंबियों ने अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अंगीकार कर लिया था और वह संख्या दो-ढाई हजार से ज्यादा नहीं थी। उस समय मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इन में से कोई भी जबरन धर्मपरिवर्तन का मामला नहीं था। फ़िल्मकार ने जब कोई प्रमाण पेश नहीं किया तो कोर्ट के आदेश पर 32000 के इस आंकड़े को हटा दिया गया और इस संख्या को घटाकर केवल तीन कर दिया गया। कथित रूप से जिन तीन लड़कियों की कहानी फ़िल्म में कही गयी है और जिसके बारे में फ़िल्मकार का दावा है कि यह सत्य घटनाओं पर आधारित है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी दि ‘केरला स्टोरी’ पर आदेश पारित करते हुए ‘कोर्ट ने निर्माताओं से एक डिस्क्लेमर जोड़ने को कहा कि ये घटनाओं का काल्पनिक लेखा-जोखा है और इसका कोई डेटा नहीं है जो इस दावे का समर्थन करते हैं कि केरल में 32000 महिलाओं को इस्लाम में परिवर्तित होने और आतंकवादी समूह आईएसआईएस में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था’। लेकिन कोर्ट ने फ़िल्म को न केवल प्रतिबंधित करने से इन्कार कर दिया बल्कि पश्चिम बंगाल की सरकार के प्रतिबंध लगाने के आदेश को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज ने कहा था कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं घटा है जिससे शांति भंग होने की आशंका हो।
लेकिन फ़िल्म देखकर लौटने वालों की प्रतिक्रिया बताती है कि यह फ़िल्म ‘दि कश्मीर फाइल्स’ से कहीं ज्यादा मुस्लिम विरोधी प्रचार करने और लोगो के दिमागों में जहर भरने में कामयाब हो रही है। लोग यहां तक प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को जबरन निकाल बाहर किया जाना चाहिए या उनका खात्मा कर दिया जाना चाहिए। लोग यह भी प्रतिक्रिया व्यक्त् कर रहे हैं कि हर हिंदू माता-पिता को चाहिए कि वे इस फ़िल्म को देखें और अपनी बेटियों को भी दिखायें। स्पष्ट है कि यह फ़िल्म न केवल हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा कर रही हैं बल्कि अपने घर-परिवार की बहू-बेटियों पर अंकुश लगाकर उनकी आज़ादी छीनना चाहते हैं।
भारत का संविधान प्रत्येक बालिग नागरिक को यह आजादी देता है कि वह किसी भी धर्म, जाति और नस्ल के व्यक्ति से विवाह कर सकते हैं। लेकिन ‘लव जिहाद’ के झूठ के बहाने हिंदू परिवारों में मुस्लिम समुदाय के प्रति नफ़रत और घृणा ही नहीं उन्हें उनसे दूर रहने का भी आह्वान करती है। इसका अर्थ यह भी है कि मुसलमानों से किसी भी तरह के सामाजिक और वैयक्तिक संपर्क रखने से बचा जाये।ये फ़िल्में दरअसल देश को नफरत और घृणा के ऐसे दलदल में धकेल रही है कि इसका परिणाम गृहयुद्ध में निकल सकता है। यह फ़िल्म न केवल हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा कर रही हैं बल्कि अपने घर-परिवार की बहू-बेटियों पर अंकुश लगाकर उनकी आज़ादी छीनने को भी प्रेरित कर रही है।
भारत का संविधान प्रत्येक बालिग नागरिक को यह आजादी देता है कि वह किसी भी धर्म, जाति और नस्ल के व्यक्ति से विवाह कर सकते हैं। लेकिन ‘लव जिहाद’ के झूठ के बहाने हिंदू परिवारों में मुस्लिम समुदाय के प्रति नफ़रत और घृणा ही नहीं उन्हें उनसे दूर रहने का भी आह्वान करती है। इसका अर्थ यह भी है कि मुसलमानों से किसी भी तरह के सामाजिक और वैयक्तिक संपर्क रखने से बचा जाये। मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध भड़काने की इन कार्रवाइयों के बावजूद भारत के मुसलमान जिनकी आबादी बीस करोड़ से ज्यादा है, काफी संयम से काम ले रहे हैं।
आइएसआइएस जैसे संगठनों में जिनमें सौ से अधिक देशों के लोग शामिल है, भारत के सौ नागरिक भी मुश्किल से हैं। इस्लामी आतंकवाद के सबसे बड़े संगठन जिसकी सदस्य संख्या लगभग चालीस हजार बतायी जाती है, उसमें मुस्लिम आबादी के तीसरे सबसे बड़े देश भारत के महज सौ लोगों का शामिल होना इस देश की धर्मनिरपेक्षता की मजबूत बुनियाद को दर्शाता है और जिसे मौजूदा सरकार खोखला करने में लगी है। ऐसी फ़िल्में इस काम को और आसान कर देती है।
सिनेमा का अपने राजनीतिक प्रचार के लिए इस्तेमाल करने की आरएसएस-भाजपा की मुहिम कामयाबी के साथ जारी है। इतिहास के सांप्रदायीकरण और विकृतिकरण के बाद अब उनकी नज़र लोकप्रिय हिंदू पौराणिक कथाओं की ओर गयी है। ‘आदिपुरुष’ एक ऐसी ही फ़िल्म है जिसमें रामायण की कथा का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले तक हिंदी में रामकथा को चाहे वह फ़िल्मों में इस्तेमाल हुई हो या टेलीविजन धारावाहिक के रूप में धार्मिक आख्यान के लोकप्रिय दृश्यांकन पर ही बल रहा है और ऐसा करते हुए रामायण के सभी प्रमुख चरित्रों को ठीक वैसा ही रहने दिया गया है जो वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कृत रामचरितमानस में व्यक्त हुए हैं। रामायण के ये चरित्र जनमानस में भी इन्हीं ग्रंथों के आधार पर ही अपना अस्तित्व बनाये हुए हैं।
लेकिन पहली बार रामायण की कथा को और उनके चरित्रों को मौजूदा सांप्रदायिक राजनीति की जरूरत के अनुसार ढालने की कोशिश की गयी है। रावण जो पौराणिक आख्यान में एक ब्राह्मण है इस फ़िल्म में एक क्रूर मुस्लिम शासक की तरह नज़र आता है। सोने की बनी लंका स्याह रंग की नजर आती है। बजरंग बली हनुमान नहीं बल्कि बजरंग दल के नेता नजर आते हैं जिनकी भाषा भी टपोरियों जैसी हैं। राम जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में देखा जाता रहा है, वह इस फ़िल्म में एक उग्र युद्धोन्मादी शासक नज़र आते हैं। संवादों को भाजपा के राजनीतिक लक्ष्यों के वाहक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है।
‘भगवा झंडा गाड़ देंगे’ जैसे चलताऊ संवाद राम के मुख से कहलाया गया है। फ़िल्म निर्देशक ओम राउत ने दावा किया है कि फ़िल्म की कहानी ‘वाल्मीकि रामायण’ पर आधारित है लेकिन यदि ऐसा होता तो राम नहीं सीता कथा के केंद्र में होती। वाल्मीकि रामायण में राम द्वारा सीता को वनवास भेजना, लव-कुश का राम से युद्ध होना और सीता का धरती में समा जाना इन प्रसंगों को उठाने की हिम्मत जाहिर है कि पितृसत्ता में यकीन करने वाले दक्षिणपंथी सांप्रदायिक राजनीति में यकीन करने वाले फ़िल्मकार कभी नहीं कर सकते।
वीएफएक्स का अधिकतम इस्तेमाल करके चमत्कारों से चकाचौंध करने की कोशिश मुमकिन है कि फ़िल्म को बॉक्स ऑफिस पर कामयाब बना दे लेकिन क्या हिंदू जनता राम, सीता आदि की परंपरागत छवियों के इस विकृतिकरण को सहज ही स्वीकार करेगी और अगर ऐसा करती है तो यह इस बात का प्रमाण होगा कि सांप्रदायिक फासीवादी राजनीति के चंगुल में फंसती जा रही जनता अपनी सांस्कृतिक परंपरा से पूरी तरह विच्छिन्न हो चुकी है और अब उनके लिए धर्म, पुराण कथाएं और आराध्य देवी-देवताओं का ज्ञान भी व्हाट्सअप विश्वविद्यालयों से हासिल कर रहे हैं।
(जवरीमल्ल पारख साहित्य और सिनेमा के गंभीर अध्येता हैं। गुडगांव में रहते हैं।)