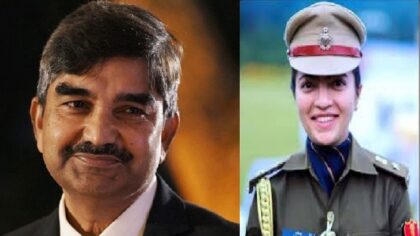संस्कृति के लाक्षागृह में प्रवेश कर चुके लोकतंत्र के बचाव लिए जन-गंगा तक पहुंचने के लिए कोई तो सुरंग होनी चाहिए। भारत की लोकतांत्रिक राजनीति की भयानक स्थिति यह है कि एक तरफ लाक्षागृह में आग लगी है और दूसरी तरफ जन-गंगा खौल रही है।
सुरंग में अटका लोकतंत्र अब करे तो, क्या करे! वर्तमान सत्ताधारी दल और उसके नेतागण जब 1975 की इमरजेंसी की याद इस मासूमियत से करते हैं, जैसे वे दिन कितने बुरे थे और आज के दिन कितने अच्छे हैं! निश्चित रूप से भारत के लोकतंत्र के लिहाज से वे दिन बहुत बुरे थे, लेकिन इस का मतलब यह नहीं है कि आज के दिन बहुत अच्छे हैं।
लिखित-अलिखित या घोषित-अघोषित के अंतर को ठीक से समझा जा सके तो लोकतंत्र के लिहाज से आज के दिन इमरजेंसी के दिन से भी बहुत बुरे हैं।
संविधान की चर्चा करती हुई संसद वहां तक पहुंच गई, जहां तक पहुंच जाने की आशंका किसी को नहीं थी। अब तो खुले आम आपराधिक षडयंत्र रचे जा रहे हैं! कौन रच रहा है? जिन लोगों को अपराध के घटने देने से रोकने का पदाधिकार प्राप्त है, वे ही आपराधिक षडयंत्र रचने में लगे हुए हैं।
अनोखी बात यह है कि नाखून कटवाकर शहीद की लाइन में खड़े होनेवालों की जमातवाले अपने पक्ष में सहानुभूति की लहर बनाने में कामयाब भी हो रहे हैं। भारत के आजादी के आंदोलन में बहुत सारे लोगों की भागीदारी रही है। उसके नायक भी अनेक हैं, भले ही ‘वीर पूजा’ कुछ की ही होती है, पूजा का प्रसाद कुछ को ही मिलता है।
आजादी को ठोस रूप देनेवालों में भी अनेक का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आजादी के मतलब को जमीनी स्वरूप देनेवाले वास्तविक शिल्पकार के रूप में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हमेशा याद किये जायेंगे।
सत्ता-लोलुपता और सत्ता अहंकार का मिश्रित प्रभाव में अपमानजनक तरीके से बाबासाहेब के उल्लेख के विरोध के प्रति सत्ताधारी दल भले ही ऊपर-ऊपर से आक्रामक दिखने की कोशिश में विपक्ष के विरुद्ध आपराधिक षडयंत्र रचने में लगे हुए हैं, लेकिन वे भीतर-ही-भीतर हिले हुए हैं।
उन्हें पता है कि वे अपनी विचारधारा को स्थाई रूप से स्थापित करने के निर्णायक दौर में हैं। हजारों साल से चलते आये समानता के हक, सभ्य एवं उत्तरोत्तर बेहतर जीवन-मूल्यों और जीवनयापन के तौर-तरीका के ब्राह्मण-बौद्ध संघर्ष में बाबासाहेब ने आधुनिक कानूनी प्रावधानों को संविधान में समाहित कर दिया।
भारत के ‘मुट्ठी भर’ लोगों के वर्चस्व और सत्ता षडयंत्र को कानूनी रूप से पंगु बना देनेवाले बाबासाहेब इन ‘मुट्ठी भर’ लोगों को कैसे अच्छे लग सकते थे। बाबासाहेब के प्रति कांग्रेस के व्यवहार की आलोचना करनेवाले अपने दल के बाहर के लोगों के साथ कैसा राजनीतिक और सामान्य व्यवहार करते हैं! यह क्या किसी को बताने की जरूरत है?
दुनिया जानती है, बाबासाहेब कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। फिर भी बाबासाहेब के प्रति कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू सहित कांग्रेस के बड़े नेताओं का बाबासाहेब के प्रति कैसा सलूक और व्यवहार था, यह सब ऐतिहासिक दस्तावेज है।
ऐतिहासिक प्रसंग देखें तो राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ और उस समय के दक्षिण-पंथ के लोगों का बाबासाहेब के प्रति कैसा व्यवहार था, ‘सब कुछ’ साफ-साफ दिख सकता है। वैसे भी कांग्रेस ने जो किया वह आज की भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ के लोगों के लिए बाबासाहेब को अपमानित करने का कोई नैतिक आधार नहीं देता है।
बाबासाहेब भेद-भाव और ब्राह्मणवाद से ग्रस्त हिंदू समाज में तत्काल आमूलचूल नैतिक सुधार की जरूरत समझते थे। हिंदू समाज में तत्काल आमूलचूल नैतिक सुधार की जरूरत के प्रति राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का तब क्या रवैया था, आज ही क्या रवैया है? और नहीं कुछ तो बाबासाहेब की किताब ‘एनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ का इतिहास और मतलब ही समझ लें।
राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मिलान कर लें। महात्मा गांधी ने बाबासाहेब की किताब ‘एनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ पर टिप्पणी करते हुए यों ही नहीं बाबासाहेब को हिंदुत्व की राजनीति के लिए चुनौती कहा था। आज की ऐतिहासिक घड़ी में हिंदुत्व की राजनीति उस चुनौती के सामने है।
संसद परिसर में जो धक्का-मुक्की हुई वह दुर्भाग्यजनक है। यह दुर्भाग्य योजनाबद्ध तरीके से घटित हुआ प्रतीत होता है। लाइट कैमरा साउंड बिल्कुल दुरुस्त था, बस एक्शन ताल-मेल में नहीं था, रीटेक की गुंजाइश नहीं थी। बाकी सब स्क्रिप्ट के ‘हिसाब’ से चल रहा है।
ऐसा लग रहा है कि इस एपीसोड को बैकग्राउंड संगीत के बल पर दृष्टि के बिना ही पूरा कर लिया जायेगा। धक्का-मुक्की के मामले में इतनी कठोर कानूनी कार्रवाइयों का सामना भारत के लोकतांत्रिक परिसर को शायद ही पहले कभी करना पड़ा हो।
लोकतंत्र के शुभ-चिंतक इस घटना से उत्पन्न समस्या के सुलझाव के लिए भांति-भांति की युक्तियों का सुझाव दे रहे हैं। सुलझाव के सुझाव का आदर तब होता है जब किसी को सुलझाव की जरूरत हो! असल में शासकों का सामाजिक-समूह सुलझाव नहीं स्थाई समाधान चाहता है, ‘फाइनल सोल्युशन’! ‘फाइनल सोल्युशन’ क्या होता है! जो होता है वह इतिहास को मालूम है। बहुत कष्टकर और विनाशकारी होता है।
आखिरकार संविधान में ऐसा क्या है, जो ‘उन की नजर’ में भारतीय नहीं है! बहुत गौर करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ध्यान देने से ही ‘सब कुछ’ साफ-साफ समझ में आ जाता है। किसी भी किस्म की समानता, जिस की गारंटी संविधान के प्रावधानों से मिलती है ‘उनकी नजर’ में भारतीय नहीं है।
फटा सुथन्ना पहने जिसका गुन हरचरना गाता है भारत भाग्य विधाताओं को उस हरचरना से अपनी समानता का कोई भी सिद्धांत किसी भी रूप में पसंद नहीं है।
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जिस संविधान के शिल्पकार हैं उसका पहला और मौलिक सिद्धांत है फटा सुथन्ना पहने और सूट-बूट धारण किये महामना में कोई अंतर नहीं है, कम-से-कम वोट के मामले में तो अनिवार्य रूप से! ईवीएम (Electronic Voting Machines) का मतलब तो अभी खुलना बाकी है।
आखिरकार, ईवीएम (EVM) का गैर-जरूरी कसरत कब तक साथ दे सकता है! कुछ भी कहना मुश्किल है। बाबासाहेब का संविधान वैज्ञानिक मिजाज का आग्रह और अपील रखता है जो ‘उनकी नजर’ में आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के रास्ता का सबसे बड़ा बाधक है।
बाबासाहेब का संविधान अधिकार की बात करता है जबकि उन्हें ‘सब कुछ’ का प्रार्थना और कृपा से होना पसंद है। है, इस संविधान में और भी ‘बहुत कुछ’ है जो ‘उनकी नजर’ में उनके अनुकूल नहीं है।
उन्हें किसी भी प्रकार का अंकुश पसंद नहीं है। संविधान नये भारत भाग्य विधाताओं के लिए हर कदम पर अंकुश का काम करता है और हर प्रकार की निरंकुशता का अवरोधक है। आखिरकार निरंकुशता अपने हर विशेषण को निरर्थक बना देती है। लोकतांत्रिक निरंकुशता में न लोकतंत्र का कोई सार बचता है और सांस्कृतिक निरंकुशता में संस्कृति का कोई अर्थ बचता है।
रूपक में कहना हो तो निरंकुशता उसी तरह से अपने सारे विशेषणों का अर्थ अपने में वैसे ही सोख लेती है, जैसे अंधकार में सारे रंग निरर्थक हो जाते हैं। ‘चुनावी तानाशाही’ हो या लोकतांत्रिक निरंकुशता लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार के निषेध से ही जन्म लेती है और उसी से फलती-फूलती है।
कभी-कभी निरंकुशता भी उदारतापूर्वक बहुत कुछ देती है, लेकिन निरंकुशता के ‘बहुत कुछ’ में अधिकार शामिल नहीं होता है। निरंकुशता के उदारतापूर्वक देने में अधिकार नहीं शामिल होता है, कृपा शामिल होती है। ध्यान रहे, निरंकुशता की कृपा भी अंततः मनुष्य को कष्ट ही पहुंचाती है।
खुद के अंध-विश्वास मुक्त होने का प्रमाण पेश करने के लिए घंटों अपने काफिले को बिल्ली के रास्ता काटने के इंतजार में रोके रखने के खेल के पीछे की राजनीति को समझना बहुत मुश्किल तो नहीं है!
तो इस बार संघर्ष कुछ भिन्न प्रकार का है। निर्णायक दौर का यह संघर्ष किसी की समझ में आ रहा है, किसी की समझ में नहीं आ रहा है। देखना होगा कि आखिर होता क्या है।
(प्रफुल्ल कोलख्यान स्वतंत्र लेखक और टिप्पणीकार हैं)