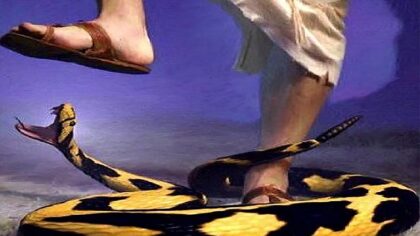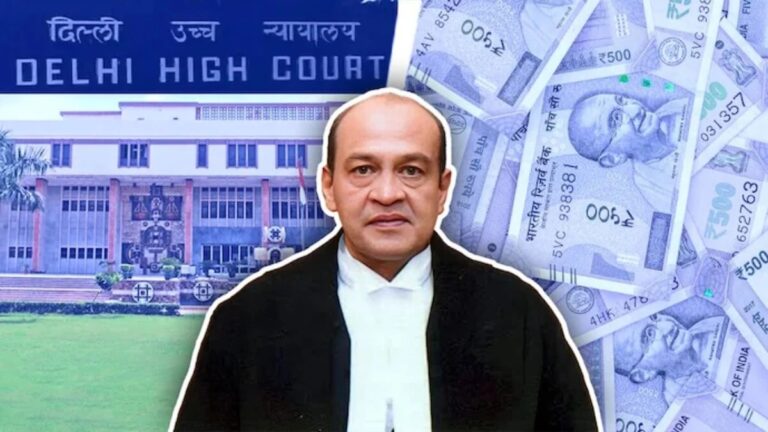आजकल डॉ. भीमराव अंबेडकर के कुछ अधूरे और संदर्भ से काटकर पेश किए गए कथनों के आधार पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। दक्षिणपंथी तबका उनके कुछ वाक्यों को हथियार बनाकर मुस्लिम समुदाय की देशभक्ति पर सवाल उठा रहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस पूरे संदर्भ को स्पष्ट किया जाए।
जब हम किसी विचारक के विचारों को समझने का प्रयास करते हैं, तो हमारे लिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक होता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही महान क्यों न हो, हर युग और हर मसले में सही हो, यह मान लेना न तो बौद्धिक ईमानदारी है, न ही तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है।
डॉ. भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का निर्माता और सामाजिक न्याय का योद्धा माना जाता है, उनके विचारों को भी इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अंबेडकर एक गंभीर चिंतक थे, जिन्होंने भारत के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक मसलों पर गहराई से विचार किया। उनकी अनेक बातें आज भी प्रासंगिक हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि उनके प्रत्येक कथन को हर दौर में अक्षरशः सही माना जाए।
यह लेख अंबेडकर की प्रसिद्ध पुस्तक Pakistan or The Partition of India में मुस्लिम समुदाय और इस्लाम की अवधारणाओं पर की गई उनकी कुछ टिप्पणियों को केंद्र में रखकर उनके मूल आशय, ऐतिहासिक संदर्भ, और आज के दौर में उनके दुरुपयोग पर प्रकाश डालता है।
अंबेडकर की यह पुस्तक 1940 के दशक में लिखी गई थी, जब भारत स्वतंत्रता संग्राम के निर्णायक मोड़ पर था और हिंदू-मुस्लिम संबंध तनावपूर्ण थे। इस पुस्तक में उन्होंने राष्ट्रीय एकता को लेकर अपनी चिंताओं का उल्लेख किया और इस सिलसिले में इस्लाम की ‘उम्माह’ की अवधारणा पर चर्चा की। उनका तर्क था कि ‘उम्माह’-जो विश्व भर के मुसलमानों को एक धार्मिक बिरादरी के रूप में जोड़ने की अवधारणा है-कभी-कभी राष्ट्रीय निष्ठा से ऊपर हो सकती है। उनके अनुसार, यह बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश में एकीकृत राष्ट्रभावना के लिए चुनौती बन सकती है।
यह टिप्पणी उस दौर की वास्तविकताओं से उपजी थी, जब मुस्लिम लीग ने ‘दो राष्ट्र सिद्धांत’ को सामने रखा और पाकिस्तान की मांग को गति दी। अंबेडकर की यह चिंता इस्लाम पर कोई व्यक्तिगत हमला नहीं थी, बल्कि उस समय के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को समझने की एक कोशिश थी।
आज जब हम उनकी टिप्पणी को पढ़ते हैं, तो उसका आकलन वर्तमान राजनीतिक माहौल में नहीं, बल्कि उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करना चाहिए। 1940 के दशक में सांप्रदायिक तनाव, दंगे, और राजनीतिक ध्रुवीकरण अपने चरम पर थे। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा-दोनों की जिद और सांप्रदायिकता-ने हालात को और जटिल बना दिया था। अंबेडकर न तो मुस्लिम अलगाववाद के समर्थक थे और न ही हिंदू राष्ट्रवाद के। उनका सपना एक ऐसा भारत था, जिसमें सभी बराबरी के साथ जी सकें। इसलिए उनकी बातें उस समय के आवश्यक विमर्श का हिस्सा थीं, न कि किसी धार्मिक समुदाय के खिलाफ पूर्वाग्रह।
अब यह देखना आवश्यक है कि ‘उम्माह’ की अवधारणा, जिसे अंबेडकर ने एक चुनौती के रूप में देखा, क्या वास्तव में राष्ट्रीय एकता के लिए बाधक रही? ‘उम्माह’ इस्लाम की एक नैतिक और धार्मिक अवधारणा है, जो कहती है कि विश्व भर के मुसलमान एक साझा बिरादरी हैं। इस विचार ने पैगंबर मुहम्मद के युग और प्रारंभिक खलीफा काल में एक मजबूत सामाजिक-सांस्कृतिक इकाई का रूप लिया था। परंतु जैसे-जैसे इस्लामी शासन का विस्तार हुआ, भूगोल, संस्कृति और राजनीति ने मुसलमानों के बीच विविधता और मतभेद उत्पन्न किए। फिर खलीफा व्यवस्था का पतन हुआ, और उम्माह का विचार एक सैद्धांतिक आदर्श बनकर रह गया।
बीसवीं सदी में जब खिलाफत आंदोलन चला, तो यह उम्माह के पुनर्जागरण का प्रयास था। भारत में इस आंदोलन ने मुसलमानों को एकजुट किया और हिंदू-मुस्लिम एकता को भी मजबूत किया, लेकिन यह लंबे समय तक टिक न सका। मुस्लिम बहुल देशों के बीच भी राजनीतिक मतभेद और क्षेत्रीय स्वार्थ इस एकता के मार्ग में बाधक बने।
भारत-पाकिस्तान का बँटवारा, ईरान-इराक युद्ध, सऊदी अरब और ईरान के बीच तनातनी जैसे उदाहरण इस बात को सिद्ध करते हैं कि राष्ट्रीय हित धार्मिक भाईचारे से ऊपर होते हैं। इसलिए अंबेडकर की वह टिप्पणी उनके समय और भारत के संदर्भ में उनकी चिंता थी, लेकिन उसे आज के दौर में एक शाश्वत सत्य मान लेना देश, काल और परिस्थितियों के विपरीत होगा।
दुर्भाग्यवश, आज यही बात कुछ हिंदूवादी समूहों द्वारा मुस्लिम समुदाय पर अविश्वास जताने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। यह न केवल अंबेडकर की बातों की गलत व्याख्या है, बल्कि इतिहास को तोड़-मरोड़ने की कोशिश भी है। हिंदूवादी राजनीति की जड़ें उसी दौर में पड़ी थीं, जब हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों ने ‘हिंदू राष्ट्र’ की बात शुरू की।
यह ‘राष्ट्रवाद’ वास्तव में एक सांप्रदायिक और जातिवादी सोच थी, जो सवर्ण हिंदुओं के वर्चस्व को कायम रखना चाहती थी। ये संगठन न केवल मुसलमानों के, बल्कि दलितों और आदिवासियों के अधिकारों के भी खिलाफ थे। 1930-40 के दशकों में हिंदू महासभा ने खुलकर जाति व्यवस्था की वकालत की, जो अंबेडकर के विचारों के एकदम विपरीत थी।
इसके विपरीत, मुसलमानों की एक बड़ी संख्या ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, और हकीम अजमल खान जैसे नेताओं ने न केवल कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया, बल्कि एक साझा भारत की कल्पना को आगे बढ़ाया। खिलाफत आंदोलन ने हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की।
असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में लाखों मुसलमानों ने भाग लिया। यह सही है कि मुस्लिम लीग ने अलगाव की राह पकड़ी, लेकिन वह पूरे मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। इसलिए आज जब अंबेडकर की टिप्पणियों का उपयोग मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाने के लिए किया जाता है, तो वह एकतरफा और दुर्भावनापूर्ण होता है।
यह भी स्मरण रखना चाहिए कि अंबेडकर हिंदू धर्म की जातिवादी संरचना के घोर विरोधी थे। उन्होंने अपनी पुस्तक Annihilation of Caste में स्पष्ट कहा था कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज की सबसे बड़ी बीमारी है। 1956 में बौद्ध धर्म अपनाकर उन्होंने परंपरागत हिंदू सामाजिक व्यवस्था को खारिज कर दिया। ऐसे विचारक के नाम पर आज उन्हीं ताकतों द्वारा सांप्रदायिक नफरत फैलाना एक गहरी साजिश है, जिनके खिलाफ अंबेडकर ने जीवनभर संघर्ष किया।
अंबेडकर को हमें एक गतिशील विचारक के रूप में देखना चाहिए, जिनके विचार समय के साथ विकसित हुए। 1940 के दशक में वे देश की एकता और विभाजन की चिंता में डूबे थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद उनका ध्यान दलित अधिकारों, सामाजिक परिवर्तन और एक समावेशी संविधान के निर्माण पर केंद्रित हुआ। उनके नेतृत्व में बना संविधान सभी को समानता का अधिकार देता है-चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो।
अंततः, अंबेडकर की बातों को संदर्भ से काटकर प्रस्तुत करना न केवल इतिहास के साथ अन्याय है, बल्कि सामाजिक सौहार्द के लिए भी हानिकारक है। हमें अंबेडकर को उनके समग्र विचार-संसार में समझना होगा-एक ऐसे चिंतक के रूप में, जो किसी एक वर्ग के नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के पक्ष में थे, जो समानता, सम्मान और न्याय की चाह रखता है।
(डॉ. सलमान अरशद स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)