दोस्तों, मैं तक़रीबन दो साल से बीमारी के मुख़्तलिफ़ मदारिज (पड़ाव) तय कर रहा हूं। अब पिछली सी शिद्दत मेरी बीमारी में बाक़ी नहीं है। फिर भी मेरे लिए लिखना कुछ ख़ासा दुश्वार मरहला है।
क़ज़ा ने था मुझे चाहा, ख़राब-ए-वादा-ए-उल्फ़त
फ़कत ख़राब लिखा, बस न चल सका क़लम आगे।
मैं अपनी तहरीर की कोशिश के बारे में क्या लिखूं? ये कोशिश ना-तमाम (अपूर्ण) ‘दाना-ओ-दाम’ से शुरू होती है। ‘गरहन’, ‘कोख़जली’, ‘अपने दुःख मुझे दे दो’, ‘हाथ हमारे क़लम हुए’ अफ़सानों के मजमूए हैं। एक छोटा सा नॉवेल ‘एक चादर मैली सी’ है। दूसरा क़द्र-ए-तवील (बहुत बड़ा) नॉवेल ‘नमक’ है, जो मेरी बीमारी की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका है। ड्रामों के मजमूए हैं- ‘सात खेल’ और ‘बे-जान चीजे़ं’।
मैं असल में कोई ज़ूद-गो अदीब (अधिक लिखने वाला लेखक) नहीं हूं। मैं क़लम उठाकर काग़ज़ को स्याह करना चाहूं भी, तो कभी क़लम रुक जाता है और कभी काग़ज़ की मासूमियत आड़े आ जाती है। ये आपका करम है कि आपने मुझे इनाम के क़ाबिल समझा। ये भी सच है कि ज़िंदगी का बेश्तर हिस्सा लिखने में सर्फ़ (खर्च) हुआ है। यानी लिखने के बारे में सोचने-समझने और फिर कभी-कभी लिखने में लिखना, मेरे लिए अज़ाब (यातना) नहीं रहा है।
शुरू-शुरू में ऐसा मालूम होता था कि हर तजुर्बे और ख़याल को काग़ज़ पर उतारूं। मगर आहिस्ता-आहिस्ता फ़न्नी शुऊर (कला से संबंधित अच्छे-बुरे की तमीज़) की गिरफ़्त मज़बूत होती गई। कभी-कभी ये गिरफ़्त इतनी सख़्त हो गई कि मैं महीनों कोई अफ़साना न लिख पाया। गाहे-गाहे (कभी-कभी) ऐसा भी हुआ है कि क़लम रोके नहीं रुकता था।
शुऊर और ला-शुऊर (अचेतावस्था) में कोई इतनी सीधी जंग नहीं होती है कि काग़ज़ के पैड्स पे ख़ून-खराबे की नौबत आए, मगर एक कशमकश तो चलती ही रहती है। वही ‘हेमलेट’ का तज्ज़ियाती (विश्लेषणात्मक) सवाल यानी ‘‘क्या लिखूं, क्या न लिखूं?’’
और फिर अफ़साना क्या है? ये सवाल मेरे अफ़सानों के साथ-साथ बदलता रहा है। यूं कि कभी एक बच्चे को (की) कहानी सुनाने का ख़याल आया, तो ‘भोला’ लिखी। कभी एक और बच्चे के ज़रिए आज के दौर की सीता की विपदा लिखना हुई तो ‘बब्बल’ लिखी। बच्चे और कहानी का बड़ा रब्त (संबंध) था, है और रहेगा। इसलिए कि कहानी सुनने की ख़्वाहिश ही अफ़साना निगार को कहानी लिखने पर मजबूर करती है।
टेक्निक बदलती रहती है। हां, कभी-कभी ऐसा भी दिल चाहा है कि अपने चारों तरफ़ फैले हुए हंगामा-ज़ार (कोलाहल) पर भी नज़र डाली जाए, तो मैंने ‘जनाज़ा कहां है’ लिखी। और जब दहशत-ओ-ज़ुर्म की फ़िज़ा को मुसल्लत (आधिपत्य) होते हुए देखा, तो ‘बोलो’ लिखी। ग़रज़ कि कम लिखते हुए भी अस्सी कहानियां, पैंतालिस साल में लिखी हैं। और अब भी लिखने की ख़्वाहिश है। अपने हाथों में क़लम उठाकर काग़ज़ पर नज़रें जमाकर देखता हूं और सोचता हैं कि किसी ने कहा था,
कभी पहले से काग़ज़ पर स्याह लफ़्ज़ों में कुछ लिखना
कभी नज़रों से लिखकर, यूं ही काग़ज़ को जला देना।
यानी क़लम और काग़ज़ का रिश्ता क़ायम है। और मैं ज़रूर लिखूंगा। ना जाने कब गुस्ताव फ्लॉबेर ने मोपासां से कहा था कि
“देखो, वो सामने पेड़ है। उसके बारे में कहानी लिख लाओ।”
और जब मोपासां कहानी लिखकर ले गया, तो फ्लॉबेर ने कहा,
“तुम तो न जाने क्या लिख लाए ? शाखें, पत्तियां, फल वगैरह भी हैं, पर कहानी पेड़ के बारे में कहनी थी। पेड़ के जिस्म की एनाटॉमी (रचना विज्ञान) के बारे में नहीं!”
और न जाने कितनी बार मोपासां को पेड़ पर नज़रें जमा कर उसके आर-पार देखना पड़ा। और फिर वो पेड़ की कहानी लिख पाया। पता नहीं मैं ऐसे तजुर्बात-ओ-ख़यालात (अनुभव और विचारों) से पेड़ की पूरी तर्जुमानी कर रहा हूं या नहीं। मगर मेरी कोशिश यही रही है कि पूरे पेड़ की कहानी न सही किसी एक शाख़, किसी फल या ज़र्द पत्ते की कहानी लिखूं।
कभी-कभी पेड़ के बारे में कम, उसकी जड़ों के बारे में ज़्यादा लिख गया हूं कि असली पेड़ तो ज़मीन के अंदर ही है। पता नहीं क्या लिखना चाहता था, क्या लिख गया हूं? मगर जो लिखा है, वो पूरी ईमानदारी और जतन से लिखा है। शायद इसीलिए अब भी लिखने की ख़्वाहिश बाक़ी है।
(राजिंदर सिंह बेदी का लेख, प्रकाशन का साल- 1980, उर्दू से हिंदी लिप्यंतरण- ज़ाहिद ख़ान और इशरत ग्वालियरी)


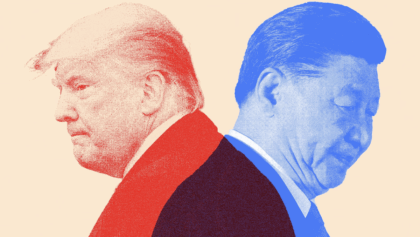











ख़ूबसूरत लिप्यान्तरण। बधाई ।