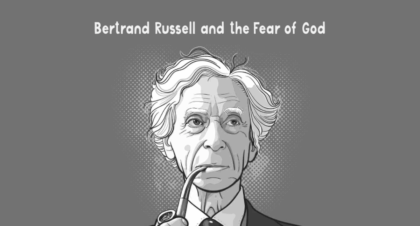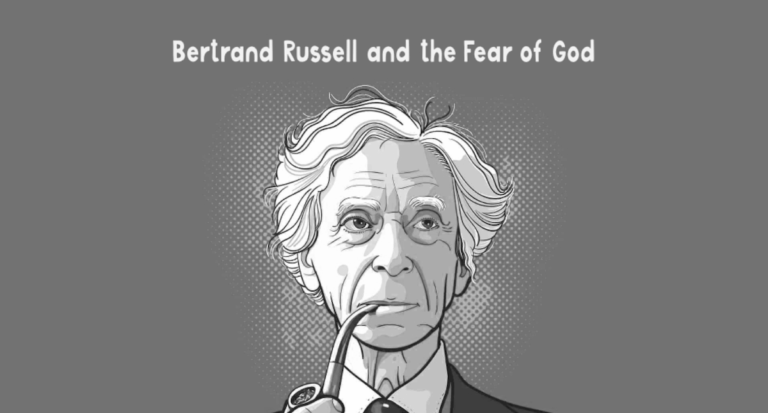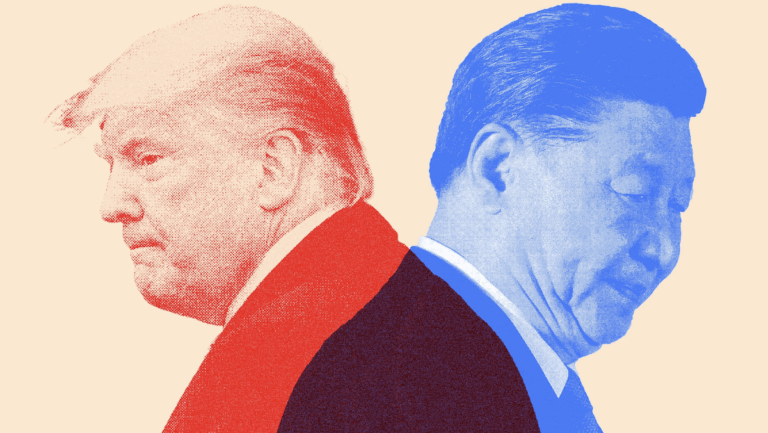कौन जानता था कि बचपन में खेला गया छुक छुक गाड़ी का खेल एक दिन सचमुच उनकी रेल बनकर उन्हें घर पहुंचाने का सबब बन जाएगा। यदि सुरक्षित घर पहुंचा ही देता तो भी कम से कम खेल खेलने का लुत्फ आया समझ लेते, मगर रास्ते में यूं डब्बों का बिखर जाना एक उम्मीद का बिखर जाना है, एक संसार का उजड़ जाना है । इस तरह तो कभी रेल भी न बिखरी होगी जैसे उनकी ज़िंदगी बिखर गई। वो जिन्हें जीते जी रेल न मिल सकी उनकी लाशों को स्पेशल रेल से घर पहुंचाया गया। रेल का ये खेल सचमुच किसी को रास न आया।
ज़िंदगी क्या किसी मुफ़लिस की क़बा है जिसमें
हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं
(फैज़ )
फैज़ साहब का यह शेर आज घर लौटते लाखों मजदूरों की मजबूरियों को इस शिद्दत से बयां करता है। मानो फटती बिवाइयों से अभी अभी फूट पड़ा हो। कभी बेबसी कभी रुदन के बीच अपने वतन, अपने घर लौटने की बेकरारी आहिस्ता-आहिस्ता आक्रोश में तब्दील होती जा रही है।
सुनहरे और उज्ज्वल भविष्य का ख्वाब लिए जो महानगरों की ओर भागे चले आए थे उनके ख्वाबों के ऐसे अंजाम का अंदाजा तो किसी को न था। उम्मीद और आकांक्षाओं की गगन छूती अट्टालिकाएं यूं ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगी किसी ने सोचा न था। लोगों के मकान बनाते जो अपनी गृहस्थी संवारने में लगे रहे वो अचानक सड़कों पर बेघरबार होकर भटकने को मजबूर हो गए हैं। इमरान-उल-हक़ चौहान का एक शेर है-
ख़्वाब, उम्मीद, तमन्नाएँ, तअल्लुक़, रिश्ते
जान ले लेते हैं आख़िर ये सहारे सारे
नवउदारवाद और क्रोनी कैपिटलिज्म की मृग मरीचिका में इन महानगरों की ओर खिंचा आया यह आदम सैलाब आज फिर वहीं उन्हीं राहों पर आकर खड़ा हो गया है जहां से इसने अपनी यात्रा शुरू की थी। घर से महानगर का सफर जब शुरु हुआ तब भी ऐसा नहीं कि इनकी राहों में फूल ही फूल बिखरे हुए थे। राह तब भी कांटों भरी ही थी मगर तब सफर की इब्तदा थी, मन में जीवन संवारने का उत्साह था, ज़िंदगी को बेहतर बनाने का ऐसा जुनून कि ये अपने ख्वाबों की ताबीर संवारने सजाने तमाम तकलीफों को हंसते हंसते सहे जाते रहे ।
अब फर्क इतना है कि सफ़र वापसी का है , घर वापसी का। उस घर की ओर वापसी का जिसे ये अपनी महत्वाकांक्षाओं के अथाह समुंदर में कहीं डुबा आया था । आज जब यह समुन्दर इस भोथरे विकास की कीमत मांग रहा है तो ये घबराकर भाग रहे हैं । आखिर हर विकास की एक कीमत तो होती ही है । मगर यह कीमत चुकाता वही वर्ग है जो आज बदहवास सा अपने घर की ओर , अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है । भूखे बदहवास लोगों की बस एक ज़िद है, बस एक धुन, एक जिद्दी धुन सी सवार है और वो है घर वापसी की धुन। इस धुन के आगे सरकार के कारे राग दब गए हैं ।
जो लोग मौत को ज़ालिम क़रार देते हैं
ख़ुदा मिलाए उन्हें ज़िंदगी के मारों से
दूसरी ओर इनकी घर वापसी से पूंजीपतियों के कान खड़े हो गए हैं । एक भय, खौ़फ सा पसर गया है पूरे पूंजीपति वर्ग में और वो है उनके अपने धंधे के अस्तित्व का। उन्होंने मजदूर के चेहरे का आक्रोश भांप लिया है, सरकार से और आम जनता से पहले ही। वे खौ़फ़ज़दा हैं कि घर वापसी को बेचैन ये मजदूर हालात संभालने के बाद फिर वापस उनकी चाकरी में लौटेगा कि नहीं ? आनन-फानन में ये पूंजीपति वर्ग सरकार पर दबाव डालकर इनकी घर वापसी के सारे रास्ते बंद कर देना चाहता है, लोकतंत्र के तमाम श्रम कानूनों को ध्वस्त कर तमाम हकों को खत्म कर शोषण का एक नया दौर शुरू कर देना चाहता है। नई सदी में अधिकार विहीन, बेबस लाचार कामगारों की नई जमात, बंधुआ मजदूरी की नई अत्याधुनिक प्रथा शुरु करने को बेताब हो उठा है ये पूंजीपति वर्ग।
और आश्चर्य तो ये है कि इस नई प्रथा के बंधुवाओं में सिर्फ अनपढ़ गंवार देहाती मजदूर ही नहीं, पढ़े लिखे ऊंची-ऊंची डिग्रीधारी श्वेत धवल कपड़ों में सजे धजे कॉर्पोरेट के गुलाम भी बेआवाज़ शामिल हैं मगर वो खामोेश हैं, उन्हें गुलामी की आदत सी पड़ चुकी है । सुविधाओं के गुलाम हो चुके ये सफेदपोश आखिर कहां जायेंगे, वापस आ ही जायेंगे। अब मगर पेट से ज्यादा दिल पर गहरी चोट खाए इन मजदूरों को रोक पाना बहुत कठिन हो गया है । यहां तक कि सरकारें भी अब इनकी ज़िद से घबरा उठी हैं।
ये जान लीजिए मगर इस धरती पर वे ही बचेंगे जो बेधड़क, चिलचिलाती धूप में तपती धरती पर निकल पड़ते हैं नंगे पांव। और इस पृथ्वी को बचाएंगे भी ये ही। फिर चाहे वो घर से पलायन का वक़्त हो या ही घर वापसी का समय। कंधे पर अपनी अगली पीढ़ी को ढोते सर पर पूरी गृहस्थी का बोझ लिए निकल पड़ने की हिम्मत इन्हीं में होती है। साए की तरह बराबरी से चलती पत्नी का साथ भी होता है।
हर बार, बार-बार बस एक जुनून होता है। ये ही रचते हैं नया युग, नया ज़माना। इन्हीं के इरादों में, जुनून में। एयर कंडीशंड दड़बों से निकलते हमारी छद्म संवेदनाओं के ट्वीट, सोशल मीडिया पर सामूहिक विलाप के तमाम ढोंग और मोबाइल के स्क्रीन पर वर्जिश करती हमारी अंगुलियां से जाहिर करती हमारी चिंताओं से कहीं ज्यादा इन्हीं फौलाद ढालते हाथों के बीच कहीं चुपचाप बूझते कंधे पर सवार उस अगली पीढ़ी के हाथों में बचा रहेगा जीवन।
चिंता न करें ये जल्द ही आयेंगे लौटकर वापस क्योंकि हमने अपने स्वार्थों के चलते उन्हें उनके घरों तक वो सुविधाएं वो जरूरतें मुहैया ही नहीं कराई हैं । तमाम संसाधनों पर जब तक हम कब्जा जमाए रहेंगे ये घर जाकर भी बार बार लौटेंगे, और हम अपनी क्रूर मुस्कुराहटों के साथ उनका स्वागत करते रहेंगे । जरा दम ले लें इस बार थकान तन की नहीं है मन की है , ज़रा इस थकान से राहत पा लेने दीजिए वे आयेंगे ज़रूर आयेंगे लौटकर। वंचितों की ये आवाजाही बदस्तूर जारी रहेगी जब तक वे सब कुछ जीतकर अपने क़ब्ज़े में नहीं कर लेते। अभी तो वे उधेड़बुन में हैं, असमंजस में हैं…..
अब उस के शहर में ठहरें कि कूच कर जाएँ
‘फ़राज़’ आओ सितारे सफ़र के देखते हैं
( अहमद फराज़)
(जीवेश चौबे पत्रकार और लेखक हैं।)