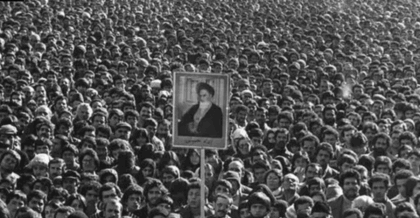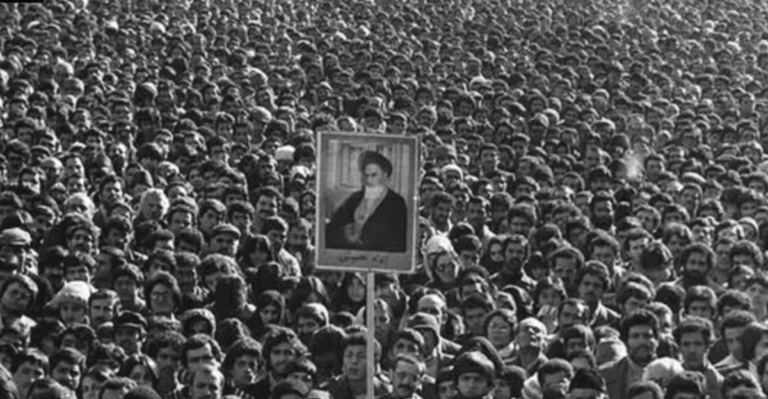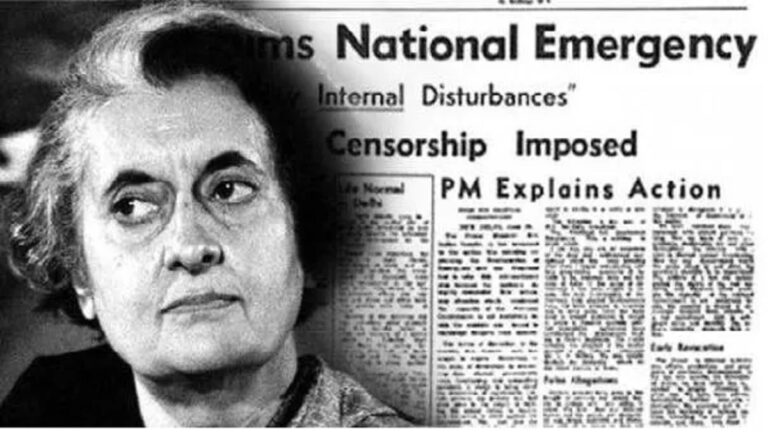जोशीमठ में भू-धसाव की खबर ने सबका ध्यान खींचा। इससे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के अलावा, दूसरे हिमालयी राज्यों में भी भय और चिंता पैदा हो गई कि कहीं उनका भी ऐसा ही हश्र न हो जाए। अधिकांश हिमालयी इलाके भी जोशीमठ क्षेत्र की तरह एक ऐसे ‘विकास’ के शिकार हैं, जिसने पहाड़ को खुर्द बुर्द-खोखला और तबाह कर रखा है। यही वजह है की इन इलाकों में आपदाओं की आशंका हमेशा बनी रहती है।
जोशीमठ का धसना अभी रुका नहीं है। घरों और खेतों में नई दरारें आ रही हैं और पुरानी दरारें चौड़ी होती जा रही हैं। यहां के लोगों को डर है कि भारी बारिश में ज़मीन के बड़े-बड़े हिस्से नीचे खिसक सकते है। पुनर्वास की मांग को लेकर उनका धरना जनवरी से अप्रैल की शुरुआत तक जारी रहा। तब उन्हें त्वरित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए धरना बंद करने के लिए कहा गया। इसकी एक बड़ी वजह सरकार की तरफ से बद्रीनाथ यात्रा को बिना किसी झंझट के शुरू करना था। स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू करने की तैयारी में हैं क्योंकि उचित पुनर्वास योजना के अभाव में उनके पास अपने क्षतिग्रस्त घरों में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह स्थिति ऐसे प्रश्न उठाती है जो अधिकांश हिमालयी क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक हैं।
पहला सवाल ये है कि ऐसी आपदाओं के लिए कोई जवाबदेही तय क्यूं नहीं होती? हिमालयी क्षेत्र के पारिस्थितिक और भूवैज्ञानिक रूप से संवेदनशील और भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक सक्रिय होने के बावजूद हिमालयी राज्यों में जलविद्युत परियोजनाओं को बड़ी संख्या में बनाया जा रहा है। अध्ययनों से पता चला है कि इन परियोजनाओं के हरित ऊर्जा के दावे सही नहीं हैं। ये “जोखिम भरे ढांचे” हैं जो सामाजिक और पारिस्थितिक रूप से अन्यायपूर्ण साबित हुए हैं।
विभिन्न शोध यह भी बताते हैं कि उत्तराखंड में 2013 और 2021 की बाढ़ जैसी आपदाओं को पैदा करने और बढ़ाने में इन परियोजनाओं की भूमिका है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित रवि चोपड़ा विशेषज्ञ समिति ने भी ये पाया था। समिति ने तर्क दिया था कि ग्लेशियरों के घटने से बनी जोशीमठ जैसी जहां भी कच्ची जमीन हैं वहां ऐसी परियोजनाओं का निर्माण आपदा को निमंत्रण देने जैसा है।
जोशीमठ में तपोवन विष्णुगाड परियोजना 2005 में अपने शुरू होने के बाद से ही पूरे क्षेत्र में सामाजिक-पारिस्थितिक समस्याओं का कारण बनी है। 2021 की बाढ़ में सैकड़ों श्रमिक इसकी टनल में जिंदा दफन हो गए। यहां आपदा से आगाह करने के लिए कोई अलार्म सिस्टम तक नहीं लगाया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह परियोजना जोशीमठ शहर के साथ-साथ आसपास के कई गांवों में भी नुकसान के लिए जिम्मेदार है। वे करीब दो दशकों से इसका विरोध कर रहे हैं।
यह बात कि जोशीमठ पुरानी भूस्खलन के मलबे पर बना है। 1976 की एम सी मिश्रा समिति की रिपोर्ट ने यह सिफ़ारिश की थी कि यहां भारी मशीनरी का प्रयोग, ब्लास्टिंग, ड्रिलिंग और पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए। फिर भी इस परियोजना ने यहां सुरंगों का एक जाल बनाया, बोरिंग मशीन और विस्फोटकों का उपयोग करके इस नाजुक भूगोल और इलाके की स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। यह परियोजना भूवैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। बार बार आने वाली आपदाओं के कारण इस परियोजना का काम भी खटाई में पड़ता रहा है। यही वजह है कि इसके कार्यान्वयन में एक दशक से भी ज्यादा की देरी हो चुकी है। ऐसी परियोजना से होने वाले विनाश का बोझ स्थानीय लोग क्यों और कब तक झेलते रहेंगे?
दूसरा सवाल, स्थानीय लोगों को इलाके की सुरक्षा के बारे में अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है, जबकि वे अपने क्षतिग्रस्त घरों में जाग कर रातें काटने को मजबूर हैं? सात महीने के बाद भी जोशीमठ में भूमि धसाव के कारणों, प्रभावों और भविष्य के खतरों के बारे में कोई व्यापक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। सरकार ने जनवरी में सभी विशेषज्ञ संस्थाओं को भूस्खलन के बारे में कुछ भी जानकारी देने पर रोक लगा दी थी। और अब तक आपदा का अध्ययन करने के लिए अपने द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट साझा नहीं की है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपदा की स्थिति से निपटने का यह तरीका कभी नहीं होता है।
तीसरा सवाल, यदि सरकार सभी जोखिमों के बावजूद ऐसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर आमादा है तो उसे प्रभावित लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित क्यों नहीं करना चाहिए? हिमालयी राज्यों में ऐसी परियोजनाओं को चलाते बरसों हो गए हैं। लेकिन सरकार ने इनके प्रभावों और प्रभावितों के पुनर्वास के प्रति जिम्मेदारियों को परिभाषित करने के लिए कोई स्पष्ट दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं। पर्वतीय जगहों पर ऐसी परियोजनाओं का प्रभाव तुरंत नहीं दिखता, बल्कि उनके प्रभाव दीर्घकालिक और व्यापक होते है। वे कुछ समय अंतराल के बाद भी प्रकट होते हैं और उन क्षेत्रों को भी प्रभावित करते हैं जो परियोजना से एकदम सटे हुए नहीं होते। इसलिए ऐसी परियोजनाओं के ‘प्रभावितों’ की पहचान और पुनर्वास के प्रति परियोजना की जिम्मेदारियों को सही से परिभाषित करना जरूरी है।
विकास परियोजनाओं द्वारा अनैच्छिक विस्थापन की स्थिति में एक उचित पुनर्वास नीति बनाने का उत्तराखंड सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है। पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, सरकार के प्रयास ‘एकमुश्त निपटान’ तक ही सीमित हैं। जोशीमठ में तो मुआवजे का भुगतान केवल घरों के लिए ही किया जा रहा है। यह राशि अपर्याप्त है और अधिकांश अभी भी इसका इंतजार कर रहे हैं। चूंकि लोग कहीं और जाकर बस पाने की स्थिति में नहीं हैं इसलिए अधिकांश लोग असुरक्षित घरों में रहने के लिए वापस आ गए हैं।
सरकार का ज़ोर आपदा के बाद भी यात्रा पर्यटन को सुचारू रूप से चलाने पर ही रहा, इसलिए आपदा को कम करके भी दिखाया जाता रहा। आपदा के बावजूद पर्यटकों की संख्या पर कोई सीमा नहीं रखी गई। इससे बड़ा सवाल उठता है: इस तरह अगर पहाड़ रहने के लिए अनुपयुक्त स्थानों में तब्दील कर दिये जाएंगे तो पहाड़ के निवासी आखिर कहाँ जाएंगे? ऐसे ‘विकास’ की उत्तराखंड के लोगों के लिए क्या प्रासंगिकता रह जाती हैं जिसने उनके घरों को रहने लायक नहीं छोड़ा है?
(श्रुति जैन के इंडियन एक्सप्रेस, 3 अगस्त 2023 में प्रकाशित लेख पर आधारित।)