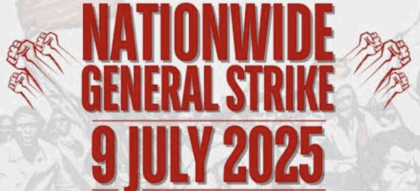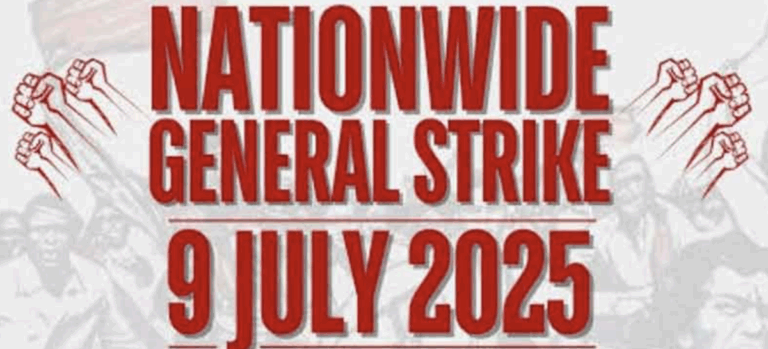नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन करने के चलते यूएपीए (ग़ैरक़ानूनी गतिविधि निरोधक क़ानून, 1967) के तहत गिरफ्तार प्रदर्शनकारी छात्र-छात्राओं नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तनहा को एक साल से ज्यादा समय तक जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति जे. भंभानी ने दिनांक 15 जून 2021 को अपने जमानत आदेश से न्यायिक व्याख्या के क्षेत्र में एक हलचल सी मचा दी है। इस सुविस्तृत, सुविचारित और सुव्यवस्थित ढंग से लिखित आदेश में न्यायाधीशद्वय ने पूर्व में पारित उच्चतम न्यायालय के अनेक फैसलों से उद्धरणों और नज़ीरों के जरिये अनेक ऐसी टिप्पणियां की हैं जो मानवाधिकारों, नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता संबंधी विधिक व्याख्याओं में लंबे समय तक प्रतिध्वनित होती रहेंगी।
अदालत का आदेश हमारे समय की बुनियादी चिंताओं से भरा हुआ है। वह आतंकवाद संबंधी क़ानूनों को राज्य द्वारा हथियार बनाने पर चिंता जाहिर करती है। आज, जबकि कार्यपालिका अपनी शक्तियों का अतिक्रमण करती जा रही है, नागरिक अधिकारों का दायरा निरंतर संकुचित होता जा रहा है, प्रतिरोध की हर आवाज का गला घोंट देने की प्रवृत्ति बन गयी है, किसी क़िस्म की आलोचना बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है, स्वतंत्र और निष्पक्ष अभिव्यक्ति की सभी खिड़कियों को एक-एक करके बंद किया जा रहा है, विरोध करने वालों पर आतंकवाद और राजद्रोह के कठोर क़ानून थोप दिये जा रहे हैं, किसी भी हालत में विरोध करने वालों को जमानत न मिले, इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया जा रहा है, जेलें विचाराधीन क़ैदियों से ठुंसी पड़ी हैं, ऐसे में इस आदेश के रूप में यह न्यायिक पहल सत्ता की अधिनायकवादी प्रवृत्तियों के लिए एक धक्के जैसी है और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले सभी लोगों के लिहाज से एक स्वागत योग्य क़दम है।
दोषसिद्धि से पहले हर अभियुक्त को निर्दोष माना जाए
हमारे देश की जेलों में यातनाएं भुगत रहे क़ैदियों में से 70 प्रतिशत विचाराधीन क़ैदी हैं। इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें सत्ता और रसूख वाले ताक़तवर लोगों ने क़ानून लागू करने के लिए जिम्मेदार एजेंसियों के साथ मिल कर फंसाया है। बड़ी संख्या में क़ैदियों के पास न क़ानूनी दांवपेंच की समझ है, न उचित क़ानूनी सलाह और मदद हासिल कर पाने की हैसियत है। न्यायापालिका के लंबित मामलों के बोझ तले दबे इन क़ैदियों की जिंदगी एक अंधी सुरंग बन चुकी है। वर्तमान आदेश के जरिये न्यायाधीशों द्वारा जेल की जगह जमानत को नियम बनाने का आह्वान ऐसे क़ैदियों के लिए सुरंग के भीतर रोशनी की एक उम्मीद की तरह से है। आदेश में कहा गया है कि, “जमानत का उद्देश्य न तो दंडात्मक है, न ही अवरोधात्मक, बल्कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियुक्त की केवल उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए है। दंड केवल दोष सिद्ध हो जाने के बाद ही शुरू होता है, इसलिए समुचित सुनवाई और अपराधी घोषित होने से पहले हर व्यक्ति को निर्दोष माना जाना चाहिए।” हालांकि इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ऐसे विचाराधीन क़ैदियों से देश की जेलें भरी हुई हैं। कोविड की इतनी भीषण त्रासदी के बावजूद तमाम बुजुर्ग मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों को जमानत नहीं मिल सकी है, क्योंकि सरकार हर हाल में जमानत रोकने पर आमादा है तथा अदालतें पर्याप्त संवेदनशील नहीं हैं।
जमानत एक नियम और जेल एक अपवाद माना जाए
जमानत के उद्देश्य को व्याख्यायित करते हुए अदालत कहती है कि, “यह जाहिर सी बात है कि मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक अभियुक्त को जेल में रखने से उसे भारी मुसीबतें झेलनी पड़ सकती हैं। किसी को उसके पिछले आचरण से असम्मति के लिए, अथवा दोषसिद्धि से पूर्व ही उसे जेल का स्वाद चखाने या सबक सिखाने के लिए जेल में रखना बिल्कुल गलत है। किसी को जेल में रखने की जरूरत का आधार केवल मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित करना ही होना चाहिए।” अदालत स्पष्ट करती है कि केवल तीन शर्तों को सुनिश्चित करते हुए जमानत दे देनी चाहिए। “लगाये गये आरोपों से संतुष्ट होने के अलावा अदालत को तार्किक ढंग से इस बात का आकलन कर लेना चाहिए कि अभियुक्त फरार न हो जाए, साक्ष्यों को नुकसान न पहुंचाये और गवाहों को न डराये-धमकाये।” अभियोजन की तरफ से आरोप-पत्र में उद्धृत 740 गवाहों की भारी-भरकम सूची की ओर इंगित करते हुए अदालत कहती है कि इन गवाहियों के पूरा होने में तो वर्षों लग जाएंगे, वह भी तब, जब सुनवाई शुरू होगी। ऐसे में इन अभियुक्तों के त्वरित सुनवाई के अधिकार का क्या होगा?
आरोप-पत्र तथ्यों पर आधारित हो, अटकलबाजियों पर नहीं
अदालत ने कहा है कि आरोप-पत्र जितना महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, उसे तैयार करने में अक्सर उतनी मेहनत नहीं की जाती है। उसे एक सुनिश्चित प्रारूप में तैयार किया जाना चाहिए और उसे तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। स्पष्ट तथ्यों के आधार पर जमानत का निर्णय लेना अदालत के लिए आसान होता है। वर्तमान आरोप-पत्र की तीखी आलोचना करते हुए अदालत कहती है कि, “हम अपने आप को आपके इस (जमानत न देने के) निवेदन से अप्रभावित और असहमत पाते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि यह आरोप किसी विशिष्ट ठोस तथ्य पर आधारित नहीं है और हमारे विचार से प्रस्तुत आरोप-पत्र में केवल चेतावनी देने वाली और अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दावली हमें आपसे सहमत नहीं कर पाएगी।”
आतंकवाद तथा क़ानून और व्यवस्था के सामान्य मामलों को गड्डमड्ड न किया जाए
आसिफ इकबाल तनहा के संबंध में अदालत के आदेश में आतंकवाद की व्याख्या काफी विस्तार से की गयी है। इसके लिए एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्स्टेंसेज ऐक्ट 1985), टाडा (टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव ऐक्टिविटीज प्रिवेंशन ऐक्ट 1987), मकोका (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऐक्ट 1999), पोटा (प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऐक्ट 2002) और यूएपीए में वर्णित आतंकवाद की व्याख्याओं की तुलना करते हुए अदालत ने निष्कर्ष निकाला है कि, “यूएपीए को लागू करने और 2004 तथा 2008 में उसमें संशोधन करने के पीछे संसद की मंशा और मुराद यह थी कि इसके दायरे में केवल उन आतंकवादी गतिविधियों से निपटा जा सके जिनसे ‘भारत की सुरक्षा’ पर गंभीर प्रभाव पड़ने का अंदेशा हो, न इससे कम, न इससे ज्यादा। अगर ऐसा नहीं होता तो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 में संसद द्वारा यूएपीए को शामिल ही नहीं किया जा पाता, क्योंकि इस सूची में संसद की विधायी क्षमता के दायरे में केवल दो प्रविष्टियां हैं, प्रविष्टि-1 और प्रविष्टि-2, जो दोनों ही भारत की सुरक्षा और भारत की सुरक्षा संबंधी अपराधों के बारे में हैं। कभी भी ऐसी मंशा नहीं थी कि यूएपीए के दायरे में रोजमर्रा के सामान्य अपराध लाये जाएंगे, चाहे वे कितने भी संगीन और जघन्य क्यों न हों।”
अदालत का मानना है कि, “हालांकि यूएपीए के अनुच्छेद 15 में ‘आतंकवादी कार्रवाई’ की परिभाषा विस्तृत और कुछ हद तक अस्पष्ट है, फिर भी इस पदबंध से आतंकवाद के अनिवार्य चरित्र का ही आशय होना चाहिए और परंपरागत अपराधों को ‘आतंकवादी कार्रवाई’ के दायरे में लाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।” अदालत ‘आतंकवादी कार्रवाई’ को परिभाषित करते हुए इसमें कुछ अवयवों के शामिल होने को अनिवार्य मानती है। ये हैं, राज्य की सुरक्षा को खतरा, और आतंकी हमले। राज्य की सुरक्षा को खतरे में उसकी एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और संप्रभुता पर खतरा शामिल है। आतंकी हमलों को तीन समूहों में रखा गया है। पहला, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले, यानि संसद, विधान सभाओं और आर्थिक केंद्रों पर हमला करके देश की आर्थिक संरचना को तोड़ने की कोशिश। दूसरा, राष्ट्रीय गौरव के प्रतीकों और सुरक्षा के रणनीतिक महत्व के केंद्रों पर हमले, यानि लाल क़िला, सैन्य संस्थानों और शिविरों तथा रेडियो स्टेशनों आदि पर हमले। तीसरा, नागरिकों पर हमले करके लोगों को व्यापक पैमाने पर आतंकित करने की कोशिश।
जाहिर है कि ‘आतंकवादी कार्रवाई’ की इतनी सुस्पष्ट व्याख्या कोई नयी बात नहीं है, बल्कि विद्वान न्यायाधीशद्वय स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों के अनुशीलन के बाद उनको उद्धृत करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। इसके बावजूद अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग यूएपीए जैसे डरावने क़ानूनों के शिकंजे में कस कर रखे गये हैं तो यह प्रवृत्ति भारतीय लोकतंत्र के भविष्य पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा करती है।
यूएपीए जैसे सख्त क़ानूनों को बार-बार इस्तेमाल करके महत्वहीन न बना दिया जाए
गृह मंत्रालय के एक खुलासे के अनुसार यूएपीए के तहत पंजीकृत मुकदमों में दोषसिद्धि की दर मात्र 2.2 प्रतिशत है। फिर भी केंद्रीय एजेंसियां धड़ल्ले से इस क़ानून का इस्तेमाल करती जा रही हैं। शेष 97.8 प्रतिशत लोगों को वर्षों तक, और कभी-कभी दशकों तक (कुछ मामलों में तो 14 साल और 23 साल तक) जेल में गुजारने के बाद “बाइज्जत(?) बरी” कर दिया जाता है। अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो झूठा आरोप लगाने के लिए जिम्मेदार लोगों को कठघरे में खड़ी कर सके और सजा दे सके। अदालत ने कहा है कि, “प्रस्तुत आरोप-पत्र में बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, जो यूएपीए के अनुच्छेद 15 के तहत कोई संभावित ‘आतंकवादी कार्रवाई करने’, अनुच्छेद 17 के तहत किसी आतंकवादी कार्रवाई के लिए ‘धन इकट्ठा करने’ या अनुच्छेद 18 के तहत किसी आतंकवादी कार्रवाई की ‘साजिश रचने’ अथवा ‘तैयारी करने’ को विशिष्ट और ब्यौरेवार ढंग से दिखा सके। प्रस्तुत आरोप-पत्र में हम किसी ऐसी मौलिक तथ्यात्मक सामग्री को पहचान पाने में असमर्थ हैं जो यूएपीए की धारा 15, 17 या 18 के तहत परिभाषित अपराधों की श्रेणी के उपयुक्त हो।”
अदालत चेतावनी के अंदाज में कहती है कि, “हर मामले को यूएपीए की अत्यंत संगीन और गंभीर धाराओं के तहत दर्ज करने की लापरवाही संसद की उस नीयत और उद्देश्य को ही बेमतलब बना देगी, जिसके चलते उसने एक ऐसा क़ानून बनाया जिसके जरिये ऐसे अपराधों से निपटा जा सके जो राष्ट्र के अस्तित्व के लिए ही खतरा साबित हो रहे हों। अपराध संबंधी संगीन प्रावधानों का बारंबार ग़ैरजरूरी इस्तेमाल अंततः उन्हें महत्वहीन बना देगा।”
अदालतें खुद अपने दिमाग़ का इस्तेमाल करें
यूएपीए के प्रावधानों के अनुसार यूएपीए लगाने से पहले केंद्र सरकार से इसकी पूर्वानुमति लेनी होती है। नियमतः एक स्वतंत्र अधिकारी एकत्रित साक्ष्यों का अध्ययन करके इसकी अनुमति देता है। इस मामले में भी ऐसा किया गया था। प्रायः अदालतें केवल यही देखती हैं कि इस औपचारिकता का पालन हुआ है अथवा नहीं। अगर पालन हुआ होता है तो अदालतें यूएपीए की प्रासंगिकता पर सवाल ही नहीं उठातीं और उधर से आंखें बंद कर लेती हैं। जाहिर है कि शक्तियों के संकेंद्रण के वर्तमान दौर में, जब गृह मंत्रालय के इशारे पर, और कभी-कभी तो मात्र उसे खुश करने के लिए सब कुछ चल रहा हो, तो ऐसे में यह अनुमति एक औपचारिक कार्यवाही से अधिक कुछ नहीं रह जाती होगी, जिसे बाद में भी, कभी भी पूरा करा लिया जाता होगा, या ऐसी पूर्वानुमति के सादे कागजों पर दस्तखत करके पहले ही सौंप दिये जाते होंगे, जैसा कि पिछले दिनों दिल्ली पुलिस की बेनामी प्राथमिकियों (एफआईआर) में दिखाई दिया था। जाहिर है कि वर्तमान आदेश ने अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के दागदार दामनों को भी सामने ला दिया है, लेकिन आदेश के खिलाफ तुरंत अपील की कार्यवाही ने दिखा दिया है कि शर्मिंदा होने के किसी भाव की गुंजाइश दूर-दूर तक नहीं है।
इसीलिए उच्च न्यायालय ने खुद अदालतों का आह्वान किया है कि वे केवल कथित ‘स्वतंत्र प्राधिकारी’ से अनुमति लेने की औपचारिकता की जांच करके अपने कर्तव्य की इतिश्री न समझ लें, बल्कि वे खुद अपने दिमाग़ का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित करें कि वर्णित अपराधों की प्रकृति यूएपीए में शामिल करने लायक है भी, कि नहीं।
शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन का अधिकार लोकतंत्र की बुनियाद है
अदालत सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के एक हिस्से को उद्धृत करते हुए कहती है कि, “अनुच्छेद 19(1)(बी) और (सी) के तहत तर्कसंगत सीमाओं के साथ विरोध-प्रदर्शन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।” सभा करने के अधिकार पर अदालत कहती है कि, ” ‘नमक सत्याग्रह’, ‘आमरण अनशन’ और ‘करो या मरो’ की भारत भूमि पर हथियार-रहित विरोध प्रदर्शन कोई विधिक अभिशाप नहीं है। इसकी व्याख्या करने की भला क्या जरूरत है कि न्यायोचित असंतोष की अभिव्यक्ति का अवसर किसी भी लोकतंत्र का खास गुण है। सीधी कार्रवाई या शातिपूर्ण प्रदर्शनों के माध्यम से अपनी शिकायतों की अभिव्यक्ति तो भारतीय राजनीतिक जीवन की बहुप्रशंसित और बहुमूल्य विशेषता है। संगठित, अहिंसक विरोध-प्रदर्शन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण हथियार थे, और शातिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिया गया है।” लेकिन इसके बावजूद हम रोज ब रोज देख रहे हैं कि राजसत्ता ऐसे किसी भी विरोध या विरोध-प्रदर्शन के प्रति अत्यंत असहिष्णु हो चुकी है। इसी वजह से हमारे संवैधानिक अधिकारों में कटौती और उनके अवमूल्यन की नजीरें रोज ब रोज देखने को मिल रही हैं। वर्तमान आदेश ने इन अधिकारों को नये सिरे से रेखांकित करके एक जरूरी काम किया है।
संघवाद की सीमाओं का अतिक्रमण न होने दिया जाए
संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत अधिकार क्षेत्रों की तीन अनुसूचियां बनायी गयी हैं। पहली अनुसूची के विषयों पर क़ानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, दूसरी अनुसूची के विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और तीसरी समवर्ती सूची है जिसके विषयों पर दोनों अपने-अपने दायरे में क़ानून बना सकते हैं। जहां तक अपराधों का सवाल है, केंद्र की सूची में भारत की सुरक्षा का मामला है, राज्यों की सूची में सार्वजनिक व्यवस्था का मामला है और समवर्ती सूची में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) संबंधी अन्य क़ानून कुछ शर्तों के साथ हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारत की सुरक्षा संबंधी क़ानून यूएपीए केंद्र के दायरे में आता है और सार्वजनिक व्यवस्था राज्यों के दायरे में। अब अगर केंद्र सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी सामान्य अपराधों पर भी यूएपीए लगाने लगेगा तो यह संघवाद की व्यवस्था का भी अतिक्रमण होगा। अदालत ने अपने आदेश में इस अतिक्रमण के खिलाफ चेतावनी दी है।
क़ानून की भाषा में वैज्ञानिकता, यानि स्पष्टता और सटीकता हो, ताकि दुरुपयोग न हो सके
अक्सर क़ानूनी शब्दावली के निश्चित पारिभाषिक अर्थ न होने के कारण उनके सुविधाजनक अर्थ निकाल लिए जाते हैं। आरोप-पत्रों में ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करके एजेंसियां जरूरी तथ्यों की कमी पर परदा डालने के लिए करती हैं। अतः अदालतों के लिए जरूरी है कि यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे शब्दों के अन्यथा अर्थ न निकाले जाएं। आदेश में कहा गया है कि, “अदालतों के लिए यह जरूरी है कि अनुच्छेद 15 में आये हुए पारिभाषिक शब्दों और मुहावरों को इस्तेमाल करते हुए इस बात की सावधानी बरतें कि उनका बिल्कुल वास्तविक मंतव्य निकले अन्यथा उनका हल्के अंदाज में किया गया इस्तेमाल आतंकवादी कार्रवाई जैसे अत्यंत जघन्य अपराध को महत्वहीन बना देगा, बिना यह जाने कि किस तरह से वह परंपरागत जघन्य अपराध से भिन्न है।”
अभियोग लगाने वाली एजेंसियां उपयुक्त तथ्य न होने के बावजूद आतंकवाद की धारा लगाने की कोशिश में आरोप को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करने के लिये शब्दजाल का प्रश्रय लेती हैं। वर्तमान आरोप-पत्र में इसी का उल्लेख करते हुए सावधान किया गया है कि, “प्रस्तुत आरोप-पत्र में निहित आरोपों के वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने पर, हमारे विचार से, इसमें मात्र शब्दाडंबरपूर्ण बातों से बुने हुए आरोपों के अलावा ऐसे विशिष्ट, ब्यौरेवार, तथ्यपरक आरोपों का पूर्ण अभाव है, जो इसे यूएपीए के अनुच्छेद 15,17 या 18 के तहत अपराधों में शामिल करने की योग्यता रखते हों।”
राज्य का दुराग्रह लोकतंत्र के लिए खतरा है
असंतोष और विरोध की अभिव्यक्ति का अधिकार लोकतंत्र की बुनियाद है, लेकिन ऐसे मामले अब तेजी से बढ़ने लगे हैं जिनमें शासक वर्ग इसे अपनी हेठी मानते हुए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना ले रहा है और किसी भी क़ीमत पर इसे कुचलने को आमादा हो जा रहा है। इसके लिए वह अपनी सभी एजेंसियों का इस्तेमाल करते हुए सामान्य सी संवैधानिक मांग अथवा सरकारी नीतियों की छोटी सी आलोचना को भी संगीन आतंकी कार्रवाई के रूप में चित्रित करके पेश करने के लिए किसी भी हद तक उतरने से गुरेज नहीं कर रहा है। अदालत कहती है कि, “हम यह व्यक्त करने के लिए विवश हैं, कि ऐसा लगता है, कि असंतोष को दबाने की व्यग्रता में, राज्य के दिमाग में संवैधानिक रूप से गारंटीप्राप्त विरोध करने के अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच की विभाजक रेखा किसी हद तक धुंधली पड़ गयी है। यदि इस मानसिकता को बढ़ावा मिलता है, तो यह लोकतंत्र के लिए दुखद दिन होगा।”
लेकिन आदालत की यह आशंका किसी चेतावनी से ज्यादा एक हक़ीक़त को बयान कर रही है। वास्तव में हमारे शासकों के इसी रवैये के चलते भारत लोकतांत्रिक देशों की वैश्विक सूची में 2014 के 27वें स्थान से फिसलते-फिसलते 2020 में 53वें स्थान पर पहुंच गया है, और दुनिया का यह सबसे बड़ा लोकतंत्र आज एक ‘दोषपूर्ण लोकतंत्र’ रह गया है। हमारे लोकतंत्र के लिए वे दुखद दिन पहले ही आ चुके हैं। यही कारण है कि जिन विरोध प्रदर्शनों को किसी भी लोकतंत्र के स्वास्थ्य की निशानी के तौर पर देखा जाता उन्हीं को हमारे देश में आतंकवाद के रूप में देखा जा रहा है और उनके दमन के लिए सारी हदें पार कर दी जा रही हैं। सरकार का यही रुख आंदोलनकारी किसानों के प्रति भी है। शायद भीतर से डरी हुई सभी व्यवस्थाएं विधिसम्मत विरोधों को भी अपने खिलाफ साजिशों के तौर पर देखने लगती हैं।
क्या ये व्याख्याएं राजद्रोह के मामलों पर भी असर डालेंगी?
भारत 2021 की प्रेस की स्वतंत्रता की 180 देशों की वैश्विक सूची में 142वें स्थान पर है। देश में बड़ी संख्या में मानवाधिकार कार्यकर्ता, सच्चे, स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकार, दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए काम कर रहे एक्टिविस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट, पर्यावरणवादी, सरकार की भेदभाव वाली और सांप्रदायिक नीतियों की मुखर आलोचना करने वाले बुद्धिजीवी या तो यूएपीए के तहत आतंकवादी गतिविधियों में, या राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून (रासुका) के तहत राजद्रोह के आरोप में वर्षों और दशकों से जेलों में बंद हैं। हाथरस में दलित लड़की के बलात्कार और हत्या की रिपोर्टिंग के लिए जा रहे पत्रकार पर रासुका लगा दिया जाना अभी हाल की घटना है। यहां तक कि कोविड से होने वाली मौतों की सही संख्या उजागर करने वाले पत्रकारों को भी उत्पीड़ित करने और धमकी देने की खबरें आती रही हैं। इसी तरह सरकार द्वारा लाख परदा डालने के बावजूद सही खबरों को प्रकाश में लाते रहने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों, वेबसाइटों, ऑनलाइन न्यूज पोर्टलों और ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर भी नकेल कसने के लिए क़ानून ला चुकी है और उन्हें धमकाती जा रही है।
यूएपीए और रासुका, ये दोनों क़ानून अत्यंत सख्त हैं और इन दोनों के ही तहत अभियुक्त मुकदमे की अंतिम सुनवाई से पहले ही, जमानत के बिना, वर्षों तक जेलों में बंद रहने के लिए अभिशप्त हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के यूएपीए पर वर्तमान आदेश में जिस तरह से क़ानूनी शब्दों की सटीक व्याख्या, आरोप-पत्र को शब्दाडंबरों की बजाय तथ्यों पर आधारित बनाने, जमानत को नियम मानने और दोषसिद्धि से पहले अभियुक्त को निर्दोष मानने का आह्वान किया गया है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी पहल रासुका के तहत राजद्रोह के झूठे आरोपों में जेलों की अंधेरी कोठरियों में बंद असंख्य अभियुक्तों को भी न्याय दिलाने की दिशा में मशाल बन कर रास्ता दिखान का काम करेगी।
*****
आखिर क्या बात है कि राज्य इन विद्यार्थियों को जेल में सड़ाने के लिए इतना उतावला दिख रहा है। अदालत तो इस जमानत आदेश में भी साफ-साफ कहती है कि, “खतरे और आतंक की ‘संभावना’ के इस पहलू पर चिंतापूर्वक ध्यान देने के बाद हमारा विचार यह बना है कि हमारे राष्ट्र की बुनियाद इतनी मजबूत है कि उसे दिल्ली के केंद्र में स्थित एक विश्वविद्यालय की सीमा में एक समन्वय समिति के रूप में काम कर रहे कॉलेज के विद्यार्थियों या अन्य लोगों द्वारा संगठित किसी प्रदर्शन द्वारा हिलाये जाने की कोई संभावना नहीं है, वह प्रदर्शन चाहे कितना भी सरकश क्यों न हो।” लेकिन दिल्ली पुलिस फिर भी इस जमानत को रुकवाने के लिए तत्काल सर्वोच्च न्यायालय चली गयी। हलांकि यह जमानत तो नहीं रोकी गयी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश की प्रस्थापनाओं को नजीर के रूप में इस्तेमाल करने से अन्य न्यायालयों को फिलहाल रोक दिया है।
दरअसल पिछले कुछ वर्षों में एक मजबूत राज्य की तलाश में हमने एक हठी और दुराग्रही कार्यपालिका को अपने ऊपर थोप लिया है। लेकिन अब सभी समझदार लोगों को इस बात का अहसास होने लगा है कि ऐसा राज्य एक बहुलवादी लोकतंत्र की जड़ों में मट्ठा डाल देता है और शक्तियों के संकेंद्रण की उसकी अधिनायकवादी भूख अंततः उसे चुनने वाली अपनी जनता के ही खिलाफ खड़ी कर देती है। बाहरी तौर पर लोकतंत्र का ढांचा यथावत दिखते हुए भी उसकी अंतर्वस्तु, उसकी आत्मा गायब हो चुकी है। इसलिए लोकतंत्र के संविधान-सम्मत तीनों पायों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका’ के बीच ‘नियंत्रण और संतुलन’ का संबंध बना रहना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से रह-रह कर निराश करती आयी न्यायपालिका की वर्तमान पहल इस संबंध की बहाली और लोकतंत्र के पुनर्जीवन की कुछ उम्मीद जगाती है। यह पहल खुद न्यायपालिका की अपनी प्रासंगिकता और अस्तित्व की भी अपरिहार्य शर्त है।
(शैलेश स्वतंत्र लेखक हैं।)