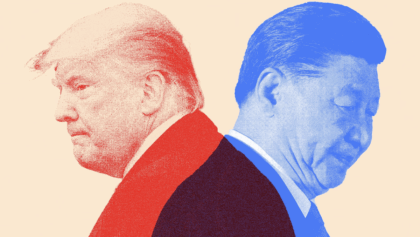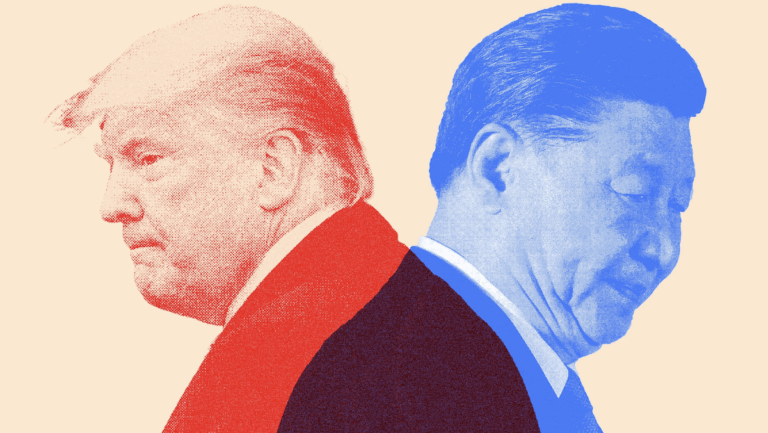करीब पांच दशक पुराने आपातकाल के काले कालखंड को हर साल 25-26 जून को याद किया जाता है, लेकिन पिछले दस वर्षों से उस दौर को कुछ ज्यादा ही याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सिर्फ़ सालगिरह पर ही नहीं, बल्कि हर मौक़े-बेमौक़े आपातकाल को याद करते रहते हैं। इस बार भी 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में आपातकाल को याद किया गया। स्पीकर ओम बिड़ला ने आपातकाल की ज्यादतियों के वर्णन से भरा एक लंबा-चौड़ा निंदा प्रस्ताव पढ़ा और उसे पारित कराया। इससे पहले सत्र की शुरुआत के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीवी कैमरों के सामने आपातकाल को याद करते हुए एक लंबा भाषण दिया। कई अखबारों ने तो गृह मंत्री अमित शाह के नाम से आपातकाल की ज्यादतियों को याद करते हुए लेख भी छापे।
आपातकाल के बाद पांच दशकों के दौरान देश में अब सात ग़ैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए हैं, जिनमें से मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तीन के अलावा शेष सभी आपातकाल के दौरान जेल में रहे हैं। जेल में रहने वालों में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी शामिल किया जा सकता है, हालांकि उन्हें कुछ ही दिन जेल में रहना पड़ा था। बाक़ी समय उन्होंने पैरोल पर रहते हुए बिताया था। लेकिन उनमें से किसी ने कभी भी आपातकाल को इतना ज्यादा और इतने कर्कश तरीक़े से याद नहीं किया, जितना कि मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। हालांकि मोदी को 2002 की गुजरात की वह महीनों तक चली राज्य प्रायोजित सांप्रदायिक हिंसा कभी याद नहीं आती जो उनके ही मुख्यमंत्रित्व काल में हुई थी।
राजनीतिक विमर्श में आपातकाल मोदी का प्रिय विषय रहता है, इसलिए वे आपातकाल को सिर्फ़ 25-26 जून को ही नहीं बल्कि अक्सर याद करते रहते हैं। यह और बात है कि मोदी आपातकाल के दौरान एक दिन के लिए भी जेल तो दूर, पुलिस थाने तक भी नहीं ले जाए गए थे।
जेल के बाहर भूमिगत रहकर उन्होंने आपातकाल विरोधी संघर्ष में कोई हिस्सेदारी की हो, इसकी भी कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। जबकि उस दौरान भूमिगत रहे जार्ज फर्नांडीज, कर्पूरी ठाकुर जैसे दिग्गजों के अलावा समाजवादी नेता लाडली मोहन निगम और द हिंदू अख़बार के तत्कालीन प्रबंध संपादक सीजीके रेड्डी जैसे कई कम मशहूर लोगों की गतिविधियां भी जगज़ाहिर हो चुकी हैं।
कहा जा सकता है कि मोदी संघ और जनसंघ के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आपातकाल के एक सामान्य दर्शक रहे हैं। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रदर्शित होकर फ्लॉप रही उनकी बॉयोपिक ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ में जरूर उन्हें आपातकाल के भूमिगत महानायक के तौर पर पेश करने की फूहड़ और हास्यास्पद कोशिश की गई थी।
एक राजनीतिक कार्यकर्ता होते हुए भी आपातकाल से अछूते रहने के बावजूद अगर मोदी मौक़े-बेमौक़े आपातकाल को चीख़-चीख़कर याद करते हुए कांग्रेस को कोसते हैं तो इसकी वजह उनका अपना यह ‘आपातकालीन अपराध बोध’ ही हो सकता है कि वे आपातकाल के दौर में कोई सक्रिय भूमिका निभाते हुए जेल क्यों नहीं सके जा सके!
यह भी दिलचस्प और उल्लेखनीय है कि आपातकाल लागू होने के बाद गिरफ्तार किए गए आरएसएस के तत्कालीन सर संघचालक मधुकर दत्तात्रेय देवरस उर्फ बाला साहेब देवरस ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जेल से पत्र लिख कर आपातकाल का समर्थन करते हुए आरएसएस पर से प्रतिबंध हटाने तथा जेल में बंद जनसंघ और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को रिहा करने का अनुरोध किया था। इंदिरा गांधी ने उनका यह अनुरोध ठुकरा दिया था। उसके बाद जेलों में बंद आरएसएस और जनसंघ के हजारों कार्यकर्ता व्यक्तिगत माफीनामे लिख कर जेल से बाहर आए थे। उन माफीनामों में कहा गया था कि वे जेल से छूटने के बाद किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। आरएसएस और जनसंघ के कई नेताओं व कार्यकर्ताओं ने तो गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने घरों पर लगीं सावरकर, डॉ. हेडगेवार और गोलवलकर की तस्वीरें हटा कर उनकी जगह महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी की तस्वीरें टांग दी थीं।
बहरहाल आपातकाल के नाम पर उनकी चीख़-चिल्लाहट को उनकी प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि मोदी कांग्रेस को कोसने के लिए गाहे-बगाहे आपातकाल का ज़िक्र करके अपने उन कार्यों पर नैतिकता का पर्दा डालना चाहते हैं, जिनकी तुलना आपातकालीन कारनामों से की जाती हैं- मसलन न्यायपालिका, चुनाव आयोग, सतर्कता आयोग, सूचना आयोग, रिज़र्व बैंक जैसी महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्ता का अपहरण. प्रवर्तन निदेशालय ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग जैसी एजेंसियों का और सेना तथा अन्य सुरक्षा बलों का अंधाधुंध राजनीतिक इस्तेमाल।
प्रधानमंत्री की देखादेखी उनके कई मंत्री और भाजपा के नेता तथा प्रवक्ता भी अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमले के लिए आपातकाल को ही हथियार के रुप में इस्तेमाल करते हैं। इसका नज़ारा टीवी चैनलों पर रोज़ाना होने वाली निरर्थक बहसों में भी देखने को मिलता है। कोई भी मुद्दा हो, जब भाजपा प्रवक्ताओं के पास कहने को कुछ नहीं होता है तो वे आपातकाल का ज़िक्र करने लगते हैं। उनके फ़िक्स और सधे हुए डायलॉग होते हैं- ‘आपातकाल में जब हुआ, तब आप कहां थे’, ‘हम पर अंगुली उठाने से पहले ज़रा आपातकाल को याद कर लीजिए’, ‘जिन्होंने देश पर आपातकाल थोपा था, वे हमें लोकतंत्र का पाठ न पढ़ाएं’ आदि-इत्यादि।
आपातकाल के ज़िक्र वाले मोदी के तमाम भाषण हों या उनकी पार्टी के नेताओं-प्रवक्ताओं के कुतर्की बयान, सबसे ध्वनि यही निकलती है कि हमारी सरकार जो कर रही है उसमें कुछ ग़लत नहीं है और ऐसा तो कांग्रेस के शासनकाल में भी होता रहा है।
आपातकाल की 49वीं सालगिरह के मौक़े का इस्तेमाल भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चिर-परिचित अंदाज़ में कांग्रेस को कोसने और अपनी पीठ थपथपाने के लिए किया। मोदी ने कहा कि 25 जून की तारीख़ भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का काला दिन है और इसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए। उनकी इस बात से कौन इनकार कर सकता है ! बेशक आपातकाल को हमेशा याद रखा जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही यह तथ्य भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस ‘तानाशाह’ इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था, उसी इंदिरा गांधी ने चुनाव भी कराए थे, जिसमें वे और उनकी पार्टी बुरी तरह पराजित हुई थी।
जिस जनता ने इंदिरा गांधी को आपातकाल के लिए यह निर्मम लोकतांत्रिक सज़ा दी थी उसी जनता ने तीन साल बाद हुए मध्यावधि चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस को दो तिहाई बहुमत के साथ जिता दिया। इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बनीं।
ज़ाहिर है कि देश की जनता ने इंदिरा गांधी को लोकतंत्र से खिलवाड़ करने के उनके गंभीर अपराध के लिए माफ़ कर दिया था। हालांकि इस माफ़ी का यह आशय क़तई नहीं था कि जनता ने आपातकाल को और उसके नाम पर हुए सभी कृत्यों को जायज़ मान लिया था।
निस्संदेह आपातकाल हमारे लोकतांत्रिक इतिहास का ऐसा काला अध्याय है जिसे कोई मोदी या कोई अमित शाह याद दिलाए या न दिलाए, देश के लोगों के ज़ेहन में हमेशा बना रहेगा। लेकिन आपातकाल को याद रखना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इससे भी ज़्यादा ज़रूरी इस बात के लिए सतर्कता बरतना है कि कोई भी हुकूमत आपातकाल को किसी भी रूप में दुहराने का दुस्साहस न कर सके।
सवाल है कि क्या आपातकाल को दोहराने का ख़तरा अभी भी बना हुआ है या किसी नए आवरण में आपातकाल आ चुका है और भारतीय जनमानस उस ख़तरे के प्रति सचेत है?
नौ साल पहले आपातकाल के चार दशक पूरे होने के मौक़े पर उस पूरे कालखंड को शिद्दत से याद करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने देश में फिर से आपातकाल जैसे हालात पैदा होने का अंदेशा जताया था। एक अंग्रेजी अख़बार को दिए साक्षात्कार में आडवाणी ने देश को अगाह किया था कि ”लोकतंत्र को कुचलने में सक्षम ताक़तें आज पहले से अधिक ताक़तवर है और पूरे विश्वास के साथ यह नहीं कहा जा सकता कि आपातकाल जैसी घटना फिर दोहराई नहीं जा सकती।”
बकौल आडवाणी, “भारत का राजनीतिक तंत्र अभी भी आपातकाल की घटना के मायने पूरी तरह से समझ नहीं सका है और मैं इस बात की संभावना से इनकार नहीं करता कि भविष्य में भी इसी तरह से आपातकालीन परिस्थितियां पैदा कर नागरिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है। आज मीडिया पहले से अधिक सतर्क है, लेकिन क्या वह लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध भी है? कहा नहीं जा सकता. सिविल सोसायटी ने भी जो उम्मीदें जगाई थीं, उन्हें वह पूरी नहीं कर सकी है। लोकतंत्र के सुचारु संचालन में जिन संस्थाओं की भूमिका होती है, आज भारत में उनमें से केवल न्यायपालिका को ही अन्य संस्थाओं से अधिक ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।”
आडवाणी का यह बयान हालांकि नौ साल पुराना है लेकिन इसकी प्रासंगिकता नौ साल पहले से कहीं ज़्यादा आज महसूस की जा सकती है। आधुनिक भारत के राजनीतिक विकास के सफर में लंबी और सक्रिय भूमिका निभा चुके एक तजुर्बेकार राजनेता के तौर पर आडवाणी की इस आशंका को अगर हम अपनी राजनीतिक और संवैधानिक संस्थाओं के मौजूदा स्वरूप और संचालन संबंधी व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम पाते हैं कि आज देश आपातकाल से भी कहीं ज़्यादा बुरे दौर से गुज़र रहा है।
इंदिरा गांधी ने तो संवैधानिक प्रावधानों का सहारा लेकर देश पर आपातकाल थोपा था, लेकिन आज तो औपचारिक तौर पर आपातकाल लागू किए बग़ैर ही वह सब कुछ बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा हो रहा है जो आपातकाल के दौरान हुआ था। फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि आपातकाल के दौरान सब कुछ अनुशासन के नाम पर हुआ था और आज जो कुछ हो रहा है वह विकास और राष्ट्रवाद के नाम पर।
केंद्र सहित देश के लगभग आधे राज्यों में सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर भी हाल के वर्षों में ऐसी प्रवृत्तियां मज़बूत हुई हैं, जिनका लोकतांत्रिक मूल्यों और कसौटियों से कोई सरोकार नहीं है। सरकार और पार्टी में सारी शक्तियां एक समूह के भी नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द सिमटी हुई हैं।
आपातकाल के दौर में उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने चाटुकारिता और राजनीतिक बेहयाई की सारी सीमाएं लांघते हुए ‘इंदिरा इज़ इंडिया-इंडिया इज़ इंदिरा’ का नारा पेश किया था। आज भाजपा में तो अमित शाह, रविशंकर प्रसाद, शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडनवीस आदि से लेकर नीचे के स्तर तक ऐसे कई नेता हैं जो नरेंद्र मोदी को जब-तब दैवीय शक्ति का अवतार बताने में कोई संकोच नहीं करते। वैसे इस सिलसिले की शुरुआत बतौर केंद्रीय मंत्री वैंकेया नायडू ने की थी, जो बाद में उपराष्ट्रपति बनाए गए. हद तो यह है कि अब तो खुद मोदी ही अपने को ईश्वर का दूत बताने लगे हैं। लेकिन बात नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार की ही नहीं है, बल्कि आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति की ही यह बुनियादी समस्या रही है कि वह हमेशा से व्यक्ति केंद्रित रही है। हमारे यहां संस्थाओं, उनकी निष्ठा और स्वायत्तता को उतना महत्व नहीं दिया जाता, जितना महत्व करिश्माई नेताओं को दिया जाता है।
इससे न सिर्फ़ राज्यतंत्र के विभिन्न उपकरणों, दलीय प्रणालियों, संसद, प्रशासन, पुलिस, और न्यायिक संस्थाओं की प्रभावशीलता का तेज़ी से पतन हुआ है, बल्कि राजनीतिक स्वेच्छाचारिता और ग़ैरज़रूरी दख़लंदाज़ी में भी बढ़ोतरी हुई है।
यह स्थिति सिर्फ़ राजनीतिक दलों की ही नहीं है। आज देश में लोकतंत्र का पहरुए कहे जा सकने वाले ऐसे संस्थान भी नज़र नहीं आते, जिनकी लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर प्रतिबद्धता संदेह से परे हो। आपातकाल के दौरान जिस तरह प्रतिबद्ध न्यायपालिका की वकालत की जा रही थी, आज वैसी ही आवाज़ें सत्तारूढ़ दल से नहीं बल्कि न्यायपालिका की ओर से भी सुनाई दे रही है। यही नहीं, कई महत्वपूर्ण मामलों में तो अदालतों के फैसले भी सरकार की मंशा के मुताबिक़ ही रहे हैं।
जिस मीडिया को हमारे यहां लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मान्यता दी गई है, उसकी स्थिति भी बेहद चिंताजनक है। आज की पत्रकारिता आपातकाल के बाद जैसी नहीं रह गई है। इसकी अहम वजहें हैं- बड़े कॉरपोरेट घरानों का मीडिया क्षेत्र में प्रवेश और मीडिया समूहों में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने की होड़। इस मुनाफ़ाख़ोरी प्रवृत्ति ने ही मीडिया संस्थानों को लगभग जनविरोधी और सरकार का पिछलग्गू बना दिया है। सरकार की ओर से मीडिया को दो तरह से साधा जा रहा है- उसके मुंह में विज्ञापन ठूंस कर या फिर सरकारी एजेंसियों के ज़रिये उसकी गर्दन मरोड़ने का डर दिखाकर। इस सबके चलते सरकारी और ग़ैर सरकारी मीडिया का भेद लगभग ख़त्म सा हो गया है।
पिछले चार-पांच सालों में जो एक नई और ख़तरनाक प्रवृत्ति विकसित हुई वह है सरकार और सत्तारूढ़ दल और मीडिया द्वारा सेना का अत्यधिक महिमामंडन। यह सही है कि हमारे सैन्यबलों को अक्सर तरह-तरह की मुश्किल भरी चुनौतियों से जूझना पड़ता है, इस नाते उनका सम्मान होना चाहिए लेकिन उनको किसी भी तरह के सवालों से परे मान लेना तो एक तरह से सैन्यवादी राष्ट्रवाद की दिशा में क़दम बढ़ाने जैसा है।
आपातकाल कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि सत्ता के अतिकेंद्रीकरण, निरंकुशकता, व्यक्ति-पूजा और चाटुकारिता की निरंतर बढ़ती गई प्रवृत्ति का ही परिणाम थी। आज फिर वैसा ही नज़ारा दिख रहा है। आपातकाल के दौरान संजय गांधी और उनकी चौकड़ी की भूमिका सत्ता-संचालन में ग़ैर-संवैधानिक हस्तक्षेप की मिसाल थी, तो आज वही भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निभा रहा है।
संसद को अप्रासंगिक बना देने की कोशिशें जारी हैं। असहमति की आवाज़ों को चुप करा देने या शोर में डुबो देने की कोशिशें साफ़ नज़र आ रही हैं। आपातकाल के दौरान और उससे पहले सरकार के विरोध में बोलने वाले को अमरीका या सीआईए का एजेंट क़रार दे दिया जाता था तो अब स्थिति यह है कि सरकार से असहमत हर व्यक्ति को पाकिस्तान परस्त या देशविरोधी क़रार दे दिया जाता है।
आपातकाल में इंदिरा गांधी के बीस सूत्रीय और संजय गांधी के पांच सूत्रीय कार्यक्रमों का शोर था तो आज विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आवरण में हिंदुत्ववादी एजेंडा पर अमल किया जा रहा है। इस एजेंडा के तहत दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का तरह-तरह से उत्पीड़न हो रहा है।
कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आपातकाल के बाद से अब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था तो चली आ रही है, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं, रवायतों और मान्यताओं का क्षरण तेज़ी से जारी है। यह ज़रूरी नहीं कि लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों का अपहरण हर बार बाक़ायदा घोषित करके ही किया जाए। वह लोकतांत्रिक आवरण और क़ायदे-क़ानूनों की आड़ में भी हो सकता है, और काफ़ी हद तक हो भी रहा है, जिस पर पर्दा डालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जब-तब पांच दशक पीछे लौटकर ‘कांग्रेस के आपातकाल’ को उठा लाते हैं।
(अनिल जैन वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिल्ली में रहते हैं)