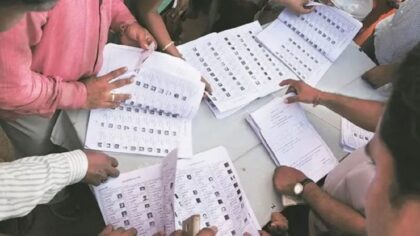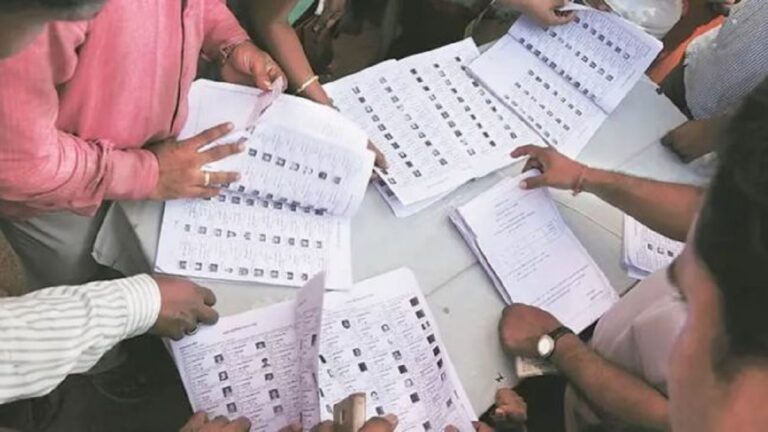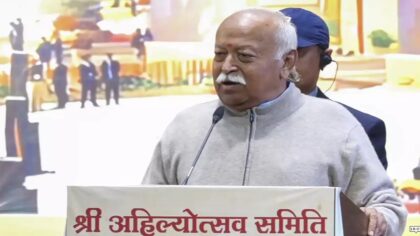लगभग 12 वर्ष पहले जिस घटना ने राष्ट्र की अंतरात्मा को झकझोर दिया और मानवता के प्रति हमारी भावनात्मक समझ को तोड़ दिया, वह निर्भया बलात्कार और हत्या का मामला था। आधी रात को, एक 23 वर्षीय महिला का चलती बस में पांच पुरुषों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया। इस जघन्य अपराध के बाद, अपराधियों ने पीड़िता को नग्न अवस्था में बस से बाहर फेंक दिया। बलात्कारियों द्वारा किए गए गंभीर आंतरिक घावों के कारण, पीड़िता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
इस घटना के बाद, कई महिला संगठनों और नागरिक समाज के सदस्यों ने महिलाओं की सार्वजनिक सुरक्षा और ‘निर्भया’ (प्रशासन द्वारा दिया गया नाम) के लिए न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिए। इन विरोधों के परिणामस्वरूप, सरकार ने यौन उत्पीड़न और बलात्कार की परिभाषा में कई संशोधन किए।
20 वर्षीय ज्योति सिंह (निर्भया) की मां, आशा देवी ने अपने अनुभवों के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देने का निर्णय लिया। अपनी दुखद अनुभवों से प्रेरित होकर, आशा ने अपनी बेटी की स्मृति में निर्भया ज्योति ट्रस्ट की स्थापना की। यह ट्रस्ट लैंगिक हिंसा के मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए मजबूत कानूनी और संस्थागत ढांचे की वकालत करने के उद्देश्य से काम करता है।
भारतीय कानून बलात्कार पीड़ितों और उनके परिवारों की पहचान गुप्त रखने का प्रावधान करता है, लेकिन 2015 में, आशा ने अपनी बेटी का नाम सार्वजनिक करने का साहसिक कदम उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसी जघन्य अपराध करने वालों को शर्मिंदा होना चाहिए, न कि पीड़ितों के परिवारों को। ऐसा करके, आशा ने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और समाज में गरिमा और शर्म की अवधारणाओं को पुनर्परिभाषित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।
हालांकि, सामाजिक मानदंड अक्सर एक महिला की गरिमा को उसके परिवार, जाति या धर्म के संदर्भ में रखते हैं। यह धारणा उस समाज की प्रमुख कथा से प्रभावित होती है, जिसमें हम रहते हैं। भारतीय दंड प्रणाली के तहत कठोर नियमों और विनियमों के बावजूद, यौन उत्पीड़न के मामले विभिन्न रूपों में बढ़ते जा रहे हैं। मथुरा बाई बलात्कार मामले के बाद से, जिसमें महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक आदिवासी महिला मथुरा का दो कांस्टेबलों ने बलात्कार किया था और सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपियों को बरी कर दिया था, विधायी प्रयासों का ध्यान सजा की कठोरता बढ़ाने पर केंद्रित है-जो कि एक शीर्ष-डाउन दृष्टिकोण है।
शीर्ष-डाउन दृष्टिकोण की अप्रभावशीलता
एक शीर्ष-डाउन दृष्टिकोण में निर्णय लेने की प्रक्रिया उच्चतम स्तर पर होती है और फिर निर्देश बाकी संगठन तक पहुंचाए जाते हैं। यह विधि आमतौर पर औपचारिक संगठनात्मक कार्यों के लिए अपनाई जाती है। भारत में, यह दृष्टिकोण औपनिवेशिक शासन के दौरान उत्पन्न हुआ, जब ब्रिटिश शासन ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न अनुशासनात्मक तंत्र लागू किए। उनका मानना था कि किसी उपनिवेश पर शासन करने के लिए जनता पर नियंत्रण अनिवार्य था, जिससे शासन में एक trickle-down प्रभाव को बढ़ावा मिला।
सामाजिक परिवर्तन और व्यवहार में बदलाव के लिए शीर्ष-डाउन दृष्टिकोण अप्रभावी है
ऐसे दृष्टिकोण के सफल होने के लिए, कानून का लोगों द्वारा आत्मसात किया जाना भी आवश्यक है। हालांकि, कानून, जो समानता का समर्थन करता है, और समाज, जो अक्सर असमानता के सिद्धांतों पर आधारित होता है, के बीच एक disconnect बना हुआ है। यह समझ का अभाव समाज के उस मूलभूत आधार से आता है, जहां सामाजिक अंतर्विरोध उत्पन्न होते हैं और एक-दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं।
विधानमंडल के प्रयासों का उद्देश्य उन स्थितियों को नियंत्रित करना है, जिनके तहत समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के खिलाफ विभिन्न अत्याचार किए जाते हैं। हालांकि, असली चुनौती इन समस्याओं के मूल कारणों को संबोधित करने की है। मोनाश यूनिवर्सिटी, एंटी डेथ पेनल्टी एशिया नेटवर्क (ADPAN), और SAME नेटवर्क द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट “ए डेडली डिस्ट्रैक्शन: व्हाई द डेथ पेनल्टी इज़ नॉट द आंसर टू रेप इन साउथ एशिया” में यह बताया गया है कि अधिकांश बलात्कार पीड़ितों का शोषण उनके परिचित लोगों द्वारा किया जाता है।
इस तरह के कानून पीड़ितों को अपराधों की रिपोर्ट करने से हतोत्साहित कर सकते हैं, खासकर यदि इससे परिवार के किसी सदस्य को मौत की सजा का सामना करना पड़े। परिणामस्वरूप, बलात्कार के लिए मौत की सजा इस अपराध के पहले से ही कम रिपोर्टिंग दर को और कम करने का जोखिम पैदा करती है। निर्भया कांड के बाद, यौन उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों में 50% की वृद्धि हुई है।
न्याय की मध्यकालीन समझ
जब आर.जी. कर बलात्कार घटना हुई, तो समाज के प्रगतिशील वर्गों ने बलात्कारी को फांसी देने की मांग की। विश्व स्तर पर, मौत की सजा का अक्सर यह भ्रम पैदा करने के लिए उपयोग किया गया है कि न्यायिक निष्पादन के माध्यम से महिलाओं को घातक हिंसा से बचाया जा सकता है। यह विश्वास पितृसत्तात्मक धारणा से उत्पन्न होता है कि बलात्कार “मृत्यु से भी बदतर” है।
ऐसी मध्यकालीन न्यायिक प्रणाली महिलाओं को संपत्ति मानती है और बलात्कार को संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन मानती है। यह दृष्टिकोण यह समझने में मदद करता है कि भारत में ऐतिहासिक रूप से ऊंची जातियों के पुरुषों ने दलित और आदिवासी महिलाओं पर यौन हिंसा क्यों की। मध्यकालीन भारत में, दलित समुदायों के पास अक्सर अपनी संपत्ति नहीं होती थी, जिसके कारण समाज की शासक प्राधिकरण द्वारा दलित महिलाओं की गरिमा को अस्वीकार कर दिया जाता था।
गरिमा और न्याय को नए सिरे से परिभाषित करना
दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए: पहला, महिलाओं को जाति, वर्ग, धर्म आदि की पहचान देने से पहले एक व्यक्ति के रूप में मान्यता देना और दूसरा, न्याय के प्रति हमारे दृष्टिकोण को पुनर्परिभाषित करना। गरिमा एक महिला की स्वायत्तता और उसके कार्यों में निहित है। संविधान जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें गरिमापूर्ण रोजगार जीवन को बनाए रखने के लिए एक मौलिक पहलू है। न्याय की मध्यकालीन अवधारणाएं व्यक्तियों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के साथ सह-अस्तित्व में नहीं रह सकतीं।
इसके अलावा, यदि हम सच्चा न्याय चाहते हैं, तो हमें न्याय की प्रतिशोधात्मक समझ से दूर होना होगा। सामाजिक परिवर्तन के लिए नागरिक समाज और जन समुदाय की लोकतांत्रिक आवाजों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में लोगों की अधिक भागीदारी न्याय प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए अनिवार्य है।
हमें एक दंडात्मक दृष्टिकोण से एक न्याय-केंद्रित दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। पीड़ित मुआवजा और त्वरित न्याय वितरण प्रणाली महत्वपूर्ण कदम हैं, लेकिन ये व्यापक सामाजिक सुधार की आवश्यकता को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। एक सुधारात्मक दृष्टिकोण की मांग है कि हम सार्थक बदलाव प्राप्त करने के लिए अपनी रणनीतियों और प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करें।
(निशांत आनंद कानून के छात्र हैं)