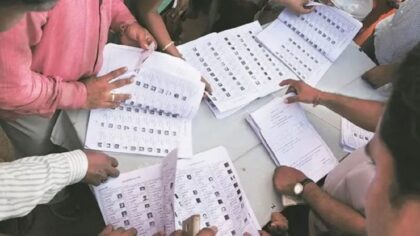बिहार सरकार ने जातीय सर्वेक्षण करवाया और गांधी जयंती के दिन उसके आंकड़े भी जारी कर दिए। तब कहा गया था कि अगले दिन- यानी तीन अक्टूबर को नीतीश कुमार सरकार विभिन्न जातियों की आर्थिक स्थिति से संबंधित इकट्ठे हुए आंकड़ों को भी सार्वजनिक कर देगी। लेकिन अब बताया गया है कि ये आंकड़ें विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान जारी किए जाएंगे। यानी उन आंकड़ों को जानने का इंतजार अब लंबा हो गया है। ये आंकड़े महत्त्वपूर्ण हैं, और उन्हें जानने की बेसब्री प्रमुख रूप से दो कारणों से हैः
- पहली वजह तो यह है कि उन आंकड़ों से पता चलेगा कि बिहार की 13 करोड़ की आबादी में धन और आय के पैमाने पर कितने लोग किस तबके में आते हैं।
- साथ ही गरीब, मध्य वर्ग और धनी तबकों में किन जातियों की कितनी आबादी है।
- उन आंकड़ों से यह भी मालूम होगा कि विभिन्न जातियों के अंदर कितने लोग वर्गीय सीढ़ियां चढ़ते हुए उच्च वर्ग में पहुंच चुके हैं। संभवतः इससे यह भी मालूम होगा कि जिस राज्य में 1978 से ओबीसी (अन्य पिछड़े वर्ग) के लिए आरक्षण लागू है, वहां इस नीति का लाभ विभिन्न जातियों के अंदर कितने लोगों को और किस रूप में मिला है।
आशा की जानी चाहिए बिहार सरकार संभवतः विभिन्न जातियों और उन जातियों के अंदर विभिन्न वर्गों की शैक्षिक स्थिति के आंकड़े भी जारी करेगी।
अगर इन मुद्दों पर विशिष्ट जानकारी सामने आई, तो बेशक बिहार सरकार का यह प्रयास सार्थक होगा। लेकिन अगर इन बिंदुओं पर इस सर्वेक्षण से नई और विशिष्ट सूचनाएं सामने नहीं आईं, तो इस पूरे प्रयास की प्रासंगिकता पर जरूर ही सवाल उठाए जाएंगे।
जहां तक बिहार की जातीय संचरना का सवाल है, उसको लेकर जातीय सर्वेक्षण से ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, जिससे इससे संबंधित समझ में कोई नाटकीय बदलाव आए। मोटे तौर पर इससे पहले से मौजूद अनुमान की ही पुष्टि हुई है। ज्यादातर राज्यों में बहुजन के दायरे में समझी जाने वाली जातियों (ओबीसी, अनुसूचित जातियों और जनजातियों) की आबादी कुल जनसंख्या में 80 फीसदी से ज्यादा है, यह बात सामान्य जानकारी का हिस्सा रही है। बिहार में यह संख्या 83 प्रतिशत सामने आई है।
बहुजन समाज भी श्रेणीबद्ध है- यानी उसके अंदर सामाजिक-शैक्षिक और आर्थिक आधार पर विषमता है। इसीलिए बिहार में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था करने के साथ ही इन जातियों को दो एनेक्सरों में बांटा गया था। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें पिछड़ा और अति-पिछड़ा नाम दिया। इसी तरह उन्होंने अनुसूचित जातियों के बीच दलित और महा-दलित की श्रेणियां बनाईं। लेकिन उनके बीच विषमता सिर्फ आर्थिक आधार पर ही नहीं है। बल्कि विभिन्न पिछड़ी/शोषित जातियों के अंदर सामाजिक और शैक्षिक खाइयां भी हैं।
यह एक बड़ी वजह है, जिससे गुजरे दो- ढाई दशकों में विभिन्न पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के अंदर अपनी विशेष जातिगत पहचान को जताने की प्रवृत्ति मजबूत हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं प्रवृत्तियों का लाभ उठा कर ओबीसी और दलित दोनों श्रेणियों के अंदर गहरा विभाजन पैदा करते हुए अपनी पैठ बनाई है। भाजपा की इस सफलता ने 1990 और 2000 के दशकों में उत्तर भारत में उभरी सामाजिक-राजनीतिक परिघटना को एक तरह से पलट दिया है।
भाजपा इसमें इसलिए भी कामयाब हो पाई, क्योंकि जो पार्टियां मंडलवादी राजनीति के जरिए मजबूत हुई थीं, उन्होंने विभिन्न पिछड़ी या शोषित रही जातियों की आर्थिक एवं शैक्षिक प्रगति का कोई एजेंडा पेश करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। सत्ता में रहने के दौरान उन्होंने इस दिशा में कोई खास पहल भी नहीं की।
इसीलिए आज बनी एक समझ यह है कि जातीय सर्वेक्षण दोधारी तलवार साबित हो सकता है। आखिर जब बिहार के जातीय सर्वेक्षण से हासिल हुए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार संबंधी आंकड़े सामने आएंगे, तो उन्हें राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल (यू) के शासनकाल को भी परखने का एक पैमाना समझा जाएगा। लोग यह पूछेंगे कि 33 साल से बिहार पर राज कर रही इन दोनों पार्टियों (जो अब एक साथ हैं) की सरकारों ने पिछड़ी/दलित जातियों और अल्पसंख्यकों के लिए कितने और किस गुणवत्ता के स्कूल खोले, स्वास्थ्य देखभाल की उन्होंने कैसी व्यवस्था की, उनकी रोजगार संबंधी पहल क्या रही और बिहार की आर्थिक प्रगति के मोर्चे पर उनका रिकॉर्ड क्या है?
दूसरे राज्यों के संदर्भ में ऐसे सवाल वहां सत्ता में रही तमाम पार्टियों से पूछे जाएंगे और अंततः ये प्रश्न उन सभी पार्टियों से पूछे जाएंगे, जो गुजरे दशकों में केंद्र की सत्ता में किसी ना किसी रूप में सहभागी रही हैं।
मुद्दा यह है कि जातीय जनगणना की तेज हो रही मांग के पीछे मकसद क्या है? (बिहार सरकार ने तकनीकी कारणों से वहां हुई जातीय जनगणना को जातीय सर्वेक्षण कहा है। तकनीकी कारण यह है कि भारतीय की वैधानिक व्यवस्था के मुताबिक जनगणना सिर्फ केंद्र सरकार करवा सकती है। बहरहाल, व्यावहारिक रूप में वहां जो हुआ, वह जातीय जनगणना ही है।)
जातीय जनगणना की मांग के साथ- ‘जिसकी जितनी आबादी, उसका उतना हक’ का नारा फिर प्रबल हुआ है। तो यह माना जा सकता है कि ऐसा हक दिलवाना जातीय जनगणना का मकसद है। हालांकि अभी तक किसी दल ने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह हक राजनीतिक सत्ता और अर्थव्यवस्था दोनों जगहों पर मांगा जा रहा है- या मांगा जाएगा। अब प्रश्न है कि यह हक संबंधित जातियों को कैसे दिलवाया जाएगा?
परंपरागत समझ के मुताबिक ऐसा आरक्षण के जरिए किया जाएगा। जातीय जनगणना की मांग के समर्थकों का कहना है कि वे ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी’ की सोच के तहत आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग करेंगे। अभी तक जो विमर्श सामने है, उसमें यह मुद्दा यहीं तक सिमटा हुआ है। तो फिलहाल संदेश यही है कि इंदिरा साहनी मामले में ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में कुल आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तय कर दी थी, उसे खत्म करने की मांग आने वाले दिनों में जोर पकड़ेगी। मगर इस बारे में दो बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिएः
- सुप्रीम कोर्ट ने यह एक कृत्रिम सीमा तय की थी, जिसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। इसीलिए तमिलनाडु में पहले से लागू 69 प्रतिशत आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी जारी रहा है।
- दूसरी बात यह कि जब नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के लिए (व्यावहारिक रूप से जिसका अर्थ सवर्ण जातियां हैं) 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की, तो उससे 50 फीसदी की सीमा अपने-आप टूट गई। इसलिए सामाजिक आधार पर आरक्षण को इस सीमा से आगे बढ़ाने कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं बची है। ऐसा फैसला अब सिर्फ राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर रह गया है।
प्रतिनिधित्व का एक दूसरा मोर्चा राजनीतिक सत्ता है। अभी तक किसी दल ने यह नहीं कहा है कि वह संसद और विधानमंडलों में भी अनूसूचित जाति- जनजातियों की तर्ज पर आबादी के अनुपात में ओबीसी के लिए भी आरक्षण की मांग करेगा। इसलिए फिलहाल यह प्रतिनिधित्व देने का मुद्दा पार्टियों की अपनी नीति पर निर्भर है। इस बिंदु पर प्रतिनिधित्व देने के मामले में भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड संभवतः बाकी सभी दलों से कमजोर नहीं है। बल्कि अति पिछड़ी जातियों और महा-दलित जातियों को सियासी नुमाइंदगी देने के मामले में संभव है कि उसका रिकॉर्ड बेहतर नजर आए।
ऐसे में अगर जातीय जनगणना का मकसद पिछड़ी जातियों की बहुसंख्या का आंकड़ा सामने लाकर भाजपा को घेरना है, तो मुमकिन है कि यह दांव ठीक उसी तरह ना पड़े, जैसा अनुमान मीडिया के एक हिस्से में लगाया जा रहा है। वैसे भी अगर मकसद इतना सीमित है, तो इसे राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित एक चाल ही कहा जाएगा।
लेकिन अगर उद्देश्य सचमुच सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करना है, तो फिर विकास नीति संबंधी बड़े सवाल उठेंगे। विकास नीति का संबंध अर्थव्यवस्था की दिशा और लक्ष्यों को तय करने की योजना से होता है।
यह कहा गया है कि जातीय संचरना के आंकड़े सामने आने के बाद पिछड़ी जातियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर कल्याण योजनाएं बनाना संभव हो पाएगा। अब यह दुनिया भर में स्वीकृत धारणा है कि विकास नीति में विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रमों को भी जरूर जगह मिलनी चाहिए। मगर पहली बात यह है कि कोई स्पष्ट विकास नीति होनी चाहिए।
इसीलिए जातीय जनगणना की मांग के लिए उत्साह दिखा रहे दलों के सामने यह बताने की चुनौती है कि उनकी विकास नीति क्या है? नई विकास नीति किन रूपों में अब तक अपनाई गई ऐसी नीतियों से अलग होगी? अगर पिछली विकास नीतियां सभी समूहों और जातियों के पिछड़ेपन को दूर नहीं कर पाईं, तो जाहिर है, नई नीति को उन नीतियों से अलग प्रकार का होना चाहिए।
यह प्रश्न इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि नव-उदारवादी अर्थव्यवस्था के तहत अपनाई गई निजीकरण और राजकोषीय किफायत (fiscal austerity) की नीतियों ने आरक्षण के दायरे को बेहद सीमित कर दिया है। इसके जरिए बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मुहैया कराना अब संभव नहीं रह गया है। जबकि भारत के राजनीतिक दायरे में (एक हद तक वामपंथी पार्टियों को छोड़ कर) कथित आर्थिक सुधार की इन नीतियों पर आम सहमति रही है। इस आम सहमति को आज भी किसी कोने से चुनौती नहीं दी जा रही है।
चूंकि नव-उदारवाद के तहत अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका घटती जा रही है, इसलिए निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात कही जाती है। लेकिन भारतीय संविधान के वर्तमान ढांचे के तहत ऐसा करने की संभावना संदिग्ध और सीमित है।
इस बीच भारतीय पूंजी के विदेशों में निवेश की बढ़ती प्रवृत्ति, पूंजी-संपन्न धनी लोगों के देश से बढ़ते पलायन, ऑटोमेशन (कारोबार/उत्पादन में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और रोबोट्स के बढ़ते इस्तेमाल) और विभिन्न कार्यों की आउटसोर्सिंग के बढ़ते जा रहे चलन के कारण निजी क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होने की संभावना सीमित हो गई है। वहां सिर्फ अति कुशल कर्मियों को अच्छी क्वालिटी की टिकाऊ नौकरी मिलने की संभावना बची है। ऐसे कर्मी तैयार करने के लिए हर स्तर पर ऊंची गुणवत्ता की शिक्षा की जरूरत है, जो आज सिर्फ धनी-मानी परिवारों के बच्चों को मिल पा रही है।
इसलिए अगर मकसद सचमुच पिछड़ापन दूर करना है, तो सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के शिकार लोगों की संख्या जानने के साथ-साथ एक ऐसी विकास नीति को अपनाने की जरूरत भी होगी, जिसमें उपरोक्त चुनौतियों का समाधान शामिल हो। इसके लिए अर्थव्यवस्था के मौजूदा स्वरूप में आमूल बदलाव की जरूरत होगी। क्या जातीय जनगणना की समर्थक पार्टियों में ऐसा करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति, साहस और बौद्धिक सामर्थ्य है? यह सवाल पिछड़े समूहों के उत्थान और गैर-बराबरी को पाटने के प्रति उनकी निष्ठा को मापने का पैमाना बनेगा।
अगर वे इस मकसद के प्रति सचमुच निष्ठावान हैं, तो फिर उन्हें निम्नलिखित मुद्दों पर ना सिर्फ विचार करना और उन्हें बहस के केंद्र में भी लाना चाहिए, बल्कि इस बारे में कार्ययोजना का एक ठोस खाका भी पेश करना चाहिएः
- पहली बात यह कि देश को फिर से नियोजित अर्थव्यवस्था की तरफ लौटाने की जरूरत है। इसलिए कि सिर्फ एक नियोजित अर्थव्यवस्था में ही आर्थिक विकास के ठोस लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं और इन लक्ष्यों को विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की जरूरत के मुताबिक स्वरूप दिया जा सकता है।
- सिर्फ नियोजन प्रक्रिया के जरिए ही रोजगार पैदा करने और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हुए विकास दर बढ़ाने की नीतियां अमल में लाई जा सकती हैं।
- ऐसा सिर्फ उसी अर्थव्यवस्था में हो सकता है कि जिसमें पब्लिक सेक्टर की केंद्रीय भूमिका हो।
- उच्च गुणवत्ता की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक परिवहन को सरकारी क्षेत्र में वापस लाने की नितांत आवश्यकता है। यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन क्षेत्रों में केंद्रीय भूमिका सरकार की हो। सिर्फ तभी गरीब और पिछड़े समूहों को आज की जरूरतों के मुताबिक शिक्षित किया जा सकेगा।
मगर इन सबके साथ संसाधनों का सवाल भी आएगा। उसके लिए टैक्स सिस्टम को प्रोग्रेसिव बनाने के अलावा कोई और चारा नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान कर व्यवस्था को लगातार प्रतिगामी बनाया गया है, जिसका नतीजा यह है कि आज जो जितना धनी है, वह आनुपातिक रूप से उतना कम टैक्स दे रहा है।
कर व्यवस्था को प्रगतिशील बनाने के साथ ही कॉरपोरेट सेक्टर में मोनोपॉली खत्म करने के विधायी कदम उठाने होंगे। कॉरपोरेट सेक्टर में मोनोपॉली और नियोजित अर्थव्यवस्था दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते।
इसके साथ कैपिटल कंट्रोल (पूंजी नियंत्रण) के सख्त नियम लागू करने होंगे, ताकि भारत में उत्पन्न पूंजी का निवेश देश की आबादी- खासकर पिछड़ी आबादी की खुशहाली के लिए हो सके।
जो जाहिर है, जातीय जनगणना का मकसद तभी हासिल हो सकता है, जब उसके साथ-साथ अर्थव्यवस्था की पिछले तीन दशक से चल रही दिशा बदलने की योजना भी पेश की जाए। वरना, यह एक राजनीतिक नारे से ज्यादा कुछ नहीं साबित नहीं होगा। अगर जातीय जनगणना की समर्थक पार्टियों ने अर्थव्यवस्था संबंधी नई पहल की उपेक्षा की, तो उनका ताजा दांव उलटा भी पड़ सकता है- क्योंकि, जैसा कि ऊपर ध्यान दिलाया गया है कि जातीय जनगणना एक ऐसी तलवार है, जो सिर्फ भाजपा को ही नहीं, बल्कि बाकी तमाम राजनीतिक दलों के वास्तविक चरित्र को भी बेनकाब कर सकती है।
(सत्येंद्र रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं।)