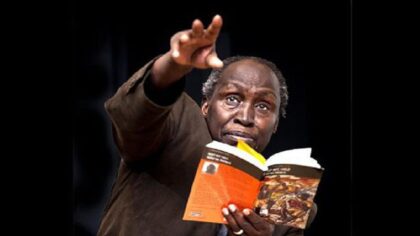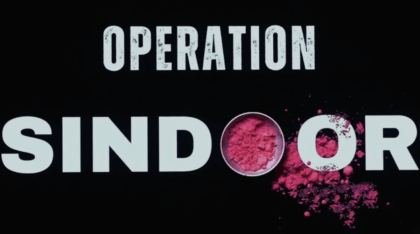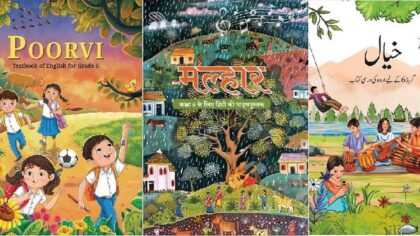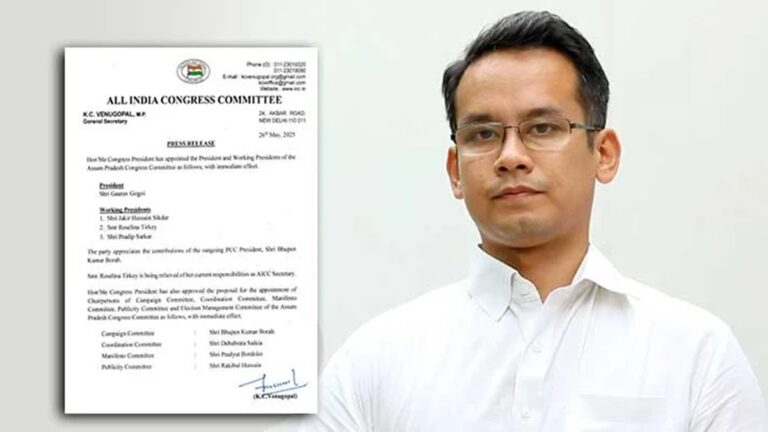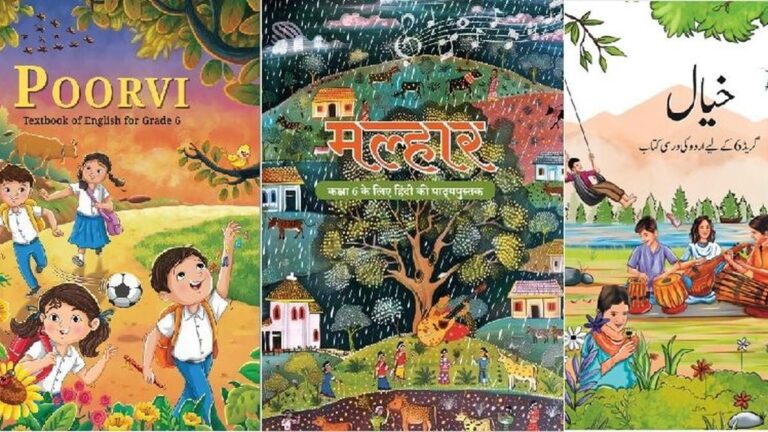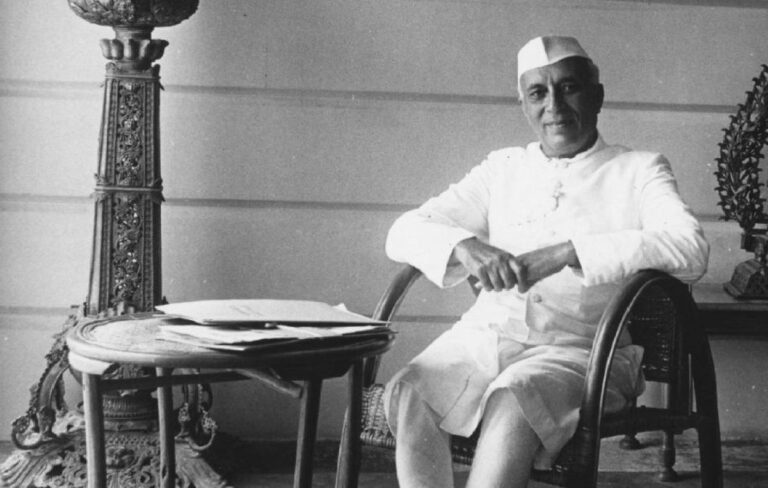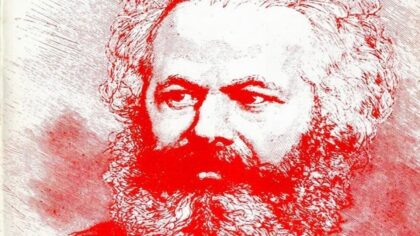कभी-कभी मुल्क के सबसे मामूली से क़दम पर जो सबसे बड़ा शोर मचता है, वो इस बात का गवाह होता है कि उस मामूली क़दम की दस्तक दरअसल कितनी गहरी है। जातिवार जनगणना की घोषणा भी ऐसा ही एक क़दम है। ये न कोई क्रांति है, न कोई नई खोज, न ही संविधान से बाहर की कोई जुर्रत। ये तो महज़ एक आईना है, लेकिन जो समाज आईने से डरने लगे, उसकी सूरत का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं।
इधर सरकार ने जातिवार जनगणना की बात क्या कही, उधर टीवी स्टूडियोज़ में मातम की महफ़िल सज गई। एंकरों की पेशानियों पर शिकन, विश्लेषकों की आवाज़ में चिंता, और संपादकीयों की पंक्तियों में राष्ट्र की “सामाजिक स्थिरता” पर मंडराता खतरा….जैसे किसी ने “राष्ट्रवाद” की चूड़ी तोड़ दी हो। टीवीपुरम् की यह बेचैनी अपने आप में गवाही है कि यह मामला सिर्फ़ आंकड़ों का नहीं, हक़ और हिस्सेदारी के उस नक्शे का है जिसे दशकों से मिटाया जा रहा था।
परंतु, हे टीवीपुरम् के संतप्त प्रवक्ता! इतना भी शोकाकुल मत होइए। आपके प्रिय सत्ताधीश इतने मासूम नहीं हैं कि वे आंकड़ों से बराबरी की फ़सल काट लेंगे। उनके मातृ-संगठन का तो इतिहास ही इस बात की गवाही है कि वे समता और न्याय की हर कोशिश को या तो तोड़ने में लगे रहे या फिर उसे प्रतीकवाद की चादर में लपेटकर निष्क्रिय बना देने में माहिर रहे। जातिवाद को “सनातन संस्कृति” का गौरव कहकर महिमा मंडित करने वाले, भला जातियों की गिनती से सामाजिक बदलाव का सेहरा क्यों पहनना चाहेंगे?
जातिवार जनगणना की मांग कोई नया आंदोलन नहीं, एक पुरानी चीख़ है
यह मांग सदियों की पीड़ा, परत-दर-परत वंचना और पीढ़ियों के संघर्ष से निकली हुई आवाज़ है। आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी अगर किसी देश में यह तय न हो सका हो कि किस तबक़े की आबादी कितनी है, तो यह आंकड़े नहीं, नीयत की नालायकी का सबूत है। क्या यह हैरत की बात नहीं कि पिछड़ी जातियों की गिनती 1931 के बाद नहीं की गई? यानी आज़ाद भारत ने एक ऐसा गणराज्य रचा जो सब कुछ गिनता रहा- टॉयलेट से लेकर मोबाइल तक-लेकिन अपने ही नागरिकों की जातिगत स्थिति नहीं।
सवाल ये है कि आख़िर सरकारों को इन आंकड़ों से डर क्यों लगता है? जवाब सीधा है- क्योंकि आंकड़े सवाल पैदा करते हैं। आंकड़े हिस्सेदारी की बात करते हैं। आंकड़े सत्ता की गद्दी पर बैठे लोगों से जवाब मांगते हैं कि आपने जिनके नाम पर वोट लिया, उन्हें उनके हिस्से का अधिकार कब दिया?
जातिवार जनगणना कोई ‘सामाजिक बम’ नहीं, बल्कि एक ‘सांख्यिकी दर्पण’ है जो दिखाता है कि कौन कहां खड़ा है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि इससे “सामाजिक विभाजन” पैदा होगा, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि इस देश में हज़ारों सालों से जाति के नाम पर जो बंटवारा था-क्या वो कोई ‘एकता का महोत्सव’ था?
सत्ता की शाइनिंग: जब आंकड़े अनकहे हों, तब ही सत्ता महफूज़ है
यह कोई संयोग नहीं कि वही शक्तियां जो हर तीसरे महीने धर्म, जनसंख्या, भू-स्वामित्व या राष्ट्रवाद के आंकड़ों से देश को भर देती हैं, वे ही जाति के आंकड़ों पर बौखला जाती हैं। उन्हें डर है कि जब जातीय संरचना की असलियत सामने आएगी, तब उनकी बहुमत की राजनीति, ‘हम सब एक हैं’ का जुमला, और ‘सबका साथ, सबका विकास’ की परछाईं-सब बिखर जाएंगी।
क्योंकि जब पिछड़े, दलित, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक आंकड़ों में अपनी तादाद देखेंगे, तब वे सिर्फ़ आंकड़ों में’ नहीं रहेंगे, वे ‘दावेदार’ बन जाएंगे। फिर बात प्रतिनिधित्व की होगी, आरक्षण की नहीं; हिस्सेदारी की होगी, कृपा की नहीं; नीति की होगी, नारे की नहीं।
जातिवार जनगणना: झूठी समानता की चादर पर सच्चाई की सलवट
जातियां अगर वाक़ई ख़त्म हो गई होतीं, जैसा कि तथाकथित ‘न्यू इंडिया’ की झिलमिलाती दुनिया दावा करती है, तो फिर जातियों की गिनती से इतना घबराना क्यों? ये डर साफ़ करता है कि ‘जाति’ अब भी हमारे समाज का सबसे सख़्त, सबसे अमिट, और सबसे विषैला सत्य है।
और ये भी कि जो लोग कहते हैं “हम सब भारतीय हैं, जात-पात क्या देखना”, वे दरअसल चाहते हैं कि सब भारतीय तो रहें, मगर सत्ता और संसाधनों की चाबी उन्हीं के पास रहे। ये वही छल है जो “वर्ण व्यवस्था” के आवरण में था-सभी की जगह तय, मगर बराबरी की कोई गारंटी नहीं।
जातिवार जनगणना का भविष्य: आंकड़ों से आगे की लड़ाई
हमें ये भी समझना होगा कि सिर्फ़ गिनती ही समाधान नहीं है। आंकड़े महज़ एक शुरुआत हैं। सवाल ये नहीं कि जातियां गिनी जाएंगी या नहीं-सवाल ये है कि क्या उस गिनती से नीतियां बदलेंगी? क्या बजट में उनका हिस्सा तय होगा? क्या विश्वविद्यालयों, नौकरियों, मीडिया, न्यायपालिका और नौकरशाही में हिस्सेदारी की बात होगी?
या फिर आंकड़ों को महज़ फाइलों की कब्रगाह में दफ़्न कर दिया जाएगा?
अगर जातिवार जनगणना को केवल आंकड़ों तक सीमित रखा गया, तो यह एक और दिखावटी कदम बनकर रह जाएगा। मगर अगर इसे सामाजिक न्याय की बुनियाद बनाया गया, तो यह इतिहास का रुख मोड़ सकता है।
आख़िर में:
जातिवार जनगणना कोई ‘वर्ग-संघर्ष’ नहीं, बल्कि ‘वास्तविकता की खोज’ है। यह वो आईना है जो सत्ता को अपना असली चेहरा दिखाता है, और जनता को अपना असली आकार। इस आईने से जो डरते हैं, वे इतिहास के सबसे बड़े दोषी हैं। और जो इसका स्वागत करते हैं, वे भविष्य के सबसे ईमानदार नागरिक।
तो हे टीवीपुरम्! आंकड़ों से नहीं, अपने डर से लड़ो। क्योंकि आंकड़े न तो क्रांति करते हैं, न साज़िश- वे बस एक सच्चाई दिखाते हैं। और अगर सच्चाई ही डरावनी हो गई है, तो फिर लोकतंत्र का रथ कब का रुक चुका है-बस उसकी आवाज़ अब तक तुम्हारी स्क्रीन तक नहीं पहुंची।
(जौवाद हसन स्वतंत्र पत्रकार हैं।)